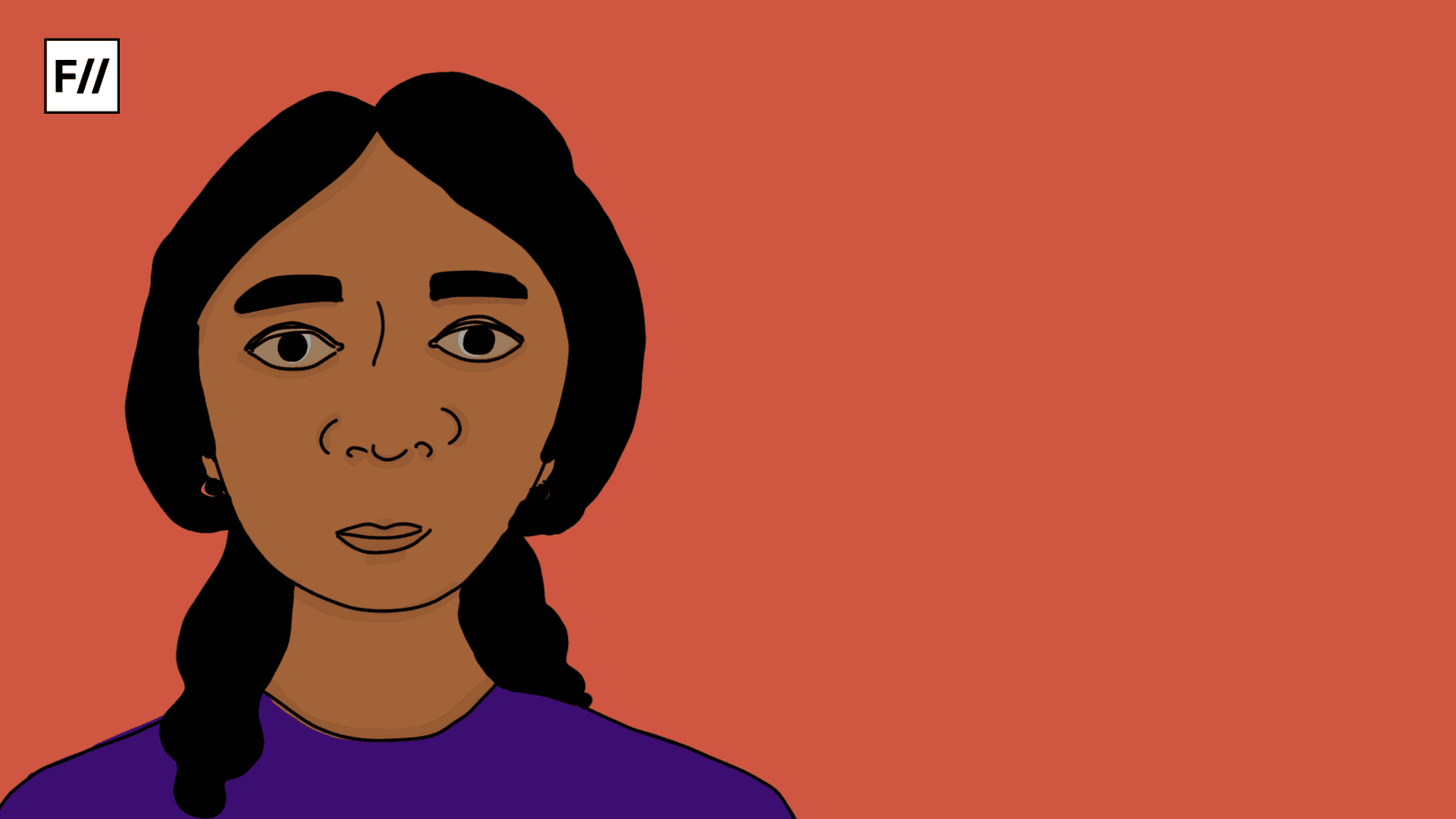पितृसत्तात्मक समाज में जब बात महिलाओं की हो, तो उनका भूगोल देह और ‘चरित्र’ के इर्द-गिर्द ही चक्कर लगाता दिखाई पड़ता है। मन की गांठ तो कभी खुलती ही नहीं। कहीं न कहीं महिलाएं भी इसे अपने अस्तित्व के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं। इस आधार पर जिंदगी जीने लगती हैं कि चरित्र को बेदाग रखना ही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि चरित्र की परिभाषा क्या है? मानवीय विवेक में जिसकी थोड़ी भी आस्था होगी, वह आपको बतलाएगा कि चरित्र का मतलब है – आदमी का वह आंतरिक गुण, जिसकी बदौलत वह न केवल पशु-जगत बल्कि अपने ही जैसे अन्य मनुष्यों से भी अलग है।
चरित्र का अर्थ क्या सिर्फ ‘यौन शुचिता’?
मगर हमारे समाज में चरित्र की गढ़ी हुई परिभाषा सिर्फ पुरुषों के लिए सुरक्षित है। औरतों के लिए तो यह पूरी तरह वर्जित है। उनके लिए यह एक ऐसी लक्ष्मण-रेखा है, जिस पर पांव रखते ही पितृसत्तात्मकता का रावण उन्हें हर ले जाएगा। उनके लिए चरित्र का सिर्फ एक ही अर्थ है – यौन शुचिता, कौमार्य की रक्षा और ‘पतिव्रत धर्म’ का पालन। नारी चरित्र की यह विशेष व्यवस्था नारियों ने खुद नहीं की, बल्कि हमारे उन पुराण-पुरुषों ने की, जो कहते हैं कि दिन के उजाले में आठ-आठ बरस तक अपनी बीवियों का मुंह नहीं देखते थे, लेकिन रात के अंधेरे में इसी दरम्यान आठ-आठ बच्चे पैदा करना न भूलते थे। और जिन्होंने अपनी औरतों को ‘बचाने’ के लिए छोटे-छोटे चोरदरवाजे भी बंद करने में कोई कोताही न की। चुनरी में दाग लगा नहीं कि ये शोर मचा देते हैं। क्या महज एक दाग भर से स्त्री का चरित्र तय हो जाता है?
पवित्रता की आड़ में पाखंड
आज भी चरित्र की इस पाखंडपूर्ण व्यवस्था का रक्षक वही पुरुष-समाज है, जो अपनी चहारदीवारी में औरतों की पवित्रता के लिए नए नुस्खे ईजाद करता है और खुली सड़कों पर हर लहंगे के पीछे और कूल्हों की हर जुंबिश पर लार टपकाता नजर आता है। यानी घर में कौमार्य की रक्षा की नियमावली और पास-पड़ोस में उसके उल्लंघन के लिए चारेबाजी – यही है वह संतुलन-बिंदु, जिस पर हमारे समाज की सारी नैतिकता टिकी है।
जाहिर है दोहरे मानदंडों वाले इस विकृत संसार में औरत की यौन-शुचिता सिर्फ एक गुलदस्ता ही हो सकती है, जिसे वह शादी की पहली रात पति नामक प्राणी को भेंट करेंगी। यह भेंट उसका अपना फैसला नहीं, बल्कि समाज के उन कर्णधारों का है, जिन्होंने एकतरफा निर्णय की पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत पति को यह अधिकार दिया है कि वह पत्नी की इच्छा या सहमति की परवाह किए बगैर उसकी बरसों संजोई ‘पवित्रता’ को भंग करे, उसे मानवीय संबंधों की दुनिया में एक गौण पुर्जे की तरह फिट कर दे और कुल मिलाकर, उसके व्यक्त्वि को रसोईघर और बेडरूम से लेकर प्रसूति-गृह तक इस तरह बिखेर दे कि उसके टुकड़ों का जोड़ तक नजर न आए।
चरित्र की इसी व्यवस्था को स्वीकार करके ही औरतों की अनगिनत पीढ़ियां अपनी पाकीजगी साबित करती आई हैं और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने इस व्यवस्था से बाहर निकालने की हिमाकत की, उसे गार्गी की तरह याज्ञवल्क्यों ने उसके भी सिर के सौ टुकड़े कर डाले।
चरित्र के दोहरे मानदंड
अगर आपने चरित्र के दोहरे मानदंडों की विकृति पर गौर किया हो, तो आप पाएंगे कि परिवार के अंदर यौन-शुचिता पर जोर देने का मूल कारण औरत के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं, बल्कि हर निजी संपत्ति की तरह औरत नामक ‘वस्तु’ पर भी पितृसत्ता का एकाधिकार मजबूत करना है। इस एकाधिकार की क्यों जरूरत है? लेकिन वंशवृद्धि और रक्तशुद्धि के लिए- संपत्ति का उत्तराधिकार और वह भी जायज उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए, यह उन्हें जरूरी लगा हो। इसके अलावा अगर कोई और नेक उद्देश्य होता – मसलन, पुरुष की बेलगाम भोगेच्छा पर रोक लगाना- तो एकनिष्ठ विवाह के साथ रंडियों, रखैलों, गीशाओं और मिस्ट्रेसों की एक समानांतर व्यवस्था चलती न दिखाई पड़ती।
हाय! ये कुलमर्यादा
कुल की मर्यादा ही वह चीज़ है, जिसके सहारे पुरुष-समाज जीवनसाथी के चुनाव जैसे निहायत निजी मामलों में भी नारी के निर्णय करने के अधिकार का अपहरण कर लेता है और उसे महंगे दामों में खरीद कर किसी भी मनचाहे व्यक्ति को औरत नामक ‘वस्तु’ का उपभोक्ता मुकर्रर कर देता हैे।
और चुनवा दी जाती है अनारकली
रिश्तों के इस व्यापार में वह पूरा ध्यान रखता है कि उसके द्वारा मुकर्रर उपभोक्ता केवल पुरुष होने के कारण ही औरत से ‘सुपीरियर’ न हो, बल्कि जातीय व सामाजिक हैसियत के लिहाज़ से खासा ‘सुपर फाइन’ हो। यानी, ले-देकर कुलमर्यादा की मान्य व्यवस्थाएं औरत को बस बिस्तर में चिन देती हैं – इस गारंटी के साथ उस बिस्तर पर बिछी चादर रक्त रंजित होगी क्योंकि वह अक्षत योनि है। अगर औरत ने किसी भी रूप में इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया, तो समाज उसे अनारकली की तरह दीवारों में चिनवा देगा।
यह सच है कि जो लोग जाति और माली हैसियत-दोनों लिहाज से समाज के निचले पायदान पर पड़े हैं, उनके यहां कुलमर्यादा का सवाल इस तरह नहीं उठता। सामंत प्रभु जब चाहे अपने इन निरीह असामियों की निरीहता का फायदा उठा कर उनकी औरतों को अपनी रखैलों में तब्दील कर ले सकता है। प्रभु वर्ग की सर्वग्रासी शान के सामने कमजोर की बीवी के मान की बात करना शायद एक अनाधिकार चेष्टा है।
और एक आवाज तक नहीं उठती
बात चाहे जितनी कड़वी लगे, पर सच्चाई यही है कि हमारे पास भी अपनी औरतों को दिखाने के लिए कोई दमदार सपना नहीं है। वरना ऐसा क्यों होता है कि हत्या और बलात्कार की घटनाएं घटती रहती हैं, मगर प्रगतिकामी ताकतों की ओर से प्रतिवाद की एक आवाज़ तक नहीं उठती? जाहिर है कि उनके इस नकारात्मक (और कई बार घातक) व्यवहार ने न केवल महिलाओं को और अधिक असहाय बना दिया है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के चक्र को – धनतंत्र बनाम जनतंत्र के निर्णायक संघर्ष को – स्वतंत्रता और समानता पर आधारित समाज-निर्माण के स्वप्न को कहीं कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के सामने सिर झुकाने को विवश कर दिया है।
आज जिस चीज की सख्त ज़रूरत है, वह है चिंतन के धरातल पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था और पुरुष-प्रभुत्ववाद के खिलाफ एक ज़बरदस्त, वास्तविक और दूरगामी सांस्कृतिक संघर्ष की। एक ऐसे संघर्ष की, जो हमारा आत्मसंघर्ष भी हो और नारी-विरोधी माहौल के खिलाफ हमारा संग्राम भी…. वह संघर्ष, जो न केवल मध्यकालीन जड़ मानसिकता और आधुनिक जीवन के विकृत उपभोक्तावाद पर तीखी चोट करे, बल्कि औरत-मर्द के रिश्तों को एक नए मानवीय आलोक में फिर से परिभाषित करे – उनकी स्वतंत्रता और समानता के ठोस व वास्तविक आधारों की खोज करें।
(महेश्वर के महिला विषयक लेखों का संग्रह ‘परचम बनता आंचल’ से कुछ भावांश साभार)