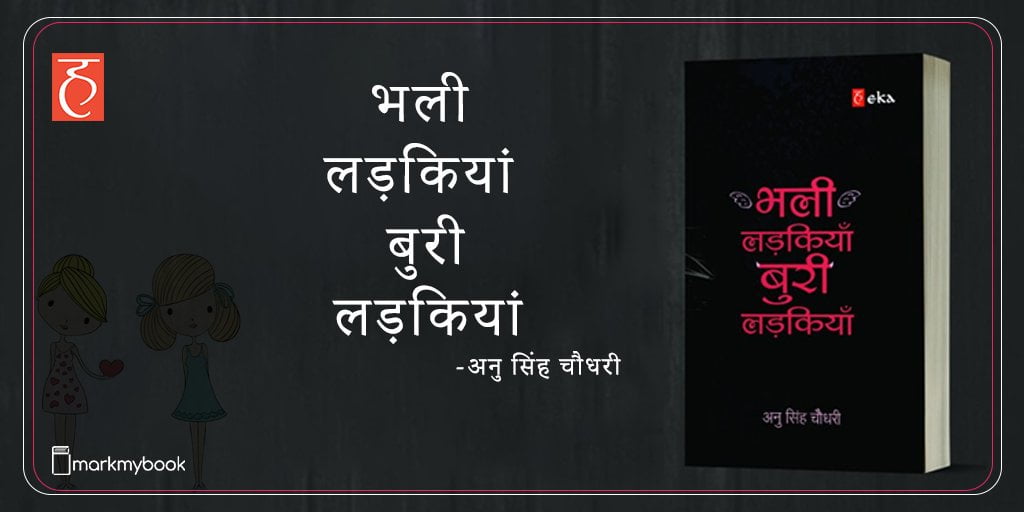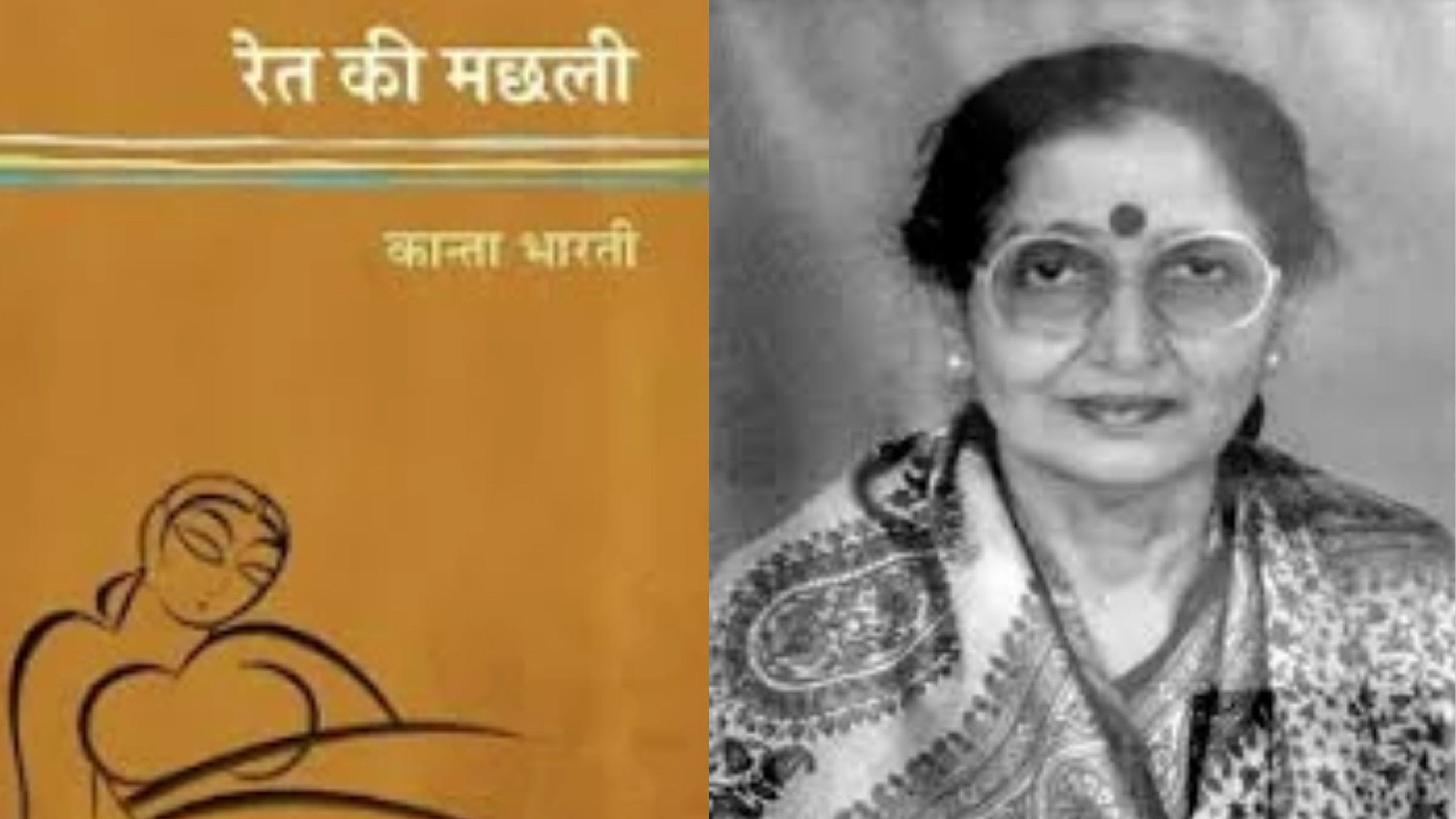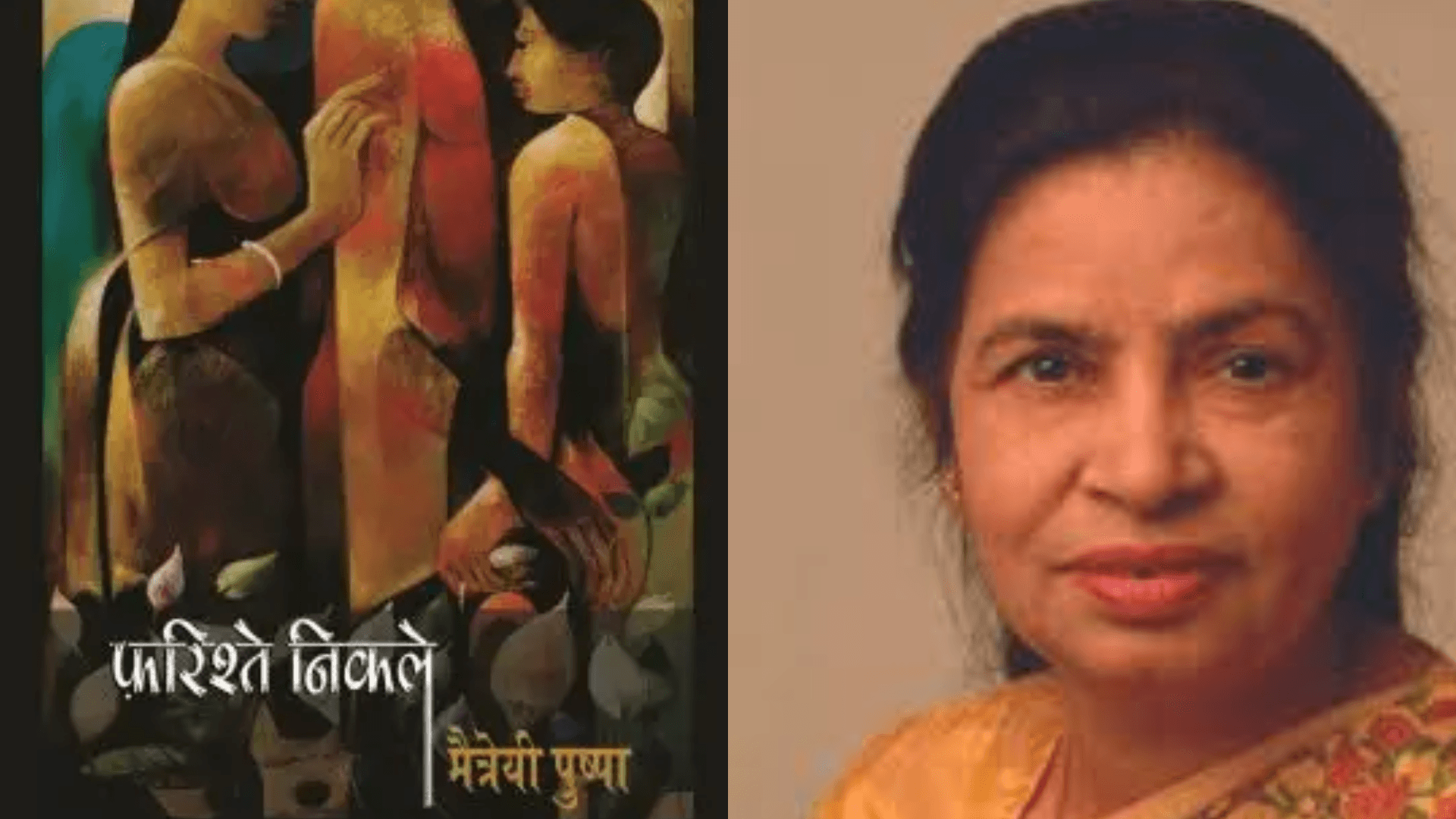लड़कियाँ तो होतीं ही हैं भली – बुरी, इन दो शेड्स के अलावा कोई तीसरा शेड कहाँ होता है भला ?
या तो बन्दी संस्कारी है या फिर बिगड़ैल।
भली लड़कियों के होने से ज़माना भला है वरना बुरी लड़कियों ने ही तो ज़माने को बिगाड़ा है !
और बदनाम बेचारा ज़माना होता है !
नहीं ?
एक किताब, एक कहानी : है तो नई फिर भी है पुरानी
इस साल की शुरुआत में लेखिका अनु सिंह चौधरी की तीसरी किताब और पहला उपन्यास ‘भली लड़कियाँ बुरी लड़कियाँ’ पाठकों के सामने आया। इससे पहले उनका एक कहानी संग्रह ‘नीला स्कार्फ’ 2014 में और 2015 में मातृत्व/पैरेंटिंग के विषय पर लिखी गई किताब ‘मम्मा की डायरी’ प्रकाशित हो चुकी है। दोनों ही किताबें पाठकों के बीच काफी पसंद की गईं। ‘मम्मा की डायरी’ तो हिंदी में पैरेंटिंग को लेकर लिखी गई अपनी तरह की अनूठी किताब ही है।
लेखिका के लिखने का अंदाज़ एकदम सरल लेकिन दिल को स्पर्श कर लेने वाला रहा है। अपनी कहानियों में उन्होंने अक्सर बहनापे/सिस्टरहुड के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है।
इसी बात का ख्याल इस उपन्यास में भी रखा गया है, जहाँ सिस्टरहुड के कॉन्सेप्ट को लेकर पूर्वाग्रह थोड़े कम हैं और ताज़गी बहुत ज़्यादा। उपन्यास का मूल विषय बहुत नया नहीं है, हिंदी में बलात्कार की घटनाओं पर पहले भी बहुत – सी कहानियाँ लिखी जा चुकी हैं, ऐसी घटनाओं को लेकर विभिन्न पक्ष रखे जा चुके हैं।
यह उपन्यास इन्हीं लड़कियों की बात करता है, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने रास्ते तलाशने के बजाय खुद बनाने की कोशिश करती हैं।
लेकिन एक बार पढ़ने के बाद अगर ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि क्या यही मूल विषय है ?क्या लेखिका बस एक ऐसी घटना, जो इस देश की हर सड़क पर हर दिन होती है, के बारे में ही लिखना चाहती थीं ?
उपन्यास में इस घटना के पहले और बाद में जो है, उसके क्या मायने हैं ?
और पढ़ें : डियर पांच बेटियों के पापा…
किस्सा-ए-दिल्ली
दिल्ली के बाहर से, दिल्ली में सिर्फ पढ़ने का अरमान लेकर आई लड़कियाँ, यहाँ की छात्र राजनीति और इस शहर की आम – सी लगती पर क्रांतिकारी ज़िन्दगी को किस तरह से अपनाती हैं, यह हमें इस उपन्यास में पढ़ने को मिलता है।लेकिन असल दुविधा लड़कियों के इस शहर को अपनाने को लेकर नहीं, बल्कि यह शहर इन लड़कियों को कितना अपनाता है, इस बाबत है।
कहानी शुरू होती है तो लगता है कि एक ही नायिका है, आखिर तक आते – आते एहसास होता है कि उपन्यास में जिन-जिन लड़कियों का ज़िक्र हुआ, असल में वे सभी नायिकाएँ हैं, बस वे समाज के ‘नायिका’ वाले खांचे में उस तरह से फिट नहीं बैठती तो समाज उन्हें इस तमगे से कहाँ नवाज़ने वाला है !
और पढ़ें : अच्छी लड़कियां गलतियाँ करके नहीं सीखतीं!
जैसा कि लेखिका एक इंटरव्यू में बताती भी हैं कि, “भली या बुरी लड़की जैसी कोई परिभाषा ही नहीं होती, बल्कि उन्हीं परिभाषाओं के दायरों को समझने और तोड़ने की कोशिश में शायद यह किताब बन गई। ऐसी कोई भी परिभाषा बनाई ही नहीं जानी चाहिए।”
और वाकई, जिन लड़कियों को ‘भला’ और ‘बुरा’ कहकर समाज वर्गों में बांटता है, उपन्यास पूरा होते – होते उन्हीं लड़कियों को लेकर यह विश्वास हो जाता है कि उनका बुरा होना इस समाज की भलाई के लिए किस कदर ज़रूरी, और भला होना फिलहाल कितना गैरज़रूरी है। लेखिका वाकई एक पुराने विषय पर नए ढंग से अपनी बात रखने में सफल हुई हैं।
असल दुविधा लड़कियों के इस शहर को अपनाने को लेकर नहीं, बल्कि यह शहर इन लड़कियों को कितना अपनाता है, इस बाबत है।
हालांकि, उपन्यास का अंत जल्दबाज़ी करता – सा जान पड़ता है। कहानी में बहुत सारी चीज़ों के खुलने की संभावना थी, लेकिन तभी उसका अंत हो गया जो कि किसी धक्के की तरह पाठक को हैरान भी करता है और परेशान भी, इसे तो अभी और लंबा होना चाहिए था !
अमूमन कहानियों में लेखक समाधान प्रस्तुत करते हैं, समस्या या हालात बताकर छोड़ देने वाली कहानी अधूरी – सी लगती है। लेकिन शायद इस उपन्यास का मकसद यही था, हालात बताकर छोड़ देना, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज के जिन स्त्री द्वेषी हालात में कोई लड़की हार मानकर आत्महत्या का विकल्प चुनती, तो कोई लड़की हिम्मत करके कानून का दरवाज़ा खटखटाती है, वहीं कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है जो अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़े।
यह उपन्यास इन्हीं लड़कियों की बात करता है, जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने रास्ते तलाशने के बजाय खुद बनाने की कोशिश करती हैं।
और पढ़ें : बेटी के स्टार्टअप प्लान पर हो ज़्यादा ख़र्च, न की उसकी शादी में
तस्वीर साभार : twitter.com