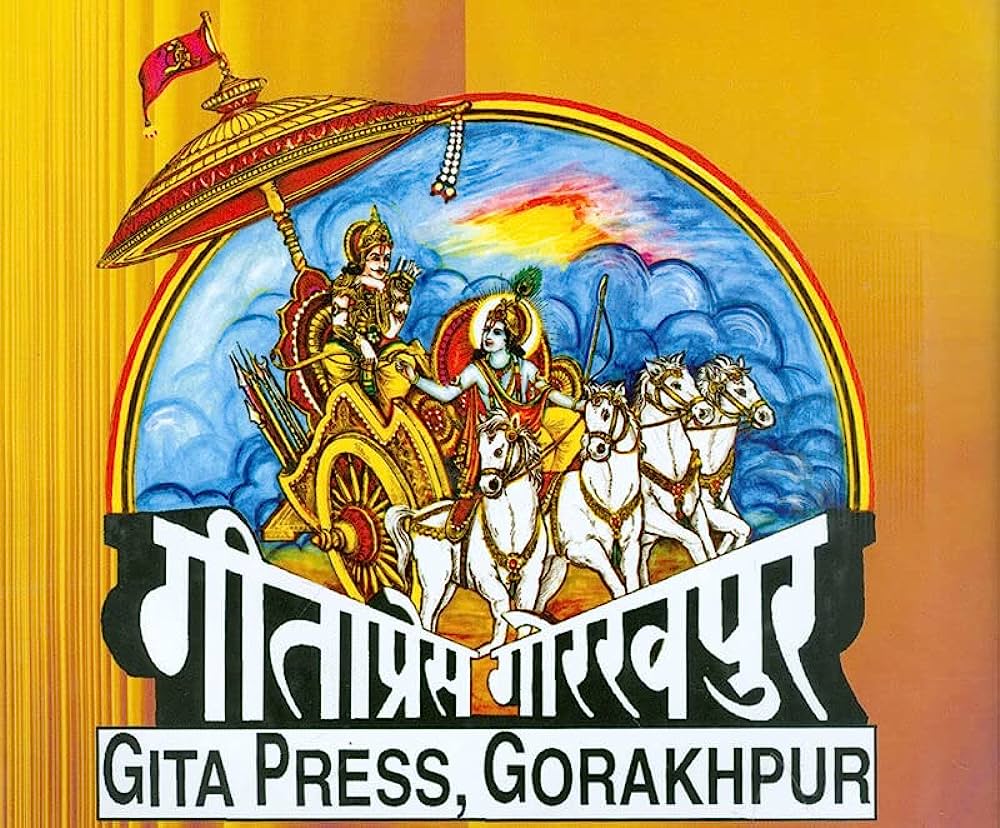कोई प्रकाशन अगर शोषकों की रीति-नीति का महिमाण्डन करने के लिए ही बना है जिनकी पुस्तकें हमेशा गैरबराबरी के समाज की घोर हिमायती हो वह प्रकाशन या उसकी धार्मिक पुस्तकें किसके लिए ज़मीन तैयार कर रही हैं। गीता प्रेस को गाँधी शांति पुरस्कार दिया गया और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुरस्कार की धनराशि जो कि एक करोड़ रुपये है को लेने से मना कर दिया। गीता प्रेस की किताबें निशुल्क भी घर-घर पहुंचाई जाती रही हैं तो पुरस्कार की राशि लेना या न लेना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं दिखता। हां एक प्रौपगैंडा ज़रूर दिखता है क्योंकि सत्ता से गीता प्रेस का गठजोड़ कितना गहरा है ये कोई छिपी बात नहीं है।
जब धर्मांधता और भेदभाव किसी सत्ता का चरित्र बन जाए तो वह इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है। अब इस तरह की खबरें वर्तमान सत्ता का मूल चरित्र लगती हैं तो बहुत अचरज तो नहीं होता लेकिन समाज को कट्टरपंथी और घोर भाग्यवादी, धर्मभीरू बनानेवाले संस्थान की सत्ता में इतनी पकड़ देख समाज के पतन के आसार और बढ़ जाते हैं। गीता प्रेस की किताबें सिर्फ़ हिंदू धर्म के महिमाण्डन के सिवा कोई मानवीय मूल्य नहीं स्थापित करतीं। साहित्य तो बहुत दूर की बात उन्होंने हमेशा स्त्री और हाशिये के समाज के मनुष्यों का घोर निरादर किया है। उनका पूरा साहित्य भंडार ब्राह्मणवादी कहानियों से भरा है जहां पाप और पुण्य के अतार्किक की बातें ही रहती हैं। स्त्रियों, दलितों को पतित ही बताया जाता रहा है। समाज को प्रगतिशील विचारों से धर्म और परंपरा की तरफ खींचने में गीता प्रेस की हमेशा से अहम भूमिका रही है।

सबसे ज्यादा गीता प्रेस ने किसी के व्यक्तित्व को लहूलुहान किया है तो वह है स्त्री। उनकी पुस्तकों में उनके मूल्यों के हिसाब में खरी न उतरने पर स्त्रियों के लिए घोर स्त्रीविरोधी दंड विधान हैं। उनके मुताबिक स्त्री सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सेविका है। उनकी पुस्तकें कहती हैं कि पति से मार खाने वाली स्त्री अपने पूर्वजन्म के कुकर्मों का फल भोग रही हैं, मसलन पति तो स्त्री को पीटकर उसका उद्धार कर रहा है। स्त्रियों और दलितों को लेकर उनकी पुस्तकों में ऐसी-ऐसी बातें हैं कि लगता है कि स्त्री और दलित उनके मनुष्य होने के अर्थ में आते ही नहीं। सती-प्रथा और बाल विवाह जैसी कितनी अमानवीय और क्रूर प्रथाओं का उनके यहां महिमाण्डन है। समाज में मनुष्य से मनुष्य की दूरी गढ़ने समाज मे ऊंच-नीच, जात-पात से ओत-प्रोत विचारों को इन किताबों के ज़रिये खूब प्रचारित किया जाता है। दशकों से ये किताबें समाज में धर्मांधता का मीठा जहर भर रही हैं।
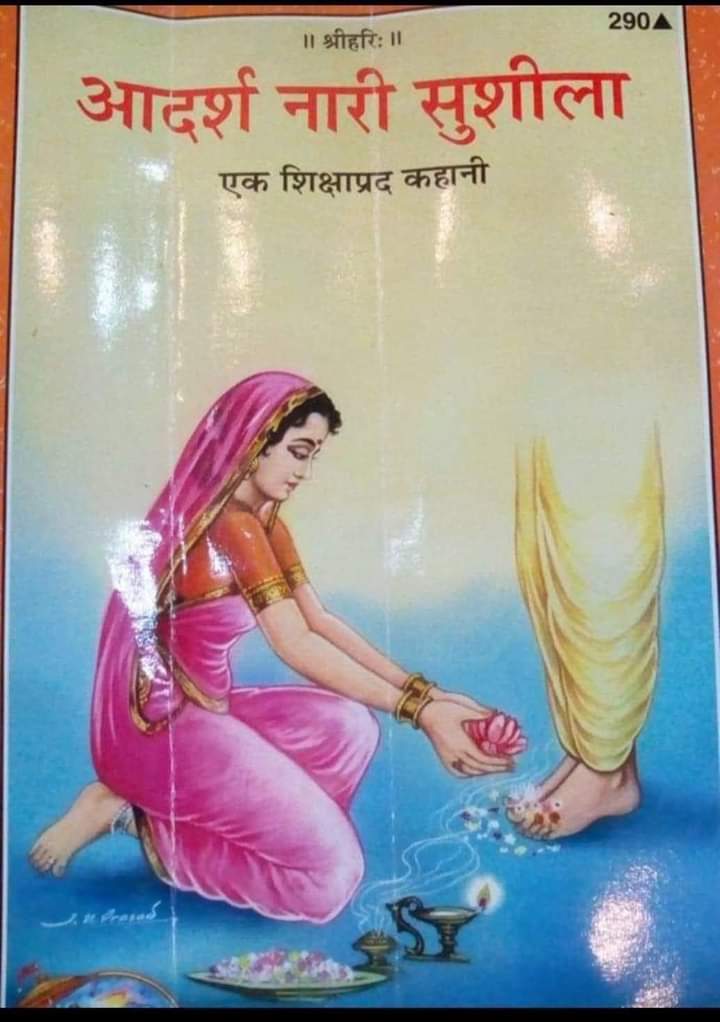
गीता प्रेस इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि गाँव के समाज में साहित्य की और किताबें तो दुर्लभ होतीं हैं लेकिन कल्याण पत्रिका बराबर पहुंचती रही है। जाहिर सी बात है प्रकाशन के पास किताबों पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धनराशि है नहीं तो मुफ्त में घर-घर किताब बाँटने का ये कार्य कैसे हो सकता था। धार्मिक पुस्तकों का मुफ्त में वितरण धार्मिक सत्ता की स्थापना के उद्देश्य से ही होती रही है। अगर संविधान या लोकतांत्रिक मूल्यों के स्तर पर देखा जाए तो गीता प्रेस पिछले कई दशकों से धर्म ग्रंथों सहित जाने कितनी और मनुष्य-विरोधी किताबें प्रकाशित करता है।

आलोचक जावेरी मल्ल पारख जी गीता प्रेस को लेकर लिखते हैं कि गीता प्रेस पिछले सौ साल से सनातन धर्म के नाम पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करता आ रहा है। वह छुआछूत में यकीन करता है। वह दलितों के मंदिर प्रवेश् के विरुद्ध है। वह स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोधी है। वह स्त्रियों के स्कूल और कालेज भेजने का विरोधी है। विधवा विवाह का विरोधी है और सती प्रथा पर गर्व करता है। और इन विचारों को वह पिछले सौ सालों से छोटी-छोटी पुस्तकों द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रचारित करता रहा है। ये पुस्तकें लाखों-लाख की संख्या में अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें कही गई ज्यादातर बातें संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हैं और जिन पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, लेकिन विडंबना यह है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से गीता प्रेस को रेलवे स्टेशनों पर अपने बुक स्टाल खोलने की अनुमति मिलती रही है और धर्म की आड़ में संविधान विरोधी बातें फैलाने की छूट भी मिली हुई है।
राज्य जब प्रतिगामी मूल्यों के प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत करता है तो निश्चित ही उसकी समाज को पीछे की तरफ धकेलने की मंशा होती है। नहीं तो गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण का कोई भी अंक आप उठा कर देख लीजिए वहां आधुनिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लोप ही मिलेगा। तमाम तरह के भ्रमित करने वाले तर्को से वहां जनमानस को धर्मांधता की तरफ जाने का उपदेश दिया जाता है। संतो महात्माओं का नाम लेकर वहां वर्ण-व्यवस्था को स्थापित करने जैसे कार्य वहां मिल जाएंगे। अगर कोई यह कहे कि धार्मिकता या पारंपरिक मूल्यों पर कोई प्रकाशन कार्य कर रहा है यह उनकी वैचारिकता है तो इसमें यह बात आती है कि कोई संस्थान अगर धार्मिक कर्मकांड या रीतिनीति को स्थापित कर रहा तो ये उसकी निजता या स्वतंत्रता हो सकती है लेकिन जब राज्य ऐसे बलों को बढ़ावा दे तो किसी भी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी।
गीता प्रेस की किताबें सिर्फ़ हिंदू धर्म के महिमाण्डन के सिवा कोई मानवीय मूल्य नहीं स्थापित करतीं। साहित्य तो बहुत दूर की बात उन्होंने हमेशा स्त्री और हाशिये के समाज के मनुष्यों का घोर निरादर किया है। उनका पूरा साहित्य भंडार ब्राह्मणवादी कहानियों से भरा है जहां पाप और पुण्य के अतार्किक की बातें ही रहती हैं
ऐसी किताबें जो चमत्कार की बात करें तार्किक बुद्धि समाप्त ही करेंगीं। आज जिस तरह से इसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं उससे यही लगता है कि परंपरा, आडंबरों और शोषण को धर्म से जोड़कर मनुष्य को वैचारिक विकलांग बना देती है। और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि समाज में हाशिये के जन इससे पीड़ित होते हैं । हमारे समाज सुधारक इसी धर्मांधता से लड़ते रहे हैं जिसे आज राज्य सम्मानित कर रहा है। फुले से लेकर पेरियार, आंबेडकर, राजा राममोहन, गांधी तक सब इसी रूढ़िवादी व्यवस्था से लड़ते रहे हैं। वे हमेशा तार्किकता व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया को देखने-समझने की बात करते रहे हैं।
अगर स्त्री-चिंतन की दृष्टि से बात की जाए तो उन्हें पीछे धकेलने की एक बहुत लंबी क़वायद है यह संस्थान। उनकी पत्रक कल्याण को ही उठाकर देख लिया जाना चाहिए स्त्री जीवन के तमाम समाजिक बंधनों को वहां ईश्वरीय विधान कहा जाता है। जाने कितनी सामाजिक और पारंपरिक कुरीतियों का वहां महिमामंडन किया गया है। उनके यहां स्त्री के लिए स्वतंत्र न होना ही सब प्रकार से मंगलदायक है। पूर्व में होनेवाले ऋषि, महात्माओंने स्त्रियों के लिए पुरुषों के अधीन रहने की जो आज्ञा दी है, वह उनके लिए बहुत ही हितकर जान पड़ती है।
ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे। उनका अनुभव बहुत सराहनीय था। जो लोग उनके रहस्य को नहीं जानते हैं, वे उन पर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि ऋषियों ने जो स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण किया, यह उनके साथ अत्याचार किया गया; ऐसा कहना उनकी भूल है; लेकिन यह विषय विचारणीय है। स्त्रियों में काम, क्रोध, दुसाहस, हठ, बुद्धि की कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशौच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होनेके कारण वे स्वतंत्र ताके योग्य नहीं हैं, तुलसीदास जी ने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बतलाए हैं।
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥
साहस अनृत चपलता माया । भय अबिबेक असौच अदाया ॥
अतएव उनके स्वतंत्र हो जाने से अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषों की वृद्धि होकर देश, जाति, समाज को, बहुत ही हानि पहुंच सकती है। इन्हीं सब बातों को सोचकर मनु आदि महर्षियों ने कहा है-
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि ॥ बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतंत्र ताम्॥
(मनु०५ १४७ – १४८)
“बालिका, युवती और वृद्धा स्त्री को भी स्वतंत्रता से बाहर नहीं फिरना चाहिए और घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में स्त्री पिता के वश में, यौवनावस्था में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन रहे, किंतु स्वतंत्र कभी न रहे। यह बात प्रत्यक्ष भी देखने में आती है कि जो स्त्रियां स्वतंत्र होकर रहती हैं, वे प्रायः नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं। विद्या, बुद्धि एवं शिक्षाके अभाव के कारण भी स्त्री स्वतंत्र ताके योग्य नहीं है।”
उपरोक्त दिए गए उद्धरण गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों का है। अब सवाल यहां यह उठता है कि राज्य ने गीता प्रेस संस्थान को क्यों सम्मानित किया क्योंकि गीता प्रेस कोई साहित्यिक संस्था नहीं है क्योंकि साहित्य में आसमानी बातें नहीं होती न ही साहित्य कोई पवित्र जैसी चीज होता है और वहां ये दावा नहीं होता है कि हमारी किताब मनुष्य के धरती पर पैदा होने से पहले लिखी गई है जिस पर कोई तर्क नहीं हो सकता या चमत्कारिक जैसी बातें भी साहित्य की नहीं हैं। गीता प्रेस वर्ण व्यवस्था का हिमायती है। वर्णाश्रम और सनातन का प्रचार ही इसका उद्देश्य है। सनातन धर्म में स्त्रियों अछूतों के बारे में जो प्रतिगामी मूल्य स्थापित हैं गीता प्रेस उन्हीं का प्रचार-प्रसार करने का एक सशक्त माध्यम है। अगर राज्य ऐसे अंधवाद और प्रतिगामी विचारों को पुरस्कृत कर रहा है तो निश्चित उसकी मंशा और आस्था में ये विचार मूल्यवान हैं। गीता प्रेस को पुरस्कृत करके राज्य ने साहित्य को नहीं पुरस्कृत किया एक धर्म के संचार माध्यम को पुरस्कृत किया है ।