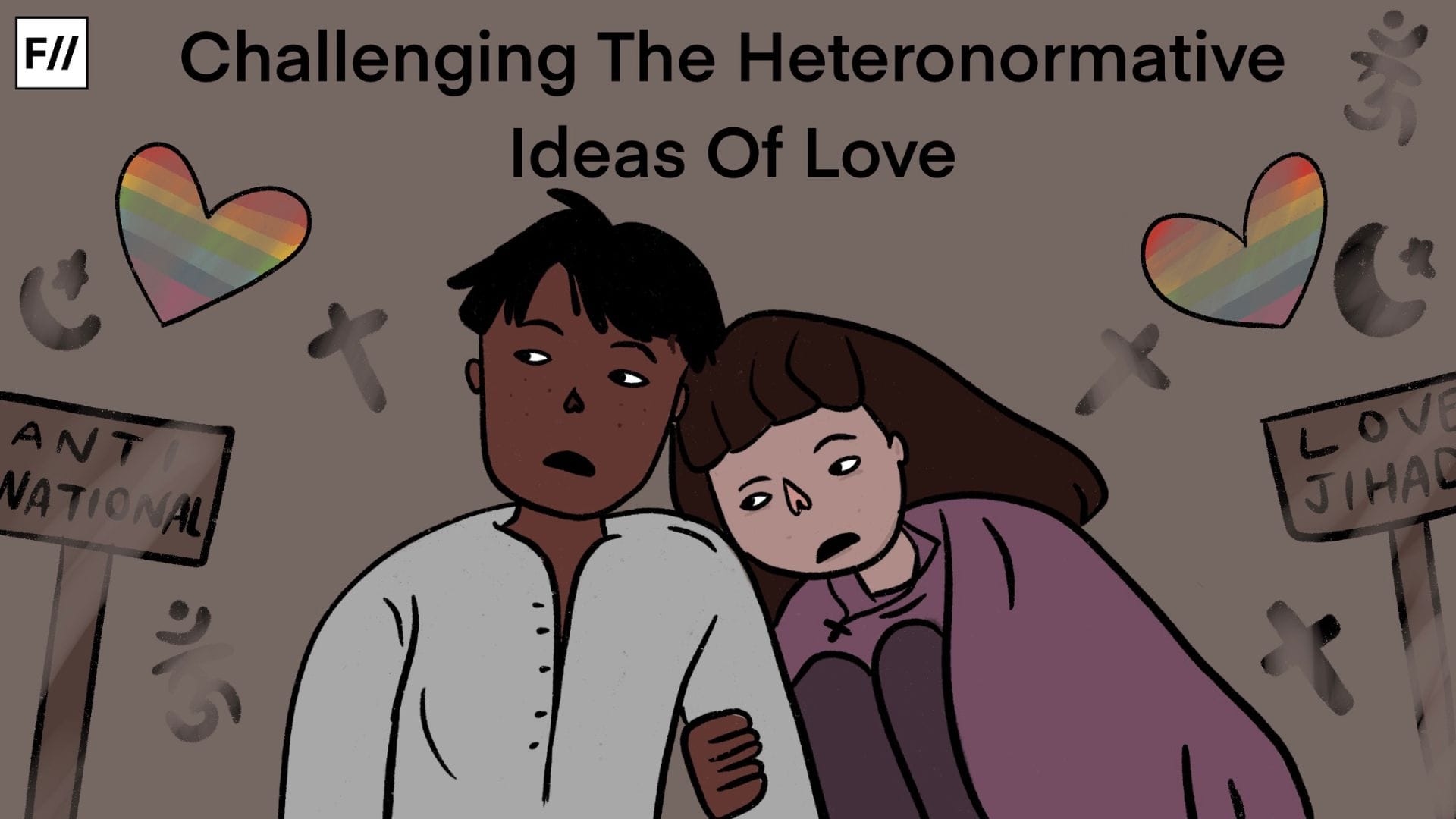भारत में, प्रजनन संबंधी 70 प्रतिशत समस्याएं पीरियड्स से जुड़ी स्वच्छता में कमी के कारण होती हैं। 21 वर्ष से कम आयु की 10 में से एक लड़की स्वच्छता उत्पादों का खर्च नहीं उठा पाती और अस्वास्थ्यकर विकल्पों का सहारा लेती है। 23 मिलियन लड़कियां पीरियड्स स्वच्छता सुविधाओं के अभाव या उपयुक्त न होने के कारण प्रतिवर्ष स्कूल छोड़ देती हैं। हाल ही में मुंबई में एक 14 वर्षीय लड़की की आत्महत्या से मौत हो गई क्योंकि वह अपने पहले पीरियड्स के दर्द से तनाव में थी। वहीं ठाणे में एक व्यक्ति ने अपनी 12 वर्षीय बहन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, कि उसके पहली बार पीरियड्स के खून के धब्बों को व्यक्ति ने शारीरिक संबंध समझ लिया। इन घटनाओं से समझ आता है कि आज भी पीरियड्स पर जागरूकता की कितनी कमी है। देश में एक ओर जहां एक तबका पीरियड्स के लिए चिंतित नहीं रहते, और इसे मैनेज करने के लिए खर्च उठा सकते हैं।
वहीं समाज का दूसरा तबका पीरियड्स की सही जानकारी से भी दूर है। हमारे देश में पीरियड्स हमेशा से ही रूढ़िवाद और मिथकों से घिरा रहा है, जो महिलाओं को सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं से बाहर रखता है। पीरियड्स पर बात करना आज भी एक टैबू है। कई समाजों में मौजूद पीरियड्स के बारे में ऐसी धारनाएं और नियम हैं, जो लोगों के, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं की भावनात्मक स्थिति, मानसिकता, जीवनशैली और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। हमारे देश में पीरियड्स के सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को संबोधित करने की चुनौती, लड़कियों के पीरियड्स और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी और समझ के स्तर के कारण और भी जटिल हो जाती है।
पीरियड्स स्वच्छता के बारे में हम जो सोचते और देखते हैं वह एक बहुत ही छोटा शब्द है, जो केवल उत्पादों तक पहुँच, पानी या स्वच्छता तक केंद्रित है। लेकिन मेन्स्ट्रूल स्वास्थ्य असल में स्वास्थ्य की एक स्थिति है जो शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ जीवन जीने के संकेतक हैं।
बात मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन और एमएचएच नीति की
अप्रैल 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों के प्रावधान के साथ-साथ, कक्षा 6 से 12 तक की सभी लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, मेन्स्ट्रूऐशन स्वास्थ्य और स्वच्छता (एमएचएच) पर एक ‘समान राष्ट्रीय नीति’ बनाने की वकालत की। पीरियड्स को आम तौर समाज या सरकार एक समावेशी मानवाधिकार मुद्दे की तरह नहीं देखती है, जहां न सिर्फ सभी जेंडर, बल्कि पीरियड हाइजीन और पीरियड हेल्थ की भी बात हो। वैश्विक स्तर पर, कम से कम 500 मिलियन महिलाओं और लड़कियों के पास पीरियड्स स्वच्छता प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है।

मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन पर बातचीत करते हुए सस्टैनबल मेन्स्ट्रूऐशन पर काम कर रही सामाजिक संस्था बूंद की संस्थापक भारती कन्नन कहती हैं, “पीरियड्स स्वच्छता के बारे में हम जो सोचते और देखते हैं वह एक बहुत ही छोटा शब्द है, जो केवल उत्पादों तक पहुँच, पानी या स्वच्छता तक केंद्रित है। लेकिन मेन्स्ट्रूल स्वास्थ्य असल में स्वास्थ्य की एक स्थिति है जो शारीरिक, मानसिक और स्वस्थ जीवन जीने के संकेतक हैं। इसमें विभिन्न पहलू जैसे कि यौवन से मेनोपॉज़ तक कैसे परिवर्तन होता है और पीरियड्स हो रहे व्यक्ति को गर्भावस्था, प्रसवोत्तर समय और इन सभी का उनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से संबंध शामिल हैं। इसलिए परिवार, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी प्रकार की जरूरतें भी इस दायरे में आती है।”
विभिन्न राज्यों में उनके विकासात्मक, लैंगिक विकासात्मक, स्वास्थ्य सूचकांकों, और उनकी स्कूली शिक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है, और इन सभी के साथ जल, स्वच्छता, स्थानीय प्रशासन, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ कार्यस्थलों के बीच संबंध के आधार पर विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक स्थानों के अलावा एक-दूसरे से जुड़ते हैं। हमें हाइपरलोकल या क्षेत्रीय संदर्भ में इनोवेटिव रणनीतियों की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से एक समान नीति नहीं हो सकती।
क्या समस्याओं का हल एक ‘समान राष्ट्रीय नीति’ है
हालांकि आज हम पीरियड्स से जुड़े कई कारकों में कुछ हद तक विकास कर चुके हैं। लेकिन पीरियड्स पर बातचीत का मतलब अमूमन सिर्फ इतना ही होता है कि किसी व्यक्ति के पीरियड्स शुरू हुए हैं। पीरियड्स के साथ देश के विभिन्न हिस्से में अलग-अलग सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़ि और मान्यताएं जुड़ी हैं। ऐसे में क्या एक समान राष्ट्रीय नीति कारगर होगी? इसपर भारती कहती हैं, “भारत को इस बात की आवश्यकता है, और वर्तमान नीति में भी यह बात है। तमाम उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके क्या होने चाहिए, यह कुछ ऐसा है जो नीति को निर्देश के रूप में प्रदान करना चाहिए, और यह स्पष्ट रूप से बताता है कि संसाधनों का उपयोग और आवंटन कहां से किया जा सकता है।”

वह आगे बताती हैं, “लेकिन विभिन्न राज्यों में उनके विकासात्मक, लैंगिक विकासात्मक, स्वास्थ्य सूचकांकों, और उनकी स्कूली शिक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है, और इन सभी के साथ जल, स्वच्छता, स्थानीय प्रशासन, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ कार्यस्थलों के बीच संबंध के आधार पर विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं, जो सार्वजनिक स्थानों के अलावा एक-दूसरे से जुड़ते हैं। हमें हाइपरलोकल या क्षेत्रीय संदर्भ में इनोवेटिव रणनीतियों की जरूरत है। लेकिन निश्चित रूप से एक समान नीति नहीं हो सकती।”
आज भी देश में एक बड़ा तबका पानी और शौचालय की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में उचित मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन एक विशेषाधिकार बन जाता है। मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन प्रबंधन सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिवर्ष 23 मिलियन लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जिसमें सैनिटरी पैड की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में जानकारी शामिल है।
क्या सरकार मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन को लेकर सोच रही है
मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन में एक बहुत बड़ी रुकावट रूढ़िवाद और पितृसत्तात्मक विचारधारा है, जहां पीरियड्स पर बातचीत पर मनाही है। साथ ही, आज भी देश में एक बड़ा तबका पानी और शौचालय की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में उचित मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन एक विशेषाधिकार बन जाता है। मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन प्रबंधन सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिवर्ष 23 मिलियन लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, जिसमें सैनिटरी पैड की उपलब्धता और पीरियड्स के बारे में जानकारी शामिल है। इस विषय पर झारखंड के निश्चय फाउंडेशन के संस्थापक तरुण कुमार कहते हैं, “गांव के स्कूलों में सरकार बच्चियों के लिए जो नैपकिन मुहैया करा रही है, उससे किशोरियाँ भी संतुष्ट नहीं हैं।”

वे आगे बताते हैं, “अमूमन इनकी क्वालिटी इतनी खराब रहती है कि आप इससे हाइजीन बनी रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। कई बार इन उत्पादों में एक्स्पाइरी डेट निकल चुकी होती है। दिल्ली में बैठे नीतिनिर्माण करने वाले ये नहीं समझ पाते कि देश के ग्रामीण इलाकों की क्या हालत है। अगर सरकार वाकई मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन और स्वास्थ्य पर काम करना चाहती है, तो अच्छे क्वालिटी के सस्ते सैनिटेरी नैपकिन जरुरतमन्द महिलाओं को सामान्य दुकानों से या राशन की दुकानों से मुहैया करा सकती है।” निश्चय फाउंडेशन स्कूली छात्राओं को निशुल्क सैनिटरी पैड देने और मेन्स्ट्रूऐशन स्वास्थ्य पर जागरूकता पर काम कर रही है।
दिल्ली में बैठे नीतिनिर्माण करने वाले ये नहीं समझ पाते कि देश के ग्रामीण इलाकों की क्या हालत है। अगर सरकार वाकई मेन्स्ट्रूऐशन हाइजीन और स्वास्थ्य पर काम करना चाहती है, तो अच्छे क्वालिटी के सस्ते सैनिटेरी नैपकिन जरुरतमन्द महिलाओं को सामान्य दुकानों से या राशन की दुकानों से मुहैया करा सकती है।
क्या पैड्स मुहैया कराना काफी है
सरकार ने बार-बार मुफ़्त पैड्स पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत में लगभग 77 फीसद महिलाएं आज पीरियड्स के दौरान सुरक्षा के स्वच्छ तरीकों का उपयोग करती हैं। लेकिन क्या हम इस मुद्दे पर विचार करते समय जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और धार्मिक कारकों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं? इस विषय पर भारती कहती हैं, “सुप्रीम कोर्ट का सभी लड़कियों के लिए मुफ्त पैड अनिवार्य करना एक स्वागत योग्य बदलाव है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि अलग-अलग समय पर, राज्य सरकारों ने, क्योंकि यह राज्य का विषय भी है, इस पर जोर दिया है। वास्तव में यह जांचना जरूरी है कि यह क्यों कारगर नहीं हुआ और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या सिर्फ पैड उपलब्ध कराने से पीरियड्स से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हल हो जाती हैं? जैसे पीरियड्स से जुड़ी शर्म, सम्मान की जिंदगी जीना, स्वास्थ्य संसाधनों की तलाश और उन तक पहुंच बनाना, पानी और स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं, इन सभी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।”
क्या सिर्फ पैड उपलब्ध कराने से पीरियड्स से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हल हो जाती हैं? जैसे पीरियड्स से जुड़ी शर्म, सम्मान की जिंदगी जीना, स्वास्थ्य संसाधनों की तलाश और उन तक पहुंच बनाना, पानी और स्वच्छता की बेहतर सुविधाएं, इन सभी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
2005 और 2010 के बीच, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका में एमएचएच को एकीकृत किया। 2010 में, किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए मेन्स्ट्रूल स्वच्छता योजना (एमएचएस) शुरू की गई। 2011 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेन्स्ट्रूल हाइजीन प्रबंधन दिशानिर्देश जारी किए। 2015 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अतिरिक्त निर्देश जारी किए। 2012 में, निर्मल भारत अभियान में एमएचएच को एजेंडे के रूप में शामिल किया गया। इन पहलों ने भारत में स्वच्छता उत्पादों के उपयोग को जरूर बढ़ाया है। लेकिन आज भी जागरूकता और स्वच्छता उत्पादों तक विशेषाधिकार बना हुआ है। इस विषय पर मेन्स्ट्रल हेल्थ और सेक्शूऐलिटी एज्यूकेटर राजसी कुलकर्णी दिवाकर कहती हैं, “हालांकि आज गांवों में भी पीरियड्स स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता बढ़ी है। जैसे आज कई लोगों को पता है कि 2-3 घंटों में पैड बदलने की जरूरत है। पर उनके लिए कई बार इस हिसाब से पैड या सुरक्षित उत्पाद पर खर्च मुमकिन नहीं होता।”

मेन्स्ट्रूल हाइजीन, स्वास्थ्य और सस्टैनबल उत्पादों के विषय में राजसी कहती हैं, “लोगों को नए उत्पाद का उपयोग शुरू करने में भी समय लगता है। जरूरी ये है कि हम लोगों की जरूरतों को समझें, उनकी जागरूकता, सामर्थ्य और इलाके के हिसाब से अपनी योजनाओं को बनाएं। समस्या ये भी है कि पीरियड्स के विषय में काम कर रहा हर व्यक्ति या संस्था अपने अनुसार काम कर रहा है। ऐसा कोई निश्चित गाइड्लाइन नहीं है, जिसका हर कोई अनुसरण कर काम कर सके। देश में विविधता के कारण एकरूपता नहीं होगी। लेकिन, हमें हमारे पॉलिसी का आकलन महत्वपूर्ण तरीके से करने की जरूरत है। साथ ही, जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, उन्हें भी अपने योजनाओं का आकलन करने की जरूरत है।” पीरियड्स में साफ-सफाई की आम धारणा के उलट, ये सिर्फ सैनिटेरी पैड के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। गौर करें, तो ये समझ आता है कि कोई भी व्यक्ति पीरियड्स में हाइजीन को कितना महत्व दे रहा है और इसे कितना प्रभाव में ला पा रहा है इसका संबंध उसकी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति से भी जुड़ी है। सरकार को व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान, रूढ़िवाद को दूर करने की नीति और योजनाओं पर काम करना होगा। साथ ही, परिवार, समुदाय और समाज को भी समावेशी नजरिए के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी।