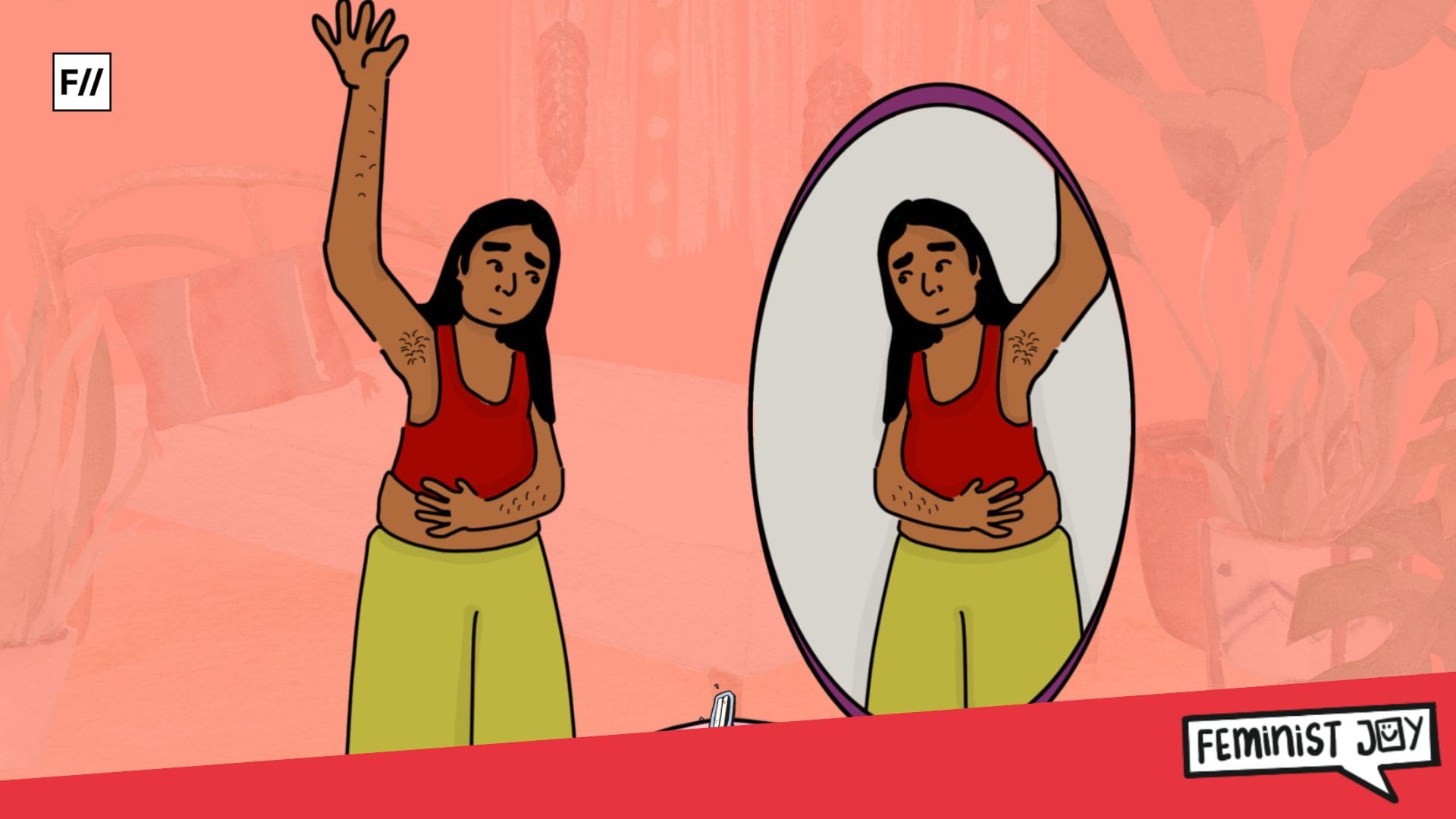नारीवाद के साथ मेरी यात्रा अजनबी तौर पर शुरू हुई थी इसलिए जब मैं अपने आपको अनजान फेमिनिस्ट कहती हूं तो इसके पीछे मेरे बचपन का पूरा परिवेश है। मैं तब से बराबरी के लिए हमेशा से लड़ती आई हूं जब मुझे फेमिनिज़म के बारे में बिलकुल पता नहीं था। मुझे लगता है मेरे पिता जी भी फेमिनिज़म से बिलकुल नहीं के बराबर परिचित होंगे। मैं अकेले दो बड़े भाइयों के बीच पली बढ़ी हूं। परिवार में छोटी होने के नाते भी यह लाड-प्यार हो सकता है लेकिन मेरे पिता जी और माँ के मुंह से हमेशा यही सुना है, “तुम तीनों में हमने किसी को कभी बेटा या बेटी के नज़रिये से कुछ कम नहीं देखा।” दोनों की बात सच भी है।
मेरे आस-पास की लड़कियां जब अपनी शादी के लिए जुटाये गये गहनों की बातें करती थीं तो कभी मैंने भी अपने पिता जी से कहा था, “सबके पास कितने सोने के गहने हैं और अभी सोना सस्ता हुआ। आप मेरे लिए लेकर क्यूं नहीं रख रहे हैं?” हालांकि मैंने मज़ाक में कहा था। फिर पिता जी का जवाब सुनकर अब लगता है वो कितने बड़े फेमिनिस्ट हैं जबकि उन्हें इसका पता भी नहीं है। बहुत धीर होकर उन्होंने मुझे जवाब दिया, “मेरी ज़िम्मेदारी तुम सबको पढ़ाना है। चाहे मुझे इसके लिए अपना खेत बेचना पड़े या कुछ और मैं इसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन इन सबके बावजूद ये सोच रखो आखिर में शादी भी मैं ही करवाऊं तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना। मेरी इतनी औकात नहीं है। सारी जमा पूँजी तुम सबकी पढ़ाई में खर्च कर देता हूं। पढ़-लिखकर कमाओ और खुद शादी करो अपने पैसों से। मैं इन सबकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा हूं।” उस दिन जैसे पंख लग गये हो। लगा जैसे पिता जी की आँखें मुझे कितनी ज़िम्मेदारी से देख रही हैं।
मैं अपनी पसंद की चीजें करने में कभी नहीं रुकी चाहे परिस्थितियां मेरे अनुकूल हों या प्रतिकूल। मेरे भीतर हमेशा का ये विद्रोह मुझसे कब कवितायें लिखवाते चला गया मुझे बिलकुल पता नहीं चला। हर छोटी चीज़ को अहमियत देते मैं उन्हें महसूस करते हुए कब उनकी तस्वीरें लेने में दिलचस्पी लेने लग गई इसका भी पता नहीं चला।
मेरे लिए बाहर निकल कर पढ़ाई करना आर्थिक तौर पर मुश्किल रहा लेकिन परिवार और पिता जी को हमेशा मैंने अपने आस-पास पाया। समाज की जो कुंठा है कि घर बेटों से चलता है इस रूढ़ि को तोड़ते हुए पिता जी मुझे और भाईयों को दिल्ली साथ पढ़ाई के लिए भेजा था। बड़े भाई का पढ़ाई में मन नहीं लगा और छोटे भाई को घर पर बीमार माँ और पिता जी के अकेले रहने पर चिंता होने लगी। तब मेरे छोटे भाई ने समझौता किया “पढ़ाई कोई भी करे तुम करो या मैं करूं कामयाब तो पिता जी का बच्चा ही होगा।” मेरे भाइयों ने भी पिता जी की वही बराबरी देखते-देखते सीख ली थी जिसकी बदौलत छोटे भाई माँ के पास घर सँभालने चले गये और मैं दिल्ली में ही रह गई। नई मंजिल, नई उड़ान भरने के लिए।
आज मैं कह सकती हूँ मेरे पिताजी कहीं भी अपने बच्चों का ज़िक्र करते हैं तो उनमें सबसे ऊपर वो मुझे रखते हुए मेरे बारे में बताते हैं। जिस बराबरी के लिए संघर्ष करते कई सदी हो गई कुछ कम पढ़े-लिखे गाँव के लोगों तक उस बराबरी का सबक कैसे पहुंचा? क्या पढ़-लिख भर लेने से रूढियों को चुनौती दी जा सकती है? इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में मैंने अपने बहुत करीब से देखा है। इन ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों के लिए मेरी हेय दृष्टि तब बननी शुरू हुई जब मैंने सुना “ब्याह करने के लिए ज्यादा पढ़ी-लिखी लड़कियां नहीं चाहिए या फिर नौकरी पेशा वाली लड़कियां नहीं चाहिए। घर चलाने में उन्हें दिक्कत होगी।”
वे अपने बच्चों के लिए नौकरानियां ढूंढते हैं या बहु उनसे पहला प्रश्न ये है? तर्क पूछने पर कहते हैं अगर दोनों बाहर जॉब करेंगे तो घर में कौन काम करेगा?, क्या उनके बेटों के लिए घर में काम नहीं होता है? जब-जब ऐसी बातें सामने आती हैं, मैं मजबूर हो जाती हूं यह भेद कर पाने में कि क्या अधिक पढ़-लिख लेने से लोग रूढ़ियों को तोड़ते हैं? पिता जी सबके साथ रहते हुए भी अलग हैं, उन्होंने अपने दोनों बेटों से मुझे कभी कम नहीं समझा। बचपन में हम तीनों की शॉपिंग पिताजी करके लाते थे। कपड़े, जूते, चप्पल लाकर रख देते थे ये कहते हुए कि ‘जिसे जो आ जाये पहन लेगा।’ इस तरह बचपन में मैंने अपने भाइयों से अलग कपड़े, जूते, चप्पल तक भी कभी नहीं पहनें।

भाइयों के साथ-साथ पिता जी मुझे भी नाई की दुकान पर ले जाते और वहीं तीनों के बालों की कटाई एक जैसी होती थी। ये बहुत छोटी-छोटी चीजें जो याद आने पर अब बहुत ख़ुशी देती हैं। वो बचपन का मेरा परिवेश था जो मुझे अब हमेशा बराबर बने रहने के लिए विद्रोही बनाता है। बचपन खत्म होने के बाद समाज अब जब कभी मुझे पुरुषों से कम आँकने की कोशिश करता है, तब मुझे बचपन में दी जाने वाली बराबरी याद आती है। मैं उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर पाती हूं। मेरा यह बर्दाश्त नहीं कर पाना ही धीरे-धीरे मुझे विद्रोही और पितृसत्तात्मक समाज में नारीवादी बनाता चला गया। मैं अपनी इस यात्रा से बिलकुल अनजान थी। नारीवाद के परिचय से पहले भी मेरी वही विद्रोही प्रकृति मेरे भीतर हिलोरें मारती रहती थीं। अब नारीवाद और लैंगिक असमानता को बहुत करीब से देख कर सुन कर समझ पाती हूं कि मैं नारीवादी बहुत पहले से थी।
मेरे लिए बाहर निकल कर पढाई करना आर्थिक तौर पर मुश्किल रहा लेकिन परिवार और पिता जी को हमेशा मैंने अपने आस पास पाया। समाज की जो कुंठा है कि घर बेटों से चलता है इस रूढ़ि को तोड़ते हुए पिता जी मुझे और भाईयों को दिल्ली साथ पढाई के लिए भेजा था।
मैं अपनी पसंद की चीजें करने में कभी नहीं रुकी चाहे परिस्थितियां मेरे अनुकूल हों या प्रतिकूल। मेरे भीतर हमेशा का ये विद्रोह मुझसे कब कवितायें लिखवाते चला गया मुझे बिलकुल पता नहीं चला। हर छोटी चीज़ को अहमियत देते मैं उन्हें महसूस करते हुए कब उनकी तस्वीरें लेने में दिलचस्पी लेने लग गई इसका भी पता नहीं चला। मैं अपनी यात्रा के कुछ पता नहीं होने पर ये ज़रूर पता लगा कर कह सकती हूं कि मैं अपने पसंद के रास्ते पर जब जिस ओर दिल खींच लेता है, बिना किसी बंधन के उस ओर चल पड़ती हूं।
मैं इंटर्नशिप करने से हमेशा कतराती थी ये सोचते हुए कि समय का नुकसान होगा लेकिन अब इस पहली पूरी यात्रा के बाद मैं अपने भीतर एक अलग आत्मविश्वास और हिम्मत महसूस कर रही हूं। जब किसी विषय पर पूरी खोज-बीन करके एक आर्टिकल तैयार करती हूँ तब मैं अपने भीतर अभी तक के छुपे हुए शोधकर्ता से मिलती हूं और लगता है जैसे कितने और कुछ मेरे अंदर छुप कर बैठे हुए है, मुझे उन सबको बाहर निकालना है। तब यह हिम्मत दुगुना नहीं बल्कि कई गुना बढ़कर मुझे प्रेरित करती रहती है। मेरी यह अनजान नारीवादी यात्रा मेरे बहुत ‘मैं’ को बाहर खींच निकाल कर मुझसे जान पहचान की यात्रा है।