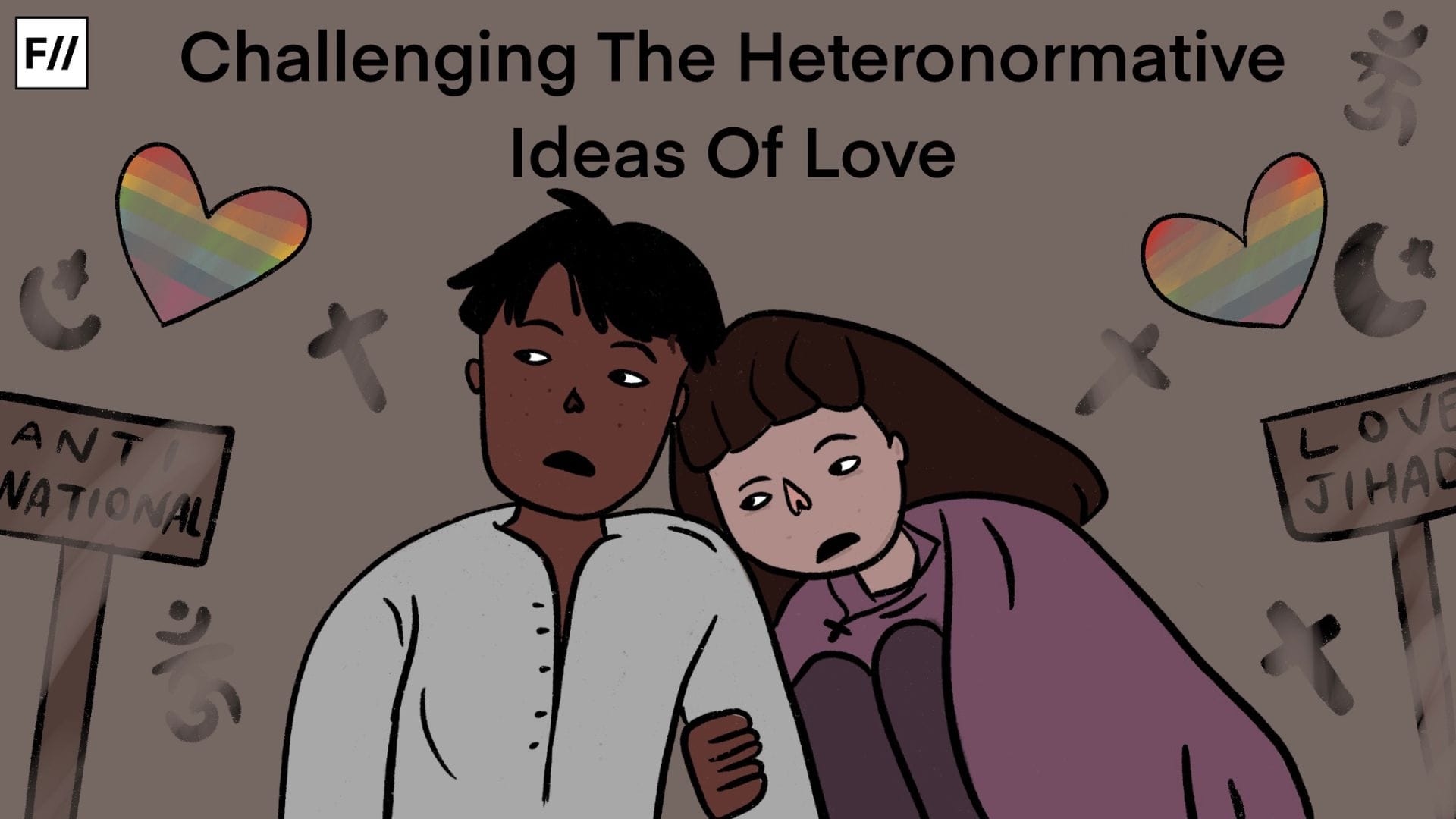हमारे समाज में अक्सर बच्चों की परवरिश को उनके खान-पान, सुरक्षा और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने तक ही सीमित समझा जाता है। इनके मानसिक सेहत और व्यक्तित्व विकास के लिए और भी ज़रूरी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा घर के बड़े-बुजुर्गों के सामने बच्चों की सहमति या असहमति भी कोई ख़ास मायने नहीं रखती। यह बात भी बचपन से ही बच्चों के मन में बिठा दी जाती है कि बड़े-बुजुर्ग सिर्फ़ उम्र में बड़े होने की वजह से आदर और सम्मान के पात्र हैं और उनकी बात माननी चाहिए। अब जबकि बच्चों की सुरक्षा और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जा रहा है फिर भी सहमति जैसे ज़रूरी मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादातर माता-पिता और अध्यापकों क्या मानना है कि बच्चों को सहमति समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े होने पर वह ख़ुद ही सीख जाएंगे। हालांकि बड़े होने पर भी जब ये अपने कॅरियर या जीवनसाथी कुछ चुनने का फैसला करते हैं तब भी घर के बड़े उसे अपनाते नहीं और अपनी मर्ज़ी थोपते हैं। ऐसे में सहमति का महत्त्व बच्चों को सिखाने के साथ ही घर के बड़ों को सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि सहमति का संबंध सिर्फ यौन शिक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि स्वस्थ रिश्ते बनाने और निभाने में भी इस की अहम भूमिका है।
बच्चों को ‘सहमति’ के बारे में सिखाना क्यों ज़रूरी है?
जब बच्चों की इच्छाओं और सीमाओं का सम्मान किया जाता है तो उन्हें यह एहसास होता है कि उनके विचार और भावनाएं मायने रखती हैं। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और वे आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे बच्चों को सही और ग़लत के बीच का फ़र्क समझने में मदद मिलती है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2016 से लेकर 2022 तक बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से मामलों में 96 फीसद की बढ़ोत्तरी देखी गई है जो कि बेहद चिंताजनक है। हालांकि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अपराधियों की मानसिकता को समझने और उनमें सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है कि कोई भी उनकी सहमति या इच्छा के बिना उन्हें छू नहीं सकता। ऐसा होने पर वे अपने माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद करीबी व्यक्ति से ऐसी बातें साझा कर सकें।
जब बच्चों को यह पता होता है कि उनकी सहमति या असहमति मायने रखती है तो वह भी दूसरों की सहमति, असहमति और सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। यह उन्हें एक संवेदनशील इंसान बनाता है जिससे वे भविष्य में परिवार, दोस्त, साथी और दूसरों के साथ रिश्ते निभाने के लिए बेहतर इंसान साबित होते हैं।
राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक डॉ. संजू सदानीरा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, “बच्चों के साथ किसी तरह की अवांछित यौनिक दुर्घटना न हो इसलिए बच्चों को बचपन से ही सहमति का मतलब सिखाना चाहिए। अगर कोई बहुत प्यार से डील करे तो ज़रूरी नहीं कि वह स्वस्थ व्यवहार हो, हो सकता उस अपनत्व और दिखाई देते प्यार के पीछे बच्चों के साथ यौन अपराध की मंशा हो। ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में भी सिखाना चाहिए जिससे ऐसी स्थिति आने पर बच्चे भरोसेमंद करीबी के साथ साझा कर सकें। बच्चों को सीखने के लिए ऐसी शॉर्ट फिल्में, कार्टून या कहानियों की सहायता ली जा सकती है, जिसमें सर्वाइवर बच्चे ने अपने शोषक को पेरेंट्स के जरिए पुलिस के हवाले करवाया हो। इसके साथ ही यह सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे बच्चे दूसरों की सहमति का सम्मान करना सीख सकें।”
स्वस्थ संबंधों की नींव
जब बच्चों को यह पता होता है कि उनकी सहमति या असहमति मायने रखती है तो वह भी दूसरों की सहमति, असहमति और सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं। यह उन्हें एक संवेदनशील इंसान बनाता है जिससे वे भविष्य में परिवार, दोस्त, साथी और दूसरों के साथ रिश्ते निभाने के लिए बेहतर इंसान साबित होते हैं। इसके साथ ही जब बच्चों को सिखाया जाता है कि वह अपने से शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के बारे में ख़ुद अपने फ़ैसले ले सकते हैं तो उनमें फ़ैसले लेने के लिए आत्मविश्वास और ज़िम्मेदारी की भावना आती है। इससे वे जीवन के हर क्षेत्र में बिना किसी दबाव के अपने फ़ैसले ख़ुद ले पाते हैं।
प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के शिक्षक मिथुन खरवार ने अपने विचार कुछ इस तरह साझा किया, “बच्चों को कम उम्र में ही सहमति का मतलब सिखाना बेहद ज़रूरी है जिससे वह अपनी और दूसरों की सीमाओं को समझ सकें। इससे उनमें आत्मसम्मान और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। यह सीख उन्हें खेल-खेल में दी जा सकती है जिससे वे इसे बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। जैसे- दूसरे बच्चों के किताबें, खिलौने या दूसरी चीजें लेने से पहले अनुमति मांगना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर एक संवेदनशील, ज़िम्मेदार और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले नागरिक बनते हैं।”
बच्चों को ‘सहमति’ के बारे में कैसे सिखाएं?
बच्चों को सहमति के बारे में सिखाने के लिए उनकी सहमति का सम्मान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कहने समझने के बजाय देखकर जल्दी सीखते हैं। बहुत सारे लोग बच्चों के प्रति प्यार जताने के लिए उन्हें छूते हैं, चूमते हैं या गले लगाते हैं, ऐसे में बच्चों की इच्छा और सहमति या असहमति को सबसे पहले देखा जाना चाहिए। अगर बच्चा असहज महसूस कर रहा हो तो उसे मना करने का अधिकार देना चाहिए। इससे बच्चों को एहसास होगा कि सहमति किसी भी इंसान के लिए कितना मायने रखती है।
इसी तरह बच्चों को दूसरों की सहमति और असहमति का सम्मान करना भी सिखाना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर बच्चा किसी चीज जैसे कि मोबाइल या दूसरों के खिलौने के लिए जिद कर रहा है तो उसे सिखाना चाहिए कि पहले दूसरों की सहमति मांगना ज़रूरी है, उसके बाद ही वह उसे ले सकता है। यहां तक कि बच्चों के खिलौने, किताबें या कोई भी सामान लेने से पहले उनसे सहमति लेनी चाहिए। बच्चों को बचपन से ही ‘न’ कहने और सुनने दोनों की आदत होनी चाहिए। बच्चों को सिखाना ज़रूरी है कि किसी चीज के लिए ‘न’ कहना भी पूरी तरह से ठीक है।
जब बच्चों को यह पता होता है कि उनकी सहमति या असहमति मायने रखती है तो वह भी दूसरों की सहमति, असहमति और सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं।
बच्चों को कार्टून और कहानियां बहुत पसंद होती हैं। इनका उपयोग बच्चों को सिखाने के लिए भी किया जा सकता है जिससे बच्चे उन्हें रुचि लेकर सीख सकें। बच्चों को कभी उपदेश वाली भाषा में नहीं सिखाना चाहिए वरना वे बोरियत महसूस करते हैं और सीखना नहीं चाहते। उन्हें कविता, कहानी या कार्टून के माध्यम से सिखाना सबसे अच्छा उपाय है। इसी तरह उनकी दिनचर्या में सहमति और असहमति को शामिल करें।
माता-पिता ख़ुद एक अच्छा उदाहरण बनें

बच्चे अक्सर घर से और अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। न सिर्फ़ बच्चों के साथ बल्कि घर में मौजूद लोगों की सहमति और असहमति का सम्मान करें। बच्चे इससे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे न कि सिर्फ़ समझाने से। इसके अलावा छोटी-मोटी चीजों में बच्चों की राय लेनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब बात उनकी दिनचर्या से जुड़ी हो। जैसे बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना ज़रूरी है लेकिन इसके साथ ही बच्चों को उनके डाइट प्लान बनाने में भी शामिल करें। इसके अलावा उनके कपड़ों, जूतों या दूसरी चीजों को खरीदते वक़्त उनकी राय लें। बच्चों से कोई बात जबरदस्ती मनवाने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें।
बच्चों को सहमति का मतलब सिखाने के लिए साझा गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। सब मिलकर कोई खेल खेल सकते हैं या फिर साथ में कोई पसंदीदा खाना बना सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे नाटक या फ़िल्में साथ में देख सकते हैं या फिर कार्यशाला में भाग ले सकते हैं, जिसमें इस तरह की बातें मौजूद हों। इस तरह बच्चों को सहमति का सम्मान करना सिखाया जा सकता है जो इनके व्यक्तित्व के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।

स्कूल और शिक्षकों की भूमिका
घर के बाद बच्चों का सबसे ज़्यादा समय स्कूल में गुज़रता है। इसलिए उन पर स्कूल में हो रही गतिविधियों का असर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। बच्चे अक्सर अपने शिक्षक की बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसलिए शिक्षकों को इस विषय में जागरुक किया जाना बेहद ज़रूरी है जिससे वह बच्चों को सहमति और असहमति सिखाने में योगदान दे सकें। इसके लिए विशेषज्ञों के दिशानिर्देश में स्कूल में शिक्षकों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप आयोजित किया जा सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को सहमति पर आपस में विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए भी विशेष कार्यक्रम रखे जा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में होने वाली गतिविधियों में भी सहमति-असहमति को मॉनिटर किया जाना ज़रूरी है। बच्चों के खेलकूद, पढ़ाई-लिखाई और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस बारे में पुणे, महाराष्ट्र की रहने वाली स्कूल शिक्षिका अर्चना ने बातचीत के दौरान बताया, “अगर बचपन से ही सही नींव डाली जाए तभी हम एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर चीजें घर स्कूल और आसपास के माहौल से सीखते हैं इसलिए सबसे ज्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को घर में और स्कूल में सहमति का मतलब सिखाया जाए और दूसरों की सहमति का सम्मान करना भी सिखाया जाए। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं न कि उपदेश देने से, इसलिए माता-पिता और शिक्षकों की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वह बच्चों के सामने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जिसे बच्चे अनुकरण कर सकें।”
बच्चों को सहमति का मतलब सिखाने के लिए साझा गतिविधियां आयोजित की जा सकती हैं। सब मिलकर कोई खेल खेल सकते हैं या फिर साथ में कोई पसंदीदा खाना बना सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे नाटक या फ़िल्में साथ में देख सकते हैं या फिर कार्यशाला में भाग ले सकते हैं, जिसमें इस तरह की बातें मौजूद हों।
बचपन से ही सहमति के बारे में सीखने से बच्चे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और सुरक्षा का एहसास भी होता है। व्यक्तिगत हितों के साथ-साथ भविष्य में आने वाले रिश्तों और समाज में उनको बेहतर नागरिक बनाने के लिए भी यह ज़रूरी है। जब बच्चों की सहमति या सहमति का ध्यान रखा जाता है तो उनके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को भी विकसित किया जा सकता है। इससे भविष्य में उनके अपराध की ओर बढ़ने की आशंका कम होती है। इस प्रकार सहमति की ऐसी न सिर्फ उन्हें सुरक्षित और आत्मविश्वास से भरपूर बनाएगी बल्कि एक संवेदनशील समझदार और जागरुक नागरिक बनाने में भी मदद करती है।