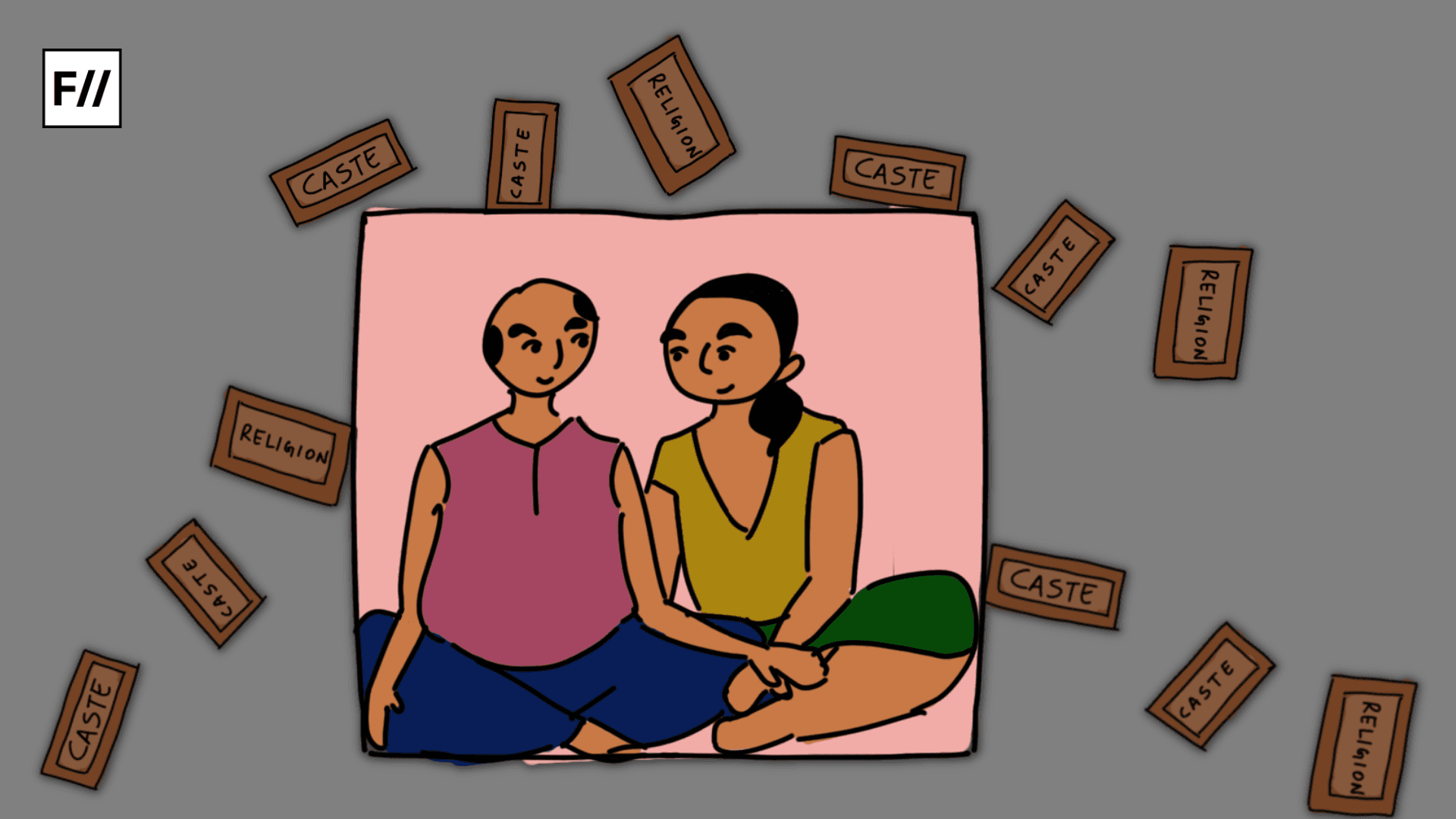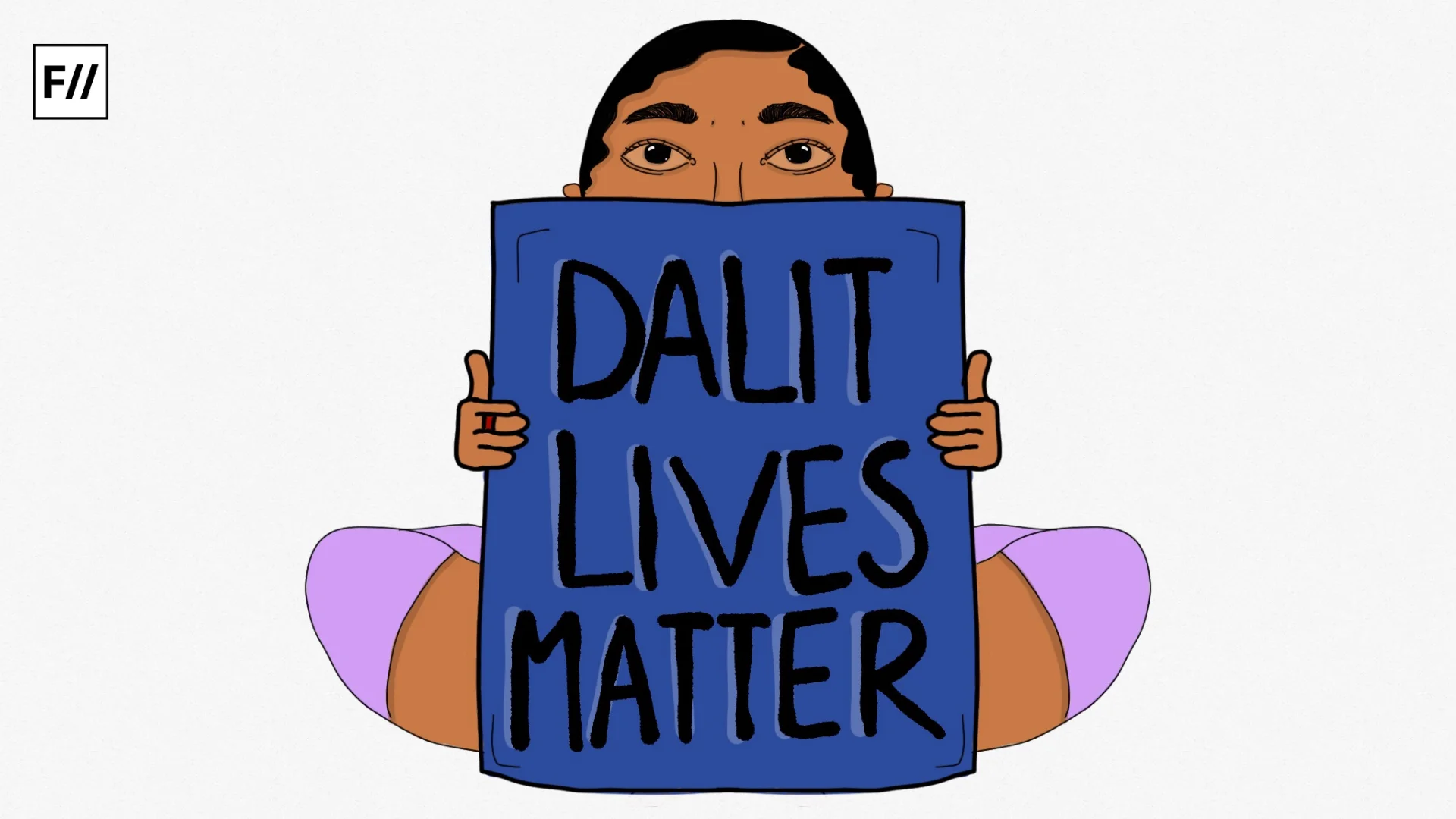भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान दर्ज़ा 1950 में ही दे दिया, लेकिन इतने दशक बीत जाने के बावजूद आज भी ज़मीनी स्तर पर यह लागू नहीं हो पाया है। समाज में जाति, धर्म, लिंग, यौनिकता आदि आधारों पर ग़ैर बराबरी और भेदभाव बना हुआ है। सदियों से हाशिए पर डाल दिए गए समुदाय ख़ासकर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। 90 के दशक से शुरू हुए क्वीयर आंदोलनों की बदौलत समय-समय पर क़ानून में कुछ सकारात्मक बदलाव ज़रूर देखने को मिले, लेकिन अभी भी ऐसे आंदोलनों की ज़रूरत बनी हुई है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए होमोसेक्सयूअल संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन शादी, एडॉप्शन जैसे मामलों में चुनौतियां अभी भी बरक़रार हैं। एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन का मकसद समानता, अधिकार और समावेशिता को बढ़ावा देना है। लेकिन इस आंदोलन के भीतर भी बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें से एक बड़ी समस्या एलीटिज़्म है, जो आंदोलन की मूल भावना समावेशिता की राह में बाधा का काम करती है।
एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन में एलीटिज़्म क्या है?
एलीटिज़्म एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन में उस स्थिति को कहा जाता है जब समुदाय के भीतर कुछ ख़ास समूहों को ज्यादा महत्व दी जाती है। इसका आधार जाति, वर्ग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, परिवेश, शिक्षा या भाषा कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब आंदोलन के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और सम्पन्न वर्ग का प्रभाव हावी हो जाता है और वंचितों पिछड़ों की आवाज दब जाती है। अक्सर देखा जाता है कि एलजीबीटीक्यू+ आंदोलनों में सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त, महानगरों में रहने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग भाग लेते हैं और चलाते हैं जबकि गरीब, ग्रामीण, दलित और अंग्रेज़ी न बोल पाने वाले क्वीयर समुदाय के लोग पीछे छूट जाते हैं। इससे आंदोलन का असली मकसद अधूरा रह जाता है।

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के रहने वाले इंटरसेक्शनल फ़ेमिनिस्ट क्वीयर एक्टिविस्ट धर्मेश चौबे इस विषय पर बताते हैं, “क्वीयर मूवमेन्ट कोई इस्टैबलिश्ड सेंट्रलाइज्ड मूवमेन्ट नहीं है। लोग अपने-अपने तरीकों से अपनी-अपनी जगह पर अपना काम करते हैं। गांवों में भी कुछ क्वीयर लोग अपनी आज़ादी से अपने तरीके से परिवारों में रहते हैं। बाकी एलीटिज़्म अपने अलग-अलग रूप में समाज के हर वर्ग में मौजूद है और एलजीबीटीक्यू+ कम्युनिटी इसी समाज का एक हिस्सा है। एजुकेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनामिक स्टेटस जैसे फैक्टर्स क्वीयर कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। यह मानकर चलना है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, इसलिए इसमें बाकी सब ठीक होगा, एक ग़लत धारणा है। दरअसल हमें आइडियल और पर्फेक्ट विक्टिम की तलाश रहती है जो कि ठीक नहीं है।”
एजुकेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनामिक स्टेटस जैसे फैक्टर्स क्वीयर कम्युनिटी में ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। यह मान कर चलना है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है इसलिए इसमें बाकी सब ठीक होगा, एक ग़लत धारणा है। दरअसल हमें आइडियल और पर्फेक्ट विक्टिम की तलाश रहती है जोकि ठीक नहीं है।
आंदोलन में शहरी बनाम ग्रामीण का बंटवारा
2 जुलाई 1999 को जब कोलकाता में भारत के पहले क्वीयर प्राइड परेड की शुरुआत हुई, इसके बाद धीरे-धीरे यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में नियमित तौर पर इसका आयोजन किया जाने लगा। हालांकि अब देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे शहरों में भी प्राइड परेड या प्राइड वॉक का आयोजन हो रहा है, लेकिन अभी भी देश के छोटे कस्बे और गांव इससे अछूते हैं। आज भारत की लगभग 65 फीसद आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में गांवों तक ऐसे आंदोलनों की पहुंच न होना समावेशिता की दिशा में एक बड़ा मसला है। बिहार के सिवान की क्वीयर समुदाय की कसक बताती हैं, “मैं बिहार की एक छोटे से कस्बे से आती हूं, यहां पर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति जागरुकता काफ़ी कम है। इससे जुड़े जो भी आंदोलन होते हैं, जैसे प्राइड परेड से लेकर क़ानूनी अधिकार के लिए संघर्ष, इन सब का असर ऐसे दूरदराज़ के इलाकों में कम ही पहुंच पाता है। हालांकि जेंडर बाइनरी के खाते में बँटे होने के बावजूद हमारे यहां की भाषा जिसमें ‘मैं’ को ‘हम’ कहा जाता है, काफ़ी हद तक समावेशी है। किसी भी जेंडर का व्यक्ति इसे इस्तेमाल करता है तो अपनी आइडेंटिटी को लेकर असमंजस और असुविधा से कुछ हद तक बच जाता है।”
मैं बिहार की एक छोटे से कस्बे से आती हूं, यहां पर एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के प्रति जागरुकता काफ़ी कम है। इससे जुड़े जो भी आंदोलन होते हैं जैसे प्राइड परेड से लेकर क़ानूनी अधिकार के लिए संघर्ष, इन सब का असर ऐसे दूरदराज़ के इलाकों में कम ही पहुंच पाता है।
महानगरों में क्वीयर समुदाय को लेकर चर्चा और विचार-विमर्श लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारे महानगरों में तो एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए ख़ासतौर पर क्लब और कैफै जैसी जगहें बन रही है, जिससे उनके लिए मिलने-जुलने और सोशलाइज करने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाती है। हालांकि गांवों में आज भी इस पर बात करना टैबू माना जाता है। गांवों में क्वीयर समुदाय के पास इतनी सहूलियत नहीं होती कि वह अपने बारे में जान सकें। अगर इंटरनेट और सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा कर भी लेते हैं, तो भी उन्हें अपनी पहचान और यौनिकता ज़ाहिर करने के लिए सामाजिक तौर पर मान्यता नहीं मिल पाता।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाली नीलम (बदला हुआ नाम) शादीशुदा गृहिणी हैं। वह बताती हैं, “मुझे एलजीबीटीक्यू+ का मतलब नहीं पता था। घरवालों ने शादी करा दी और सबकी मर्ज़ी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हालांकि हमेशा से ही शादी, बच्चे और यह ज़िंदगी रास नहीं आई, लेकिन क्या करें और कोई चारा भी तो नहीं है। समाज में रहना है तो शादी और बच्चे तो करने ही पड़ते हैं।”
मुझे हिंदी भाषा में ही पढ़ना, लिखना, बोलना सहज लगता है। लेकिन जबसे मुझे अपने ओरिएंटेशन के बारे में पता चला तब से मैंने इस बारे में इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे हिंदी में कोई ढंग की जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अंग्रेज़ी के लिखे को अनुवाद करके पढ़ पाना और भी कठिन होता है।
अंग्रेज़ी भाषा का दबदबा और क्वीयर समुदाय
क्वीयर आंदोलन में हमेशा से ही अंग्रेज़ी भाषा का दबदबा रहा है। इससे जुड़े आंदोलनों के कार्यक्रम और दस्तावेज़ ज्यादातर अंग्रेज़ी भाषा में होते हैं। यहां तक कि हिंदी भाषा में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय से जुड़ी अपनी शब्दावली ही नहीं है। जब भी किसी विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, लोग पत्र-पत्रिकाओं, किताबों और ख़ासतौर पर इंटरनेट पर मौजूद दस्तावेज खंगालते हैं। क्वीयर समुदाय के लोग भी अपनी जेंडर पहचान और यौनिकता को लेकर जब भ्रम की स्थिति में होते हैं तो यही करते हैं। अफ़सोस की बात यह है कि अब भी क्वीयर समुदाय और आंदोलनों से जुड़े दस्तावेज़ और मानक सामग्री ज़्यादातर अंग्रेज़ी भाषा में ही मौजूद है। हमारे देश में हिंदी और दूसरी स्थानीय भाषाएं बोलने वालों की संख्या अंग्रेज़ी बोलने वालों की तुलना में कहीं अधिक है। इस वजह से एक बड़ा तबका कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है।

हरियाणा की स्कूल टीचर स्नेहा (बदला हुआ नाम) ने इस बारे में अपना अनुभव साझा किया, “मुझे हिंदी भाषा में ही पढ़ना, लिखना, बोलना सहज लगता है। लेकिन जबसे मुझे अपने ओरिएंटेशन के बारे में पता चला तब से मैंने इस बारे में इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे हिंदी में कोई ढंग की जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अंग्रेज़ी के लिखे को अनुवाद करके पढ़ पाना और भी कठिन होता है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के क्वीयर कम्युनिटी ग्रुप्स में भी अंग्रेज़ी का ही बोलबाला है। इसके अलावा कम्युनिटी के जो भी लोग मिलते हैं ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलने वाले एलीट क्लास के लोग होते हैं। इन वजहों से मुझे अलग-थलग महसूस होता है।”
मुझे एलजीबीटीक्यू+ का मतलब नहीं पता था। घर वालों ने शादी करा दी और सबकी मर्ज़ी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। हालांकि हमेशा से ही शादी, बच्चे और यह ज़िंदगी रास नहीं आई, लेकिन क्या करें और कोई चारा भी तो नहीं है। समाज में रहना है तो शादी और बच्चे तो करने ही पड़ते हैं।
जाति, वर्ग और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव का असर
किसी भी तरह का आंदोलन हो, उसका सबसे ज़्यादा असर समाज में विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक होता है। किसी भी तरह की तकनीक, सुविधा या लाभ हो, समाज के संपन्न लोगों तक पहले पहुंचता है। एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। भारतीय समाज में हाशिए पर रहने वाले समुदाय जैसे दलित, आदिवासी और विकलांग, क्वीयर आंदोलनों में भी हाशिए पर ही रह जाते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से ट्रांसवुमन एक्टिविस्ट मुस्कान अंबेडकराइट सी विषय पर बताती हैं, “एलजीबीटीक्यू+ आंदोलनों में महानगरों और अंग्रेज़ी भाषा बोलने वालों का प्रभुत्व है। हमारी कम्युनिटी के अंदर भी जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, भाषा, सुंदरता के आधार पर कई वर्ग बन गए हैं। ज़माना तो हमें जज करता ही है लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी हमें जज किया जाता है। कम्युनिटी के कुछ लोग कम्युनिटी के हित से ज्यादा अपने निजी स्वार्थ को महत्त्व देते हैं, इससे भी आंदोलन कमज़ोर पड़ता है। हमें अपने आंदोलन को मजबूत करने और सफल बनाने के लिए आपस में एकजुट होना होगा तभी बदलाव मुमकिन होगा।”
एलजीबीटीक्यू+ आंदोलनों में महानगरों और अंग्रेज़ी भाषा बोलने वालों का प्रभुत्व है। हमारी कम्युनिटी के अंदर भी जाति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, शिक्षा, भाषा, सुंदरता के आधार पर कई वर्ग बन गए हैं। ज़माना तो हमें जज करता ही है लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी हमें जज किया जाता है।
कॉरपोरेट प्राइड और इंद्रधनुषी पूँजीवाद
आजकल हम देखते हैं कि प्राइड मंथ और प्राइड परेड के समय बड़े-बड़े कॉरपोरेट घराने अपने सर्विसेज और प्रॉडक्ट की ब्रांडिंग में एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन का प्रतीक इंद्रधनुषी रंग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। क्वीयर मुद्दों का बाज़ारीकरण समुदाय से जुड़े असल मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ देता है। आंदोलन का प्रतिनिधित्व जब समुदाय से जुड़े लोगों के बजाय बाहरी लोग करने लगते हैं तो कहीं न कहीं इसमें उनका अपना मकसद जुड़ा होता है। इस तरह से टोकनिज़्म और बाज़ारवाद के चलते क्वीयर आंदोलन में एलीटिज़्म और हावी हो जाता है।
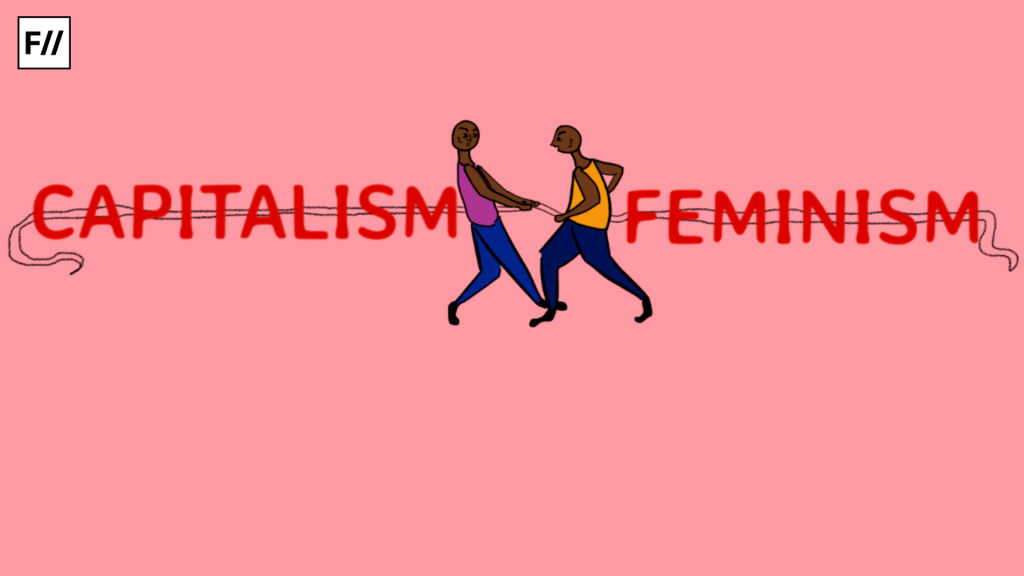
जयपुर राजस्थान के रहने वाले हिन्दी और ब्रजभाषा साहित्य आचार्य और साहित्यकार डॉ. शीताभ शर्मा ने इस बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा, “आज गांवों में इस तरह के आंदोलनों की ज़्यादा ज़रूरत है जबकि यह महानगरों में ज़्यादा दिखता है। हालांकि सोशल मीडिया के बढ़ते असर की वजह से गांव में क्वीयर समुदाय से जुड़े युवा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है। फिर भी परिवार और समाज को इसकी ख़ास जानकारी नहीं है, साथ ही जानकारी होने के बाद भी वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जेंडर बाइनरी के खांचे में बंटा समाज एलजीबीटीक्यू+ को अप्राकृतिक और विदेशी कल्चर मानता है, ऐसी ग़लत धारणाएं ख़त्म करने के लिए ऐसे आंदोलनों की पहुंच हर जगह होना चाहिए।”
भारत में एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन को समावेशी और सफल बनाने के लिए सभी तबकों की भागीदारी ज़रूरी है। क़ानूनी सुधारों के साथ हाशिए के समुदायों को जोड़ना होगा। आंदोलन को अंग्रेज़ी तक सीमित रखने के बजाय हिंदी के साथ-साथ अन्य स्थानीय भाषाओं में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसे महानगरों से आगे बढ़ाकर गांवों और कस्बों तक पहुंचाना ज़रूरी है। हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को शामिल करने से समावेशिता बढ़ेगी। स्कूलों में जेंडर और यौनिकता पर पाठ्यक्रम जोड़ना एक अहम कदम होगा। समाज को संवेदनशील बनाना क्वीयर समुदाय के अधिकारों के लिए बेहद ज़रूरी है।