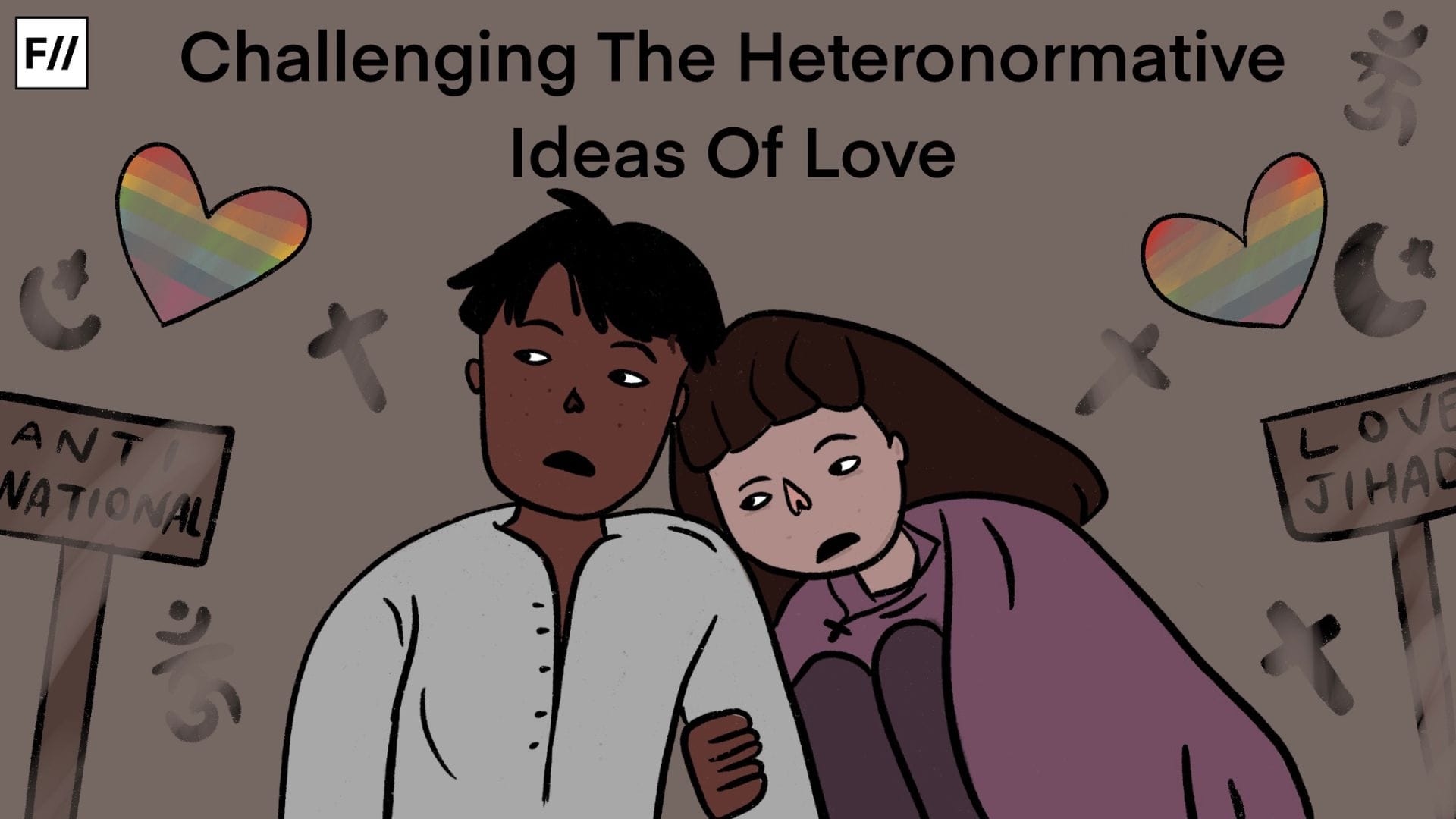भारत में कचरा बीनने वाली महिलाएं शहरी स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह वर्ग मुख्य रूप से समाज के हाशिए पर रह रहे समुदायों, विशेष रूप से दलित और आदिवासी वर्ग से आता है। हालांकि ये महिलाएं अपने काम के माध्यम से कचरे के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लेकिन उन्हें उचित पारिश्रमिक, सुरक्षा और समाज में उचित सम्मान और अधिकार नहीं मिलते। भारत में रैग पिकर्स की संख्या 1.5 से 4 मिलियन के बीच है। अहमदाबाद में लगभग 50,000 स्वरोजगार वाले कचरा बीनने वाले हैं, जिनमें से अधिकांश दलित महिलाएं हैं जो मुख्य रूप से दैनिक जीविका कमाने वाली हैं। इनका काम समय सुबह 4 बजे से 8 बजे और शाम 5 बजे से 10 बजे तक रहता है। गौर करें तो इस काम में लगभग 7-8 साल के बच्चे से लेकर 70-75 साल की बुजुर्ग महिलाएं और विकलांग व्यक्ति भी शामिल होते हैं। औसतन, ये महिलाएं 50 रुपए से 300 रुपए तक की दैनिक आय करती हैं, जो उनकी मेहनत और एकत्रित सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये महिलाएं शहरी कचरे का लगभग 20–30 फीसद पुनर्चक्रण करती हैं, जिससे कुछ हद तक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।
जातिगत और लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम और कचरा प्रबंधन
जातिगत और लैंगिक भेदभाव इन महिलाओं के काम को और कठिन बना देता है। साइंस डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार, कचरा बीनने वाली महिलाओं में 94 फीसद अनुसूचित जाति (एससी), 5 फीसद अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), और 1 फीसद अन्य वर्गों से आती हैं। दलित समुदाय से होने के कारण, ये महिलाएं अस्पृश्यता और ‘गंदे काम’ से जुड़े कलंक का सामना करती हैं। इसके अलावा, इन्हें हिंसा, यौन उत्पीड़न और असुरक्षित परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है।
भारत में बाल श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा कचरा बीनने के काम में लगा हुआ है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण छोटे बच्चे इस पेशे में प्रवेश कर जाते हैं और यह समस्या उनके परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। साल 2024 में शुरू हुई ‘राष्ट्रीय यांत्रिक सफाई पारिस्थितिकी तंत्र (NAMASTE)’ योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को सुरक्षित और स्थायी आजीविका प्रदान करना था। लेकिन जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव सीमित रहे। कचरा बीनने वाली महिलाएं सफाई के लिए दिन-रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनका संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी भी है।
गांव में खेती का काम करती थी, लेकिन शहर में कचरा बीनना बहुत मुश्किल था। हर दिन दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता है, गंदगी में बैठकर कचरा छांटना पड़ता है और फिर उसे बेचने जाना पड़ता है। अगर 200 रुपये कमाती हूं, तो उसमें से 50 रुपये तो ऑटो वाले को देने पड़ते हैं। मेरे पति के पास कोई स्थिर काम नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन यह काम करना पड़ा। मैं शादी के बाद से ही इस काम में लगी हूं और अब भी संघर्ष कर रही हूं।
ऐसे ही कचरा बीनने वाली कुछ महिलाओं से फेमिनिज़म इन इंडिया ने बात की। हमने उनसे जानने की कोशिश् की कि जमीनी चुनौतियां क्या है। कचरा प्रबंधन में लगी एक महिला बताती हैं, “हमें यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। पढ़ी-लिखी नहीं होने के कारण हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए हमें यही करना पड़ता है।” वहीं पिंकी बेन, जो इस काम में लगभग 20 साल से लगी हुई हैं, बताती हैं, “जब मैं लगभग 7-8 साल की उम्र की थी, तब मैं अपनी माँ के साथ कचरा बीनने जाती थी। तब से यही काम कर रही हूं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी यह काम करें। इसलिए मैं उन्हें पढ़ा रही हूं। मेरा बेटा अभी 10वीं कक्षा में और बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले।”
कामकाजी जगह और घरों में सुरक्षा की कमी
पिंकी बेन आगे बताती हैं कि कचरा बीनने के बाद, उसे छांटने के लिए इन महिलाओं के पास कोई उचित स्थान नहीं होता। इसलिए, वे सड़क के किनारे बैठकर कचरा छांटने का काम करती हैं। अक्सर अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के अधिकारी उन्हें वहां से हटने के लिए कहते हैं। पिंकी और उनकी जैसी अन्य महिलाएं चाहती हैं कि सरकार उनके लिए कोई उचित स्थान उपलब्ध कराए, जहां वे बिना किसी बाधा के सुरक्षित रूप से कचरा छांट सकें। इन महिलाओं के जीवन की एक और बड़ी कठिनाई उनके घर की परिस्थितियां हैं। अधिकांश महिलाओं के पति बेरोजगार हैं, और कई मामलों में वे शराब के आदी होते हैं। पिंकी बेन बताती हैं, “मेरे पति न केवल बेरोजगार हैं, बल्कि वे शराब पीकर शारीरिक हिंसा करते हैं और पैसे भी मांगते हैं। कचरा बीनने वाले लोग अत्यधिक गरीबी में जीते हैं, और उनका जीवन बेहद कठिन होता है।”
हमें यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। पढ़ी-लिखी नहीं होने के कारण हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। घर चलाने के लिए हमें यही करना पड़ता है।
वह आगे बताती हैं, “बारिश के मौसम में कचरा गीला हो जाता है, जिससे उसे सही कीमत नहीं मिलती और कई दिनों तक काम भी बंद रहता है। गीला कचरा होने के कारण हमें कम दाम मिलता है, जिससे हमारी आमदनी और घट जाती है।” इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद, ये महिलाएं हर दिन 10-12 घंटे तक कचरा बीनने और उसे अलग करने का काम करती हैं। इसके बदले वे मुश्किल से 200-300 रुपये कमा पाती हैं, और कभी-कभी तो केवल 100-150 रुपये ही मिलते हैं। आमदनी कम होने की वजह से उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है, और इतनी कम आमदनी में घर चलाना और बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता है।”
गरीबी और भेदभाव में जीने पर हैं मजबूर
कचरा बीनने के काम में लगी 65 वर्षीय विधवा लक्ष्मी बताती हैं, “मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए झुग्गी में रहती हूं। मैं मुंह के कैंसर से पीड़ित हूं। लेकिन दवाइयों और खाने का खर्च निकालने के लिए अब भी कचरा बीनने जाती हूं। शादी के बाद जब मैं अहमदाबाद आई, तो मेरी सास कचरा बीनती थीं। मैं भी उनके साथ जाने लगी। गांव में खेती का काम करती थी, लेकिन शहर में कचरा बीनना बहुत मुश्किल था। हर दिन दूर-दूर तक पैदल जाना पड़ता है, गंदगी में बैठकर कचरा छांटना पड़ता है और फिर उसे बेचने जाना पड़ता है। अगर 200 रुपये कमाती हूं, तो उसमें से 50 रुपये तो ऑटो वाले को देने पड़ते हैं। मेरे पति के पास कोई स्थिर काम नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरन यह काम करना पड़ा। मैं शादी के बाद से ही इस काम में लगी हूं और अब भी संघर्ष कर रही हूं।”
मेरे पति न केवल बेरोजगार हैं, बल्कि वे शराब पीकर शारीरिक हिंसा करते हैं और पैसे भी मांगते हैं। कचरा बीनने वाले लोग अत्यधिक गरीबी में जीते हैं, और उनका जीवन बेहद कठिन होता है।
गुजरात में कचरा बीनने वालों में बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित-बहुजन और नाडिया समुदाय के लोग शामिल हैं। इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं, जो सार्वजनिक स्थानों पर काम करने के कारण अक्सर यौन हिंसा और उत्पीड़न का सामना करती हैं। कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थिति उन्हें शारीरिक हिंसा और मानसिक तनाव की ओर धकेलती है। अधिकांश कचरा बीनने वाली महिलाओं के पास पहचान पत्र नहीं होते, जिससे वे सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहती हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ कचरा बीनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें घर और परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। उनके पास अपने जीवन के फैसले लेने की स्वतंत्रता नहीं होती और पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के अवसर भी नहीं मिलते।
क्या हो सकता है समाधान
महिलाओं को कचरा छांटने के लिए सुरक्षित और निश्चित स्थान दिया जाए, ताकि वे बिना किसी भय के काम कर सकें। उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच, मुफ्त इलाज और सुरक्षा उपकरण (दस्ताने, मास्क, जूते) दिए जाएं ताकि वे बीमारियों से बच सकें। उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं ताकि वे इस पेशे में जाने के लिए मजबूर न हों। कचरा बीनने वाले समुदायों को उचित आवास, पानी, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलें। पहचान पत्र, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज मुहैया कराया जाए, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। कचरा बीनने वाली महिलाएं खतरनाक और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करती हैं। वे शीशे के टुकड़े, नुकीली वस्तुओं और गंदे कचरे के संपर्क में आती हैं, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जहरीले कचरे से त्वचा रोग, श्वसन समस्याएं और अन्य गंभीर स्वास्थ्य विकार होने की आशंका रहती है। सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि इन महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन मिले।