कैमरे के पीछे की दुनिया वह जगह है जहां रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का एक अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। यह मंच कला, तकनीक, और अलग-अलग दृष्टिकोणों से बनता है। लेकिन इस चमचमाते और संभावनाओं से भरे उद्योग के पर्दे के पीछे लैंगिक असमानता की गंभीर समस्या छिपी हुई है। यह असमानता महिलाओं, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों के लिए न केवल एक बाधा बनती है, बल्कि उनकी भागीदारी को सीमित करके समाज की विविधता और समावेशिता को भी प्रभावित करती है। हर जगह चाहे वह फिल्म निर्देशन हो, सिनेमैटोग्राफी, या पोस्ट-प्रोडक्शन, इन सभी क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व स्पष्ट रूप से दिखता है। फिल्म, फोटोग्राफी और मीडिया जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में यह असमानता केवल अवसरों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन कहानियों और दृष्टिकोणों को भी रोक देती है, जो इन समुदायों से हो सकती है। यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विविधता और समावेशिता से ही किसी भी रचनात्मक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
विश्व का सबसे ज्यादा फिल्म निर्माण करने वाले हमारे देश में फिल्में और वेबसीरीज़ लैंगिक समानता के मानदंडों पर खरी नहीं उतरती हैं। यूएन वुमन की रिपोर्ट अनुसार 11 देशों में लोकप्रिय फिल्मों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी बोलने वाले पात्रों में से 31 प्रतिशत महिलाएं थीं और केवल 23 प्रतिशत में महिला मुख्य पात्र थीं। यह संख्या महिला फिल्म निर्माताओं के मामले में लगभग 21 प्रतिशत के करीब थी। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट अनुसार अमेज़न प्राइम वीडियो की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की शीर्ष 25 मीडिया एवं मनोरंजन फर्मों में अध्ययन किए गए 135 निदेशक/सीएक्सओ पदों में से केवल 13 फीसद पद महिलाओं के पास थे। रिपोर्ट ने भारतीय मनोरंजन उद्योग की कठोर सच्चाई को उजागर किया है। यह उद्योग, जो कहानियों को आकार देता है और सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करता है, फिर भी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने में पीछे है।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट अनुसार अमेज़न प्राइम वीडियो की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की शीर्ष 25 मीडिया एवं मनोरंजन फर्मों में अध्ययन किए गए 135 निदेशक/सीएक्सओ पदों में से केवल 13 फीसद पद महिलाओं के पास थे।
मनोरंजन की दुनिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी
यह मुद्दा सिर्फ स्क्रीन और बोर्डरूम तक नहीं है, यह ये तय करता है कि कहानियों को कैसे पेश किया जाएगा, किसकी आवाज़ों को सुना जाएगा, और लोग लैंगिक भूमिकाओं को कैसे समझेंगे। इन असमानताओं को खत्म करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा समावेशी उद्योग बनाने में भूमिका निभाएगा जो अपने दर्शकों की विविधता को सही ढंग से दिखाता हो। द क्विन्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ओ वुमनिया! टूलकिट देखती है कि कहानियों में महिलाओं को महज पुरुषों की मदद करने वाले पात्रों के रूप में दिखाने के बजाय, उन्हें सक्रिय रूप में प्रस्तुत किया गया है या नहीं।

इस साल, सिर्फ 31 फीसद शीर्षक इस टूलकिट के मानकों पर खरे उतरे। खासकर स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में, जहां 45 फीसद सीरीज़ और 31 फीसद फ़िल्में सफल रही, वहीं सिनेमा हॉल में प्रदर्शित फ़िल्मों का आंकड़ा केवल 18 फीसद है। दिलचस्प बात ये है कि 48 फीसद उन शीर्षकों में, जो टूलकिट पर पास हुए, महिला कमीशनिंग अधिकारियों की मेहनत थी। यह टूलकिट फिल्म निर्माताओं को पारंपरिक मानकों को चुनौती देने और विविधतापूर्ण सामग्री बनाने में मदद करती है।
इस साल, सिर्फ 31 फीसद शीर्षक इस टूलकिट के मानकों पर खरे उतरे। खासकर स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स में, जहां 45 फीसद सीरीज़ और 31 फीसद फ़िल्में सफल रही, वहीं सिनेमा हॉल में प्रदर्शित फ़िल्मों का आंकड़ा केवल 18 फीसद है। दिलचस्प बात ये है कि 48 फीसद उन शीर्षकों में, जो टूलकिट पर पास हुए, महिला कमीशनिंग अधिकारियों की मेहनत थी।
यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय मनोरंजन में महिलाओं का रचनात्मक नेतृत्व काफी कम है। अगर हम निर्देशन, लेखन, सिनेमैटोग्राफी, एडिटिंग, और प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करें, तो महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15 फीसद है। सिनेमा प्रोजेक्ट्स में ये आंकड़े केवल 6 फीसद जबकि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर यह थोड़ा बढ़कर 20 फीसद तक पहुंच जाती है। हालांकि मार्केटिंग के क्षेत्र में कुछ सुधार नजर आता है। यहां ट्रेलर में महिलाओं को 29 फीसद तक बात करने का मौका मिलता है। स्ट्रीमिंग कंटेंट में भी स्थिति बेहतर है। जैसे, ‘मेड इन हेवन सीजन-2,’ ‘बू’, ‘रेनबो रिश्ता’, ‘आर्या सीजन-3’, और ‘स्वीट कारम कॉफी’ जैसे शो में ट्रेलर में महिलाओं का समय 55 फीसद से ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि मनोरंजन में समानता पाने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना होगा। रचनात्मक और व्यवसायिक दोनों जगह अब भी पुरुषों का दबदबा है। इसके लिए बड़े बदलावों की जरूरत है।
असमानता के प्रमुख कारण
मीडिया और फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न भी एक गंभीर समस्या है। कार्यस्थलों पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित माहौल न मिलने के कारण वे अपने करियर के विकल्प बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। #MeToo आंदोलन ने इस समस्या को उजागर किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों और करियर के बीच चुनाव करने पर मजबूर किया जाता है। विशेष रूप से भारतीय समाज में, महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे परिवार की देखभाल को प्राथमिकता दें। इससे वे अपने पेशेवर जीवन में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पातीं। यह मुद्दा पुरुषों पर लागू उस तरह कभी भी नहीं होता, जिससे असमानता और बढ़ जाती है।

महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर तकनीकी रूप से कमतर आँका जाता है। यह सोच समाज में बहुत गहराई से फैली हुई है और यह उन्हें तकनीकी क्षेत्र से दूर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। जब महिलाओं या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सिनेमैटोग्राफी या निर्देशन जैसे क्षेत्रों में आने का मौका मिलता है, तो उन्हें बार-बार अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए कहा जाता है। यह पूर्वाग्रह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है, बल्कि यह संस्थागत ढांचे में भी दिखाई देता है। पुरुषों के चलाए जाने वाले उद्योगों में अच्छे नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है। हालांकि, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को वो मौके नहीं मिलते जो उन्हें चाहिए, जिससे उनके लिए इस क्षेत्र में बने रहना कठिन हो जाता है। पुरुष सहकर्मी अक्सर मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, लेकिन महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर इस नेटवर्क से अलग- थलग कर दिया जाता है।
यूएन वुमन की रिपोर्ट अनुसार 11 देशों में लोकप्रिय फिल्मों के विश्लेषण से पता चलता है कि सभी बोलने वाले पात्रों में से 31 प्रतिशत महिलाएं थीं और केवल 23 प्रतिशत में महिला मुख्य पात्र थीं। यह संख्या महिला फिल्म निर्माताओं के मामले में लगभग 21 प्रतिशत के करीब थी।
जेंडर असमानता का प्रभाव
जब उद्योग में जेंडर असमानता बनी रहती है, तो यह विभिन्न दृष्टिकोणों और कहानियों के सामने आने में बाधा बनती है। फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में विविधता का अभाव समाज को उन कहानियों से वंचित करता है जो इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनुभवों को दर्ज करती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समान काम के लिए भी कम वेतन दिया जाता है। यह आर्थिक असमानता न केवल उनके जीवन स्तर को प्रभावित करती है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और करियर की संभावनाओं को भी कमजोर करती है। कैमरे के पीछे की असमानता का असर भी समाज पर पड़ता है। मीडिया और फिल्म उद्योग समाज को प्रतिबिंबित करने के साथ-साथ उसे आकार भी देता है। जब विविध जेंडर्स को प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो समाज में उनकी भागीदारी को नजरअंदाज किया जाता है।
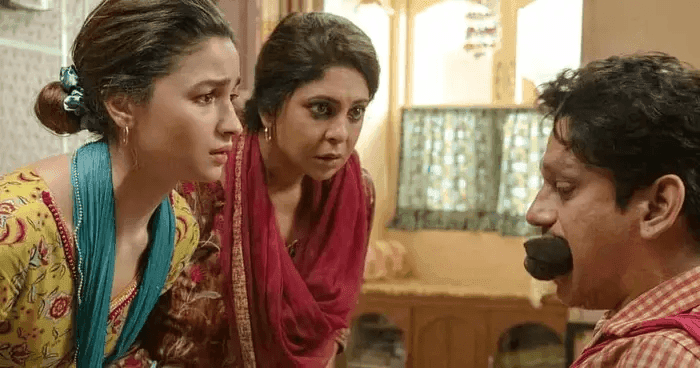
यह न केवल उनके लिए पहचान की कमी पैदा करता है, बल्कि समाज में समावेशिता की भावना को भी कमजोर करता है। जेंडर असमानता से जुड़े भेदभाव, पूर्वाग्रह और कार्यस्थल की असुरक्षा से महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में मानसिक तनाव और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। यह उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। इन प्रभावों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कैमरे के पीछे जेंडर असमानता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे उद्योग और समाज पर प्रभाव डालती है। इसे दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास और नीतिगत बदलाव जरूरी हैं।
जब उद्योग में जेंडर असमानता बनी रहती है, तो यह विभिन्न दृष्टिकोणों और कहानियों के सामने आने में बाधा बनती है। फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में विविधता का अभाव समाज को उन कहानियों से वंचित करता है जो इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अनुभवों को दर्ज करती है।
समाधान और भविष्य की राह

कैमरे के पीछे की जेंडर असमानता एक जटिल समस्या है, लेकिन इसे दूर करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। इन प्रयासों से न केवल मनोरंजन उद्योग में समानता आएगा बल्कि यह समाज में समावेशिता और विविधता को भी बढ़ावा देगा। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों के लिए सक्रिय समितियां होनी चाहिए। सख्त यौन उत्पीड़न विरोधी नीतियां लागू करके सभी कार्यस्थलों पर पॉश नीतियों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। लोगों में जागरूकता की जरूरत है ताकि ये धारणा बदले कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर तकनीकी या नेतृत्व भूमिकाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। वेतन और पदोन्नति की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता हो ताकि समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो सके। फिल्म और मीडिया में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आवाज़ को प्रमुखता दी जाए। एक समावेशी मनोरंजन उद्योग बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जब अलग-अलग जेंडर और समुदायों को कैमरे के पीछे और सामने भी समान अवसर मिलेंगे, तो यह न केवल कहानियों की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि समाज को भी नई दिशा देगा।
द क्विन्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ओ वुमनिया! टूलकिट देखती है कि कहानियों में महिलाओं को महज पुरुषों की मदद करने वाले पात्रों के रूप में दिखाने के बजाय, उन्हें सक्रिय रूप में प्रस्तुत किया गया है या नहीं। इस साल, सिर्फ 31 फीसद शीर्षक इस टूलकिट के मानकों पर खरे उतरे।
कैमरे के पीछे जेंडर असमानता सिर्फ एक व्यक्तिगत या संस्थागत समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज में गहराई तक जड़ जमाए भेदभाव और पूर्वाग्रह का प्रतीक है। महिलाओं, ट्रांसजेंडर और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों के लिए सीमित अवसर न केवल उनकी भागीदारी को बाधित करते हैं, बल्कि रचनात्मकता, विविधता और समावेशिता को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह आवश्यक है कि हम इस असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएं। शिक्षा, प्रशिक्षण, नीतिगत बदलाव, और सुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। साथ ही, समाज की सोच में बदलाव और उन आवाज़ों को मंच देना भी ज़रूरी है जो लंबे समय से अनसुनी रही हैं। जब कैमरे के पीछे हर जेंडर के लोग समानता और सम्मान के साथ काम करेंगे, तभी कला, तकनीक, और मनोरंजन का यह क्षेत्र अपनी पूरी तरह से विकसित हो सकेगा।




