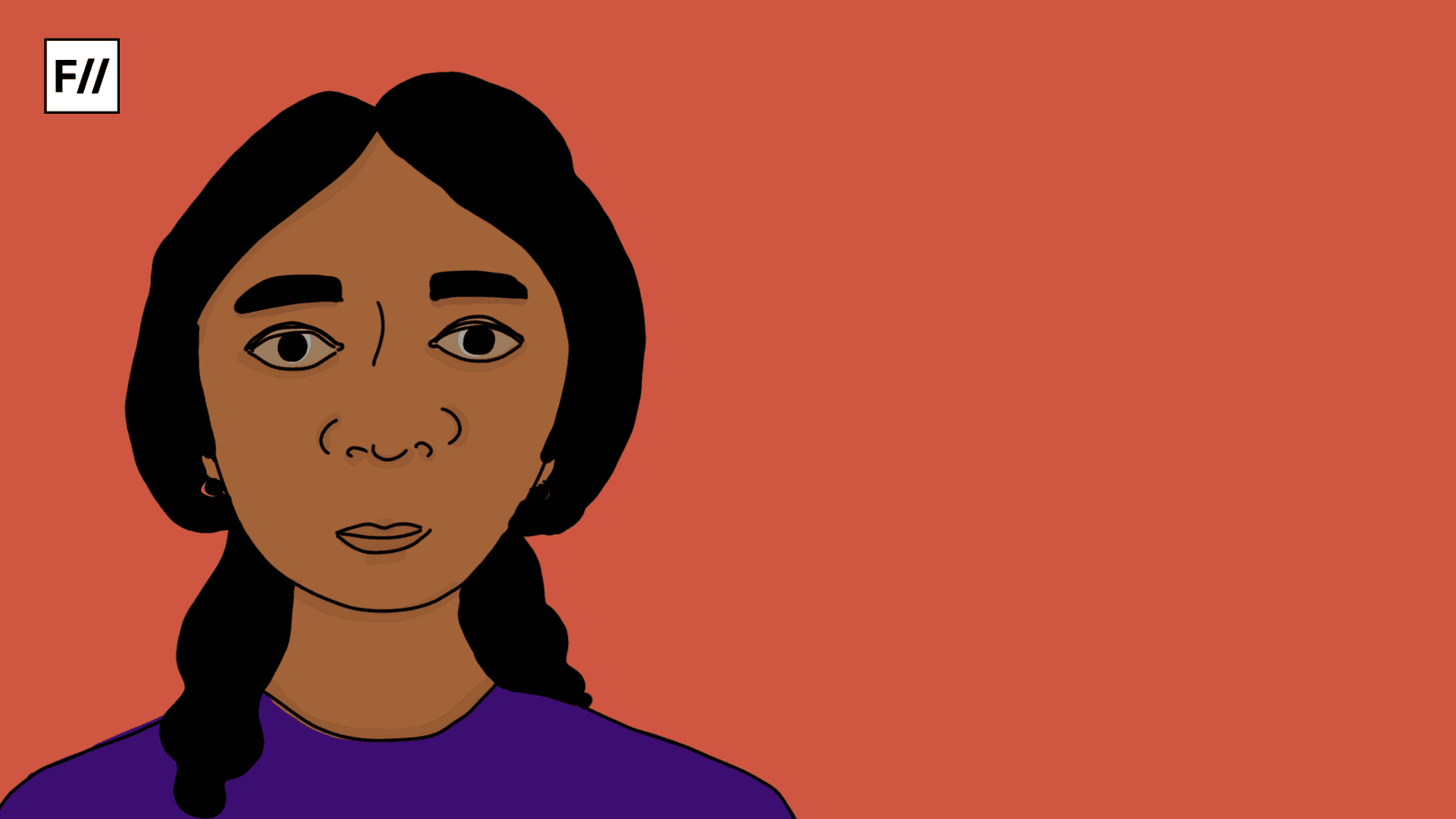भारत में तलाक की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में अक्सर कई साल लग जाते हैं। इस लंबे समय के दौरान पति और पत्नी दोनों कानूनी रूप से ऐसे रिश्ते में बंधे रहते हैं जो पहले ही टूट चुका होता है। कई बार यह रिश्ता शत्रुतापूर्ण, भावनात्मक रूप से खाली या मानसिक रूप से असहनीय हो जाता है। आर्थिक अस्थिरता, समाज का दबाव और लंबी अदालत की कार्यवाही मिलकर व्यक्ति के जीवन को एक तरह से अधर में लटका देती है। ऐसे हालात में क्रूरता हमेशा मारपीट या खुले दुर्व्यवहार के रूप में नहीं होती, बल्कि कभी-कभी कानून द्वारा उस रिश्ते को जबरन जारी रखने से भी पैदा होती है, जो वास्तविक रूप से समाप्त हो चुका होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह स्वीकार किया है कि मानसिक क्रूरता केवल शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं होती।
समर घोष बनाम जया घोष के मामले में न्यायालय ने कहा कि मानसिक क्रूरता में ऐसा व्यवहार भी शामिल हो सकता है जो पति-पत्नी के लिए साथ रहना असंभव बना दे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रूरता का मूल्यांकन पक्षकारों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी सैद्धांतिक या नैतिक आदर्श के आधार पर। इसके बावजूद, जब अदालतें ऐसे दंपतियों को वर्षों तक कानूनी रूप से विवाहित बने रहने के लिए मजबूर करती हैं, तो यह देरी स्वयं क्रूरता का कारण बन जाती है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, मानसिक क्रूरता ऐसा आचरण है जो पीड़ा पहुंचाता है और जीवनसाथी के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। हालांकि, मानसिक क्रूरता को किसी एक सख्त परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि समाज और उसके मूल्य समय के साथ बदलते रहते हैं।
समर घोष बनाम जया घोष के मामले में न्यायालय ने कहा कि मानसिक क्रूरता में ऐसा व्यवहार भी शामिल हो सकता है जो पति-पत्नी के लिए साथ रहना असंभव बना दे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि क्रूरता का मूल्यांकन पक्षकारों की वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी सैद्धांतिक या नैतिक आदर्श के आधार पर।
अनुच्छेद 21 और गरिमापूर्ण अलगाव का अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में इस अधिकार की व्याख्या करते हुए इसमें गरिमा, आत्मनिर्णय (स्वायत्तता) और मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने निजी और अंतरंग मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवाह एक निजी और अंतरंग संबंध है, इसलिए यह इन संवैधानिक मूल्यों से अलग नहीं हो सकता। इसी कारण, पति या पत्नी को ऐसे विवाह से बाहर निकलने का पूरा अधिकार होना चाहिए जिसमें अब कोई भावनात्मक जुड़ाव न बचा हो या जहां व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच रही हो।
किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से टूट चुके विवाह में जबरन बांधे रखना उसकी स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन है। जीवन का अधिकार केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऐसा जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है जो मानसिक पीड़ा से मुक्त हो। जब राज्य या कानून की कठोर प्रक्रिया के कारण किसी व्यक्ति को लंबे समय तक मानसिक तनाव सहना पड़ता है, तो यह भी जीवन के अधिकार का हनन है। भारतीय न्यायालय अक्सर टूटे हुए रिश्तों को बचाने के लिए बहुत अधिक समय लेते हैं। जब तलाक कानून विवाह को समाप्त करने के बजाय केवल सहन करने पर जोर देता है, तो वह वैवाहिक स्थायित्व के आदर्श को व्यक्ति की गरिमा से ऊपर रख देता है। ऐसी स्थिति में यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बन जाता है।
विवाह एक निजी और अंतरंग संबंध है, इसलिए यह इन संवैधानिक मूल्यों से अलग नहीं हो सकता। इसी कारण, पति या पत्नी को ऐसे विवाह से बाहर निकलने का पूरा अधिकार होना चाहिए जिसमें अब कोई भावनात्मक जुड़ाव न बचा हो या जहाँ व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंच रही हो।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं को होने वाला नुकसान
यह सही है कि तलाक के मामलों में होने वाली देरी सभी पक्षकारों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके प्रभाव पुरुषों और महिलाओं पर एक समान नहीं होते। लंबे समय तक चलने वाली तलाक की कार्यवाही के दौरान महिलाओं को अक्सर आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बदनामी और बच्चों या परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी का अधिक बोझ उठाना पड़ता है। कई बार अंतहीन मुकदमेबाजी एक दबाव बनाने का तरीका बन जाती है, जिसका इस्तेमाल एक पक्ष दूसरे पक्ष को मानसिक और आर्थिक रूप से थकाने के लिए करता है। ऐसे मामलों में कानूनी देरी तटस्थ नहीं रहती, बल्कि उत्पीड़न का साधन बन जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार चेतावनी दी है कि वैवाहिक मुकदमेबाजी को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
साल 2013 में के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि लंबी और कष्टदायक मुकदमेबाजी अपनेआप में मानसिक क्रूरता हो सकती है। यही तर्क उन व्यवस्थागत देरी पर भी लागू होना चाहिए, जिन्हें कभी-कभी न्यायिक प्रक्रिया स्वयं बढ़ावा देती है। हालांकि भारत की कानूनी व्यवस्था महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन मामलों की अत्यधिक लंबी अवधि पत्नी के लिए गंभीर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक बोझ बन जाती है। कई परिस्थितियों में यह बोझ पति से भी अधिक हो सकता है।
साल 2013 में के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि लंबी और कष्टदायक मुकदमेबाजी अपनेआप में मानसिक क्रूरता हो सकती है। यही तर्क उन व्यवस्थागत देरी पर भी लागू होना चाहिए, जिन्हें कभी-कभी न्यायिक प्रक्रिया स्वयं बढ़ावा देती है।
यह समस्या केवल हिंदू विवाह अधिनियम के मामलों तक सीमित नहीं है। अन्य धर्मों की महिलाएं भी इससे प्रभावित होती हैं।
जैसे, निशा (नाम बदला हुआ) को उसके पति ने दस साल पहले तलाक दे दिया था। एक रात उसने निशा को उसके दो बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। निशा के पिता ने बेटी और बच्चों के भरण-पोषण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। लेकिन आज दस साल बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली है। मामला अब तक जिला अदालत में ही अटका हुआ है। इस लंबे संघर्ष ने निशा को अवसाद और चिंता का मरीज बना दिया है।
भारतीय न्यायालयों और यथार्थवादी दृष्टिकोण
लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवादों को लेकर न्यायपालिका की असहजता कोई नई बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में स्वीकार किया था कि जब भावनात्मक रूप से रिश्ता पूरी तरह टूट चुका हो, तब भी पति-पत्नी को जबरन विवाहित बनाए रखना किसी काम का नहीं है। जब कोई दंपत्ति साथ रहने में असमर्थ हो, लंबे समय से अलग रह रहा हो और सुलह के सभी प्रयास असफल हो चुके हों, तो विवाह व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसे ‘भावनात्मक रूप से मृत’ विवाह को जारी रखना केवल कड़वाहट और पीड़ा को बढ़ाता है। साल 2023 संविधान पीठ ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में इस सोच को और आगे बढ़ाया।
न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत वह सीधे विवाह को समाप्त कर सकता है, यदि उसे लगे कि रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और उसे जारी रखना अन्याय होगा। पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय कानूनी औपचारिकताओं में फंसे मृत विवाहों से होने वाली लंबी मानवीय पीड़ा का ‘मूक दर्शक’ नहीं बन सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के एक अन्य फैसले में यह भी कहा कि विवाह संस्था गरिमा, आपसी सम्मान और साथ निभाने पर आधारित होती है। जब ये मूल बातें पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, तो किसी दंपत्ति को कानूनी रूप से बंधे रहने के लिए मजबूर करना किसी के हित में नहीं होता। किसी व्यक्ति को असफल और टूटे हुए विवाह में बनाए रखना उसके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।
जब कोई दंपत्ति साथ रहने में असमर्थ हो, लंबे समय से अलग रह रहा हो और सुलह के सभी प्रयास असफल हो चुके हों, तो विवाह व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से समाप्त हो जाता है। ऐसे “भावनात्मक रूप से मृत” विवाह को जारी रखना केवल कड़वाहट और पीड़ा को बढ़ाता है।
विधायी निष्क्रियता की कीमत
साल 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश की थी कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने को तलाक का एक कानूनी आधार बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया। कानून में इस सुधार के अभाव में, तलाक के मामलों में देरी से होने वाले अन्याय को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अपरिवर्तनीय टूटन को वैधानिक आधार के रूप में शामिल न करने से एक गंभीर असमानता पैदा हो गई है। राहत अक्सर केवल उन्हीं लोगों को मिल पाती है जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने में सक्षम हैं, जबकि समान परिस्थितियों में फंसे अन्य लोग वर्षों तक निचली अदालतों में भटकते रहते हैं।
इससे न केवल सर्वोच्च न्यायालय पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है, बल्कि कानून के सामने समानता का सिद्धांत भी कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में तलाक का परिणाम मामले की वास्तविक परिस्थितियों पर कम और इस बात पर अधिक निर्भर करने लगता है कि कोई पक्ष कितनी देर तक मुकदमेबाजी सह सकता है। कई बार वकील भी मामलों को जानबूझकर लंबा खींच देते हैं। इसके अलावा, जब पक्षकारों को तलाक के लिए दोष-आधारित आधारों का सहारा लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इससे बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाने और झूठे दावों की संभावना बढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया और अधिक खराब हो जाती है।
साल 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिफारिश की थी कि विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने को तलाक का एक कानूनी आधार बनाया जाना चाहिए। इसके बावजूद संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया।
भारत में तलाक की कानूनी प्रक्रिया केवल एक न्यायिक सवाल नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य और स्वतंत्रता से जुड़ा गहरा मानवीय मुद्दा है। जब कोई विवाह भावनात्मक, सामाजिक और व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुका हो, तब उसे केवल कानूनी औपचारिकताओं के नाम पर वर्षों तक जीवित रखना स्वयं एक तरह की क्रूरता बन जाता है। ऐसी देरी विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक नुकसानदेह होती है, क्योंकि सामाजिक संरचना, आर्थिक निर्भरता और देखभाल की जिम्मेदारियाँ उन्हें पहले से ही असमान स्थिति में खड़ा करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों के ज़रिए यह स्पष्ट किया है कि विवाह का उद्देश्य केवल कानूनी बंधन नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, साथ और गरिमा है।
जब ये तत्व पूरी तरह खत्म हो जाएं, तो कानून का दायित्व रिश्ते को जबरन बचाने का नहीं, बल्कि व्यक्ति को पीड़ा से मुक्त करने का होना चाहिए। लेकिन विधायी स्तर पर सुधार के अभाव में यह राहत अभी भी सीमित लोगों तक ही पहुंच पा रही है। अब ज़रूरत है कि संसद विवाह के अपरिवर्तनीय टूटन को तलाक का एक स्पष्ट और वैधानिक आधार बनाए, ताकि लोगों को वर्षों तक मुकदमेबाजी में फंसे रहने से बचाया जा सके। न्याय का अर्थ केवल प्रक्रिया का पालन नहीं, बल्कि समय पर और मानवीय समाधान भी है। गरिमापूर्ण अलगाव का अधिकार जीवन के अधिकार का ही विस्तार है। जब तक कानून इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक टूटे हुए विवाहों में फंसे लोगों की पीड़ा बनी रहेगी।