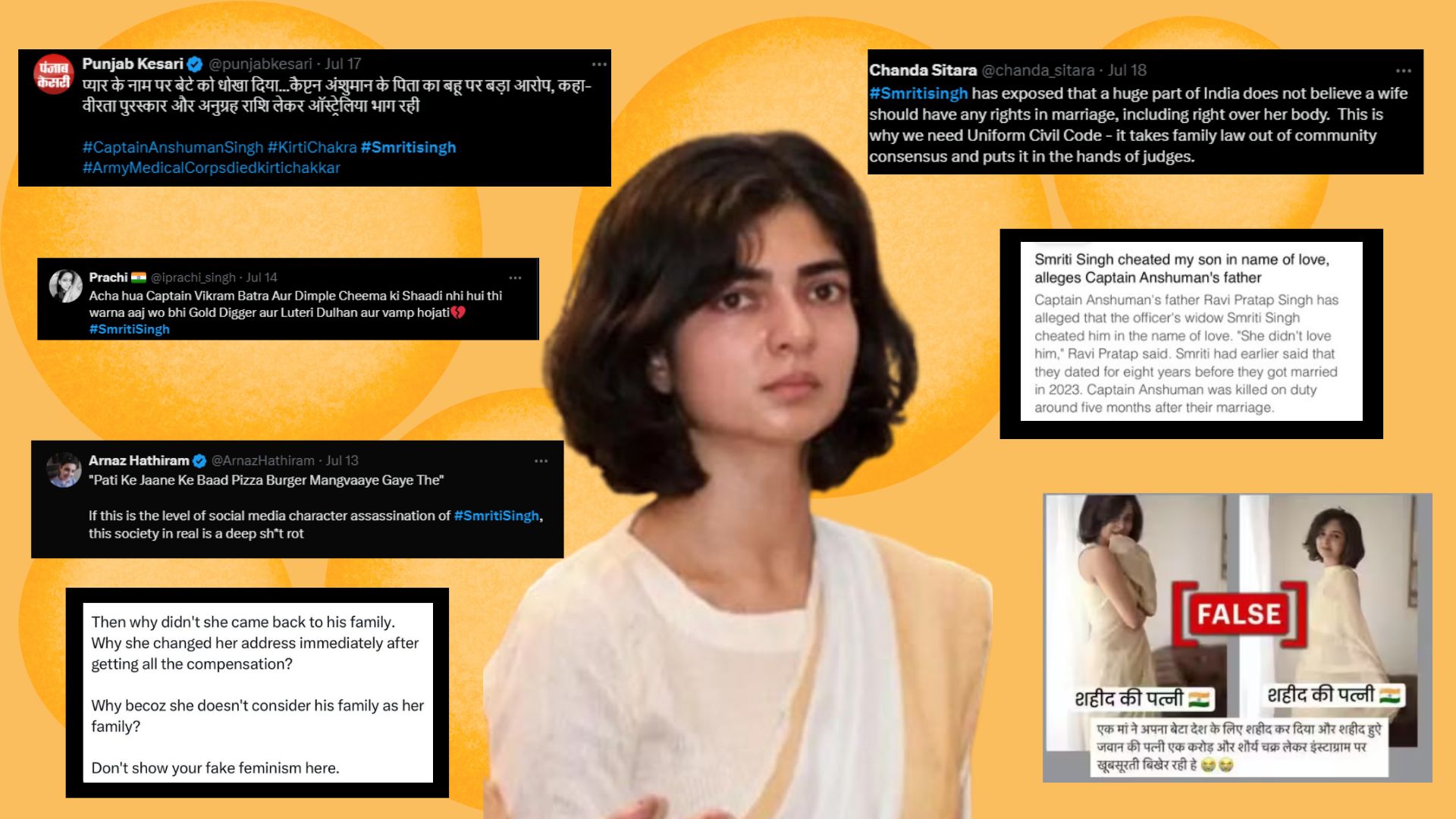भारत में पुरुष की परवरिश एक पितृसत्तात्मक समाज में होती हैं और महिलाओं के साथ उनका संपर्क बहुत कम होता है| इतना ही नहीं, उन्हें सेक्स के बारे में न के बराबर शिक्षा व जानकारी दी जाती है| संभव है कि ऊपरी सामाजिक-आर्थिक वर्ग के युवकों की इस स्थिति में कुछ बदलाव हो रहा हो, लेकिन अधिकाँश युवकों के लिए यह स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है| अधिकाँश लड़के पुरुषत्व की भावना के बारे में ऐसे विचार रखते हैं, जिसके तहत यौन गतिविधियों और अन्य क्षेत्रों में पुरुष की प्रधानता दिखाई पड़ती है| ऐसा तर्क दिया जाता है कि यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और युवकों व महिलाओं, दोनों की ही संवेदनशीलता को कम करने के लिए पुरुषत्व (और नारीत्व) के बारे में मौजूदा विचारों को चुनौती देना ज़रूरी है|
पूरी दुनिया की तरह भारत में भी महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुष के स्वामित्व के सामने झुकें| इस तरह के विचारों से लड़कियों की ज़ल्दी शादी और उत्पीड़क यौन संबंधों को बढ़ावा मिलता है| वहीं पुरुष पितृसत्तामक सोच के तहत या फिर कई बार समाज के दबाव में यौन व्यवहारों में भी अपने वर्चस्व को क़ायम रखने के लिए अक्सर ऐसे व्यवहार अपनाता है, जो हिंसात्मक होते है| जैसे- ‘यौन व्यवहार को हमेशा अपने अधिकार के रूप में देखना, फिर इसमें उनके साथी की सहमति हो या न हो| या फिर तथाकथित पुरुषत्व के नाम पर कई साथियों के साथ यौन संबंध रखना और इसे अपने वर्चस्व की शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना | ठीक इसी तरह महिलाओं पर भी यौन व्यवहारों को लेकर समाज का दबाव रहता है लेकिन इसके बावजूद भारत में उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि आमतौर पर पुरुषों की तरह महिलाओं के एक से अधिक यौन साथी नहीं होते|
और पढ़ें : ‘युवा, सेक्स और संबंध’ से जुड़ी दूरियां जिन्हें पूरा करना बाकी है
ऐसा भी बताया जाता रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर आधारित भूमिकाओं में अंतर बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ लड़के पुरुषों के लिए आरक्षित स्वायत्ता, इधर-उधर जाने की स्वतन्त्रता और अधिक अवसरों जैसे विशेषाधिकारों का लाभ उठाते हैं, वहीं लड़कियों को अपने इधर-उधर जाने की स्वतन्त्रता और शिक्षा के अवसरों पर अंकुश का सामना करना पड़ता है| सामाजिक परिस्थितियों में अंतर से प्रजनन व्यवहार और आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है| जेंडर आधारित हिंसा, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और पौरुष दर्शाने के लिए समलैंगिकों के प्रति घृणा जैसे ऐसे ही कुछ नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं|
महिलाओं पर नियन्त्रण और अपनी ख़ास स्थिति को स्थापित करने के लिए यौन बल को सबसे ख़ास माना गया है|
अगर जेंडर मानकों की असमानता के बारे में जानकारी में वृद्धि हुई है, फिर भी इन मानकों को प्रभावित करने या इनके कारण आने वाले बदलावों को मापने के लिए बहुत कम अध्ययन किये गये हैं| पुरुषों को परिवार नियोजन के प्रयासों में भागीदारी बनाने के कार्यों से ऐसा लगता है कि सही फैसले लेने के लिए पुरुषों को भी और अधिक जानकारी की ज़रुरत होती है|
एक अध्ययन के तहत जब पुरुषत्व के बारे में पूछे जाने पर युवकों ने शारीरिक बल और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही असली मर्द की खासियत बताई गयी है| युवकों की तरफ से पुरुषत्व को समझे और व्यक्त किये जाने के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है| कुल मिलाकर, कोई इंसान वास्तव में पुरुष तभी होता है जब वह सुंदर, बलिष्ठ और पौरुष से पूर्ण हो| इन सभी ख़ासियतों को इसलिए ख़ास माना जाता है क्योंकि महिलाएं इनके प्रति आकर्षित होती हैं और इनसे पुरुष की यौन शक्तियां भी बढ़ती हैं, जिनसे वह स्त्रियों को यौन रूप से संतुष्ट कर सकता है| महिलाओं पर नियन्त्रण और अपनी ख़ास स्थिति को स्थापित करने के लिए यौन बल को सबसे ख़ास माना गया है| पुरुष में नारी सुलभ गुण नहीं होने चाहिए जो कि समलैंगिक पुरुषों का प्रतीक माना जाता है| समलैंगिक पुरुषों की व्याख्या करते हुए सूचना प्रदाताओं ने इन्हें नीचा दिखाने वाली परिभाषाओं का इस्तेमाल किया|
और पढ़ें : युवाओं के लिए युवाओं से उनकी अपनी बात
सामाजिक रूप से पुरुष वो है जो अपने बच्चों, पत्नी, माता-पिता और भाई-बहनों की देखभाल कर सकता हो| इसके साथ ही, दूसरों पर हावी हो पाने के गुण को भी असली मर्द की ख़ासियत के साथ जोड़कर देखा गया| दूसरे पुरुषों के विरोध में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शारीरिक या मौखिक आक्रमण किये जाने को भी प्राय: पुरुषत्व का गुण बताया गया है| जैसे – ‘पुरुष लड़ाई लड़ते हैं और जीतते हैं|’ पर इसके साथ-साथ अपने पुरुषत्व को सिद्ध करने के लिए इस आक्रमकता का इस्तेमाल महिलाओं – पत्नियों, प्रेमिकाओं या जान-पहचान की स्त्रियों – पर प्रभाव के लिए भी किया गया| उत्तरदाताओं ने अक्सर महिलाओं को एक वस्तु की संज्ञा दी जिसे पुरुषों ने अपनी संपत्ति के रूप में देखा जाता रहा है| अपने यौन बल को दर्शाने के लिए पुरुष प्राय: यौन उत्पीड़क व्यवहारों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अपशब्दों का इस्तेमाल, सीटी बजाना या जबरन चुंबन लेना या यौन संबंध बनाने जैसी उत्पीड़क गतिविधियाँ भी शामिल हैं| बहुत बार उत्पीड़न की यह प्रक्रिया उन महिलाओं या लड़कियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, जो उनके पुरुषत्व को चुनौती देती हैं|
पूरी दुनिया की तरह भारत में भी महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वह पुरुष के स्वामित्व के सामने झुकें|
साफ़ है कि जेंडर की अवधारणा महिला और पुरुष को दो सांचे में ढालती है, जिसके तहत पूरी कट्टरता से वे अपने-अपने लिए बताये कामों और अधिकारों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध किये जाते है और जैसे ही कोई भी वर्ग जेंडर आधारित अपनी भूमिका को चुनौती देता है तो तरह-तरह की चुनौतियों और हिंसा का सामना करना पड़ता है| ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक समाज का युवा वर्ग जेंडर के सांचे में पिसता रहेगा? और कब तक मर्दानगी और जननांगी की परिभाषाओं और मानकों में खुद को ढालता रहेगा?
यह लेख क्रिया संस्था की वार्षिक पत्रिका युवाओं के यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकार (अंक 2, 2007) से प्रेरित है| इसका मूल लेख पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें |
अधिक जानकारी के लिए – फेसबुक: CREA | Instagram: @think.crea | Twitter: @ThinkCREA
तस्वीर साभार : in.one.un.org