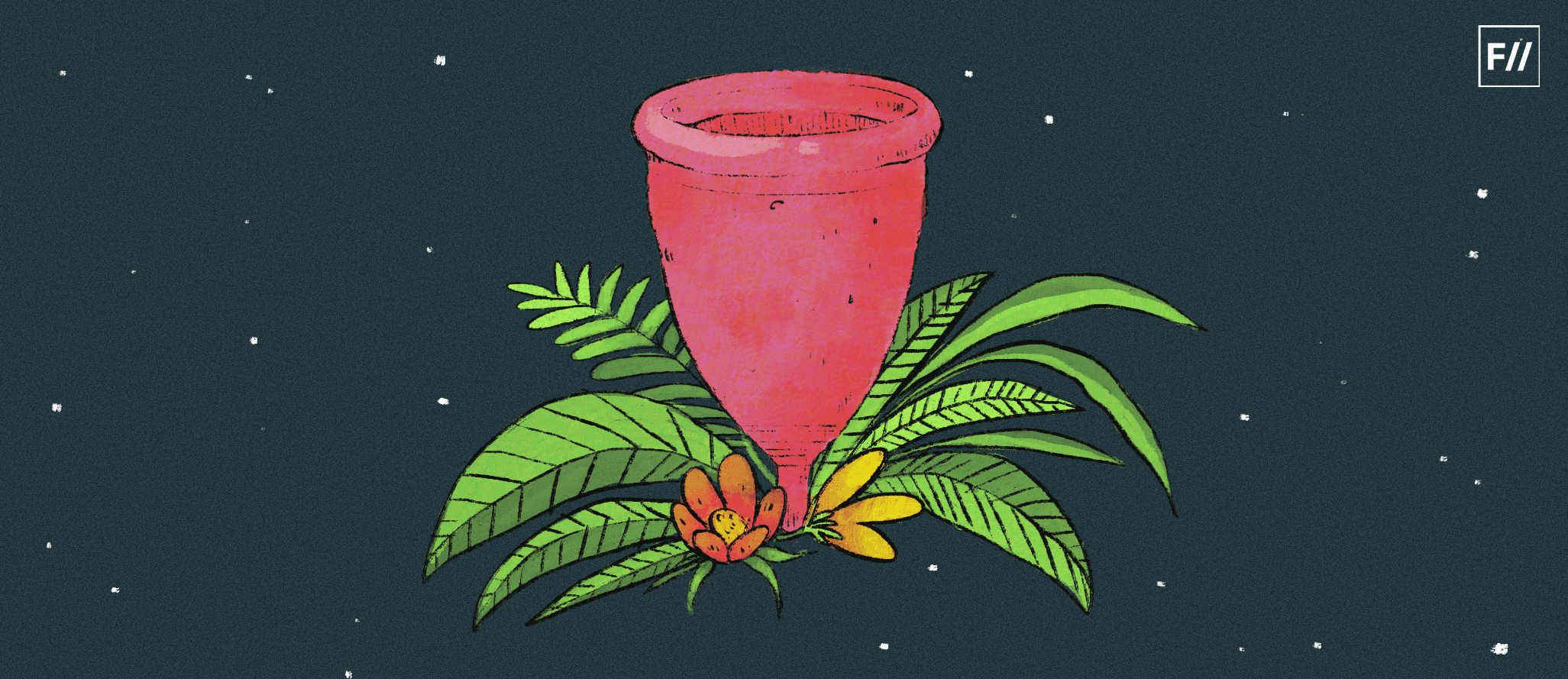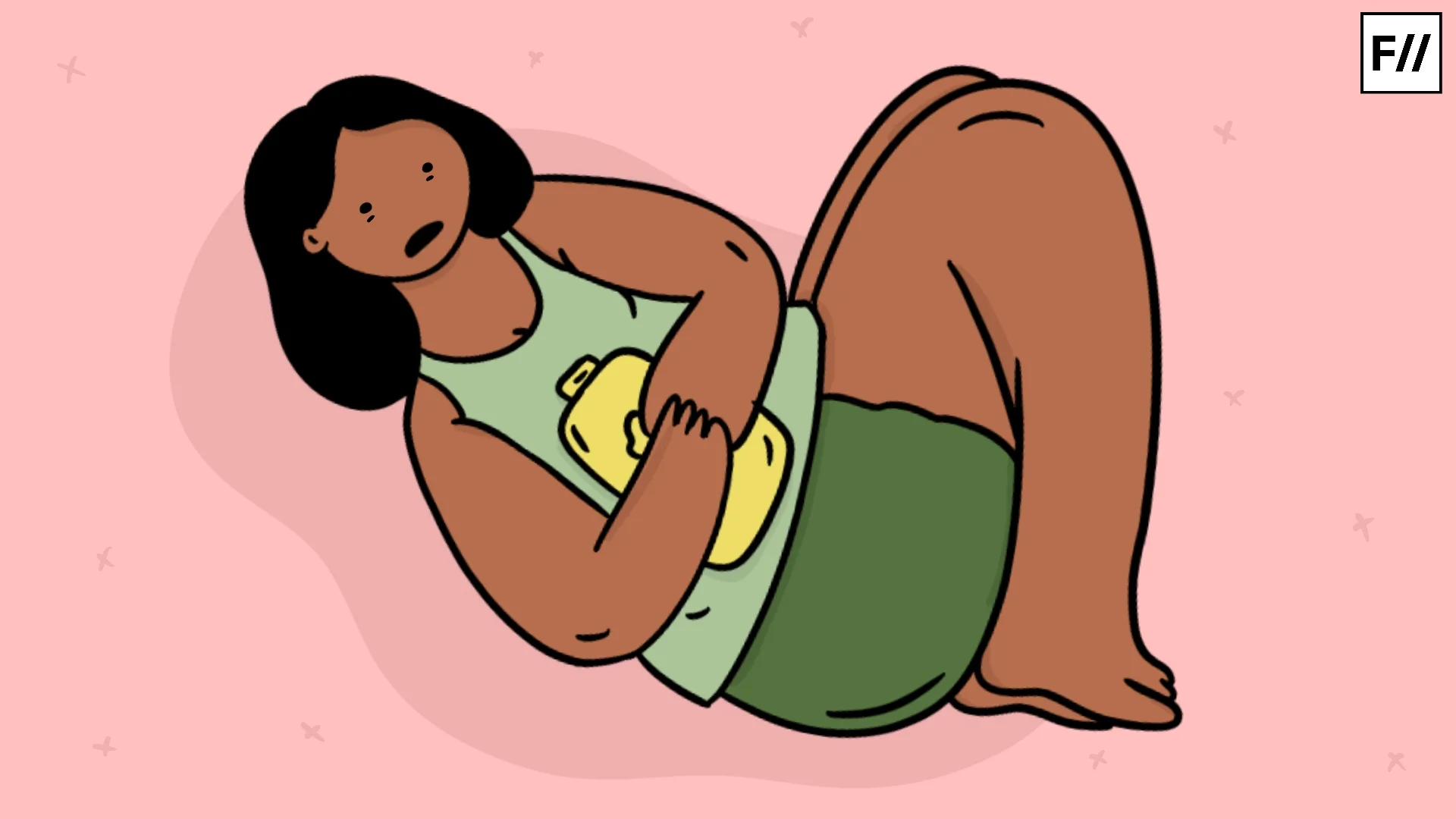चुनाव शुरू हो चुका है और अलग-अलग राज्यों, गांवों और कस्बों में जोर-शोर से चुनाव के जुड़े अभियान, रैली और तैयारियां चल रही हैं। कुछ इलाकों में मतदान का पहला और दूसरा फेज़ भी हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के घोषणापत्र भी निकल चुके हैं। भारत में, चुनाव में अक्सर रोजगार, गरीबों का कल्याण या महिलाओं का सशक्तिकरण मुद्दा बनता है। स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक नीतियां और स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा अक्सर नीति निर्माताओं के बीच चर्चा का विषय रहा है।
देश में अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर एक को अच्छा और किफ़ायती स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया हो। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद ये और भी जरूरी हो गया है। फिर भी, वे शायद ही कभी राजनीतिक मुद्दा बनते हैं।
2019 में लोकनीति-सीएसडीएस के एक अध्ययन में पाया गया कि लोग सरकार से बुनियादी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब मतदान की बात आती है, तो मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता।
जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर है दूसरे सर्वेक्षण
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने में जितनी भूमिका स्वास्थ्य बजट की है, उतनी ही सही आंकड़ों और योजनाओं तक लोगों की पहुँच की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) डेटा बताता है कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 में लगभग 27 प्रतिशत था। 2017-18 में इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और 2019-20 में यह बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया।

आउट ऑफ पॉकेट एक्स्पेन्स (ओओपीई) किसी चिकित्सा सेवा के लिए लोगों का अपने जेब से किए गए भुगतान को बताता है। ये ऐसे भुगतान हैं जो सरकार या किसी स्वास्थ्य बीमा सहित किसी तीसरे पक्ष द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) डेटा बताता है कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यय के संबंध में स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय का हिस्सा 2016-17 में लगभग 27 प्रतिशत था। 2017-18 में इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई और 2019-20 में यह बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया।
जनगणना के आंकड़ों पर आधारित डेटा में समस्या
एनएचए डेटा से पता चलता है कि भारत में ओओपीई में भारी गिरावट आ रही है। यह 2016-17 में मौजूदा स्वास्थ्य व्यय के 63 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 55 प्रतिशत हो गया और इसमें गिरावट जारी है। 2019-20 में यह लगभग 52 प्रतिशत था। ओओपीई का अनुमान लगाने के लिए, यह सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य’ और ‘उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दौर का उपयोग करता है। लेकिन चूंकि देश की पूरी आबादी को अपने सर्वेक्षण में शामिल करना संभव नहीं है, इसलिए एनएसओ डेटा एकत्र करने के लिए एक नमूना सर्वेक्षण करता है। यह सैंपलिंग फ्रेम डिजाइन करने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करता है।
हमारे देश में हर साल स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 फीसद है, जबकि चीन में यह 3 फीसद, ब्राज़ील में 4 फीसद और दक्षिण अफ्रीका में 4.5 फीसद है।
सरकार के और वैश्विक संस्थाओं के आंकड़ों में अंतर
वैश्विक मेडिकल जर्नल लैन्सेट के अनुसार एक और विवाद वाला मुद्दा ये है कि सरकार के किए गए लगातार दावों में विश्वसनीयता की कमी है। सरकार के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण महज 0·48 मिलियन लोगों की मौत हुई, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अनुमान छह से आठ गुना ज्यादा हैं। अप्रकाशित 2021 सिविल पंजीकरण रिपोर्ट सरकार के अनुमान की पुष्टि या खंडन करने में मदद करेगी।

नमूना पंजीकरण प्रणाली सर्वेक्षण और मिलियन डेथ स्टडी के नए परिणामों का प्रकाशन 2020-21 के दौरान मृत्यु दर में बदलाव के प्रमुख सवालों का समाधान कर सकता है। यह कैंसर, आत्महत्या से मौत और बाल मृत्यु दर में जारी गिरावट जैसी संभावित अच्छी ख़बरों पर शायद कोई प्रमाण भी दे सकेगा। लेकिन, अफसोस की बात है कि ये अध्ययन अगर जारी होते भी हैं, तो भी ये हालिया चुनाव के बाद होने की संभावना है।
क्या राजनीतिक पार्टियों ने तैयार किया फ्रेमवर्क
संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्र और राज्य सरकारों का बजट व्यय वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1 फीसद और वित्त वर्ष 22 में 2.2 फीसद था, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 1.6 फीसद था। हमारे देश में हर साल स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 फीसद है, जबकि चीन में यह 3 फीसद, ब्राज़ील में 4 फीसद और दक्षिण अफ्रीका में 4.5 फीसद है। हालांकि घोषणापत्र में लगभग सभी पार्टियों ने चुनिंदा योजनाओं से रूप में व्यापक वादे करते हैं।
सरकार के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण महज 0·48 मिलियन लोगों की मौत हुई, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अनुमान छह से आठ गुना ज्यादा हैं। इसके साथ ही 150 सालों में पहली बार, एक पूरा दशक बीत गया, जिसमें भारत या उसके लोगों पर कोई आधिकारिक व्यापक डेटा नहीं था।
पर घोषणापत्र के हर वादे को पूरा करने के लिए जरूरी बजट के बारे में कोई बात नहीं होती। न ही इस बजट के स्रोत पर बात होती है। लैन्सेट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई। इसके साथ ही 150 सालों में पहली बार, एक पूरा दशक बीत गया, जिसमें भारत या उसके लोगों पर कोई आधिकारिक व्यापक डेटा नहीं था। यह वादा कि अगली जनगणना 2024 में किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेक्षण होगा, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जनगणना सभी राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षणों का भी आधार है।
क्या जनता सचमच जागरूक नहीं हैं

आम तौर पर देश का एक बड़ा हिस्सा चाहे या अनचाहे प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। कोविड के बाद लोगों को और भी ज्यादा मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है। सरकार के पास आंकड़ों की कमी होने से चुनाव के मद्देनजर कोई ठोस रणनीति पेश नहीं किया जाता। योजनाओं के घोषणा के बावजूद, योजनाओं के कार्यान्वयन में खामियां रहती हैं। 2019 में लोकनीति-सीएसडीएस के एक अध्ययन में पाया गया कि लोग सरकार से बुनियादी चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब मतदान की बात आती है, तो मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता।
स्क्रॉल में छपी के खबर अनुसार एक सर्वे के अनुसार लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में विकास के स्तर में सुधार के लिए स्वास्थ्य को शिक्षा और रोजगार के बराबर महत्व देते हैं।
न ही राजनीतिक दल आम तौर पर अपने घोषणापत्र या अभियान में स्वास्थ्य व्यवस्था के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देते हैं। वोटर्स के लिए विकास का मुद्दा भर कह देना आसान है। लेकिन ये तय करने की जिम्मेदारी महज मतदाताओं की नहीं हो सकती। सरकार को अपने मुद्दे चुनने होंगे जिनपर वे लक्ष्य तैयार कर काम कर सकें। सार्वजनिक स्वास्थ्य का चुनावी मुद्दा न बनने का एक करण ये भी है कि आम तौर अपने अधिकारों के लिए सबसे जागरूक मध्यम वर्ग चिकित्सा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक नहीं जाते। स्क्रॉल में छपी के खबर अनुसार एक सर्वे के अनुसार लोग अपने स्थानीय क्षेत्र में विकास के स्तर में सुधार के लिए स्वास्थ्य को शिक्षा और रोजगार के बराबर महत्व देते हैं।
बीमारियों का बोझ और डेटा में कमी
भारत पर बीमारियों का भारी बोझ है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग से होने वाली कुल मौतों का पांचवां हिस्सा, खासकर युवा वयस्कों में होता है। इसी तरह डेटा की कमी भी लोगों को ही नहीं नीतिनिर्माताओं को भटका सकती हैं। 2013 में, एक सरकारी समिति ने कथित तौर पर पाया कि देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या पहले के अनुमान से कम से कम 20-30 गुना अधिक होगी। इसी तरह, 2015 में, भारत में तपेदिक (टीबी) से होने वाली अनुमानित मौतों की संख्या को 2014 की अनुमानित संख्या की तुलना में दोगुना करने की जरूरत है।
2013 में, एक सरकारी समिति ने कथित तौर पर पाया कि देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की वास्तविक संख्या पहले के अनुमान से कम से कम 20-30 गुना अधिक होगी। इसी तरह, 2015 में, भारत में तपेदिक (टीबी) से होने वाली अनुमानित मौतों की संख्या को 2014 की अनुमानित संख्या की तुलना में दोगुना करने की जरूरत है।
जब बुजुर्गों की बात लाई गई
2014 में अधिकतर पार्टियों ने अपने घोषणापत्रों में ‘पेंशन’ के विषय को शामिल किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि देश के नागरिक, और विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिक, अपने पेंशन फंड के संबंध में अधिक सुरक्षा के हकदार हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी योजना पर चर्चा नहीं की। दूसरी ओर, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अतिरिक्त कर लाभ और उच्च ब्याज दरों जैसे विचारों की खोज की जाएगी। भाजपा ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में वरिष्ठ नागरिकों को स्वयंसेवकों या कार्यकर्ताओं के रूप में शामिल करने के लिए योजनएं तैयार करने की बात कही।
वहीं सीपीआई (एम) ने अपने 2014 के घोषणापत्र में बुजुर्ग पेंशन पर ध्यान दिया था और एआईटीएमसी ने घोषणापत्र में बुजुर्गों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज, सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ने के साथ, पहले से कहीं ज्यादा साक्ष्य और ज्यादा सूचित रिपोर्टिंग; मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रही है। इससे सरकार के बनाए गए योजनाओं पर नीतिगत बहस हो पा रही है। इसलिए, केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा में सुधार करना और भी जरूरी हो जाता है। सही डेटा, स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक नीति तैयार करने में मददगार साबित होगी।