आम तौर पर समाज ने पुरुषों के लिए भी कुछ मानदंड बनाए हैं। एक गुस्सा करता हुआ पुरुष भले आपको आए दिन दिखता हो, लेकिन एक संवेदनशील पुरुष जो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, ऐसे पुरुष बहुत कम दिखते हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक तौर पर वे खुदको व्यक्त नहीं कर पाते, खेल का क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां समाज उन्हें कमजोर होने या अपनेआप को अभिव्यक्त करने का मौका देता है। अमूमन खेल में कोई सामाजिक या सांस्कृतिक मापदंड तय नहीं होता। खेल का मैदान या खेल की जगह ये नहीं कहती कि पुरुष ऐसा ही रहेगा, ये ही करेगा।
आमतौर पर अगर कोई पुरुष पितृसत्तातमक मानदंडों को तोड़ता है, वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, तो उसे कमजोर कहा जाता है। लेकिन खेलों में जो रोते या खुलकर अपनी कमजोरी या नाकामियों को अपनाते पुरुषों की हम तारीफ़ करते हैं। हमारे पितृसत्तातमक समाज ने ये तय कर दिया है कि अगर कोई पुरुष का अर्थ ही कठोर होना है। अक्सर खुदको अभिव्यक्त करने से उन्हें ‘कमजोर और नामर्द’ जैसे बेतुकी बातें सुनने को मिलती है। अगर कोई लड़की जन्म लेती है, तो उसे जीवन के पहले पड़ाव से आखिरी पड़ाव तक बताया जाता है कि उसके लिए कौन से खेल सही हैं, कैसे कपड़े सही हैं, या किस तरह का व्यवहार उचित है।
समाज में जहां महिलाओं का रोना कई सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में अच्छा या सटीक माना जाता है, वहीं पुरुषों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने से समाज रोकता है। बचपन से ही लड़कों को ये सिखाना कि वे कुछ भी कर सकते हैं।
तेज बोल नहीं सकती, ज़ोर से हंस नहीं सकती, ये सारे मानदंड लड़कियों को अक्सर सुनने और मानने पड़ते हैं। वहीं जब लड़का पैदा होता है, तो उसे आमतौर पर किसी चीज़ के लिए रोक नहीं जाता। वो किसी भी प्रकार के खेल खेल सकता है, घर से कहीं भी बाहर जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी कपड़े पहनने का तरीका पहले से सुनिश्चित रहता है। उसे बचपन से ही यही बताया जाता है कि तुम लड़के हो, इसलिए तुम कमजोर नहीं हो सकते। लड़कियों की तरह मत रोया करो, ये हर मोड़ पर उन्हें बताया और समझाया जाता है। पुरुषत्व का मतलब सख्त, गुस्सा करने वाला, न रोने वाला है। शायद इसलिए पुरुष अपनेआप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं।
पितृसत्ता कैसे पुरुषों को प्रभावित कर रही है
भारतीय समाज को पुरुषवादी समाज माना जाता है। बहुत सारे पुरुष ये बताते हुए बहुत गर्व भी महसूस करते हैं। पुरुषत्व की पारंपरिक अवधारणा काफी कठोर है। हमारे समाज में सच्चे अर्थों में ‘पुरुष’ का अर्थ है आवाज तेज हो, गुस्सा दिखाने या हिंसक होना उनकी ताकत के रूप में गिनती हो। कोई भी परिस्थिति हो, अपनेआप को ऐसा दिखाना कि कुछ हुआ ही नहीं। इस समाज में किसी प्रकार की भावना को व्यक्त करने से पुरुष को कमजोर कहा जाता है। उनकी तुलना महिलाओं से की जाती है। रोते हुए लड़कों को अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों की तरह नहीं रोना चाहिए।

समाज में जहां महिलाओं का रोना कई सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में अच्छा या सटीक माना जाता है, वहीं पुरुषों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने से समाज रोकता है। बचपन से ही लड़कों को ये सिखाना कि वे कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें हारना नहीं है, एक अलग प्रकार का दबाव बनाता है। यह पुरुषों को हमेशा आत्मनिर्भर, बहादुर, कठोर और भावनात्मक रूप से मजबूत रहने के लिए कहती है ताकि बतौर ‘पुरुष’ वे ‘सम्मान’ बनाए रख सकें।
टेनिस की दुनिया में यह दिन भले ही अपनेआप में खास था, लेकिन इसने पुरुषों और उनके भावनात्मक रूप से कमजोर होने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया।
सिनेमा का प्रभाव

इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप बॉलीवुड में देख सकते हैं। कबीर सिंह या एनिमल जैसी फिल्मों को बहुत पसंद किया गया। लेकिन उसमें पुरुष को एक निर्दिष्ट रूप में दिखाया गया। सिनेमा हमें बहुत प्रभावित करता है और ऐसे मानदंड दिखाने से जनता नकारात्मक रूप में भी प्रभावित होती है। लोग ऐसे व्यवहार को आदर्श समझते हैं और पुरुष अपने निजी जीवन में वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। इससे महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सोच को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, हिंसा की घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है। पुरुष जीवनभर समाज में अपने आस-पास सिर्फ नकारात्मक मानदंड ही सीखते हैं और उसीके अनुसार चलते हैं।
खेल का मैदान और पुरुषों की भावना
पितृसत्ता पुरुषों को भी उतना ही प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर खेल के मैदान पर अगर कोई पुरुष सामाजिक तौर पर अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है। समाज ने पुरुषों को न खुशी में खुश और न दुखी में दुख दिखाने का इजाज़त देता है। पितृसत्ता पुरुषों के लिए भी एक बंधन के रूप में काम करता है। साल 20222 में टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने अपना विदाई मैच खेला, जो खिलाड़ी और हर अन्य टेनिस प्रशंसक के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। स्टेडियम में बैठे लोग से लेकर हर व्यक्ति खास तौर पर टेनिस के दिग्गज और यहां तक कि उनके प्रतिद्वंद्वी राफेल नडाल की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से पीछे नहीं हटे। टेनिस की दुनिया में यह दिन भले ही अपनेआप में खास था, लेकिन इसने पुरुषों और उनके भावनात्मक रूप से कमजोर होने के तरीके के बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया।
कुछ दिनों पहले भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने फुटबॉल जीवन से संन्यास लेने का फैसला किया। वे अपने करियर के अंतिम मैच में भावुक होते नजर आए। सामाजिक रूप से, पुरुषों और महिलाओं के लिए रोने की स्वीकृति में एक बड़ा अंतर होता है।
पुरुषों का भावुक होना और समाज के मानदंड
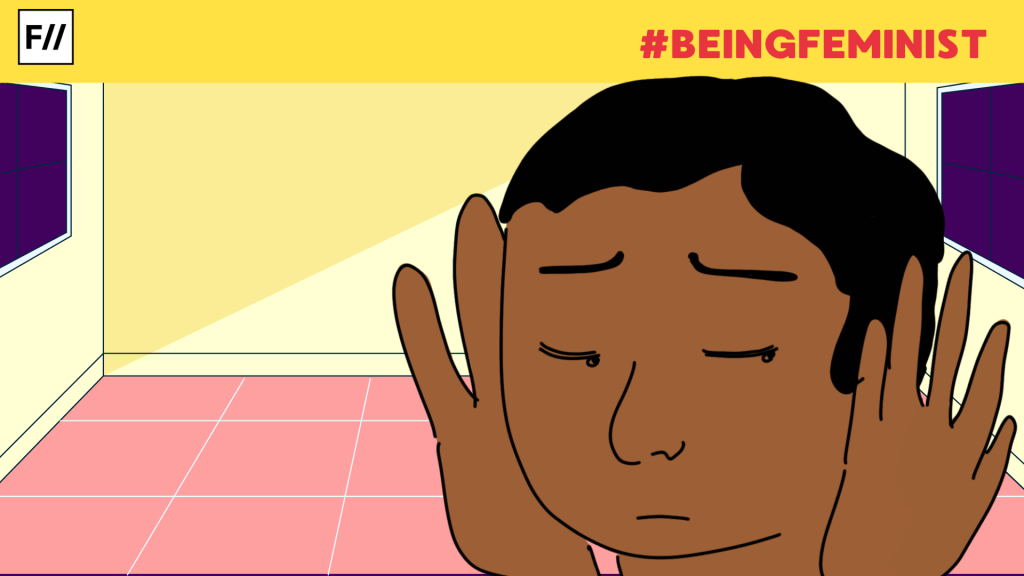
खेलों में हम पुरुषों को अपनेआप को अभिव्यक्त करते हुए देखते हैं। वे खेल में हारने पर दुखी होते हैं और जीतने पर खुश होते हैं। कुछ दिनों पहले भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अपने फुटबॉल जीवन से संन्यास लेने का फैसला किया। वे अपने करियर के अंतिम मैच में भावुक होते नजर आए। सामाजिक रूप से, पुरुषों और महिलाओं के लिए रोने की स्वीकृति में एक बड़ा अंतर होता है। जहां महिलाओं के लिए रोना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया मानी जाती है, पुरुषों के लिए इसे ‘कमजोरी’ के रूप में देखा जाता है। यह सोच पुरुषों को अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर करती है, जिससे वे भावनात्मक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं। चाहे खेल का मैदान हो या घर, हम अक्सर देखते हैं कि पुरुष अपनेआप को बहुत उत्तेजित दिखाते हैं। हालांकि किसी स्थिति पर गुस्सा या नाराज़गी एक सामान्य भावना है, लेकिन यह हिंसक होने इजाज़त नहीं देता।
पारंपरिक मान्यताएं ज्यादातर पुरूषों को उनके पिता या कोई रोल मॉडल के अनुरूप बनाती है। अमूमन वे पुरुष पितृसत्ता के गहरे जाल में फंस जाते हैं। हम अक्सर समाज में लोगों को कहते सुनते हैं कि पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। हमें भी यही करना चाहिए। जो पुरुष रूढ़िवादी विचारधारा का पालन करते हैं, उनके लिए पहनने, खाने से लेकर नौकरी तक के नियम समाज ने पहले से बनाए हुए हैं। सामाजिक तौर पर पुरुष को संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें खुद को अभिव्यक्त करना चाहिए। अगर पुरुष सामाजिक तौर पर खुद को अभिव्यक्त करते हैं, तो इससे उनकी मानसिक तनाव भी कम होगी। इससे वो महिलाओं का साथ भी बेहतर रूप में दे पाएंगे या समाज में लैंगिक समानता में अपनी भागीदारी दे सकते हैं।




