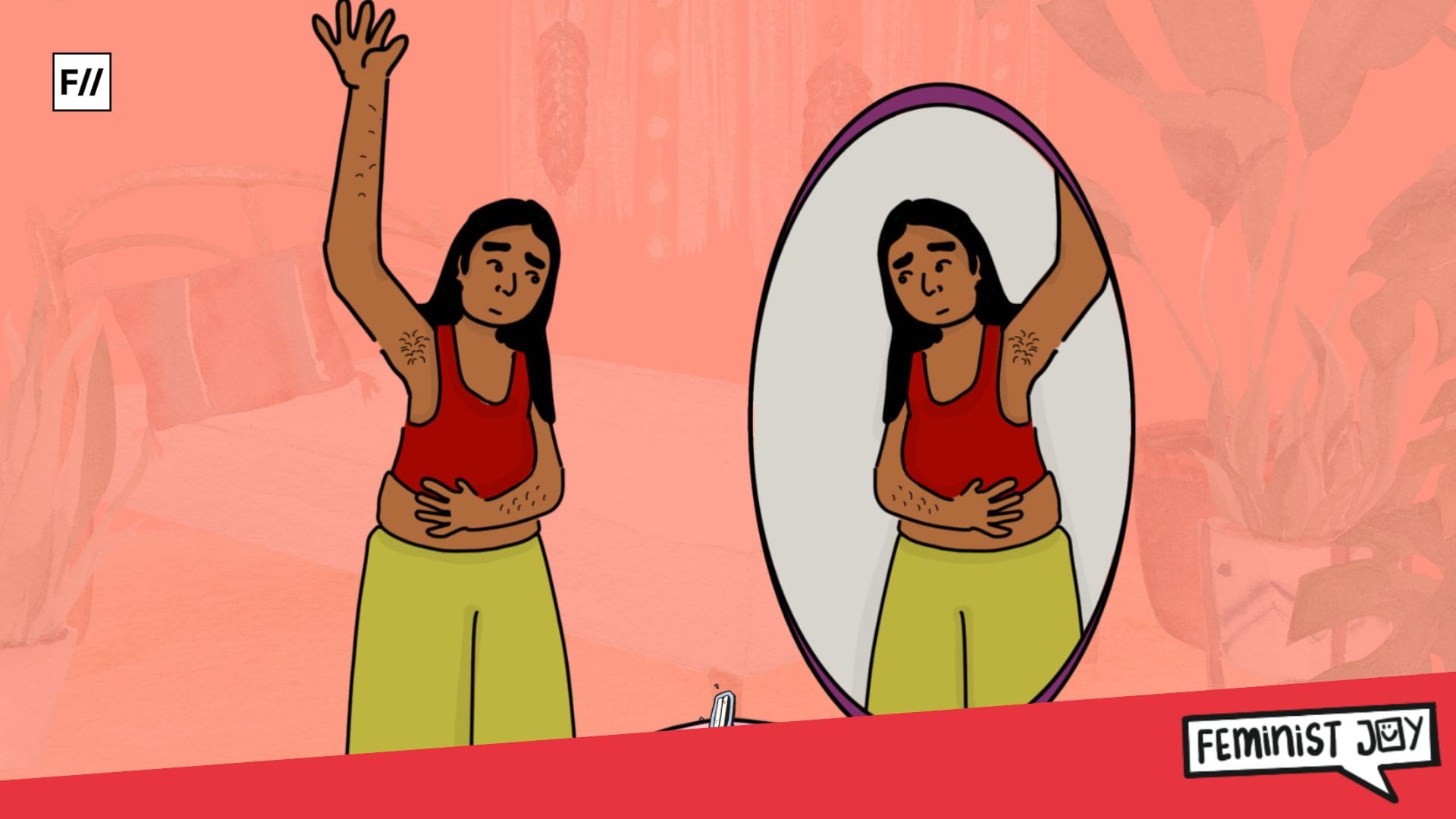भारत में पितृसत्ता की जड़े बहुत गहरी हैं। आपको देश की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी इकाई में पितृसत्ता मौजूद मिलेगी और इन सबकी शुरुआत घरों से होती है, जहां हर बच्चे की सामाजिक नींव रखी जाती है। भारत में ज्यादातर मध्यवर्गीय परिवार पितृसत्ता की बनी-बनाई व्यवस्था के अनुकूल चला करते हैं। जब मैं पैदा हुआ तब मेरा परिवार भी उसी व्यवस्था के तहत था। उस समय मेरे घर में मर्दों का काम बाहर कमाना और औरतों का काम रसोई संभालना हुआ करता था। मर्द जब चाहे औरतों पर हाथ उठा सकते थे और औरतों को बिना कोई विरोध किए इसको सहना पड़ता था। पर वक़्त ने सब बदल दिया। ख़ासकर मुझे।
मैंने बचपन में मान लिया था कि मुझे बहुत पैसे कमाकर घर के हर काम के लिए नौकर रखने हैं। मैं मानता था घर के काम मेरे नहीं है। इनके लिए नौकर होने चाहिए। झाड़ू लगाना, बर्तन-कपड़े धोना और खाना बनाने जैसे काम कभी भी माँ ने मुझे नहीं करने दिए और न ही बचपन में मैंने ये काम कभी अपने पापा को करते देखा था। मुझे नहीं मालूम कि कब और कैसे मेरे मन में ये बात घर कर गई कि घर के काम लड़कों को नहीं करने हैं।
मैंने बचपन में मान लिया था कि मुझे बहुत पैसे कमाकर घर के हर काम के लिए नौकर रखने हैं। मैं मानता था घर के काम मेरे नहीं है। इनके लिए नौकर होने चाहिए।
स्कूल नहीं सोच में बदलाव
जब मैंने 10वीं पास कर बॉयज स्कूल छोड़ को-एड स्कूल में दाख़िला लिया तब मैंने एक अलग दुनिया देखी। यहां लड़के और लड़कियों में खास भेदभाव नहीं होता था। मुझ को नए वातावरण में एडजस्ट होने में वक़्त नहीं लगता जिस कारण मैं उस स्कूल में ज़ल्दी ही एडजस्ट हो गया। आप मान सकते हैं कि यह वो वक़्त है जब मेरी नारीवादी बनने की शुरुआत हुई। यहां मैंने पहली बार हमउम्र लड़कियों से बिना शर्म और झिझक के बात की और उन्हें समझना शुरू किया। इसी दौरान मुझे समझ आया कि लड़कियों और लड़कों में सर्वनाम के अलावा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। पर यहां भी लड़कियों के संग भेदभाव तो था ही। यहां आने के बाद मैंने पितृसत्तात्मक समाज को बारीकी से समझना शुरू किया और इसमें मेरी सबसे ज्यादा मदद मेरी पहली महिला साथी ने की।

पितृसत्ता और नारीवाद के बारे में स्नातक और स्नातकोत्तर के समय में मैंने पढ़ना शुरू किया। पर इस बारे में मेरे विचारों की नींव स्कूल में ही रख दी गई थी। बॉयज स्कूल से पढ़ने वाले लड़कों का उनकी माँ और बहन के अलावा किसी और लड़की से शायद ही कुछ ख़ास इंटरेक्शन होता हो। को-एड स्कूल में पढ़ने पर दोनों लिंगों में एक-दूसरे से अलग-तलक होने का भाव घर नहीं करता है। हाँ! पर दोनों को भलीभांति एकदूसरे की शारीरिक और मानसिक क्षमता का पता ज़रूर चल जाता है। पढ़ाई, खेल, और अन्य किसी भी गतिविधियों में दोनों ही जेंडर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर काम करते हैं न कि लैंगिक आधार पर।
मुझ को नए वातावरण में एडजस्ट होने में वक़्त नहीं लगता जिस कारण मैं उस स्कूल में ज़ल्दी ही एडजस्ट हो गया। आप मान सकते हैं कि यह वो वक़्त है जब मेरी नारीवादी बनने की शुरुआत हुई।
मेरे जीवन में एक लड़की साथी का आना
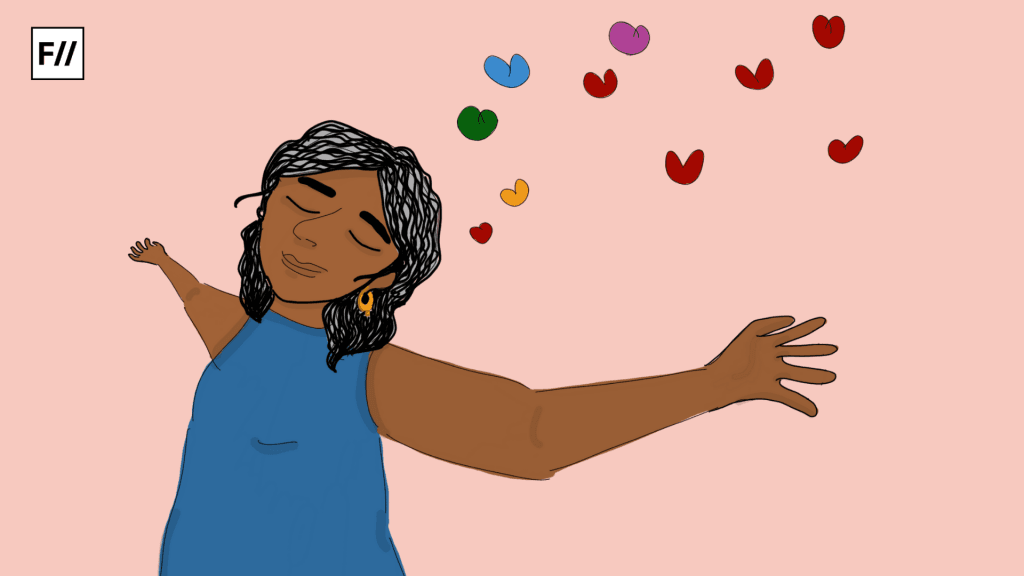
स्कूली दिनों में मेरी मुलाक़ात मेरी साथी से हुई जिसने मेरी ज़िन्दगी के नारीवादी पक्ष को मेरी आँखों के सामने रख दिया। जितना उसने मुझे एक लड़की होना क्या होता है समझाया, शायद ही कोई और मुझे समझा सकता था। रोज़ाना उठाई जाने वाली लड़कियों की तकलीफ़ें; घर से कॉलेज सफ़र करते हुए लड़कों का यौन हिंसा, घर में भाई और बहन में काम को ले कर भेदभाव झेलना, समाज की लड़कियों से कोमल, त्यागी और सहज होने की अपेक्षाएं रखना और काफ़ी कुछ। उससे मिलने के बाद मुझे नहीं पता कब और कैसे मैंने कपड़े-बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू लगाने जैसे घर के काम करना शुरू कर दिए। फिर धीरे-धीरे मुझे खाना बनाने में मज़ा भी आने लगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुझे मेरे जैसा बनाने में मेरी साथी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होती, तो शायद मैं कभी भी लड़कियों और लड़कों में होने वाले भेदभाव को बारीकी से नहीं समझ पाता और न ही आज मैं ये लेख लिख रहा होता। मैंने इसी दौरान समझा कि घर के काम तो सबको आने चाहिए। आप किसी भी जेंडर के क्यों न हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वर्तमान समय में ये सर्वाइवल स्किल (survival skill) है, जो समाज में अच्छे जीवन शैली जीने के लिए ज़रूरी है।
घर से हो अधिकारों और बराबरी की बात
लड़कियों की रोज़ाना के संघर्षों को समझने के बाद वो मेरे लिए एलियन नहीं रही। वो मुझे हर दूसरे व्यक्ति की तरह समान लगी। मैंने अब बदलाव की पहल घर से ही की। मैंने भाई और पापा को रसोई के काम करने के लिए प्रोत्सहित किया। कभी उनके बनाए खाने की तारीफ़ कर, तो कभी उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है इसका एहसास दिलाकर। फिर मुझे बाद में पता चला कि पापा तो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। बस उन्होंने शादी के बाद खाना बनाना बंद कर दिया था। पर पिछले 7-8 साल से पापा को काफ़ी बार खाना बनाते देखा है। पिछले बीते साल में तो कई बार। भाई को भी कई बार अपने पसन्द की टेस्टी डिश बनाते देखा है। पर दोनों लोग सफ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं हैं। पापा को सफ़ाई पसन्द है पर अच्छे से सफ़ाई नहीं कर पाते हैं और शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है।
स्कूली दिनों में मेरी मुलाक़ात मेरी साथी से हुई जिसने मेरी ज़िन्दगी के नारीवादी पक्ष को मेरी आँखों के सामने रख दिया। जितना उसने मुझे एक लड़की होना क्या होता है समझाया, शायद ही कोई और मुझे समझा सकता था। रोज़ाना उठाई जाने वाली लड़कियों की तकलीफ़ें; घर से कॉलेज सफ़र करते हुए लड़कों का यौन हिंसा, घर में भाई और बहन में काम को ले कर भेदभाव झेलना, समाज की लड़कियों से कोमल, त्यागी और सहज होने की अपेक्षाएं रखना और काफ़ी कुछ।
माँ अगर माँ नहीं होती तो क्या होती?
एक बार माँ ने मुझे बताया कि उन्हें खाना बनाने में मज़ा आता है। मैंने ये तक देखा है कि जब भी वो कुछ नया बनाती हैं या उनका बनाया खाना कोई और खाता है, तो उन्हें ये जानने की काफ़ी इच्छा रहती है कि “खाना कैसा था”। पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि वो बचपन से ही केवल खाना बनाना और घर की सफ़ाई जैसे काम करना चाहती थी। उनके भी अपने सपने थे जो न उन्होंने किसी को बताए और न ही किसी ने जानना चाहा। वो भी उन्हें कहीं पीछे छोड़ आई। शायद उनको इस बात का कभी एहसास ही न रहा हो। जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पढ़ाई की होती तो वो शायद मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जाना चाहती।
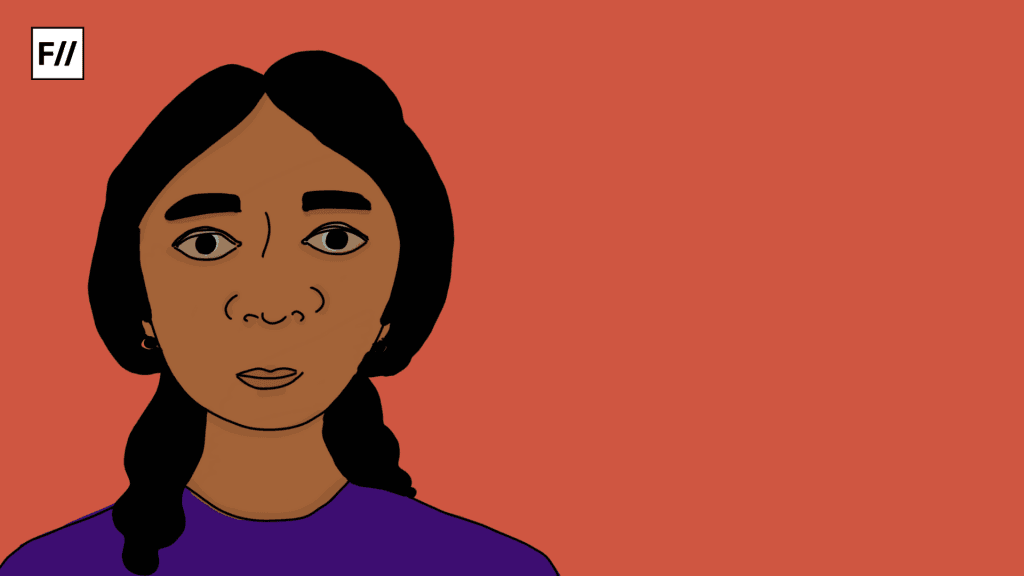
ये कहने के पीछे मेरी माँ का एक्सट्रोवर्ट होना है। मैंने उन्हें अनजान लोगों से बड़ी सहजता से बात करते देखा है। बात ही नहीं उनके बारे में जानकारी या कोई काम की जानकारी भी आराम से निकलते देखा है। जो बड़े से बड़े कम्यूनिकेटर अभी तक सही से नहीं कर पाते हैं। ये सब बताते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये भी कितना अजीब है कि ये निर्णय भी मैं यानी एक पुरुष उनके लिए करना चाह रहा हूं। जो अभी भी मेरे अंदर कहीं न कहीं बची पितृसत्ता की गवाही दे रहा है। पितृसत्ता मुझे हर बार हैरान कर देती है। ये बताकर कि उसकी जड़ कितनी गहरी हैं, जिसे निकाल फेंकने में हमें अभी भी कई और साल लगेंगे।
मैंने उन्हें अनजान लोगों से बड़ी सहजता से बात करते देखा है। बात ही नहीं उनके बारे में जानकारी या कोई काम की जानकारी भी आराम से निकलते देखा है। जो बड़े से बड़े कम्यूनिकेटर अभी तक सही से नहीं कर पाते हैं। ये सब बताते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये भी कितना अजीब है कि ये निर्णय भी मैं यानी एक पुरुष उनके लिए करना चाह रहा हूं।
माँ ने हमेशा अपने से आगे परिवार को रखा है, जिस कारण उन्होंने अपने जीवन में कितने त्याग किए, मैं नहीं जानता। शायद ऐसी महिला को ही तो पितृसत्तात्मक समाज में आदर्श नारी कहा जाता है। पर कभी-कभी लगता है अगर वो स्वार्थी हो कर अपने लिए अपना जीवन जीतीं, तो उनकी ज़िन्दगी आज कुछ और होती। उनका जीवन कुछ भी रहा हो, पर उन्होंने अपने पास की हर लड़की को एक लड़के जितनी स्वतंत्रता और समानता देने की कोशिश की है। शायद उन्हें हमेशा से एहसास था कि लड़की और लड़कों में कोई अंतर नहीं। माँ या माँ की तरह और व्यक्तियों को देखकर लगता है कि समाज से पितृसत्ता को खत्म करने में सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का ही होगा, जो जाने-अनजाने में पितृसत्ता के ख़िलाफ़ अनकही लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात न ही कोई करता है और शायद ही कोई कभी करे।