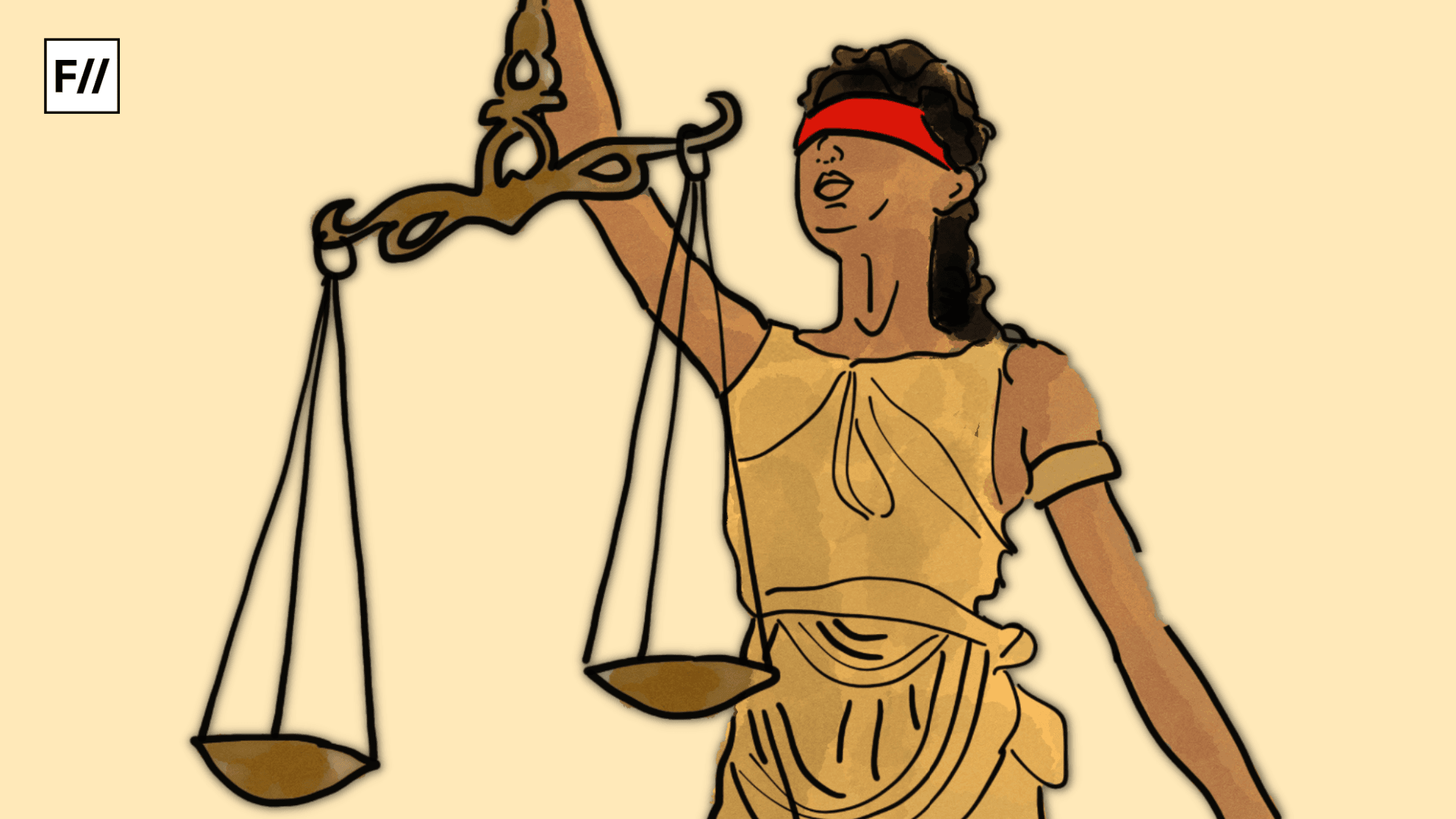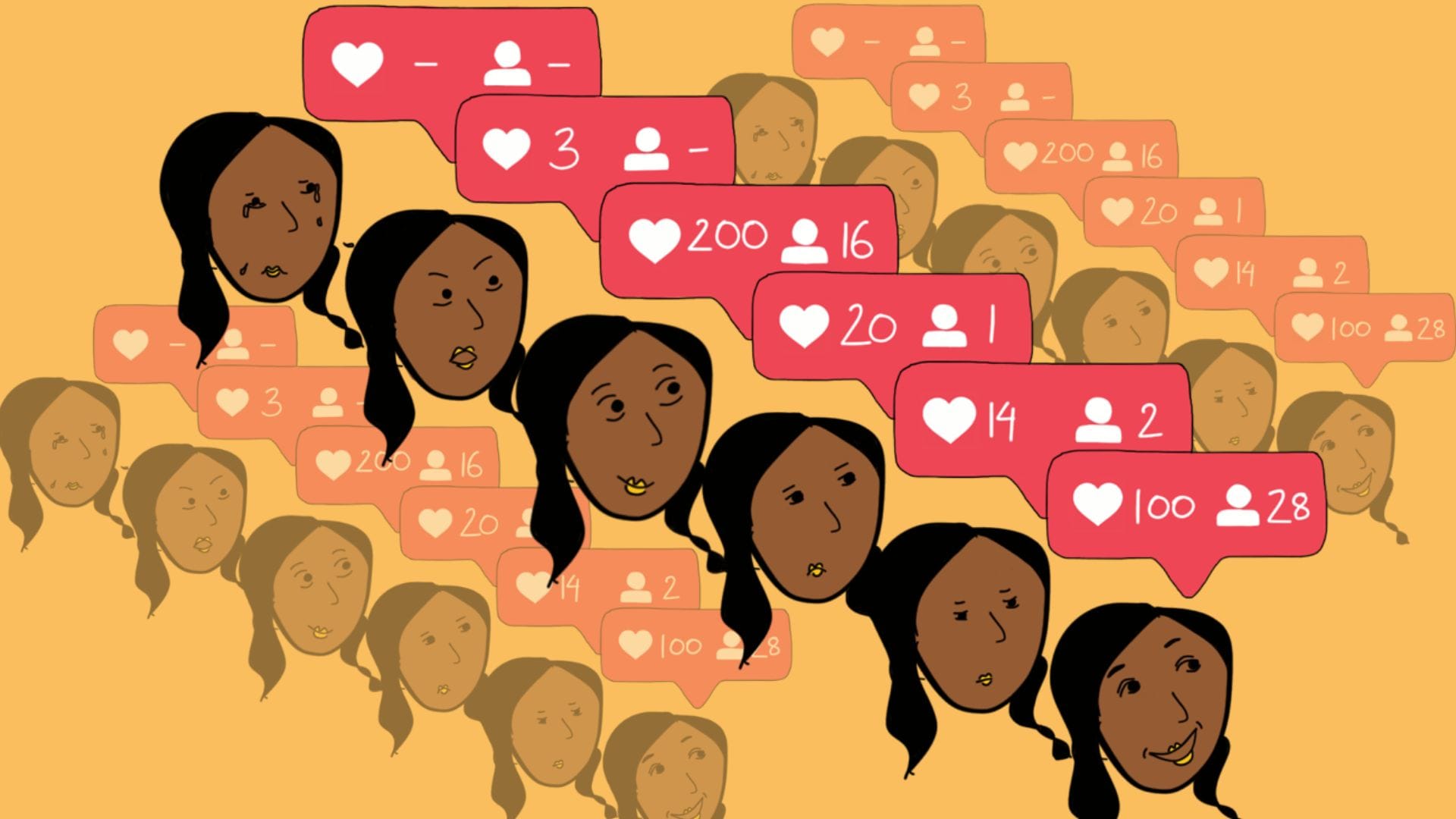भारत का क़ानूनी इतिहास बहुत लंबा और जटिल रहा है। समय के साथ, इसने समाज और संस्कृति की बदलती परिस्थितियों को दिखाया है। हालांकि, महिलाओं को हमेशा से ही क़ानूनी दृष्टिकोण से नुकसान उठाना पड़ा है। अफसोस की बात है कि आज भी भारत में महिलाओं के लिए कुछ क़ानून भेदभावपूर्ण और हानिकारक हैं। महिलाओं को समानता और अधिकार देने के लिए कई आंदोलनों ने भारतीय क़ानून में सुधार की मांग की है। इन आंदोलनों ने महिलाओं से संबंधित क़ानूनों में कई बदलाव लाए हैं। फिर भी, इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस लेख में हम उन क़ानूनों का जिक्र करेंगे जो महिलाओं के लिए ज़रूरी हैं।
1. भरण-पोषण का अधिकार
प्रत्येक शादीशुदा महिला को अपने पति से सहायता या कानूनी रूप से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, भले ही वे एक साथ नहीं रह रहे हों। यह अधिकार भारत में महिलाओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे कानूनों द्वारा संरक्षित है। हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 24 के अनुसार, पत्नी या पति में से कोई भी वित्तीय सहायता मांग सकता है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होता है कि उनके पास खुद का समर्थन करने के लिए आय का कोई स्रोत नहीं है।
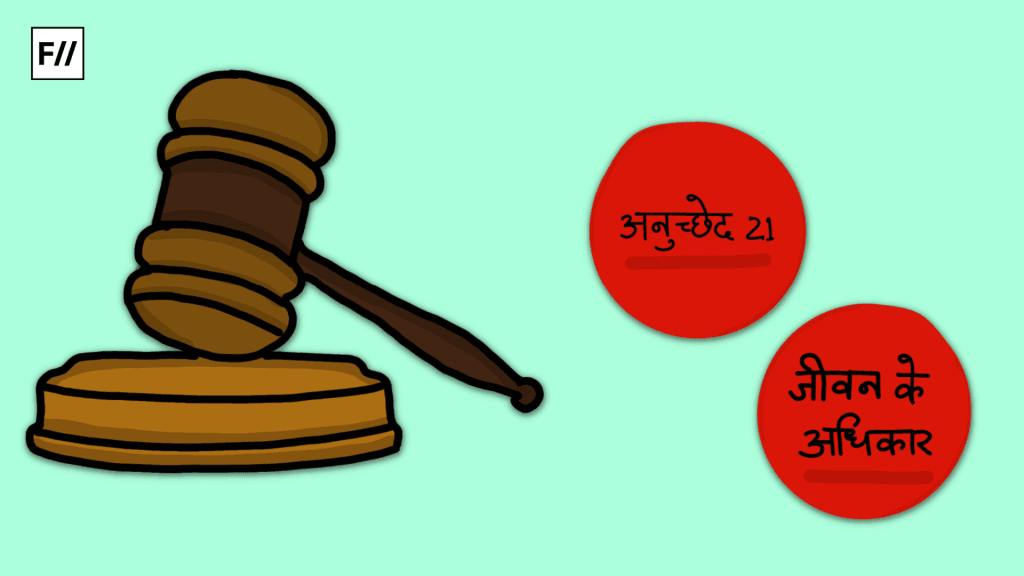
इसके आलावा, एक पत्नी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने का कानूनी अधिकार है, जिसका मतलब है कि यदि पति अपनी पत्नी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है, यदि वह अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, बशर्ते उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त साधन हों, और पत्नी व्यभिचार में नहीं रह रही हो या उचित कारण के बिना उसके साथ रहने से इनकार नहीं किया हो। यह अधिकार धर्म या व्यक्तिगत कानून की परवाह किए बिना लागू होता है।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976) भारत सरकार द्वारा पारित एक कानूनी अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच समान काम के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है।
2. समान वेतन का अधिकार
सबसे महत्वपूर्ण श्रम अधिकारों में से एक है समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (Equal Remuneration Act, 1976) भारत सरकार द्वारा पारित एक कानूनी अधिनियम है, जिसका उद्देश्य पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच समान काम के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समानता सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, चाहे वह किसी भी प्रकार के कार्य में हों। महिला श्रमिकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता है।ईआरए भर्ती और पदोन्नति जैसे रोजगार संबंधी मामलों में लिंग के आधार पर महिलाओं के खिलाफ़ भेदभाव पर भी रोक लगाता है। यह कामकाजी महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में उचित मुआवजे की मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार देता है।
3. कार्यस्थल पर यौन हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (POSH) के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार है। यदि कोई महिला किसी भी प्रकार के यौन हिंसा या उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो वह इस घटना की रिपोर्ट करने का अधिकार रखती है। यदि किसी महिला कर्मचारी को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है और वह समिति उस महिला की शिकायत पर एक्शन लेने के लिए बाध्य है। पॉश अधिनियम के अनुसार, दस या दस से अधिक श्रमिकों वाली किसी भी कंपनी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और संभालने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करना अनिवार्य है।
यदि कोई महिला किसी भी प्रकार के यौन हिंसा या उत्पीड़न का सामना करती हैं, तो वह इस घटना की रिपोर्ट करने का अधिकार रखती है। यदि किसी महिला कर्मचारी को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तो वह कार्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है।
4. घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार
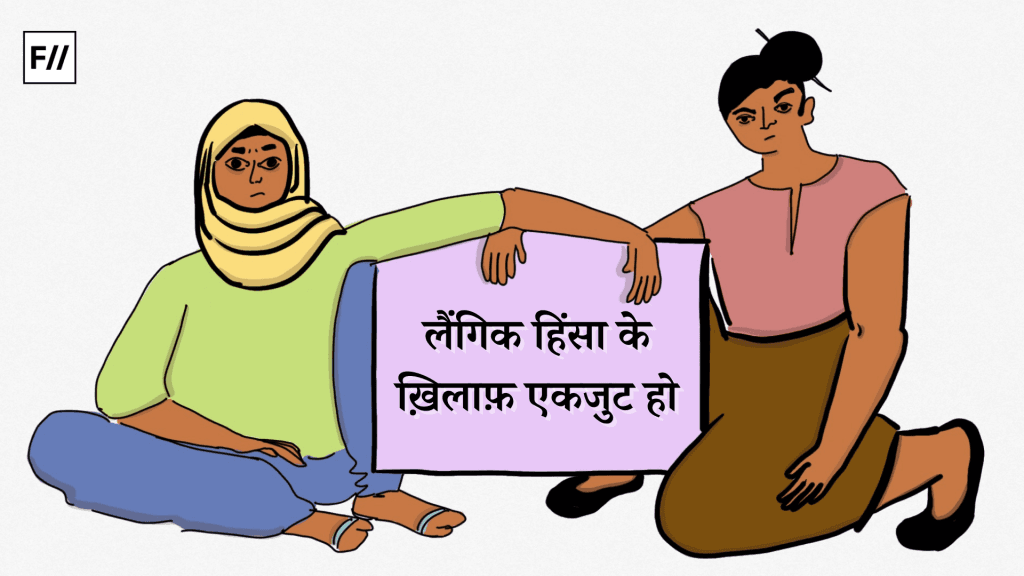
घरेलू हिंसा अधिनियम भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई महिला इस तरह के दुर्व्यवहार और हिंसा का सामना कर रही हैं, तो वह डमेस्टिक व्यालेन्स ऐक्ट (डीवीए) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें बेटी, बहु, पत्नी, बहन आदि शामिल हैं। यह कानून घरेलू दुर्व्यवहार का सामना कर रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह क़ानून सर्वाइवर महिलाओं को साझा घर में रहने का अधिकार भी प्रदान करता है।
5. यौन उत्पीड़न के मामलों में गुमनाम रहने का अधिकार
जो महिलाएं किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं, उन्हें निजता के अधिकार की रक्षा के लिए अकेले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अपना बयान दर्ज कराने का अधिकार है। यह संपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं में गोपनीयता की गारंटी भी देता है, जिससे सर्वाइवर महिला की गोपनीयता बनी रहती है।
जब तक किसी असाधारण मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश न हो, भारत में महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
6. सूर्यास्त के बाद महिलाओं नहीं किया जा सकता गिरफ्तार
जब तक किसी असाधारण मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का आदेश न हो, भारत में महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। साथ ही, किसी महिला से उनके आवास पर केवल महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में पूछताछ करने का अधिकार है।
7. मुफ़्त कानूनी सहायता का अधिकार

जहां कोई महिला अपनी कानूनी सहायता के लिए भुगतान नहीं कर सकती, उस महिला को इसे मुफ़्त प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, इसे एक अधिकार माना जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। एक महिला अपनी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना मुफ्त कानूनी सहायता की हकदार है। एक महिला कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 (सी) के आधार पर मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकती है।
8. संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act) के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी महिलाओं को पति और माता-पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। संपत्ति संबंधी अधिकार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।
जहां कोई महिला अपनी कानूनी सहायता के लिए भुगतान नहीं कर सकती, उस महिला को इसे मुफ़्त प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत, इसे एक अधिकार माना जाता है।
9. महिलाओं का ‘जीरो एफआईआर’ का अधिकार
एक महिला किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी घटना की एफआईआर दर्ज करा सकती है, भले ही घटना का स्थान या विशिष्ट क्षेत्राधिकार उसके अंतर्गत नहीं आता हो। इसे जीरो एफआईआर माना जाता है जिसे बाद में संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे सर्वाइवर को बिना किसी देरी के अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि न्याय मिले। बलात्कार या हत्या जैसे किसी भी अपराध के लिए जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जस्टिस वर्मा समिति ने 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के जवाब में जीरो एफआईआर की अवधारणा पेश की थी।
10. मातृत्व संबंधी अधिकार
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत कामकाजी महिलाओं को प्रसूति अवकाश, वेतन सहित अवकाश और बच्चे की देखभाल के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। महिलाओं को 26 सप्ताह (6 महीने) तक की सवैतनिक मातृत्व अवकाश का अधिकार है। इसमें से 8 सप्ताह की छुट्टी प्रसव से पहले और शेष 18 सप्ताह प्रसव के बाद ली जा सकती है। तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह होती है। 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं और सरोगेसी से माँ बनने वाली महिलाओं को 12 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश मिलता है। साथ ही, ऐसी कंपनियां जहां 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, उन्हें कार्यस्थल पर क्रेच सुविधा प्रदान करनी होती है। हालांकि ये नियम महिलाओं को कार्यबल में आग बढ़ने के बजाय रुकावट का कारण बन जाते हैं लेकिन महिलाएं इन अधिकारों की मांग कर सकती है।