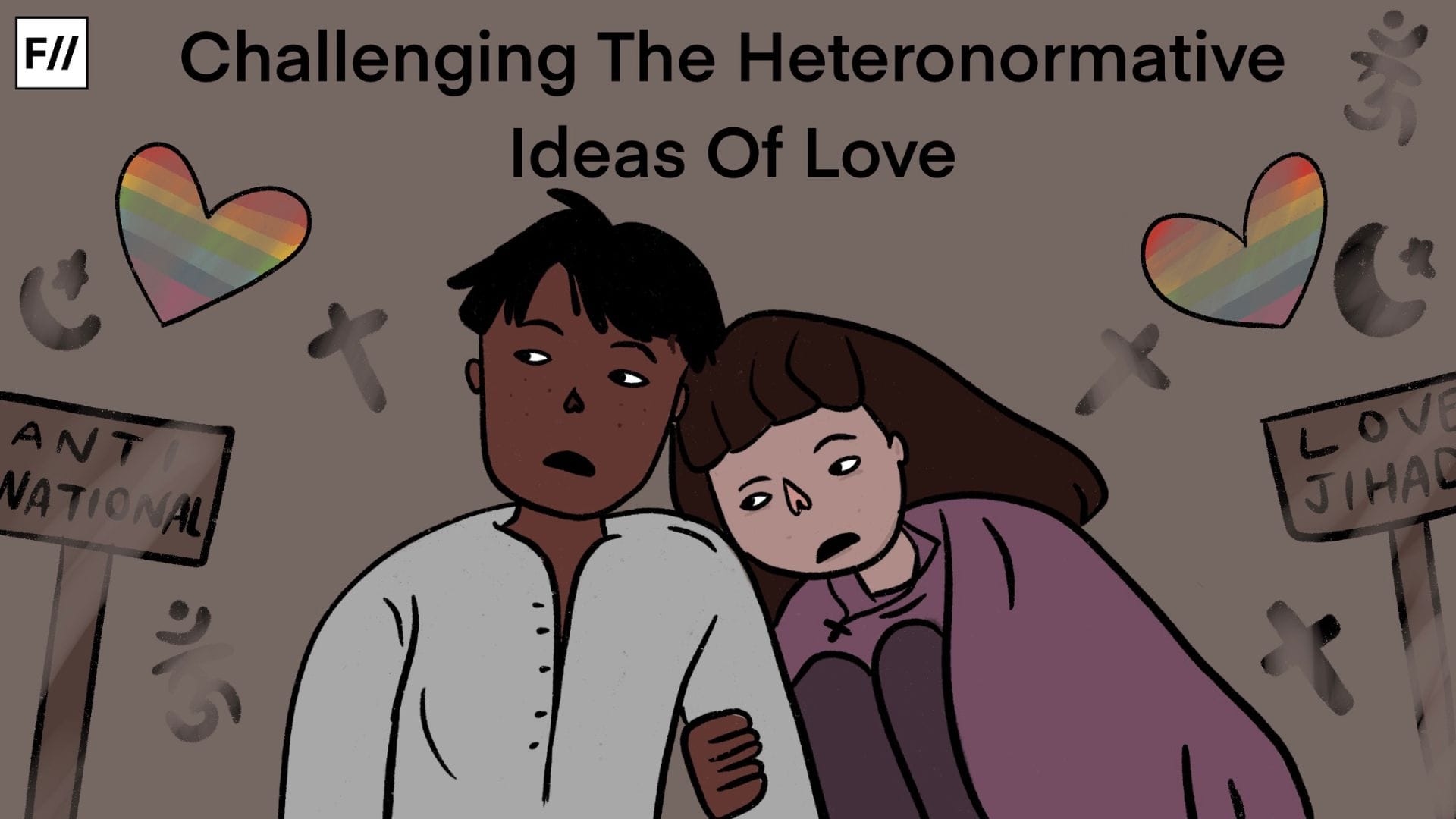हमारे घर और समाज में पाक कला निपुणता की जब भी बात होती है तो बिना विचार किये यह काम महिलाओं के हिस्से वाला माना जाता है। क्या रसोई और पाक का सम्बन्ध सीधा महिलाओं से ही जुड़ता है? बड़े-बड़े होटलों में या फिर छोटे स्टाल पे जहां कहीं बड़े-बड़े आयोजनों की व्यवस्था होती है अधिकतर पुरुष वर्ग काम करते हुए नज़र आते हैं। फिर बाहर रसोई में गर्व से खड़े होने वाले, उसे वहां खड़ा होकर रोजगार कहने वाले, घर की रसोई में वही रोजगार दोहराने में लिंग निर्भरता क्यों बीच में आ जाती है? उस समय खाना बनाने का सारा कार्यभार घर की स्त्रियों पर क्यों डाल दिया जाता है। यहां तक की खुद महिलाएं भी समाज के उसी बने बनाए ढ़ांचे को आकार देती हुई चली जाती हैं। फिल्म ‘की एंड का’ में एक डायलॉग में करीना कपूर अर्जुन कपूर के हाउसवाइफ बनने के विचार पर कहती हैं, “डैडी जैसे आगे बढ़ने का सपना नहीं देखोंगे तो मम्मी जैसे हाउसवाइफ कैसे बन कर बैठोगे?”
अपनी माँ को घर में काम करते देख अर्जुन कपूर ने महसूस किया, जिसकी पीड़ा में वह किया यानी करीना कपूर पर गुस्सा ज़ाहिर करते हुए बोलता हैं, “मेरी माँ घर पर बैठती नहीं थी। घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है जो अपने सपनों की कुर्बानियां देकर बनी होती हैं।” अर्जुन कपूर का यह उत्तर उन सभी स्त्रियों के सम्मान में प्रेरक है जिन्हें घर पर रह कर काम करने को बैठ कर काम करना कहा जाता है और उनकी यह पूरी मेहनत हेयदृष्टि की पात्र बन जाती है। महिलाएं भी अपने जैसा बनने के लिए पहले पुरुषों की तरह बनना चाहती हैं। सोचों पर यह इतना अधिक हावी होता है। समाज का यह कठोर ढांचा जिससे उबर पाने के लिए सोचना भी कठिन साबित होता है।
मेरे दिल्ली आने के बाद से मेरे दोनों भाई रसोई संभालते हैं और घर के वह सब काम करते हैं जो माँ करते हुए आई हैं। जिस तरह पिताजी को सब पुरुषों के बंटे हुए काम को गिनाया करते थे वही उनके साथ भी हुआ। वही बातें गूंजते हुए उनसे भी जा टकराई “घर में काम करने वाले लड़के घर में ही रह जाते हैं, वे कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं।”

रसोई में खड़े होना स्त्रियों का एकाधिकार नहीं है। मैंने बचपन से देखा है मेरे पिता जी को रसोई में माँ की मदद करते हुए। घर या बाहर साफ़-सफाई करते हुए। और इन सबके साथ यह भी देखा है कि कैसे आसपास के पुरुष द्वारा उनका मज़ाक बनाया जाता था। अन्य पुरुष मेरे पिता जी को काम करते देख कर यही कहा करते थे, “यह सब काम औरतों का है उन्हें करने दीजिये, आप बिगाड़ कर रखते हैं, घर की औरतों को। भला पुरुषों को यह सब शोभा देता है।” तो क्या पुरुषों के लिए काम बंटे हुए हैं? या स्त्रियों को इस तरह दोयम दर्जे का समझना ही पुरुषों को शोभा देने वाला काम है?
मैंने अपने घर के माहौल में देखा ही कि मेरे पिता जी रसोई में काम करते हुए कभी हिचक महसूस नहीं करते हैं। उनके विपरीत समाज से उनकी यह सोच उनके बेटों में भी आ गई है। पिताजी के दो बेटों के बाद मैं उनकी अकेली बेटी हूं। उन्होंने कभी मुझ पर रसोई संभालने का भार नहीं डाला। मेरे दिल्ली आने के बाद से मेरे दोनों भाई रसोई संभालते हैं और घर के वह सब काम करते हैं जो माँ करते हुए आई हैं। जिस तरह पिताजी को सब पुरुषों के बंटे हुए काम को गिनाया करते थे वही उनके साथ भी हुआ। वही बातें गूंजते हुए उनसे भी जा टकराई “घर में काम करने वाले लड़के घर में ही रह जाते हैं, वे कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं।”
घर के अंदर काम करने वाली स्त्रियों के लिए क्यों नहीं घर पर ही काम करते रहने के लिए या फिर रसोई में खड़े होकर भोजन तैयार करते ही रहने पर बातें सुनाई जाती हैं? यदि रसोई में भोजन की सारी ज़िम्मेदारी स्त्रियों के ऊपर ही सौंप दी जाती है तो उसे रोजगार क्यों नहीं कहा जायेगा? यदि वह रोजगार नहीं है तो रसोई संभालने वाली वे स्त्रियां बेरोजगार क्यों नहीं कही जाती हैं? क्या उन्हें यह अधिकार नहीं कि वह भी रोजगार पर जाए? बिना किसी टाइम टेबल, हर वक्त आवश्यकता के मुताबिक़ काम करने वाली महिलाओं के रसोई के काम को काम ही नहीं माना जाता है। मेहनत को नज़रंदाज़ तो किया ही जाता है साथ ही साथ भोजन में कमी पाये जाने पर महिलाओं को हिंसा तक का सामना करना पड़ता है।

मार्क्सवादी नारीवाद में लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ हो रहे असमान व्यवहार को पूंजीवाद से जोड़ते हुए लिखा गया है। येन फोरमैन जैसे मार्क्सवादी नारीवादी मानते हैं कि एक महिला का दृष्टिकोण उसके परिवार के व उसके दोस्तों के सराहने पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। वे महिलाएं अपने आपको श्रमिक वर्ग की भांति देखने लग जाती हैं। अतः वह अपने घर के कामों को उत्पादक के रूप में देखने लग जाती हैं। अतः उन महिलाओं को तब तक पुरुष वर्ग खंडित देखता रहेगा जब तक महिलायें पूँजी पर अपनी निर्भरता हासिल नहीं कर लेती हैं। तब जाकर वह रसोई और रसोई के बाद के हिंसात्मक कृत्यों से छुटकारा पा सकती हैं।
रसोई में खड़े होना स्त्रियों का एकाधिकार नहीं है। मैंने बचपन से देखा है मेरे पिता जी को रसोई में माँ की मदद करते हुए। घर या बाहर साफ़-सफाई करते हुए। और इन सबके साथ यह भी देखा है कि कैसे आसपास के पुरुष द्वारा उनका मज़ाक बनाया जाता था।
भारतीय समाज में लैंगिक असमानता का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था हैं। पितृसत्ता के अनुसार महिलाओं की जगह घर और वहां भी रसोई तक सीमित है। एक स्त्री को तभी संपूर्ण माना जाता है तब वह रसोई के कामों में कुशल होती है। इतना ही नहीं रसोई के काम को काम नहीं जिम्मेदारी माना जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्बे के अनुसार, “पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता हैं और उसका शोषण करता हैं।” महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे समाज में संस्कृति और रीति-रिवाजों के तौर पर हर वर्ग, धर्म में है।
हैरानी की बात तो ये है जिनके घर महिलाओं की संख्या कम होती है या परिवार में एक माँ होती है उनके घर पर बहुत सामान्य हो जाता है रसोई में पुरुषों को काम करते पाया जाना। जैसे-जैसे उन परिवारों में महिलाओं की संख्या बढती है उन पुरुषों के पैरों में रसोई तक पहुँच पाने में जंग लगती हुई नज़र आने लगती है। उस समय क्या चीज़ है जो रोकती है उन्हें वह सब करने से? समाज या उनके भीतर कहीं न कहीं दबी हुई पितृसत्ता? जो भी हो जब तक पुरुष अपने भीतर बैठे उस सत्ता को नहीं मार देगा वह हमेशा रसोई और ऑफिस के काम को लिंग के आधार पर ही देखता जायेगा।