भारतीय सिनेमा को अक्सर समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन यह समाज की सामूहिक कल्पना को भी आकार देता है। फ़िल्में और टीवी धारावाहिक जिस तरह सामाजिक वास्तविकताओं को दिखाते हैं, उनका असर लोगों की सोच और व्यवहार पर पड़ता है। ये कहानियां कई बार समाज में मौजूद अन्याय और भेदभाव को सामान्य बना देती हैं और सांस्कृतिक मानदंड तय करती हैं। इसी क्रम में घरेलू हिंसा का चित्रण सिनेमा में एक अहम विषय रहा है। घरेलू हिंसा, जो लैंगिक हिंसा का सबसे व्यापक और गहराई से जड़ें जमाए रूप है, अक्सर फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण कई गंभीर सवाल खड़े करता है। लोकप्रिय सिनेमा और टीवी शो आम तौर पर हिंसा को सिर्फ शारीरिक मारपीट या थप्पड़ जैसी घटनाओं तक सीमित कर देते हैं।
जबकि आर्थिक नियंत्रण, भावनात्मक उत्पीड़न या महिला को अहम फैसलों से बाहर रखना भी हिंसा के ही रूप हैं, जिन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इस तरह के सीमित चित्रण से लोगों की समझ अधूरी रह जाती है और यह भ्रम फैलता है कि केवल दिखाई देने वाली शारीरिक चोटें ही हिंसा हैं। भारतीय सिनेमा में एक साफ़ पैटर्न दिखाई देता है। महिलाओं की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को हमेशा दो चरम सीमाओं पर दिखाया जाता है। एक तरफ़ ऐसी कहानियां होती हैं जहां महिलाएं हिंसा और अत्याचार को चुपचाप सहती रहती हैं, जैसे यह उनका कर्तव्य या त्याग हो। यह सोच पितृसत्ता की उस उम्मीद को मज़बूत करती है कि स्त्री हमेशा सहनशील और धैर्यवान होनी चाहिए।
दूसरी तरफ़ कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जहां नायिका अचानक सब कुछ छोड़कर विद्रोह करती है। वह विवाह, परिवार और समाज की बंदिशों से आज़ाद हो जाती है। इन दोनों छोरों मौन सहनशीलता और विद्रोह के बीच की असल सच्चाई सिनेमा में बहुत कम दिखाई देती है। हक़ीक़त यह है कि ज़्यादातर महिलाएं, चाहे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही क्यों न हों, हिंसक या असुरक्षित घरों को छोड़ नहीं पातीं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कभी समाज का डर, चरित्र पर सवाल उठाने वाला कलंक, सुरक्षित ठिकाने की कमी, आर्थिक अस्थिरता और लंबे कानूनी झंझट।
हक़ीक़त यह है कि ज़्यादातर महिलाएं, चाहे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही क्यों न हों, हिंसक या असुरक्षित घरों को छोड़ नहीं पातीं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। कभी समाज का डर, चरित्र पर सवाल उठाने वाला कलंक, सुरक्षित ठिकाने की कमी, आर्थिक अस्थिरता और लंबे कानूनी झंझट।
क्या सिनेमा वास्तविक बाधाओं को दिखाता है
सिनेमा इन गहरी और वास्तविक बाधाओं को शायद ही कभी दिखाता है। महिलाओं के रोज़मर्रा के संघर्ष, छोटे-छोटे समझौते और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की रणनीतियां पर्दे से गायब रहती हैं। इस जटिलता के मिट जाने से दर्शकों के सामने जीवन की एक आसान और अवास्तविक तस्वीर ही रह जाती है। टीवी धारावाहिक, जो हर दिन हमारे घरों तक पहुंचते हैं, समाज की एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। ये धारावाहिक अक्सर भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को एक सामान्य पारिवारिक जीवन का हिस्सा दिखाते हैं, न कि हिंसा के रूप में। उदाहरण के तौर पर, लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा में नायिका के सालों तक किए गए निशुल्क घरेलू श्रम, आर्थिक निर्णयों से उसके बहिष्कार और पति के लगातार किए गए अपमान को शुरुआत में एक सामान्य वैवाहिक जीवन की तरह दिखाया गया है। नायिका का दुख तब ही स्वीकार किया जाता है जब पति की बेवफाई सार्वजनिक रूप से सामने आती है। लेकिन लंबे समय तक चली आर्थिक निर्भरता, निर्णयों से बाहर रखा जाना और गरिमा से वंचित रहना कभी भी हिंसा के रूप में नहीं देखा जाता।
इसी तरह, बालिका वधू जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले धारावाहिक में भी महिलाओं का अपमान, भावनात्मक दबाव और आर्थिक नियंत्रण बार-बार दिखाया गया है। फिर भी इसे घरेलू हिंसा नहीं, बल्कि पारिवारिक ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह समझ अब भी आम नहीं है कि किसी महिला की तनख्वाह पर नियंत्रण रखना, उसकी जरूरतों के लिए पैसे रोकना या घर के फैसलों से उसे बाहर रखना भी हिंसा के रूप हैं। भावनात्मक उत्पीड़न जैसे गैसलाइटिंग, अपमान या अलगाव को भी अक्सर ‘पारिवारिक तनाव’ कहकर उसकी लैंगिक और सामाजिक जड़ों को छिपा दिया जाता है। इसीलिए जब केवल शारीरिक हमले को सच्ची हिंसा माना जाता है तो टीवी, समाज में पीड़ा का एक ख़तरनाक क्रम रचता है जहां न दिखने वाले हिंसा को हम आम तौर पर भूल जाते हैं।
ये धारावाहिक अक्सर भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को एक सामान्य पारिवारिक जीवन का हिस्सा दिखाते हैं, न कि हिंसा के रूप में। लोकप्रिय धारावाहिक अनुपमा में नायिका के सालों तक किए गए निशुल्क घरेलू श्रम, आर्थिक निर्णयों से उसके बहिष्कार और पति के लगातार किए गए अपमान को शुरुआत में एक सामान्य वैवाहिक जीवन की तरह दिखाया गया है।
क्या घरेलू हिंसा की सच्चाई दिखा रही है सिनेमा
फ़िल्मों में जब घरेलू हिंसा दिखाई जाती है, तो उसे अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। कई बार पत्नी को थप्पड़ मारने या चुप कराने का दृश्य अचानक किसी नाटकीय मोड़ की तरह दिखाया जाता है। इसका उद्देश्य दर्शकों की सहानुभूति पाना होता है, लेकिन यह कभी आलोचनात्मक नहीं बन पाता। कुछ फ़िल्मों में तो ऐसे दृश्य हास्य या रोमांस का हिस्सा बना दिए जाते हैं, मानो पति का वर्चस्व वैवाहिक जीवन का सामान्य हिस्सा हो। जब भारतीय सिनेमा एक ‘सशक्त स्त्री‘ दिखाने की कोशिश करता है, तो अक्सर उसे एक कैरिकेचर बना देता है। आधुनिक महिला को ज़्यादातर शराब पीते, क्लब जाते, कई पुरुषों से डेट करते या यौन रूप से स्वतंत्र दिखाया जाता है।
यह समझना ज़रूरी है कि यौन स्वतंत्रता अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन सिनेमा में सशक्तिकरण को केवल इसी तक सीमित कर देना समस्या है। इसमें आर्थिक स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता या किसी के ज़बरन नियंत्रण से मुक्ति जैसी असली आज़ादी को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इस तरह, सिनेमा में महिलाओं की छवि दो अतियों में बंटी नज़र आती है। एक तरफ़ दुख सहती गृहिणी और दूसरी तरफ़ अति-पाश्चात्य आधुनिक महिला। इन दोनों के बीच भारतीय महिलाओं की असली, जटिल और रोज़मर्रा के संघर्षों से जुड़ी एजेंसी के लिए कोई जगह नहीं बचती। उनका सच्चा सशक्तिकरण, जो छोटे-छोटे निर्णयों और जीवन के व्यावहारिक संघर्षों में झलकता है, पर्दे पर अक्सर गायब रहता है।
कुछ फ़िल्मों में तो ऐसे दृश्य हास्य या रोमांस का हिस्सा बना दिए जाते हैं, मानो पति का वर्चस्व वैवाहिक जीवन का सामान्य हिस्सा हो। जब भारतीय सिनेमा एक ‘सशक्त स्त्री’ दिखाने की कोशिश करता है, तो अक्सर उसे एक कैरिकेचर बना देता है।
यहां तक कि जब फ़िल्में महिलाओं की पेशेवर उपलब्धियों का जश्न मनाती हैं, तब भी वे उन्हें घरेलू भूमिकाओं में सीमित कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर, मिशन मंगल (2019) में मंगल अभियान पर काम करने वाली महिला वैज्ञानिकों को बार-बार घर के काम करते, खाना बनाते या पारिवारिक झगड़े सुलझाते दिखाया गया। यह दिखाने का तरीका उस पुराने विचार को मजबूत करता है कि महिला की असली पहचान उसके गृहिणी होने से जुड़ी है, और उसका पेशेवर जीवन उसके बाद आता है। फ़िल्म पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं को आने वाली चुनौतियों पर बात करने के बजाय यह संदेश देती है कि ‘दोनों ज़िम्मेदारियां निभा लेना’ ही सशक्तिकरण है। इस तरह, महिलाओं के पेशेवर संघर्षों को भी घरेलू दायरे में समेट दिया जाता है।
क्या सिनेमा दिखाती है न्यायायिक प्रक्रिया की सच्चाई
सिनेमा और टीवी की एक और बड़ी कमी यह है कि वे घरेलू हिंसा की वास्तविक और ज़मीनी सच्चाइयों को नहीं दिखाते। जो महिलाएं न्याय की तलाश करती हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया बेहद मुश्किल और थकाऊ होती है। पुलिस अक्सर ऐसी शिकायतों को ‘परिवार का मामला’ कहकर नज़रअंदाज़ कर देती है, मुकदमे वर्षों तक चलते रहते हैं और सुरक्षित आश्रयों की संख्या बहुत कम होती है। ये बाधाएं महिलाओं को हिंसक माहौल छोड़ने से रोकती हैं, लेकिन पर्दे पर यह मुश्किलें शायद ही कभी दिखाई देती हैं। फ़िल्में अक्सर हिंसा को पति-पत्नी के निजी झगड़े के रूप में दिखाती हैं, जबकि असल में यह पूरे समाज, परिवार और राज्य की पितृसत्तात्मक सोच से जुड़ी समस्या है। जब हिंसा को केवल निजी विवाद के रूप में पेश किया जाता है, तो उसका सामाजिक और तंत्रगत स्वरूप अदृश्य हो जाता है। इससे आम जनता को यह लगता है कि हिंसक घर केवल ‘बुरे पुरुषों’ की वजह से हैं, जबकि असल कारण गहराई से जड़ें जमाई पितृसत्ता है।
मिशन मंगल (2019) में मंगल अभियान पर काम करने वाली महिला वैज्ञानिकों को बार-बार घर के काम करते, खाना बनाते या पारिवारिक झगड़े सुलझाते दिखाया गया। यह दिखाने का तरीका उस पुराने विचार को मजबूत करता है कि महिला की असली पहचान उसके गृहिणी होने से जुड़ी है, और उसका पेशेवर जीवन उसके बाद आता है।
भारतीय सिनेमा और टीवी में घरेलू हिंसा का चित्रण आज भी अधूरा और सीमित है। फिल्मों और धारावाहिकों में हिंसा को अक्सर केवल शारीरिक हमलों तक ही सीमित दिखाया जाता है, जबकि भावनात्मक और आर्थिक उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। कई कहानियां स्त्रियों के संघर्षों को गंभीरता से नहीं लेतीं, बल्कि उन्हें सहनशीलता या नाटकीय पलायन तक सीमित कर देती हैं। इससे पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देने के बजाय, वही पुराने मानदंड और मज़बूत हो जाते हैं। असलियत यह है कि घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि नियंत्रण, अपमान और भावनात्मक हिंसा के जरिए भी होती है। लेकिन लोकप्रिय कथाओं में इन जटिल सच्चाइयों को जगह नहीं मिलती। महिलाओं की रोज़मर्रा की रणनीतियां जैसे समझौता, बातचीत, या हिंसा से बचने की कोशिश इन कहानियों से गायब रहती हैं।
नारीवादी आलोचना की चुनौती है कि बेहतर कहानी कहने की मांग की जाए। ऐसी कहानियां जो अदृश्य हिंसा को पहचानें, सामाजिक और आर्थिक ढांचों में छिपी हिंसा को सामने लाएं और महिलाओं के सशक्तिकरण को सिर्फ़ सतही दिखावे के रूप में न पेश करें। सिनेमा और टीवी के पास समाज को बदलने की अपार शक्ति है। वे केवल समाज का आईना ही नहीं, उसकी कल्पना को नया रूप भी दे सकते हैं। लेकिन जब तक वे आर्थिक नियंत्रण, भावनात्मक अत्याचार और संस्थागत उपेक्षा को भी हिंसा के रूप में नहीं दिखाएंगे, तब तक उनका आईना अधूरा रहेगा, जो सिर्फ़ महिलाओं की सच्चाइयों के कुछ टुकड़े दिखाएगा, और उनके सबसे गहरे घावों को अंधेरे में छोड़ देगा।
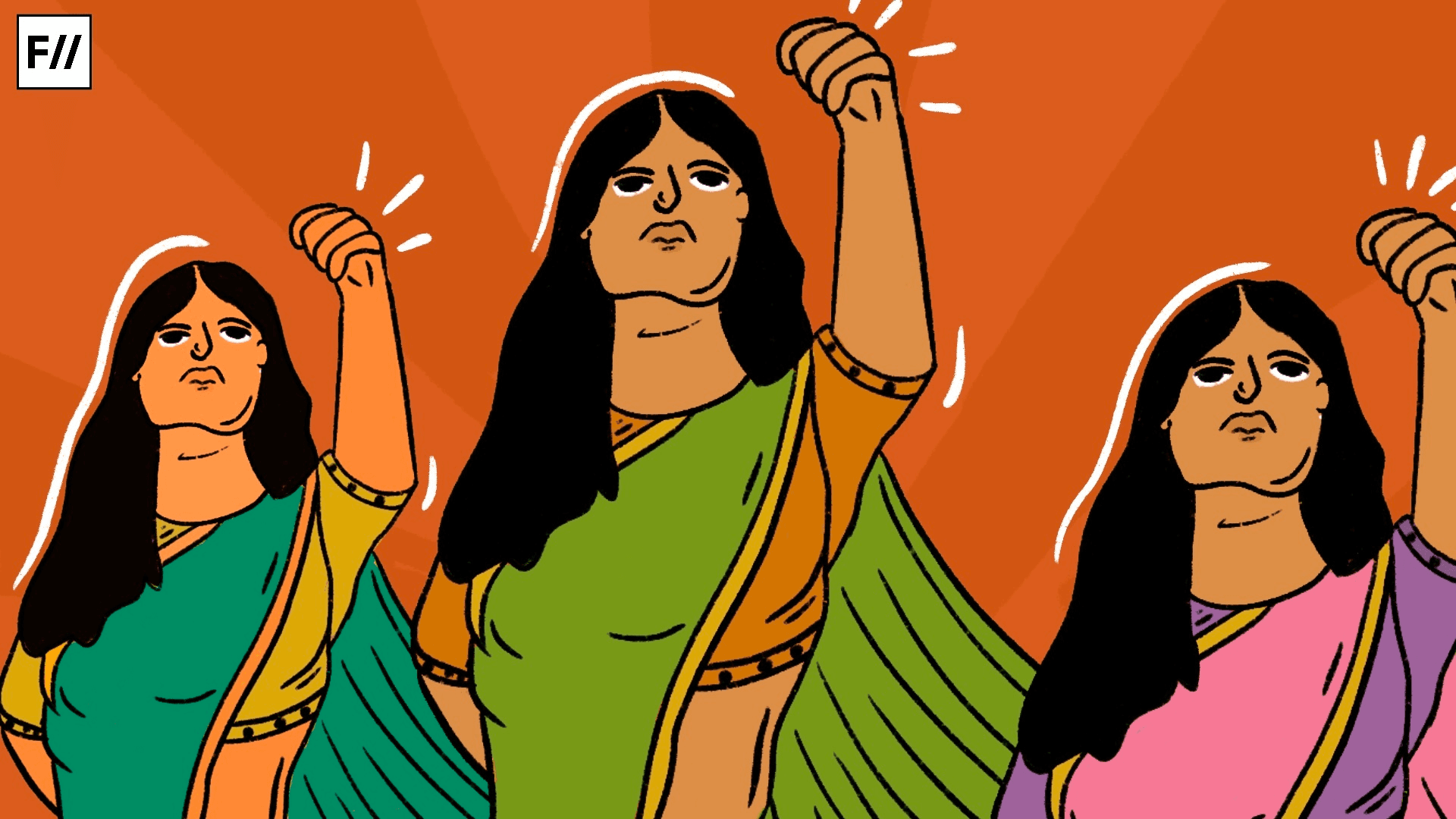




I always like to mention how Pakistani TV is centuries a head of ours because it shows actual problems, violence of their society across all classes in their shows. They don’t shy away from that reality but create relevant and important drama aroud it for the audience. By violence, I don’t just mean physical or verbal violence, But also the familial hierarchy, the patriarchal setups, The good and bad intentions of people around you exploiting the power etc.
Those shows are a century ahead of our crass unrealistic caricature-ish saas-bahu and ameer ladka- gareed ladki (or vice versa) setup.