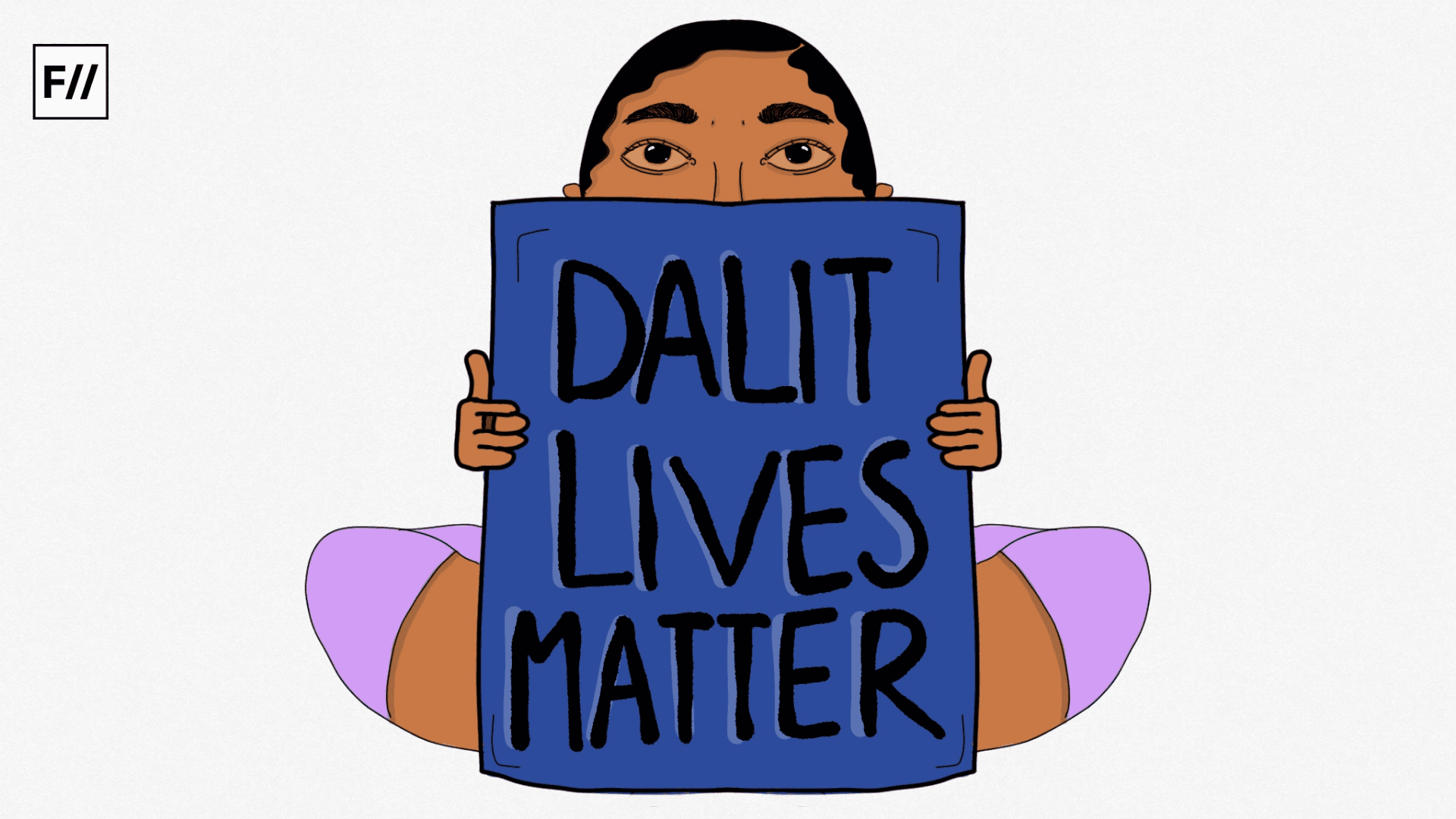जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो वह सिर्फ किसी परिवार में नहीं, बल्कि एक जाति, धर्म और समाज में जन्म लेता है। उसकी परवरिश उसी समाज की रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार होती है। आगे चलकर यही परवरिश उसके जीवन और सोच को आकार देती है। जाति की जड़ें बहुत पुरानी हैं और यह हमारे समाज की सच्चाई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अब जाति खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि जाति हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से मौजूद है। किसी के लिए यह गर्व का कारण बन जाती है, तो किसी के लिए सामाजिक उपेक्षा का। हमारी सामाजिक परवरिश हमें जाति का एहसास कराती है। जब लोग हमें किसी जाति विशेष से आने के कारण सम्मान देते हैं या फिर बहिष्कार करते हैं। जाति सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति की पहचान तय कर देती है। आज भी समाज में लोग जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। कहा तो जाता है कि अब जाति आधारित भेदभाव खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी सोच अब भी हमारी परवरिश और मानसिकता का हिस्सा बनी हुई है।
मेरी जाति का बोध मुझे कैसे कराया गया
मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव से आती हूं। मेरा जन्म एक सवर्ण जाति में हुआ, जिसे समाज में कथित तौर पर उच्च जाति माना जाता है। हमारे गांव में ज़्यादातर सवर्ण परिवार रहते थे, लेकिन जातिगत भेदभाव वहां आम बात है। मुझे घर और गांव के लोगों ने बताया था कि कुछ लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। उनके हाथ का खाना नहीं खाना है क्योंकि वे कथित तौर पर निम्न जाति यानी ‘अछूत’ हैं। धीरे-धीरे यह सोच मेरे मन में घर करने लगी। मुझे सिखाया गया कि हम उनसे अलग हैं। इसका असर यह हुआ कि मैं अपनी जाति के झूठे गौरव में बंधने लगी। गांव के माहौल में जातिगत भेदभाव एक कड़वा सच है, जो लगभग हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद होता है।
यह ‘इज्जत’ और ‘प्रतिष्ठा’ का ऐसा विषय बन जाता है, जो हमें अपने सीमित दायरों में कैद कर देता है। मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब हम सब बच्चे साथ बैठते थे, लेकिन खाना एक-दूसरे के साथ नहीं बांटते थे। जब कोई पूछता तो हम कहते कि ‘घर से मना किया है।’ धीरे-धीरे यह बात हमें स्वाभाविक लगने लगी। हम बिना सवाल किए वही करने लगे जो हमारे बड़े करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि यही समाज में रहने का नियम है। इस तरह बचपन में ही मैंने जाति को समझा। ये एक तरह से मेरे जीने का तरीका बन गया था।
मुझे याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब हम सब बच्चे साथ बैठते थे, लेकिन खाना एक-दूसरे के साथ नहीं बांटते थे। जब कोई पूछता तो हम कहते कि ‘घर से मना किया है।’ धीरे-धीरे यह बात हमें स्वाभाविक लगने लगी। हम बिना सवाल किए वही करने लगे जो हमारे बड़े करते थे, क्योंकि हमें लगता था कि यही समाज में रहने का नियम है।
आगे का जीवन: स्कूल बदला, पर जाति नहीं
पांचवीं कक्षा के बाद मेरा स्कूल बदल गया और मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने लगी। वहां हमें दोपहर में मिड-डे मील योजना के तहत खाना मिलता था। उस स्कूल में सभी बच्चे, चाहे किसी भी जाति के हों, एक साथ बैठकर खाते थे। वहां जातिगत भेदभाव जैसी कोई बात नहीं थी। घर वाले भी कहते, “बच्चे हैं, खा सकते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता।” स्कूल में हम साथ पढ़ते, साथ खेलते और सब एक जैसे थे। वहां न तो किसी उच्च जाति को कोई विशेष अधिकार था, न किसी को नीची नजर से देखा जाता था। यह शिक्षा की शक्ति थी, जहां सभी बच्चों को बराबर समझा जाता था और हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलता था। स्कूल में वह “जाति का चश्मा” जैसे गायब हो जाता था, जो समाज में हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन जाति हमारे मन में मौजूद थी—वह हमें बताती थी कि हमें किन सीमाओं से आगे नहीं बढ़ना है।
सामाजिक विज्ञान की कक्षा, जहां पहली बार जाति को समझा
मेरे जीवन में सामाजिक विज्ञान की वह कक्षा बहुत खास रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई विषय इतना रोचक भी हो सकता है। उस कक्षा में समाज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हमारे गांव और हमारे जीवन का हिस्सा था। हमारे सर हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। वे हमेशा कोशिश करते कि किताबों की बातें वास्तविक जीवन से जोड़ी जाएं। वे हमें अपने अनुभव लिखने या किसी व्यक्ति की कहानी बताने के लिए कहते। उनके इस तरीके ने मेरे अंदर की बहुत सी पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया, जो समाज के साथ-साथ मेरे भीतर भी बनी हुई थीं। सर चाहते थे कि बच्चे बिना डर के अपनी बात कहें और सीखें। उनका यह व्यवहार देखकर मुझे लगा कि शिक्षक ऐसा भी हो सकता है।
वहां हमें दोपहर में मिड-डे मील योजना के तहत खाना मिलता था। उस स्कूल में सभी बच्चे, चाहे किसी भी जाति के हों, एक साथ बैठकर खाते थे। वहां जातिगत भेदभाव जैसी कोई बात नहीं थी। घर वाले भी कहते, “बच्चे हैं, खा सकते हैं, इन्हें कुछ नहीं होता।”
यह मेरे जीवन का वह दौर था जब मैं खुद से लड़ रही थी। जाति के विशेषाधिकारों को समझ रही थी। मेरी सोच बदल रही थी। मैंने महसूस किया कि जाति सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जो हर जगह फैली हुई है। जो बात मेरे लिए सामान्य थी, वही किसी और के लिए एक दर्दनाक अनुभव थी। धीरे-धीरे जाति की परतें मेरे सामने खुलने लगीं। मैंने ठान लिया कि अपने स्तर पर हमेशा समान व्यवहार की कोशिश करूंगी। इस सोच ने मुझे जाति को नए नजरिए से देखने की ताकत दी।
मेरी दोस्त एकता दलित समाज से है। वह बताती थी कि कैसे लोग उसकी जाति देखकर उसे परखते हैं और भेदभाव करते हैं। मुझे भी उसकी दोस्ती को लेकर कई बार ताने सुनने पड़े, पर मेरे लिए उसकी जाति से ज़्यादा उसकी सच्चाई और दोस्ती मायने रखती है। कॉलेज में कमरा ढूंढना हमारे लिए मुश्किल था। मकान मालिक नाम पूछते ही जाति पहचान लेते और कहते “हम इस जाति के लोगों को कमरा नहीं देते।” गांव में भी लोग मुझे अलग नजर से देखते हैं क्योंकि मेरी दोस्त दलित है। बच्चे भी जातिसूचक शब्द बोलते हैं। यह दिखाता है कि समाज ने उन्हें झूठी ऊंच-नीच की भावना सिखा दी है। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं आम हैं। अल्मोड़ा में एक दलित युवक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने सवर्ण लड़की से शादी की थी। जब तक समाज इंसान को उसकी जाति से नहीं, इंसानियत से पहचानना नहीं सीखेगा, तब तक बराबरी का सपना अधूरा रहेगा।
जाति और महिलाओं की स्थिति
मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि उच्च जाति में पैदा हुई महिलाओं पर घर और परिवार की इज़्ज़त बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा डाली जाती है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, और कहां चुप रहना है। समाज और पुरुषों के सामने कम बोलना, कम दिखना और हमेशा संस्कारी बने रहना, उनसे यही उम्मीद की जाती है। ऐसी महिलाएं अपने घर और परिवार की मर्यादा से बंधी होती हैं। उन्हें खुलकर जीने या अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं दी जाती। जब मैं घर से बाहर निकलती हूं, तो अक्सर मुझे अपनी जाति का मान रखने और पिता की इज़्ज़त का ध्यान रखने की हिदायत दी जाती है। यह भावनात्मक रूप से बहुत नियंत्रित करने वाला अनुभव होता है। यह भी एक तरह का शोषण है, जो तब और बढ़ जाता है जब कोई स्त्री तय सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करती है। समाज ऐसे विद्रोह को स्वीकार नहीं करता और उसे बहिष्कार या उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। गाँव या कस्बों में यह दबाव और भी गहरा होता है, क्योंकि वहां हर कोई एक-दूसरे को जानता है। जब मैं अपनी किसी दोस्त के गाँव या उसके रिश्तेदारों के घर जाती हूं, तो मन में डर रहता है कि कहीं कोई यह बात मेरे घर तक न पहुंचा दे। न चाहते हुए भी जाति का डर मन में हमेशा बना रहता है।
मेरी दोस्त एकता दलित समाज से है। वह बताती थी कि कैसे लोग उसकी जाति देखकर उसे परखते हैं और भेदभाव करते हैं। मुझे भी उसकी दोस्ती को लेकर कई बार ताने सुनने पड़े, पर मेरे लिए उसकी जाति से ज़्यादा उसकी सच्चाई और दोस्ती मायने रखती है।
किताबों से मिली जातिवाद की परतों की समझ
बाबासाहब आंबेडकर की जीवनी और ओमप्रकाश वाल्मीकि की किताब ‘झूठन’ ने मुझे जाति के सवालों को गहराई से समझने में मदद की। झूठन पढ़ते समय मैं भीतर तक हिल गई थी। ओमप्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों में जो पीड़ा और तिरस्कार था, वह आज भी हमारे समाज में मौजूद है। जाति इंसानियत पर एक गहरा धब्बा है, जिसकी जकड़ में हम सभी किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। आज ज़रूरत है कि हम इस व्यवस्था के पीछे छिपे कड़वे सच को समझें। जाति हमारे समाज में इतनी गहराई से पैठ चुकी है कि शिक्षा भी इसे हमारे दिमाग से मिटा नहीं पा रही। यह व्यवस्था इतनी क्रूर है कि लोगों से उनका सम्मान और कभी-कभी जीवन का अधिकार तक छीन लेती है। जाति का यह ढांचा इंसान की सोचने और समझने की क्षमता को धीरे-धीरे खत्म कर देता है। हमें इसे पहचानने और इसके खिलाफ संवेदनशीलता से लड़ने की ज़रूरत है।
मुझे हमेशा यह महसूस होता है कि उच्च जाति में पैदा हुई महिलाओं पर घर और परिवार की इज़्ज़त बनाए रखने की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा डाली जाती है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, और कहां चुप रहना है। समाज और पुरुषों के सामने कम बोलना, कम दिखना और हमेशा संस्कारी बने रहना, उनसे यही उम्मीद की जाती है।
जाति से लड़ने का सबसे सशक्त हथियार शिक्षा है। शिक्षा न केवल व्यक्ति का विकास करती है, बल्कि उसे सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ़ आवाज उठाने की हिम्मत भी देती है। जाति एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है, जिसे समझने और चुनौती देने की जरूरत है। जब हम किसी अन्याय को पहचानने लगते हैं, तभी वह हमें खटकता है। कानूनी ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर दो लोग आपसी सहमति से प्रेम करना चाहें, तो उनकी जान न ली जाए। बदलाव धीरे-धीरे जरूर आया है, लेकिन यह बदलाव सवर्ण जातियों की मनमानी पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में सफल रहा है चाहे वह कानून के डर से ही क्यों न हो। दलित छात्रों ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। उन्हें इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही वह रास्ता है, जो समाज को बराबरी और इंसाफ की दिशा में आगे बढ़ा सकती है।