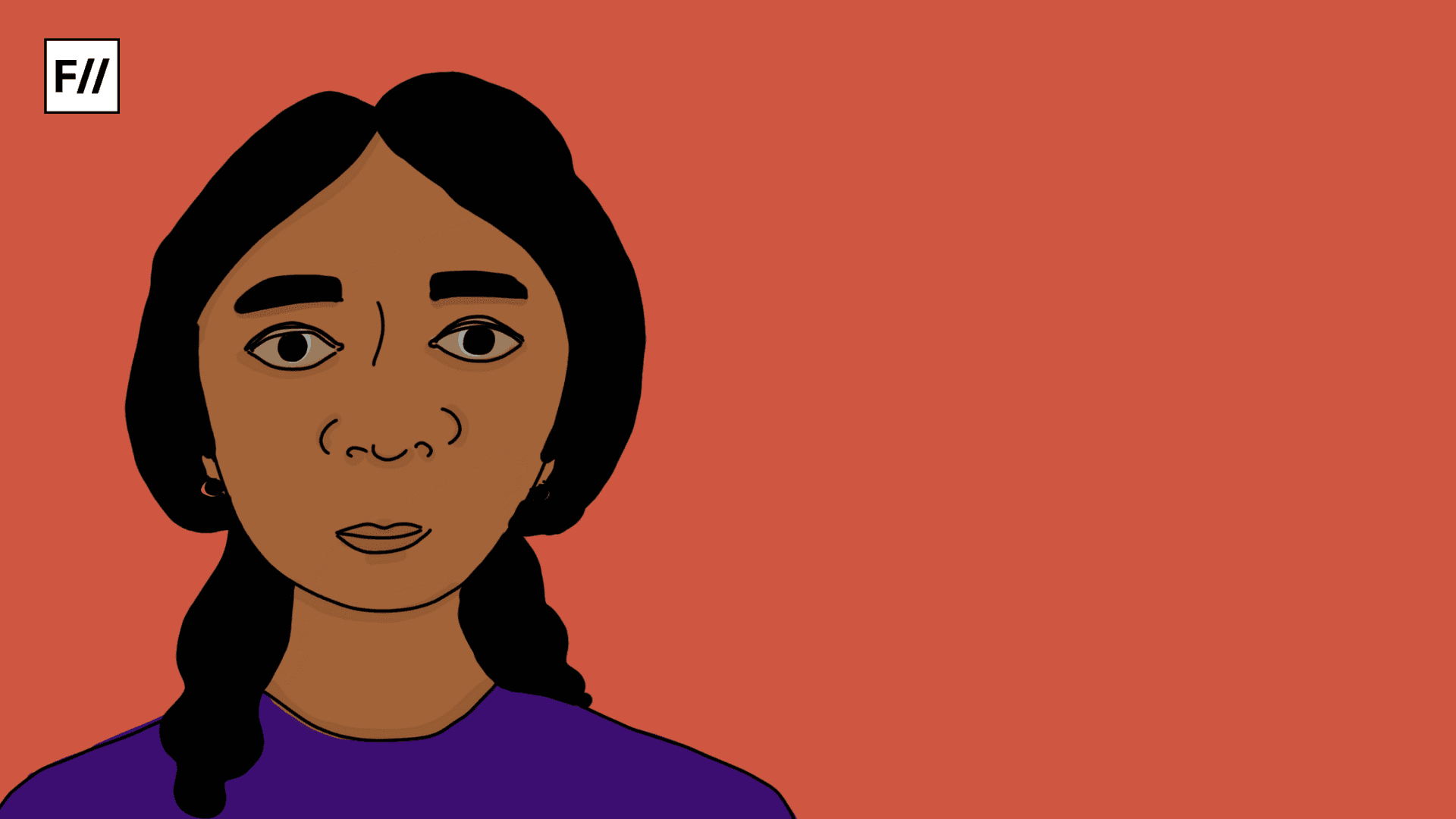किसी भी समाज और परिवार में बेटी होना हमेशा एक सामान्य अनुभव नहीं होता। इसके साथ पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक अपेक्षाओं की एक लंबी सूची जुड़ी होती है। बचपन से ही लड़कियों को घर और परिवार में सिखाया जाता है कि वे समझदार बनें, कम बोलें, धीरे बोलें, तेज़ न हँसें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। लेकिन, इन सबके साथ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो एक लड़की को बहुत छोटी उम्र से सौंप दी जाती है, वह है परिवार की ‘इज़्ज़त’ बनाए रखना। इस ज़िम्मेदारी को निभाने के बदले समाज और परिवार उसे ‘अच्छी बेटी’ की पहचान देते हैं। लेकिन, यह पहचान अपने साथ और भी अपेक्षाएँ लेकर आती है। एक अच्छी बेटी से उम्मीद की जाती है कि वह कभी ना न कहे, हर पारिवारिक मूल्य को अपनाए और अपनी खुशी, इच्छाओं और जीवन के लक्ष्यों को हमेशा परिवार से नीचे रखे। इसी दबाव के कारण कई लड़कियां और महिलाएं अपने सपनों और आकांक्षाओं को दबा देती हैं।
वे ऐसा इसलिए करती हैं ताकि परिवार की उम्मीदों पर खरी उतर सकें और समाज में ‘अच्छी बेटी’ की छवि बनाए रख सकें। साउथ एशियन थेरपिस्ट्स कलेक्टिव में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जब लड़कियों को लगातार शांत, आज्ञाकारी, सहनशील और ज़िम्मेदार बनने की सीख दी जाती है, तो इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इससे महिलाओं में चिंता, परफ़ेक्शनिज़्म और भावनात्मक थकावट बढ़ती है। धीरे-धीरे यह दबाव उनकी भावनात्मक आज़ादी और व्यक्तिगत इच्छाओं को सीमित करने लगता है। वहीं बरैन्ज़ मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं द्वारा अपनी खुशी और ज़रूरतों को लगातार दूसरों के लिए दबाना ‘गुड डॉटर सिंड्रोम’ का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। इस स्थिति में महिलाएं हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पहले रखती हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ करती रहती हैं। वे समाज और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार खुद को ढालती रहती हैं, चाहे उसकी कीमत उन्हें अंदर ही अंदर क्यों न चुकानी पड़े।
बरैन्ज़ मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महिलाओं द्वारा अपनी खुशी और ज़रूरतों को लगातार दूसरों के लिए दबाना ‘गुड डॉटर सिंड्रोम’ का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। इस स्थिति में महिलाएं हमेशा दूसरों की ज़रूरतों को पहले रखती हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ करती रहती हैं।
भारतीय समाज और ‘अच्छी बेटी’ होने के मापदंड
साउथ एशियन थेरपिस्ट कलेक्टिव की एक रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशियाई समाजों में लड़कियों को बचपन से ही ‘अच्छी बेटी’ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। परिवार और समाज उनसे उम्मीद करते हैं कि वे अपनी भावनाओं को दबाकर रखें। भारतीय सामाजिक ढांचे में ‘अच्छी बेटी’ की पहचान अक्सर परिवार की इज्जत से जोड़ दी जाती है। अच्छी बेटी वही मानी जाती है जो परिवार के फैसलों पर सवाल न करे। उसकी पढ़ाई, करियर या शादी जैसे बड़े फैसले भी परिवार की सहमति से तय होते हैं। उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सपनों को सामाजिक मर्यादाओं के भीतर ही सीमित रखे। ग्वालियर की रहने वाली 24 वर्षीय रुचिका श्रीवास्तव कहती हैं, “मेरे लिए अच्छी बेटी जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन समाज ने मुझे एक पितृसत्तात्मक ढांचे में फिट कर दिया है। मुझसे हमेशा कहा गया कि परिवार की इज्जत मेरी ज़िम्मेदारी है। बचपन से यह भी सिखाया गया कि अच्छी बेटी वही होती है जो ज़्यादा आज़ादी न ले, लड़कों से दूरी बनाए और समय पर घर लौटे।”
भारतीय समाज में ‘अच्छी बेटी’ की यह छवि केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहती। इसे नैतिकता और संस्कार जैसे शब्दों से जोड़ दिया जाता है। जो लड़कियां अपनी इच्छाओं, फैसलों और सपनों पर ज़ोर देती हैं, उन्हें अक्सर असंस्कारी, ज़िद्दी या परिवार तोड़ने वाली कहा जाता है। इस तरह ‘अच्छी बेटी’ होना एक सामाजिक पुरस्कार बन जाता है। वहीं, खुद को प्राथमिकता देना अपराध की तरह देखा जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि महिलाएं अपने ही परिवार और समाज में मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक बोझ उठाने को मजबूर हो जाती हैं। इस पर उत्तर प्रदेश से आने वाली 26 साल की नंदिनी यादव कहती हैं, “अच्छी बेटी होना मुझे एक जिम्मेदारी की तरह लगता है। जिस जिम्मेदारी को मैंने खुद से नहीं लिया है बल्कि समाज और परिवार द्वारा मेरे ना चाहते हुए भी मुझे दी जा रही है। जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे अक्सर खुद को हर तरह से भूलना और दबाना पड़ता है।”
अच्छी बेटी होना मुझे एक जिम्मेदारी की तरह लगता है। जिस जिम्मेदारी को मैंने खुद से नहीं लिया है बल्कि समाज और परिवार द्वारा मेरे ना चाहते हुए भी मुझे दी जा रही है। जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे अक्सर खुद को हर तरह से भूलना और दबाना पड़ता है।
पितृसत्तात्मक अपेक्षाएं और महिलाओं पर दोहरा बोझ
पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं से केवल घरेलू ज़िम्मेदारियां निभाने की उम्मीद नहीं की जाती। उनसे रिश्तों को संभालने, भावनाओं को नियंत्रित करने और परिवार में संतुलन बनाए रखने की भी अपेक्षा की जाती है। अमेरिकी समाजशास्त्री आर्ली होशचाइल्ड ने इस बोझ को ‘भावनात्मक श्रम’ कहा है। उन्होंने साल 1983 में इस अवधारणा को सामने रखा। उनके अनुसार, भावनात्मक श्रम किसी एक जेंडर तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा भार महिलाओं पर पड़ता है। महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर ऐसे काम करती हैं, जिनकी उनसे सामाजिक और पारिवारिक रूप से अपेक्षा की जाती है। घर के भीतर महिलाएं बच्चों की देखभाल, बुज़ुर्गों की सेवा और रोज़मर्रा के कामों को अपनी ज़िम्मेदारी मान लेती हैं। वे इसे अपनी भूमिका का हिस्सा समझती हैं। कई बार वे अपनी थकान, नाराज़गी या असंतोष को व्यक्त नहीं कर पातीं। रिश्तों में टकराव से बचना, सबको खुश रखना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना उनका अनकहा काम बन जाता है।
स्प्रिंगर नेचर जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, भारत में पारिवारिक अपेक्षाएं और लैंगिक भेदभाव महिलाओं में मानसिक थकान और तनाव का बड़ा कारण हैं। समाज में मौजूद लैंगिक पूर्वग्रह और ‘अच्छी बेटी’ बनने का दबाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। साउथ एशियन थेरपिस्ट कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि यह दबाव महिलाओं में चिंता, परफेक्शनिज़्म और भावनात्मक बोझ को बढ़ाता है। कामकाजी महिलाओं के लिए यह बोझ और गहरा हो जाता है। एक ओर नौकरी और आर्थिक योगदान, दूसरी ओर घर और रिश्तों की पूरी भावनात्मक ज़िम्मेदारी। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सभी महिलाएं इस दबाव को एक जैसा सामना नहीं करती। वर्ग, जाति और जेंडर पहचान उनके अनुभवों को प्रभावित करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, हाशिये के समुदाय और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय से आने वाली महिलाओं पर यह दबाव दोगुना होता है।
ट्रांस महिलाओं पर परिवार की खुशी और सम्मान के लिए अपनी पहचान दबाने का ज़्यादा दबाव होता है। उन्हें ऐसे सामाजिक और पारिवारिक दायरों में फिट होने की कोशिश करनी पड़ती है, जो उनकी जेंडर पहचान से मेल नहीं खाते। ट्रांस महिलाओं से सहनशील, त्यागी और समझौता करने वाली बनने की उम्मीद और भी कठोर हो जाती है।
अच्छी बेटी का बोझ और हाशिये के समुदाय
हैदराबाद की 45 वर्षीय ट्रांस महिला रचना मुंदरिया कहती हैं, “ट्रांस महिलाओं पर परिवार की खुशी और सम्मान के लिए अपनी पहचान दबाने का ज़्यादा दबाव होता है। उन्हें ऐसे सामाजिक और पारिवारिक दायरों में फिट होने की कोशिश करनी पड़ती है, जो उनकी जेंडर पहचान से मेल नहीं खाते। ट्रांस महिलाओं से सहनशील, त्यागी और समझौता करने वाली बनने की उम्मीद और भी कठोर हो जाती है। दूसरों की प्रतिक्रियाओं को संभालना, अपनी पहचान छिपाना और समाज में अपनी जगह बनाना उनके लिए भारी मानसिक बोझ बन जाता है। इसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।” लिंग आधारित सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं को जीवन के लगभग हर पड़ाव पर प्रभावित करती हैं। समाज अक्सर महिलाओं की मजबूती और त्याग की तारीफ़ करता है और उन्हें ‘अच्छी बेटी’ का खिताब देता है।
लेकिन इस सराहना में उनकी भावनाओं, थकान और मानसिक ज़रूरतों के लिए जगह नहीं होती। उनसे मजबूत बने रहने की उम्मीद की जाती है, न कि समझे जाने की। इस विषय पर कोलकाता की 29 वर्षीय मीमांसा सिंह कहती हैं, “अच्छी बेटी बनने की कोशिश में मैंने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक बोझ उठाया है। बचपन से ही माता-पिता के कामकाजी होने के कारण घर की ज़िम्मेदारियां संभालीं है। सिर्फ़ 14 साल की उम्र से ही मेरे पर शारीरिक थकान और जिम्मेदारी का बोझ आ गया। आज मैं कमाने लगी हूं तो परिवार और छोटे भाई की आर्थिक ज़िम्मेदारी भी मेरे पर है। इसके साथ ही समय पर शादी करने का दबाव भी है।”
अच्छी बेटी बनने की कोशिश में मैंने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक बोझ उठाया है। बचपन से ही माता-पिता के कामकाजी होने के कारण घर की ज़िम्मेदारियां संभालीं है। सिर्फ़ 14 साल की उम्र से ही मेरे पर शारीरिक थकान और जिम्मेदारी का बोझ आ गया।
वह आगे कहती हैं, “परिवार मुझसे सब उम्मीद करता है, लेकिन मुझे समझने का कोई स्पेस नहीं देता। बड़ी बेटी होने का मतलब ज़्यादा ज़िम्मेदारी और कम सहानुभूति होता है।” पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों को ज़्यादा आज़ादी और अवसर मिलते हैं। वहीं लड़कियों से कम उम्र में समझदार बनने, समझौता करने और परिवार को प्राथमिकता देने की उम्मीद की जाती है। साउथ एशियन थेरपिस्ट कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि ऐसी पारिवारिक अपेक्षाएं लड़कियों को बचपन से यह सिखाती हैं कि परिवार की खुशी उनकी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। यह दोहरा सामाजिक दबाव धीरे-धीरे लड़कियों के आत्मविश्वास, फैसलों और आत्म-मूल्य को कमजोर करता है। समाज महिलाओं की सहनशीलता की तारीफ़ करता है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को दबाकर चुकानी पड़ती है। इसका सीधा असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
उत्तर प्रदेश के काकोरी की रहने वाली 22 वर्षीय अनामिका चौधरी कहती हैं, “समाज बार-बार मुझे अच्छी बेटी बनने की हिदायत देता है। यह हिदायत मेरे जीवन के दायरे तय करती है। इस दबाव में कई लड़कियां खुद के साथ न्याय नहीं कर पातीं और अपनी स्वतंत्र पहचान से दूर होती जाती हैं।” जरूरी है कि हम अच्छी बेटी के इन दोहरे सामाजिक मानकों पर सवाल उठाएं। महिलाओं को अपनी इच्छाओं, सपनों और भावनाओं को महत्व देना सीखना होगा। साथ ही, खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि ज़रूरी आत्म-सम्मान है।