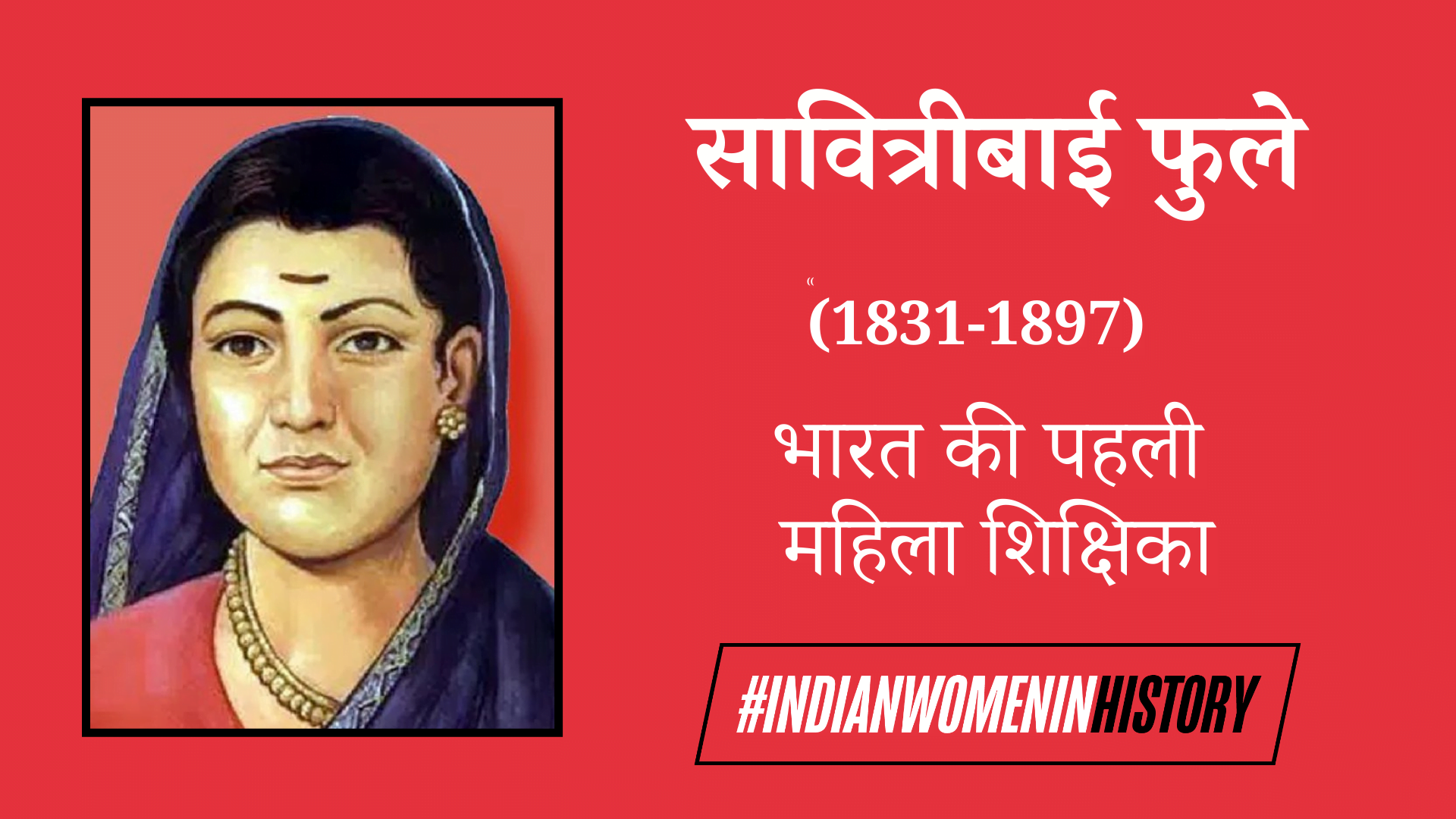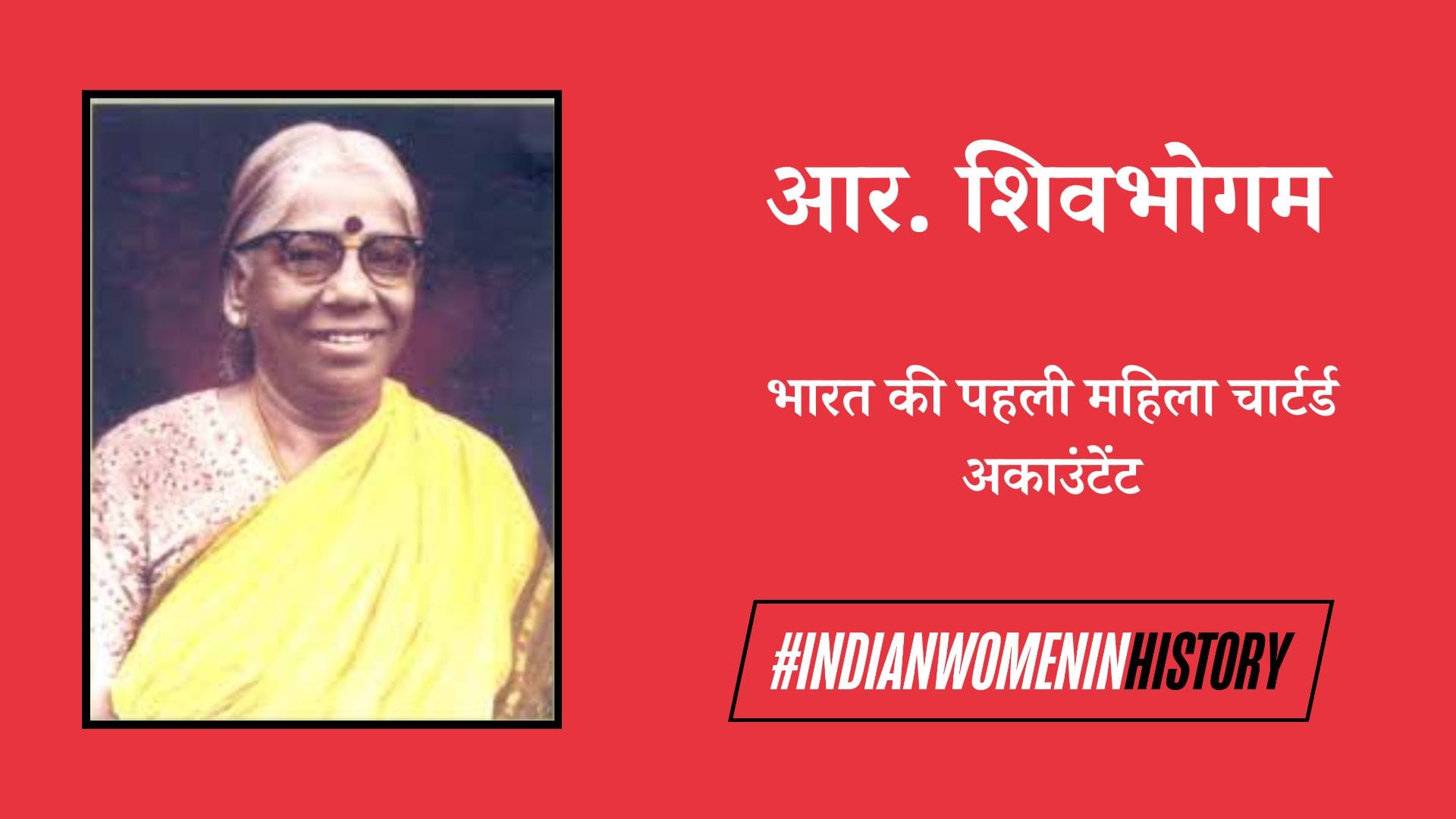भारत में हमेशा से शिक्षा प्रणाली में सभी सामाजिक तबकों को जगह नहीं दी गई थी। महिलाएं और दलित उनमें से दो ऐसे तबके थे। उन्नीसवीं सदी में जब देश में राजनैतिक गुलामी के साथ-साथ सामाजिक गुलामी का भी दौर था, तब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आज़ादी के नए द्वार खोलकर उनमें नई चेतना का सृजन किया। अंधविश्वासी समाज में सावित्रीबाई फुले एक तार्किक महिला थी। उन्होंने हर जातिगत पहचान की महिला के जीवन में शिक्षा के कारण आने वाले बदलावों की ज़रूरत को महत्ता दी। एक घटना के अनुसार बचपन में जब सावित्रीबाई अंग्रेज़ी की एक किताब के पन्ने पलट रही थी तब उनके पिताजी ने देख लिया। तब शिक्षा का हक़ केवल उच्च जाति के पुरुषों को था, पिता ने उनके हाथ से वह क़िताब हटा दी। सावित्रीबाई का निजी जीवन शिक्षा के अधिकार को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने के इर्दगिर्द रहा जिन्हें इससे वंचित रखा जाता रहा। वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं। भारत में नारीवाद की पहली मुखर आवाज़ मानी जाने वाली एक समाज सुधारिका और मराठी कवियत्री भी थीं। उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में जाना जाता था।
सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी पैदाइश का स्थान था सतारा का एक छोटा सा गांव था, नायगांव। इनके पिता का नाम खन्दोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई महज़ 10 साल की थी जब उनका बाल विवाह ज्योतिबा फूले से हो गया। वह साल था 1840। उनके पति ज्योतिराव फूले तब तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे और उनकी उम्र 13 साल थी। विवाह के बाद सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले की मदद से तालीम हासिल की। ज्योतिराव दलित चिंतक और समाज सुधारक थे। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले के बीच का पत्र संवाद उस किताब में दर्ज किया गया है जिसमें उनके भाषण के कुछ अंश प्रकाशित किए गए हैं। दोनों के बीच की साझेदारी केवल वैवाहिक रिश्ते तक सीमित नहीं थी बल्कि समाजिक बदलाव के रास्ते पर दोनों साथी बने रहे। महज़ 17 साल की छोटी सी उम्र में ही सावित्रीबाई ने लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया था।
उस दौर में समाज में कई महिला विरोधी सामाजिक कुरीतियां चरम पर थी, जैसे जातीय पहचान के आधार पर छुआछूत, सतीप्रथा, बाल-विवाह, शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव आदि। इन रूढ़ियों को तोड़कर महिलओं के हित में कई रास्ते बनाने का श्रेय सावित्रीबाई फूले को जाता है। उन्हें महिलाओं और दलितों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के पति होने के साथ-साथ उनके जीवन के इस उद्देश्य में उनके हमसफ़र, हितैषी और समर्थक रहे। भारत में नारीवादी सोच की एक ठोस बुनियाद बनाने में सावित्रीबाई का साथ उनके पति ज्योतिबा ने दिया। उन्होंने न केवल कुप्रथाओं को पहचाना बल्कि विरोध किया और समाधान पेश किया।

और पढ़ें: सावित्रीबाई फुले: ज़माने को बदला अपने विचारों से
सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए न सिर्फ पहला स्कूल ही खोला, बल्कि वे भारत की पहली महिला अध्यापिका बनीं। साल 1848 में पहला स्कूल शुरू करने के बाद फुले दंपत्ति की चुनौतियां बढ़ती गई। इससे ही जुड़ी एक घटना है जिसे सावित्रीबाई को याद करते हुए हमेशा इतिहास की स्मृति में दोहराया जाता है। सावित्रीबाई फुले ने पुणे शहर के भिड़ेवाडी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। उनके द्वारा स्थापित अठारहवां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। जब भी सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थीं, लोग उनके इस कदम से नाराज़ होकर उनपर पत्थर और गोबर फेंका करते थे। सावित्रीबाई हर जाति जिसे समाज पढ़ाई-लिखाई करने के क़ाबिल नहीं समझता था उन तबक़ों से आती लड़कियों की शिक्षा की बड़ी पक्षधर थी। बालिकाओं के लिए स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था और सावित्रीबाई हर जाति की लड़कियों को शिक्षित करना चाहती थी। ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी।
सामाजिक मुश्किलों से फुले का रोज़ सामना होता रहा। ब्राह्मणवादी पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था सावित्रीबाई से खफ़ा थी। लेकिन, वह पीछे नहीं हटी, वह पढ़ाने जाते हुए अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाने लगी। जब उन पर पत्थर और गोबर फेंके जाते तब सावित्रीबाई फूले कहती थी, “मैं अपनी बहनों को पढ़ाने का काम करती हूं, इसलिए जो पत्थर और गोबर मुझपर फेंके जाते हैं वे मुझे फूल की तरह लगते हैं।” अपने मकसद से उन्हें कोई बाधा डिगा नहीं पाई। वह अपनी कविताओं और लेखों में हमेशा सामाजिक चेतना की बात करती थी। उनकी बहुत सी कविताएं ऐसी हैं जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जाति तोड़ने और ब्राह्मण ग्रंथों से दूर रहने की बात की तरफ़ इशारा अपनी कविताओं में किया है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया।

फुले दम्पत्ति ने 28 जनवरी 1853 में अपने पड़ोसी मित्र और आंदोलन के साथी उस्मान शेख के घर में विधवाओं और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ‘बाल हत्या प्रतिबंधक गृह’ की स्थापना की। इसकी पूरी जिम्मेदारी सावित्रीबाई ने संभाली। इस जगह ज़रूरतमंद गर्भवती महिलओं को रखा जाता, उनकी देखभाल की जाती थी। उनके बच्चे के पालनपोषण के लिए इस साथ में एक पालना घर बनाया था। मात्र 4 सालों के अंदर ही 100 से अधिक विधवा स्त्रियों ने इस गृह में बच्चों को जन्म दिया। 25 दिसंबर 1873 को सत्यशोधक समाज नामक संस्था ने अपने अंतर्गत पहला विधवा पुर्नविवाह करवाया। सत्यशोधक समाज की स्थापना उसी वर्ष सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर की थी।
जब उन पर पत्थर और गोबर फेंके जाते तब सावित्रीबाई फूले कहती थी, “मैं अपनी बहनों को पढ़ाने का काम करती हूं, इसलिए जो पत्थर और गोबर मुझपर फेंके जाते हैं वे मुझे फूल की तरह लगते हैं।”
1890 में जब ज्योतिबा फुले ने अपनी आंखिरी सांस ली थी तब उनका अंतिम संस्कार भी खुद सावित्रीबाई फूले ने ही किया था जो आम तौर पर हमारे समाज में पुरुष द्वारा ही किया जाता है। ज्योतिबा के निधन के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बख़ूबी निभाया। इस संस्था ने विधवा विवाह की परंपरा को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की पहल तब की थी जब विधवाओं को सामाजिक गतिविधियों से निष्कर्ष रखा जाता था। उनके हिस्से ना तो जीवन के रंग थे ना जीवन साधारण रूप से व्यतीत करने की आज़ादी। साल 1892 में सावित्रीबाई ने विधवाओं के मदद के लिए एक संगठन बनाया। यह संगठन महिला सेवा मंडल के रूप में पुणे की विधवा स्त्रियों के आर्थिक विकास के लिए देश का पहला महिला संगठन कहलाया। संगठन की कार्यप्रणाली के अनुसार सावित्रीबाई सभी वंचित दलित और विधवा स्त्रियों से उनकी स्थिति पर चर्चा करतीं। उनकी समस्या सुनती, उनके साथ चर्चा करती और उसे दूर करने का उपाय सभी के साथ मिलकर ढूंढ़ती।

और पढ़ें: ज्योतिबा फूले की ‘गुलामगिरी’ हमेशा एक प्रासंगिक किताब रहेगी
1897 में प्लेग महामारी के चपेट में भारत के कई हिस्से का चुके थे। उस समय सावित्रीबाई फुले प्रभावित जगहों पर पीड़ितों की सहायता के लिए जातीं जबकि वह अच्छे से जानती थी कि वह खुद इस महामारी की चपेट में आ सकती हैं। पीड़ित बच्चों की देखभाल के दौरान वह इस बीमारी की गिरफ्त में आ गई। प्लेग से पीड़ित बच्चे पांडुरंग गायकवाड़ को लेकर जाते वक्त सावित्रीबाई भी प्लेग से संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे सावित्रीबाई फुले ने अपनी आखिरी सांस ली। वह अपनी आख़री सांस तक अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर संघर्षरत थी।
सावित्रीबाई को समाज में लड़कियों, महिलओं के अधिकार और उनके प्रति उनकी जागरूकता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। शिक्षा समाज को बदलने की ताक़त रखती है। जहां की शिक्षा प्रणाली में बराबरी नहीं सुनिश्चित की जाती वैसा समाज असल में शिक्षित नहीं माना जा सकता। सावित्रीबाई फुले ने मुख्यधारा व्यवस्था को महिलाओं, दलितों के नज़रिए से देखे जाने की नींव रखी। इसी नींव पर भारत का समावेशी नारीवाद अपनी जड़ें रोज़ मजबूत करता है इसलिए सावित्रीबाई हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। हालांकि समावेशी समाज के लिए काम करने वाले लोगों का मानना है कि सावित्रीबाई की कहानी मुख्यधारा में उस तरह चर्चित नहीं है जैसे होनी चाहिए। पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद का दबदबा समाज में आजतक इतना है कि सामाजिक चर्चा से लेकर अकादमिक चर्चा में उनके बारे में जितना लिखा जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए उसकी कमी है। ऐसा इसलिए है ताकि जिन तबक़ों को ऐतिहासिक रूप से और आजतक अलग कर के रखा जाता रहा है उन्हें अपने अधिकारों का, अपने इतिहास का ज्ञान हो। इसलिए शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाए जाने के समांतर में शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में बराबरी की बात करने के लिए सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन को शिक्कष दिवस के रूप में मनाए जाने की मांग रखते हैं।
और पढ़ें: फ़ातिमा शेख़ : भारत की वह शिक्षिका और समाज सुधारक, जिन्हें भुला दिया गया| #IndianWomenInHistory