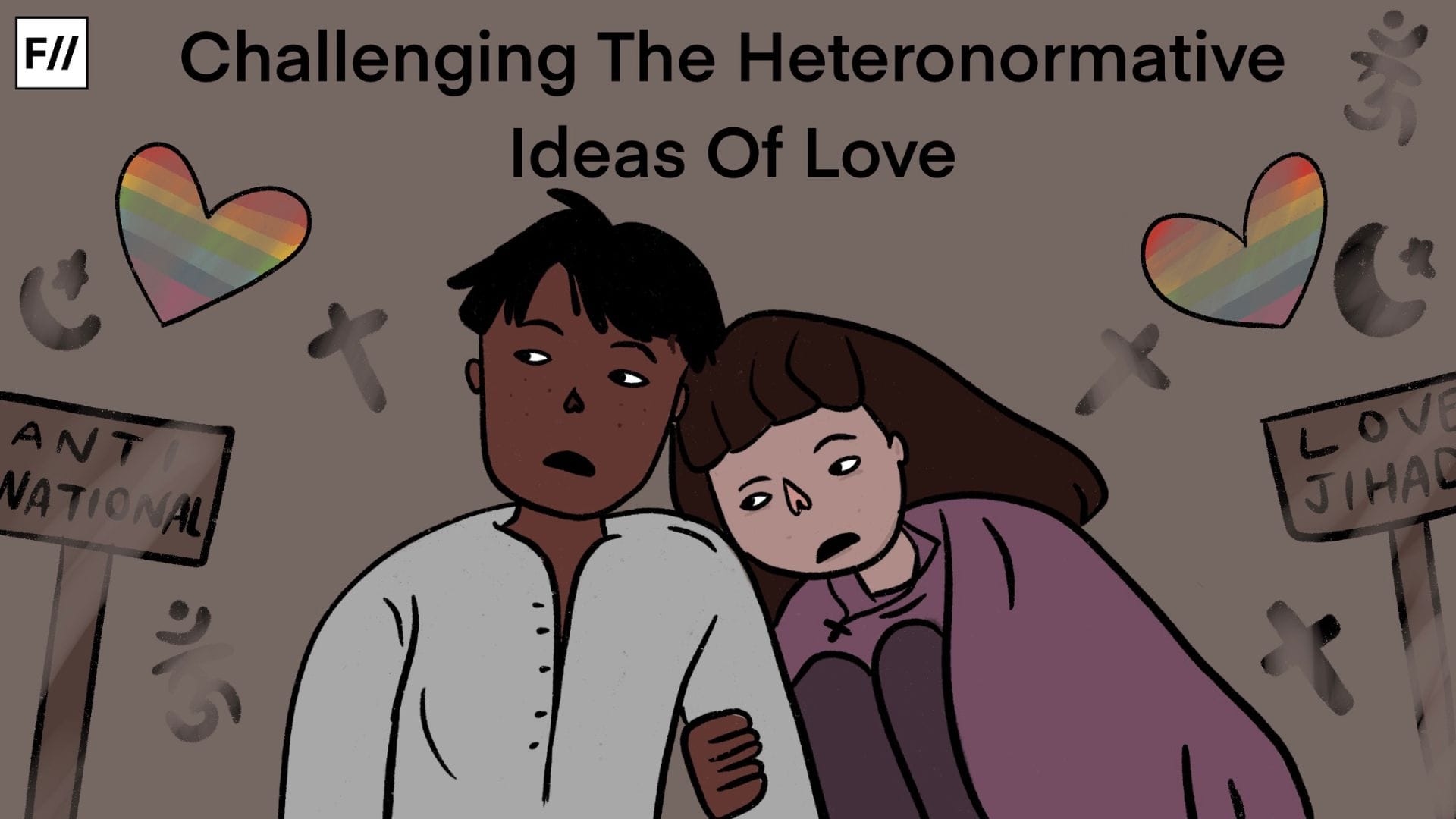शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं? आखिर क्यों महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने की तमाम कोशिशें की गई हैं और आज भी की जाती हैं? महिलाएं अगर पढ़-लिख लें, तो समाज में ऐसा कौन सा तूफ़ान आ जाएगा? सैद्धांतिक तौर पर ऐसा दावा किया जाता है कि जेंडर के सामाजिक ढाँचे महिलाओं के लिए घरेलूपन और कम परिश्रम वाले कामों और भूमिकाओं का पुनरुत्पादन करते हैं। इसी आधार पर ये ढाँचें समाज में ‘अच्छी औरतों’ का गढ़न भी करते हैं। जितनी ज़्यादा जवाबदेही, उतनी अच्छी औरत। ‘अच्छी औरतें’ उनके लिए बने ऐतिहासिक नियमों और कायदों को तोड़ने का ख़याल नहीं पालतीं। वे उन्हें मानती हैं और मनवाती हैं, जहां ‘घरेलूपन’ और ‘कमाने के कम अवसर’ उन्हें जकड़ कर रखते हैं। शिक्षा घरेलूपन के इसी जकड़न को तोड़ने का एक माध्यम है। साथ ही साथ इसका महिलाओं के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए जिसे सत्ता की पहुंच से कहीं दूर हाशिये पर रखा जाता है, कई सारे और मायने हैं। यह लेख महिलाओं की शिक्षा पर कुछ नारीवादी तर्कों पर आधारित है और इसकी प्रेरणा गिलियन पास्कल और रोजर कौक्स द्वारा इस विषय में किए अध्ययन से ली गई है।
पुनरुत्पादन के सिद्धांत
पुनरुत्पादन के सिद्धांतों का ऐसा दावा है कि शिक्षा व्यवस्थाएं या संस्थाएं सामाजिक संबंधों का पुनरुत्पादन करती हैं। नारीवादी नज़रिये से देखा जाए तो इन सामाजिक संबंधों में पुनरुत्पादन के साथ-साथ उत्पादन के संबंध भी शामिल हैं। यह उत्पादन-पुनरुत्पादन की प्रक्रिया परिवार और घरेलू जीवन के आस-पास केंद्रित होता है। इसलिए मुख्यधारा ऐसा मानती है कि स्कूलों/शिक्षा को लड़कियों की घरेलू जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। लंबे समय से स्कूलों में गृहविज्ञान जैसे विषय इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऊपरी तौर पर यदि पाठ्यक्रम जेंडर-निरपेक्ष हो भी गए, तब भी एक छिपी पाठ्यचार्या (हिडिन करिकुलम) बड़ी चालाकी से लड़कियों को घरेलूपन और अवैतनिक परिश्रम वाले कामों की ओर ढकेलती रही है। जैसे पाठ्यक्रम में इस्तेमाल हो रही किताबों में महिलाएं और पुरुष जिन भूमिकाओं में नज़र आते हैं, उससे यह संदेश साफ़ झलकता है कि हम औरतपन और मर्दानगी की परिकल्पना कैसे और किनके शरीरों के लिए करते हैं। इसमें स्कूलों और परिवार की एक महत्त्वपूर्ण सहभागिता होती है।
पुनरुत्पादन के तर्क भी स्थिर नहीं रहते हैं। स्कूल, परिवार और समाज हमें कुछ इस तरह गढ़ता है कि लड़कियों का किसी भी क्षेत्र में प्रतिशोध एक ऐसा माध्यम बन जाता है जिसके कारण वे स्त्रीसुलभ (feminine) नीतियों के जाल में फंस जाती हैं। इस तरह उभरे पितृसत्तात्मक कायदों का पुनरुत्पादन एक सांस्कृतिक रूप ले लेता है, कुछ इस कदर कि लड़कियां खुद श्रम के जेंडर के आधार पर हुए विभाजन की तरफ़दारी करने लगती हैं। इस व्यवस्था के हम आदि हो जाते हैं। यह हमारी संस्कृति बन जाती है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाते रहने में ही समाज (और उससे जुड़े हर आयाम/व्यवस्था जैसे बाज़ार, पूंजीवाद, नव-उदारवाद) का संतुलन बना रहता है। जो जैसा है, वैसा चलता रहता है। बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रतिशोध के।
वैतनिक कामों में भी महिलाओं के लिए घरेलू भूमिकाएं ढूंढ ली जाती हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे केवल वही करें जैसे वे बैठी रहें, सुंदर दिखें, कार्यस्थल पर ‘महिलाओं’ की मौजूदगी का प्रतिनिधित्व करें, चाय-कॉफी का इंतेज़ाम करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें इत्यादि।
उच्च शिक्षा की ओर लौटती वयस्क महिलाओं का दृष्टिकोण
शिक्षा के विषय पर लड़कियों और महिलाओं की प्रतिक्रियाएं को अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें तो उसमें “समायोजन” (adjustment) और “प्रतिरोध” (resistance), दोनों ही देखने को मिलती है। उनकी प्रतिक्रियाओं या किन्हीं ख़ास तबके की महिलाओं के अनुभवों को ही सभी की सच्चाई के तौर पर अपना लेना सही नहीं है। अनुभवों की भिन्नता को नज़रंदाज नहीं करना चाहिए। इस बात पर भी गौर करना ज़रूरी है कि शिक्षा के ढांचों पर किए गए अधिकांश शोध/लेखन स्कूली शिक्षा के बारे में है। शिक्षा की तरफ़ लौट रही वयस्क महिलाओं की ज़रूरतें अलग हैं, उन्हें हम स्कूली शिक्षा के समान नहीं मान सकते। यह बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि शिक्षा व्यवस्थाओं के भीतर क्या चल रहा है, पुनरुत्पादन के सिद्धांत और प्रक्रियाएं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे चलती हैं।
पेशेवर भूमिका में घरेलू भूमिका

महिलाओं की ज़िंदगी में वेतन वाले और बिना वेतन वाले, दोनों ही तरह के काम बहुत जटिल और एक-दूसरे पर आश्रित रूप से शामिल होते हैं। वेतन वाले कामों को करने के लिए सहमति अक्सर इसी शर्त पर मिलती है कि घरेलू कामों के प्रति ज़िम्मेदारी कितनी दिखाई पड़ रही है। ऐसे में हम स्वीकार कर लेते हैं कि जिन महिलाओं के दमन का कारण श्रम-बाज़ार है, उनकी स्वाभाविक पसंद तो शादी या घरेलू काम ही होते हैं। ज़रूरी है कि हम यह समझें कि महिलाओं की जीवन में वैतनिक (वेतन देने वाले) और अवैतनिक (बिना वेतन वाले) कार्य साथ-साथ चलते रहते हैं। उनका अधिकतर श्रम जिन कार्यों में रोज़ाना जाता है, उनका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। यहां तक कि वैतनिक कामों में भी महिलाओं के लिए घरेलू भूमिकाएं ढूंढ ली जाती हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे केवल वही करें जैसे वे बैठी रहें, सुंदर दिखें, कार्यस्थल पर ‘महिलाओं’ की मौजूदगी का प्रतिनिधित्व करें, चाय-कॉफी का इंतेज़ाम करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करें इत्यादि।
पास्कल और कौक्स द्वारा किए अध्ययन में जुड़ी बहुत सी महिलाएं ऐसा मानती थी कि यदि वे आगे और पढ़ लें, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें तो उनसे यह स्त्रीसुलभ वैतनिक कार्यों की अपेक्षाएं बंद हो जाएंगी। वे इन दोनों चीजों के बीच एक सीधा संबंध देखती थी। ‘अनुभव’ को भी मान्य तभी समझा जाता है जब वे वेतन देने वाले कामों से उपज रहा हो। बिना पैसों के लिए किए जाने वाले काम और पैसों के लिए किए जाने वाला काम दोनों से निकल रहे अनुभव के बीच बंटवारा है। हम काम ही उसे मानते हैं, जिसका जुड़ाव वेतन/पैसे से हो।
कई महिलाएं अपनी शिक्षा को लेकर अपने पति से मिले समर्थन और आर्थिक सहायता का ज़ोरदार उल्लेख करती हैं। यह बेशक खुशी की बात है परंतु महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने साथ के पुरुषों की अनुमति की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है?
विवाह के अनुभव बेशक सबके अलग हों, लेकिन महिलाओं की ज़िंदगी में विवाह और मातृत्व से उपजी सीमाएं भी होती हैं। माँ, पत्नी और गृहणी के रूप में नज़र आ रही एक महिला की पेशेवर स्थिति अक्सर कमज़ोर होती है। कई बार मातृत्व की ज़िम्मेदारियों से उन्हें श्रम बाज़ार यानी नौकरियां छोड़नी भी पड़ती हैं। किशोरावस्था या बचपन से हम शादियां देखते हुए बड़े होते हैं, जहां महिलाओं की मुख्य जवाबदेही घरेलू कार्यों के लिए ही होती है। शादी न करने का निर्णय बहुत ही कम लिया जाता है। दबाव से हो या अपनी इच्छा से, शादी अक्सर होती ही है। मगर जब तक काम करना गुज़ारे के लिए ज़रूरत न बन जाए (तलाक के केस में, शादी टूटने के केस में), हम शिक्षा और पेशेवर ज़िंदगी को शादी के विकल्प के रूप में नहीं देखते। लेकिन अगर हम शादी को भी एक पेशेवर ज़िंदगी के रूप में देखें, तो पाएंगे कि विवाह रोज़गार का ही एक स्वरूप है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता महिलाएं अक्सर स्वीकार कर लेती हैं क्योंकि पहला तो उनकी श्रम बाजार में पहुंच पुरुषों के मुकाबले कम होती है और दूसरा घरेलू भूमिकाओं में उनका अनुभव ज़्यादा होता है।
पर क्या सचमुच विवाह उस तरह का आर्थिक सहारा देता है?
मातृत्व या शादीशुदा ज़िंदगी बहुत से लोगों के लिए आनंद का कारण हो सकती है। लेकिन पत्नी, गृहिणी, मातृत्व ये तीनों ही महिलाओं को एक पेशेवर ज़िंदगी के जैसे ही प्रस्तावित की जाती है। घरेलू काम करने से बड़ी बात है एक गृहणी होना, बच्चे पैदा करने से बड़ी बात है एक माँ होना। महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वे इन्हीं भूमिकाओं में संतुष्ट रहें, इन्हें अपनी पहचान का स्रोत और सार्वजनिक पेशेवर ज़िंदगी का एक बेहतर विकल्प मानें। लेकिन क्या ऐसा सचमुच सभी के साथ होता है? क्या सभी महिलाएं घरेलूपन से संतुष्ट हैं? या उनकी कुछ और व्यक्तिगत और आर्थिक ज़रूरतें/इच्छाएं होती हैं?
शिक्षा की ओर लौटने के अनुमति क्यों?
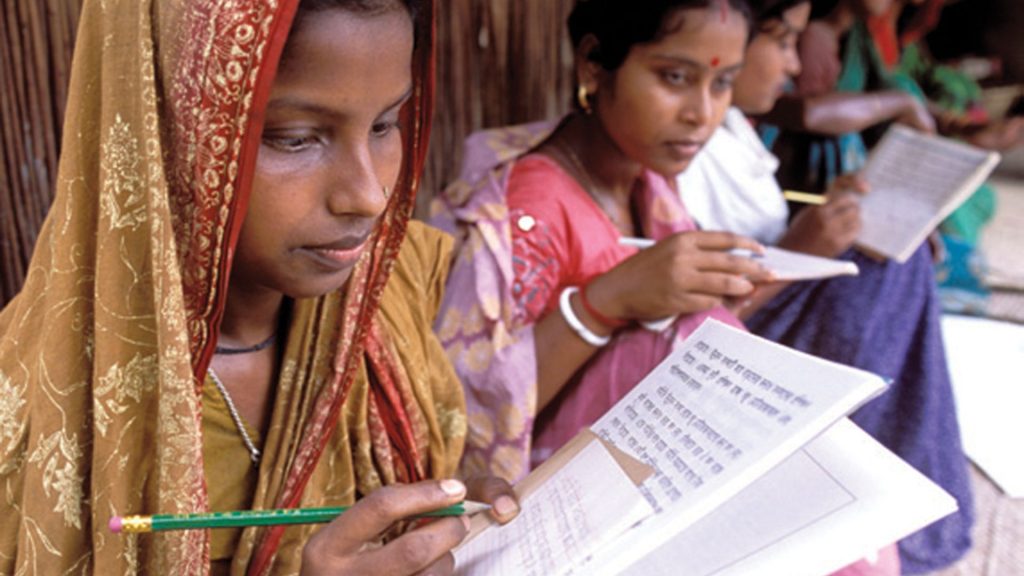
महिलाओं के लिए शिक्षा की ओर लौटने के क्या कारण हो सकते हैं? परिवार से जुड़े कारण? विवाह के टूटने से आर्थिक दबाव? अन्य आर्थिक कारण? मानसिक संतुष्टि? किसी व्यक्तिगत संकट का समाधान? भविष्य की तैयारी? पढ़ाई करने का सही समय या एक मात्र मौका? आमदनी का स्रोत, उपार्जन क्षमता में वृद्धि या सुरक्षित रोज़गार? बच्चों का हित? केवल गृहणी से अधिक कुछ होने की इच्छा? पेशेवर ज़िंदगी का विकास? कई महिलाएं अपनी शिक्षा को लेकर अपने पति से मिले समर्थन और आर्थिक सहायता का ज़ोरदार उल्लेख करती हैं। यह बेशक खुशी की बात है परंतु महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने साथ के पुरुषों की अनुमति की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है?
पास्कल और कौक्स के अध्ययन में शामिल सभी महिलाओं ने शिक्षा को काम के बाज़ार में बेहतर जगह तक पहुँचने का माध्यम माना था। शिक्षा के ज़रिए उन्हें घरेलूपन से क्षणिक छुटकारा मिलता था। शिक्षा के ज़रिए वे घर से बाहर निकलती हैं। व्यवहारिक और सार्वजनिक लिहाज़ से शिक्षा को योग्यता प्राप्त करने का माध्यम भी माना जा रहा था। शिक्षा व्यक्तिगत और निजी मामलों में भी ज़रूरी समझी जा रही थी जैसे गृहणी की भूमिका जब पहचान दिलाने में असफल रही और मातृत्व हर रोज़ की ज़िंदगी का केंद्र नहीं रहा तो शिक्षा पहचान के स्रोत की तरह भी देखा जाने लगा। ऐसा भी लगता है कि शिक्षा किशोरावस्था में घरेलूपन के लिए खाली की गई जगह को नई पहचान देकर भरने वाला है। शिक्षा को अध्ययन की महिलाओं ने वाकई एक अवसर जैसा देखा।
पास्कल और कौक्स द्वारा किए अध्ययन में जुड़ी बहुत सी महिलाएं ऐसा मानती थी कि यदि वे आगे और पढ़ लें, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें तो उनसे यह स्त्रीसुलभ वैतनिक कार्यों की अपेक्षाएं बंद हो जाएंगी। वे इन दोनों चीजों के बीच एक सीधा संबंध देखती थी।
आख़िर में उसी सवाल पर लौटते है कि महिलाएं अगर पढ़-लिख लें, तो समाज में ऐसा कौन सा तूफ़ान आ जाएगा? पर सच ही है, तूफ़ान तो आएगा! अपने अधिकारों और सदियों से चलते आ रहे मुफ़्त में किए गए अपने श्रम का हिसाब अगर महिलाएं मांग लें, तो तूफान तो आएगा। इन सवालों का लेना-देना सत्ता से है, सत्ता की दर्जाबंदी से है, पितृसत्ता के दृढ़ अस्तित्व से है। शिक्षा की सत्ता संरचनाओं में पुरुषों को (कुछ विशेष पुरुषों को) उच्च स्थान दिया गया है, इसका सबूत हर जगह देखने को मिल जाएगा। सत्ता समाज में उसी तरह संचालित है, जिससे की पुरुषों की पकड़ और विशेषाधिकार सत्ता पर बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं घरेलू भूमिकाओं से कभी अलग न हो। यदि पढ़-लिख भी लें, तो भी घरेलू बनी रहें। इसलिए हम घरेलूपन को उनके सामने बचपन से ऐसे पेश करते हैं, जैसे वह उनका धर्म हो, उनकी परम ज़िम्मेदारी हो, उनका कर्तव्य हो।
इसके लिए हर रोज़ समाज दंड और पुरस्कार की प्रणाली से यह भी सुनिश्चित करता है कि पुनरुत्पादन के सिद्धांत हर एक इंसान स्वीकार करे, माने, निभाए और दूसरों से भी (दंड देकर, पुरुस्कृत करके) मनवाए। शिक्षा प्रदान करने वाले तमाम संस्थान भी इसी समाज का एक हिस्सा हैं। वे कोई समानता फैलाने वाले कारखाना नहीं हैं। उनमें भी बहुत से संशोधन की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि समाज जो हमें पुरुत्पादन के जो नियम स्वाभाविक कह कर थमा रहा है, हम उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखें और जैसा की पास्कल और कौक्स ने अपनी लेख में कहा है, “लगातार खुद से ये सवाल करें कि आखिर इन सब में फायदा किसका है?”
स्रोतः
- Cox, R., & Pascall, G. (1994). Individualism, self‐evaluation and self‐fulfilment in the experience of mature women students. International Journal of Lifelong Education, 13(2), 159–173
- ERIC