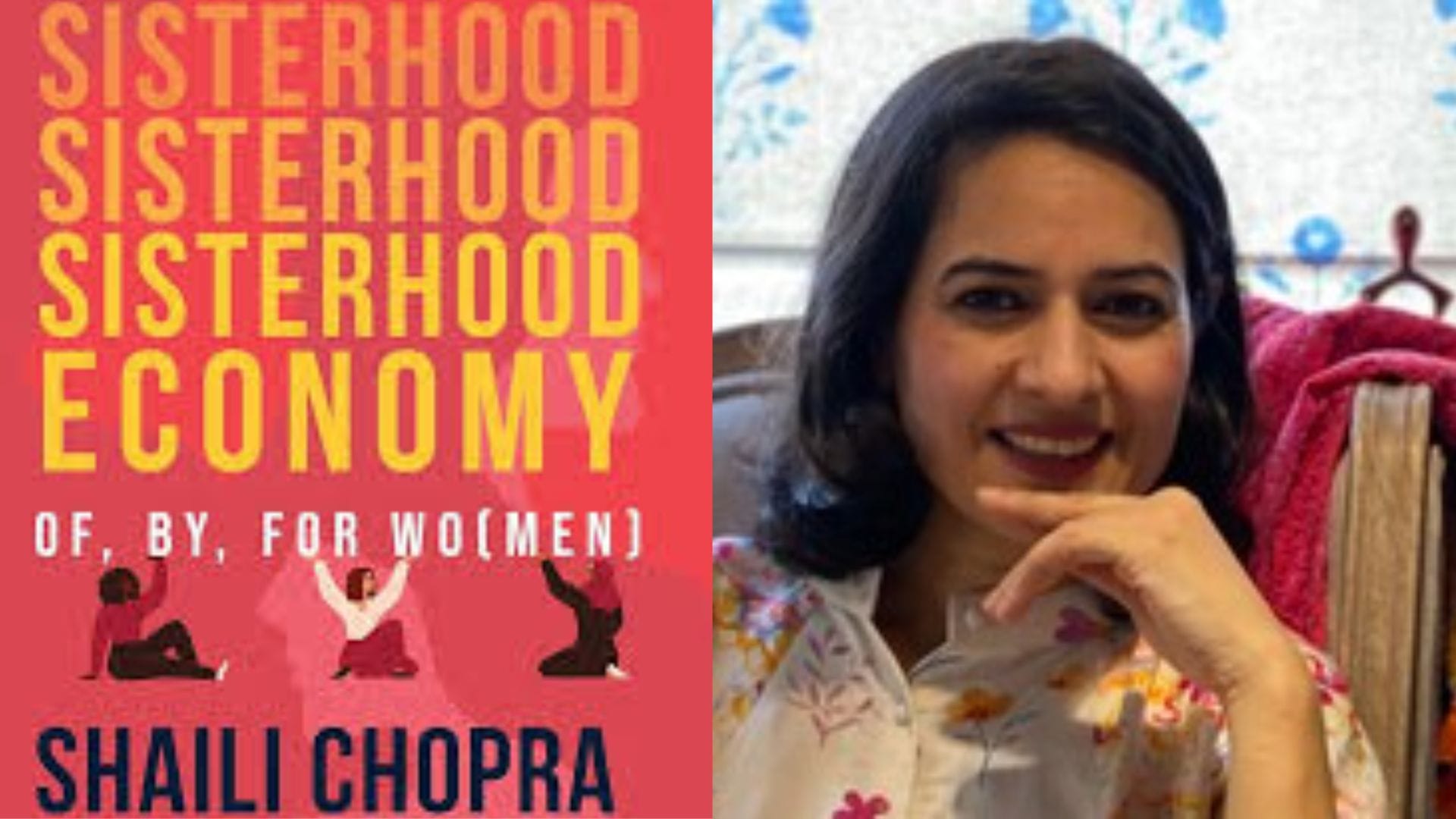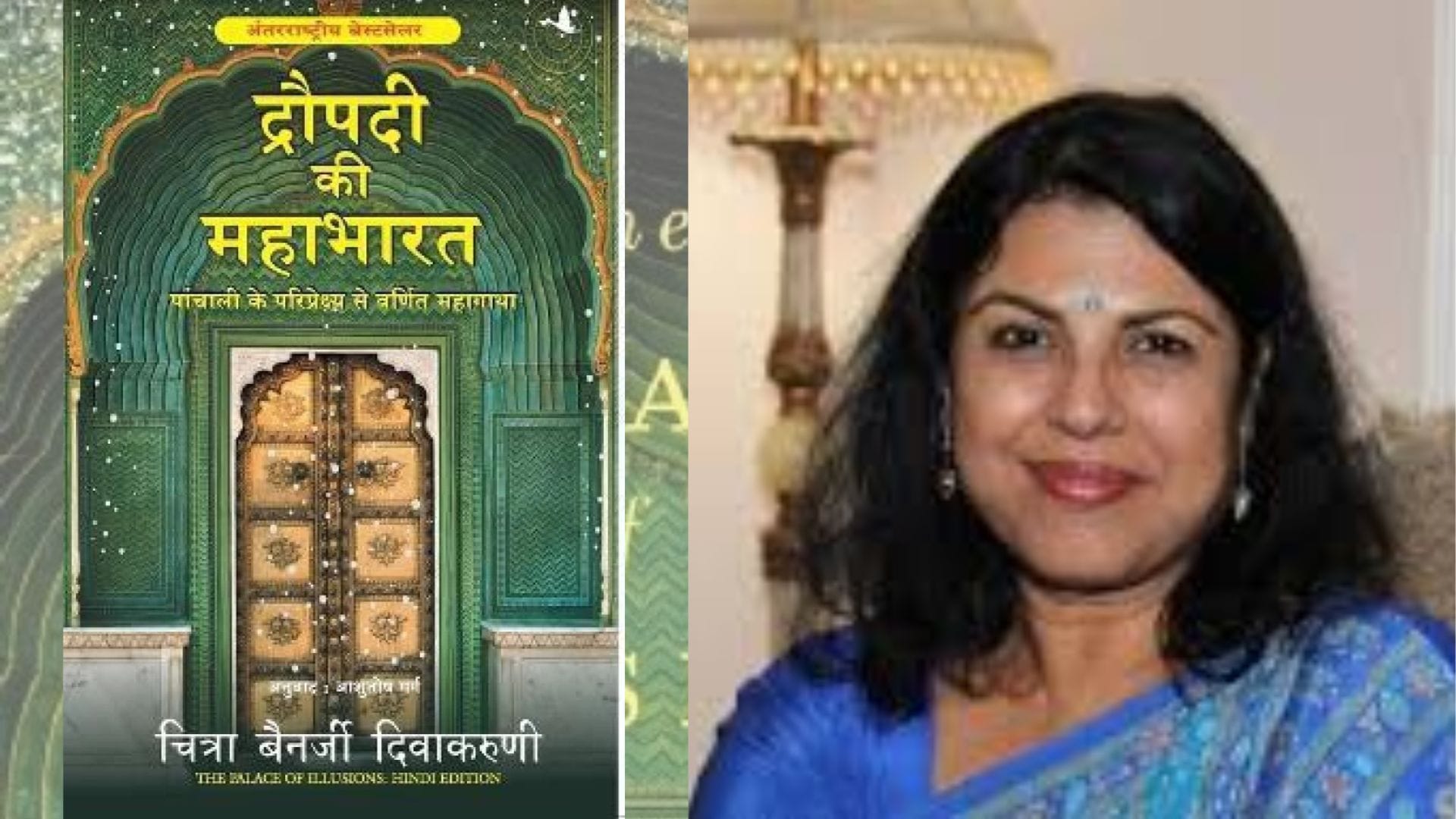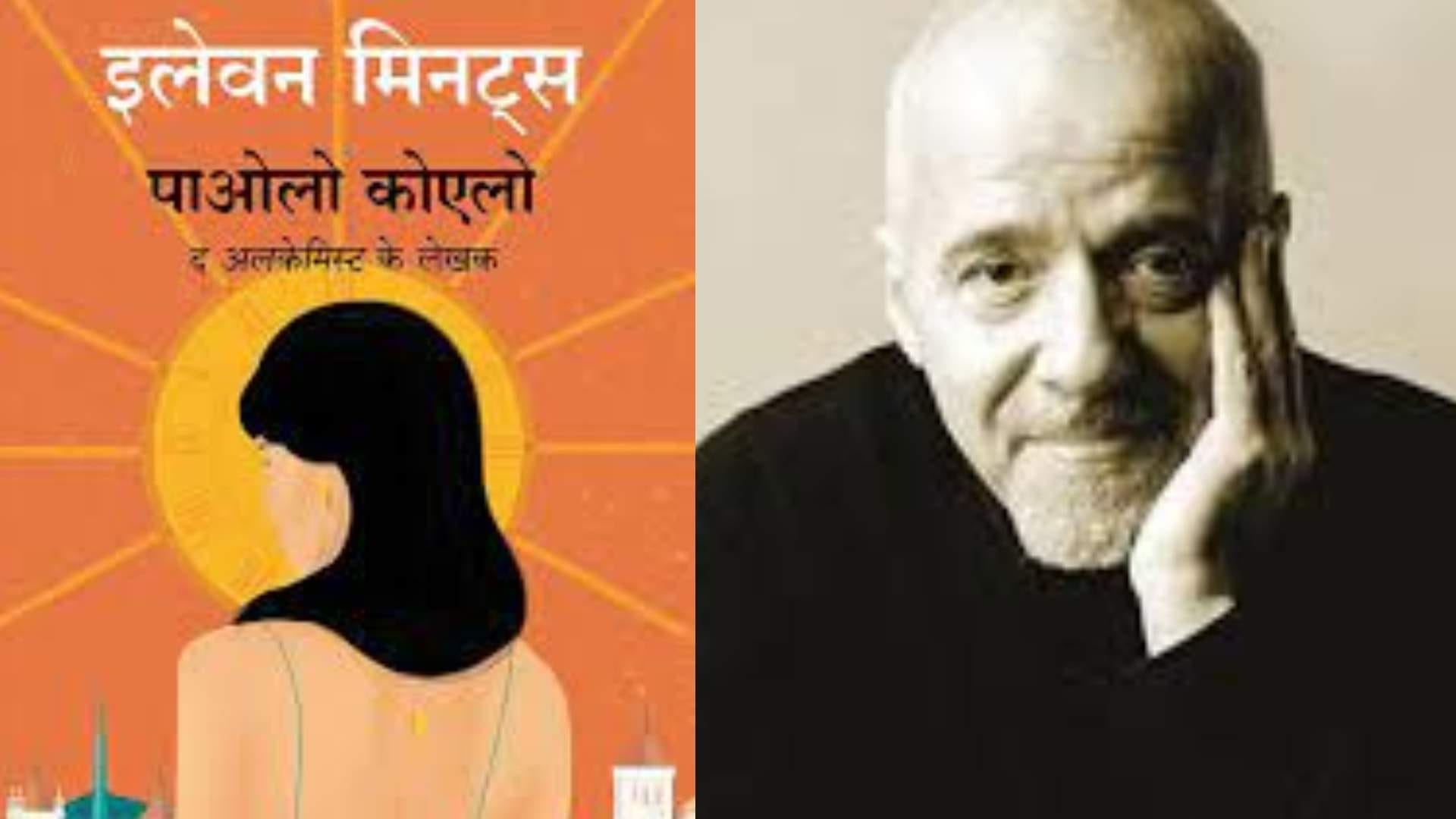जब कहीं स्त्री के साथ हुए यौन उत्पीड़न पर बहस उठती है तो बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि जिस समय यौन उत्पीड़न की घटना स्त्री के साथ हुई थी उसी समय स्त्री ने क्यों नहीं कहा, तभी क्यों नहीं उस हिंसा का विरोध किया। यौन शोषण पर स्त्री के प्रतिरोधों को फर्जी कहते हुए बहुत सहजता से कहा जाता है कि तब क्यों नहीं कहा। यह उपन्यास उस “तब क्यों नहीं कहा, का एक जबाब भी है। ऐसे सतही और संवेदनहीन सवाल करने वालों को ये उपन्यास पढ़ना चाहिए और स्त्री से किया गया उनका सवाल “तब क्यों नहीं कहा, का यहां बहुत ठोस जबाब मिलता है।
उपन्यास ‘काला जल’ तीन पीढ़ी की स्त्री की यातना का ऐसा दस्तावेज है कि पढ़ते हुए लगता है कि इन सारी स्त्रियों को, इनकी पीड़ा को तो खूब हमने देखा है लेकिन उपन्यासकार जैसे देख पाया उस संवेदना की दृष्टि से हम नहीं देख पाये थे। ये उपन्यास स्त्री जीवन के उन आधारों को रेखांकित करता है जिनके लिए वह सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और मर्यादाओं में जकड़ी, घुटती रहती है। अपने साथ हुए अन्याय को लेकर समाज से इतनी भयाक्रांत है कि अक्सर वो खुद को ही उस अपराध के लिए दोषी मान लेती है।
इस उपन्यास की भूमिका में राजेंद्र यादव ने लिखा है कि यह पढ़ते हुए मुझे बार-बार सत्यजीत राय की फ़िल्म ‘अशनि संकेत’ का ख़याल आता रहा।
उपन्यास ‘काला जल’ तीन पीढ़ियों पर आधारित है और तीन खंडों में बांटा गया है: लौटती लहरें, भटकाव और ठहराव। ध्यान से देखने पर लगता है ये सिर्फ उपन्यास का खंड नहीं है पूरे भारतीय समाज का सच भी यही तीनों खंड हैं। इस उपन्यास की भूमिका में राजेंद्र यादव ने लिखा है कि यह पढ़ते हुए मुझे बार-बार सत्यजीत राय की फ़िल्म ‘अशनि संकेत’ का ख़याल आता रहा। साल 1943 के बंगाल के अकाल के प्रारंभिक दिनों का शहर से निकट छोटा सा गाँव। कहानी एक परिवार की है और गाँव की। चावल, चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि चीजें गायब होने लगीं हैं बेकारी और भुखमरी की छायाएं गहराने लगीं हैं लेकिन फ़िल्म का निर्देशक है कि बार-बार लहलहाते खेतों, मीलों फैले हरे भरे जंगलों, नदियों, फूलों, बौरों और सुबह की खिलती हुई धूप, साँझ के सिंदूरी-साँवले आसमान को ही चटक गहरे रंग में दिखाये चला जाता है। पूरी फिल्म में कैमरा बार-बार एक ही सवाल पूछता है इस अथाह और अपार प्राकृतिक समृद्ध सम्पदा के बीच अकाल?? जैसे अपने आप उत्तर भी उजागर हो रहा है ये अकाल नहीं खड्यंत्र है।
उपन्यास में छोटी फूफी और सल्लो आपा के जीवन का एकतरह से आपस में अंतर्विरोध चलता है लेकिन विडंबना ये है कि अंत दोनों का शून्य है। बदलाव के लिए छटपटाते मोहसिन का जीवन भी एक समय बदलाव की ओर जाने को बेचैन है लेकिन अंततः भटकाव की तरफ मुड़कर संताप की ओर चला जाता है। उपन्यास में नायडू का चरित्र एक मशाल की तरह उभरता है लेकिन जाने क्या अभिशाप है इस माटी में की वो मशाल भी अंत तक बुझ जाती है। रशीदा, जाहिरा, छोटी फूफी, सालिहा जैसे सारे स्त्री पात्र समाज मे अभी भी ठीक उसी हालत में रहते हैं जैसे इस उपन्यास में सौ साल पहले रहते थे। सल्लो आपा की मौत उसी तरह हुई जैसे अब भी हमारे यहाँ जाने कितनी लड़कियों की मौत होती है। उपन्यास स्त्री जीवन के जितने कोने अन्तरे में भरे अंधेरे हैं सब में ताकता-झाँकता रहता है।
रशीदा का जीवन जिसतरह से नष्ट हुआ वो बेहद मार्मिक और वीभत्स है। यौन हिंसा के कारण उसने अपने शरीर को जगह-जगह जला डाला था। इस तरह खुद को जला-भूनकर वो शायद समझ रही थी कि खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा।
समाज में रज्जू मियां जैसे पात्र आजीवन स्त्री अपराध करते हैं और एक सभ्य सामाजिक जीवन जीते हैं। उपन्यास पढ़ते हुए किसी पात्र को पढ़कर कोई अचरज या कौंध नहीं होती, लगता इन सबको हम हमेशा देखते आये हैं। बड़ी बी को रज्जू मियां के सारे अपराध पता हैं लेकिन उन्होंने उसका कहीं कोई प्रतिरोध नहीं किया। समाज की कंडीशनिंग स्त्रियों को इसका अभ्यास कराती है कि वो पुरूष के अपराध को कैसे देखे। अपराध करने वाला पुरूष परिवार का है तो स्त्रियां आजीवन उसके विरुद्ध मुँह नहीं खोलतीं। उपन्यास के एक अंश में बड़ी बी रज्जू मियां पर नाराज होकर कहती हैं कि अब तुम मेरा मुंह न खुलवाओ वरना तुम्हारी सारी शराफत यहीं खोलकर रख दूंगी। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लाल पीले हो रहे हो, और कोई भी आये-जाये तुम्हें ताक-झांक करने की क्या जरूरत है, यही है शराफत, कहे देती हूं मुझसे तुम्हारा कुछ भी छुपा नहीं है, राई-रत्ती हाल जानती हूँ। अरे शराफत होती तो उसी दिन चुल्लू भर पानी में डूब मरे होते जिस दिन भी जाने क्या कहने जा रही थीं और जाने क्या कह जाती पर बड़ी कठिनाई अपने को उन्होंने रोका।
ये भारतीय समाज के परिवार में ढली स्त्री का चेहरा है वो सारे अपराधों को जानते हुए भी चुप रहती है और रज्जू मियां जैसे यौन-कुंठित मानसिकता के मनुष्य उसका फायदा उठाते हैं। उपन्यास की पात्र रशीदा का जीवन जिसतरह से नष्ट हुआ वो बेहद मार्मिक और वीभत्स है। यौन हिंसा के कारण उसने अपने शरीर को जगह-जगह जला डाला था। इस तरह खुद को जला-भूनकर वो शायद समझ रही थी कि खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा। रशीदा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जिस्म बदसूरत हो जाये, इतना बदसूरत कि उसमें हाथ तक न लगाया जा सके। एक रात उसने अपनी देह पर मिट्टी का तेल डालकर जल कर मर गयी।
उपन्यास का ये अंश पढ़ते हुए मेरा ध्यान गया कि समाज, स्त्री को इस तरह के अपराध के रूप में जिम्मेदार मानकर अक्सर उसे मरने की सलाह देता है । कोई स्त्री जब कभी अपने ऊपर हुए इस तरह के जुल्म की बात गाँव, घर-परिवार के सामने लाती हैं तो स्त्रियां कहतीं कि “क्या तालाब और कुएं भी नहीं रह गए थे दुनिया में तुम्हारे लिए। जैसे इस तरह स्त्री के लिए खुद की जान लेने को एक परम्परा बना दिया गया हो और आज भी इसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ। सल्लो आपा की मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी वो सीधे-सीधे समाज परिवार द्वारा की गई हत्या थी। विवाह से पहले गर्भवती लड़की की गर्भसमापन कराने में की गई हत्या का हिसाब हो तो समाज का चेहरा खून से सराबोर मिलेगा। छोटी फूफी अपने ससुराल में कितने अत्याचार सहती हैं लेकिन उससे कभी वो भयभीत नहीं होतीं लेकिन जब ससुर रज्जू मियां की बुरी नज़र देख लेती हैं तो भय से कांप जाती हैं और जब एक बार जब रज्जू मियां ने हद पार करनी चाही तो छोटी फूफी अपने पति को बताना चाहती हैं लेकिन वो छोटी फूफी को ही लताड़ता है, एक संवेदना से रहित समाज में सामन्ती पुरूष ऐसा ही हो जाता है।
उपन्यास के एक अंश में बड़ी बी रज्जू मियां पर नाराज होकर कहती हैं कि अब तुम मेरा मुंह न खुलवाओ वरना तुम्हारी सारी शराफत यहीं खोलकर रख दूंगी । मैंने ऐसा क्या कह दिया कि लाल पीले हो रहे हो, और कोई भी आये-जाये तुम्हें ताक-झांक करने की क्या जरूरत है, यही है शराफत, कहे देती हूं मुझसे तुम्हारा कुछ भी छुपा नहीं है, राई रत्ती हाल जानती हूँ।
स्त्री जीवन की तमाम त्रासदी को दर्ज करते हुए ये उपन्यास धार्मिक सौहार्द और समरूपता को भी दर्शाता है जहाँ अलग-अलग धर्म संस्कृति के लोग एक साथ बिना किसी भेदभाव के एकदूसरे के पर्व और त्योहारों को मनाते हैं। आत्मालाप की शैली में बब्बन कहते हैं कि बचपन मे होली का त्योहार कितने उत्साहपूर्वक आता था। जानते हुए भी कभी इस बात का अहसास नहीं हुआ कि ये त्योहार हमारे लिए नहीं है। उतने ही उमंग से बाल्टियां भर-भर के रंग तैयार होता और एकदूसरे को रंगने से ज्यादा रंग तैयार करने में रस आता।
साहित्य की दुनिया में काला जल उपन्यास को लेकर जो एक विशेष मन्तव्य है कि भारतीय मुस्लिम समाज ख़ासकर स्त्रियों की दशा के भीतरी यथार्थ को उसकी पूरी विडम्बना और विभीषिका के साथ जिस सूक्ष्मता से पेश करता है वह हिंदी के उपन्यासों में इस उपन्यास से पहले नहीं लिखा गया था । उपन्यास कथानक के संदर्भ में राजेन्द्र यादव ने लिखा था कि लगता है कि ये निम्नमध्यवर्गीय भारतीय मुस्लिम परिवारों की कहानी है लेकिन इस उपन्यास की ये भी विशेषता है कि इसे भारत के किसी भी हिस्से के परिवेश में रख दो एकदम फिट बैठता है।
उपन्यास एक घुटते हुए परिवेश में गहरे अवसाद जैसे रंग अपने दृश्य में चलते रहते हैं लेकिन फिर भी बेहद सजीव और जीवंत लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने बंद दायरे में घुटते-टूटते इस उपन्यास के किरदारों में कोई इस जकड़न को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, करता है लेकिन फिर वो अपनों के बीच अकेला पड़ जाता है। और परिणाम ये होता है कि इस जमे हुए काले जल में कई बार हलचल होने के वावजूद उसकी सड़ांध दूर नहीं होती । ये हमारे परम्परागत रूढ़िवादी समाज का सत्य है ।
काला जल उसी समाज की सड़ांध को चिन्हित करते हुए बदलाव के लिए एक मौन चीत्कार भी करता है। वो बताता है कि काला जल सिर्फ वही नहीं है जो किसी एक ताल में सड़ रहा है जिसकी दुर्गंध का अजगर पूरे परिवेश को लपेट रहा है, यह वह जीवन-प्रणाली भी है जिसमें अमानवीय और प्रगतिविरोधी मान्यताओं और मूल्यों की असहनीय सड़ांध ठहरी हुई है। उपन्यास पढ़ते हुए सारे स्त्री पात्र हमें इतने चीन्हे-जाने लगते हैं कि सबके दुःख अपने लगते हैं उनकी वेदना इतनी अपनी लगती है कि लगता है कि क्या संसार की सारी स्त्रियों की यातना का रंग एक है। कोई भूगोल कोई संस्कृति या धर्म हमारे दुखों को बदल नहीं पाया ,हम सदियों से चल रहे हैं अपनी दुनिया की ओर जाने के लिए लेकिन पितृसत्ता और पूँजी हमारे कदमो में बेड़ियाँ डालते रहते हैं हमें पीछे की ओर धकेलते रहते हैं।