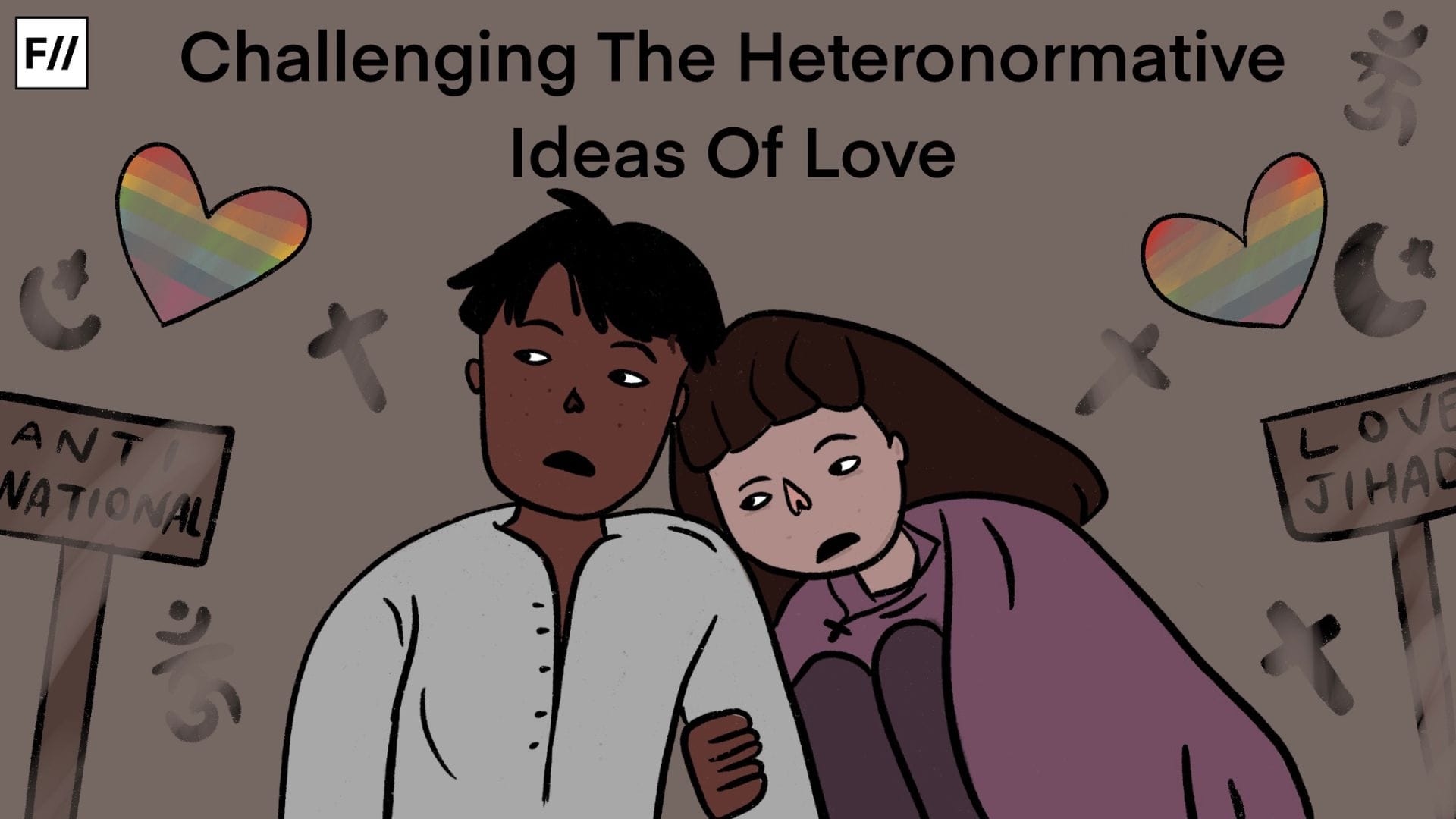घरेलू कामागार से लेकर रेडा-पटरी से सामान बेचने तक, खेतों में मजदूरी, खदान से लेकर ऊंची इमारतों में रेत-सीमेंट ढोने में महिला मजदूरों की असंगठित क्षेत्र में काम करने की भागीदारी बढ़ती जा रही हैं। भारत में 195 मिलियन महिलाएं असंगठित क्षेत्र या अवैतनिक श्रम से जुड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में कार्यरत ये महिलाएं बिना किसी सुविधा, श्रम कानून, सामाजिक लाभ जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या पेड सिक लीव की सुविधा के बिना काम पर रोज जाती हैं। इतना ही नहीं कार्यस्थल पर असुरक्षित माहौल और यौन उत्पीड़न तक का सामना करती है।
असंगठित क्षेत्र क्या है और उसमें काम करने वाली महिलाएं
असंगठित क्षेत्र की अलग-अलग और छोटी इकाइयां होती हैं, जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं। इसमें काम करने वाले लोगों को कम वेतन मिलता है और रोजगार अनियमित होता हैं। खेती मजदूरी, घरेलू कामगार, मजदूरी, ईट-भट्टे पर मजदूरी और अन्य काम इनमें शामिल है। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को दिहाड़ी और काम के हिसाब से मजदूरी मिलती है यानी जितना काम उतना पैसा।
संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार वैश्विक दक्षिण के 31 देशों में, गरीबी में रहने वाली 1 फीसदी से भी कम महिलाओं की चाइल्डकेयर तक पहुंच हैं। यही वजह है कि सुविधाओं के अभाव की वजह से ये महिलाएं अपने काम करने की खतरे से भरी जगह पर छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाती हैं।
असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति ऐसी है कि श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसे में महिलाओं की स्थिति और भी नाजुक और दयनीय हो जाती है। देश मे लगभग 94 फीसदी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत्त हैं और केवल 20 फीसदी ही शहरी केंद्रों पर कार्यरत है। आंकड़ें साफ जाहिर करते हैं कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रही हैं लेकिन जब बात इन महिलाओं के कार्यस्थ्ल पर सुविधाओं की आती है तो वह इनके लिए शून्य है।
धूल-मिट्टी, तपती धूप हर स्थिति में काम करती इन मजदूर महिलाओं को उस तरह से कामकाजी माना ही नहीं जाता हैं जिस तरह से दफ्तर जाने वाले अन्य लोगों और महिलाओं को माना जाता है। इस वजह से कार्यस्थल पर उन्हें वो सुविधाएं नहींं मिलती हैं जो एक कामकाजी, नौकरी करने वाली महिला को मिलनी है। मजदूरी, छोटा-मोटा काम करके अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी देने वाली इन कामकाजी महिलाओं कर्मचारियों को शौचालय और पीने के साफ पानी तक की पहुंच नहीं है।
काम की अन्यायपूर्ण स्थिति के साथ-साथ इन महिलाओं के बच्चों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। श्रम के बाजार में लैंगिक समानता के लिए मुख्य बाधाओं में से एक चाइलकेयर सेवाओं की कमी है। संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार वैश्विक दक्षिण के 31 देशों में, गरीबी में रहने वाली 1 फीसदी से भी कम महिलाओं की चाइल्डकेयर तक पहुंच हैं। यही वजह है कि सुविधाओं के अभाव की वजह से ये महिलाएं अपने काम करने की खतरे से भरी जगह पर छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाती हैं। वीमन इन इनफॉर्मल एम्पलॉयमेंट ग्लोबलाइज़िंग और ऑरगनाइजिंग के द्वारा हुए अध्ययन के अनुसार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाएं मातृत्व अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकेयर तक की पहुंच के बिना अधिक असुरक्षित जगहों पर काम करती हैं।
इस तरह की इन महिलाओं को कठिनाइयों और ट्रामा के साथ अपने बच्चों की देभभाल करना और ब्रेस्टफीडिंग करनी पड़ती है। समाज में हाथिये पर रहने को मजबूर और तथाकथित निम्न जाति और समुदाय से ताल्लुक रखने वाली इन महिलाओं के बच्चों के लिए नीतियां न के बराबर है। बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम न होने की वजह से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार हर तरह के विकास पर प्रभाव पड़ता है। शहरों में मजदूरी करने वाली महिला की बड़ी संख्या प्रवासियों की भी है। घर-परिवार में कोई और न होने की वजह से ये महिलाएं काम की जगह पर नवजात बच्चे को भी साथ रखती नज़र आती हैं।
कामकाजी महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा के लिए नीतियां
देश में कामकाजी महिलाओं और उनके बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए नैशनल क्रेच स्कीम (पूर्व में राजीव गांधी नैशनल क्रेच स्कीम) के तहत केंद्र राज्य और केंद्रशासित राज्य की कामकाजी महिलाओं के छह महीने से लेकर छह साल तक के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा मुहैया कराती है। इसके तरह के डे केयर में बच्चे को सुलाना, तीन साल से छह साल से कम उम्र के बच्चे को प्री स्कूल शिक्षा, न्यूट्रिशन स्पलीमेंट, ग्रोथ मॉनिटरिंग और हेल्थ चैकअप जैसी सुविधाएं शामिल है।
बच्चों की सुरक्षा के लिए सुविधा न होने की वजह से महिलाएं लैंगिक भूमिका के तहत सौंपे काम\जिम्मेदारियों की वजह से अपना काम छोड़ने को मजबूर होती है। दूसरी तरफ गरीब और मजदूरी करने वाली माँएं अपनी काम की जगह ही बच्चों को लेकर जाती है। ये कामकाजी महिलाएं बच्चों की डे केयर जैसी सुविधाओं से पूरी तरह अनजान होती है। साथ ही हाशिये के समुदाय से आने वाली और निम्न आय की वजह से फैक्ट्री या छोटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं की पहुंच चाइड केयर के लिए बने उन विकल्पों से दूर है जो निजी स्तर पर चलाए जाते हैं।
“देखो यही अंतर है कि ना चाहते हुए भी छोटी उम्र में बच्चों को काम के वास्ते छोड़कर आना पड़ता है। मेरे मन में हमेशा ठीस रहती थी लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता था। साइड में बैठकर बच्चे को दूध भी पिलाया है, ग्राहक भी संभाले है और घर के अन्य सारे काम भी किये है।”
मजदूरी करने वाली महिलाएं सरकार के द्वारा चलाई जानी वाली योजनाओं से भी अपरिचित है। इंटरग्रेटिड चाइल्ड डेवलेंपमेंट स्कीम (आईसीडीएस) के तहत ही प्राथमिक तौर पर आंगनवाड़ी केंद्र भी आते हैं जो मातृत्व और पोषण सुरक्षा, बच्चें की शुरुआती शिक्षा जैसी सुविधा प्रदान कराते हैं। हालांकि आईसीडीएस की दो मुख्य सीमाएं हैं। पहला, यह तीन साल से कम उम्र के बच्चों को पूरा नहीं करती है। दूसरा, यह दिन में केवल कुछ घंटे के लिए काम करता है जो काम के समय बच्चे को भेजने और लाने में असुविधा करती है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों के समय और बच्चों के दाखिले को बढ़ाने के दोहरे लाभ हो सकते है जो माँओं को वैतनिक काम करने की अनुमति देता है साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शुरुआती बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान को पूरा करती है।
कामकाजी महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा के लिए क्रेच की सुविधा के लिए नीतियों को व्यापक रूप से हर वर्ग तक पहुंचाने के रूप लागू करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्रेच कम आय वाली आवासीय बस्तियों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य कार्यस्थल के करीब होने चाहिए जिससे माँएं अपने छोटे बच्चों को समय पर ब्रेस्टफीडिंग भी करा सकें।
फैक्ट्रियों, छोटे उद्योग इकाईयों, ईट बनाने, इमारत बनने, कृषि मजदूरी जैसी जगहों पर महिला मजदूरों के काम करने वाली जगह पर बच्चे को साथ में रखने, पीठ पर बच्चा बांधे जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। अक्सर भावनाओं से जोड़कर देखते हुए इन तस्वीरों में मातृत्व का महिमामंडन किया जाता है। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है कन्स्ट्रक्शन साइट पर छोटे बच्चे को ले जाना, साड़ी के टुकड़ो के झूलों में तपती धूप में सुलाना केवल योजनाओं और आर्थिक क्षमता का अभाव है। क्योंकि मजदूरी करने वाली महिलाओं को कामकाजी उस तरह से नहीं माना जाता है जिस तरह से दफ्तर जाने वाली कम्प्यूटर पर काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारियों को माना जाता है। गरीब मजूदर महिलाओं के लिए न कार्यस्थल पर उपलब्ध बेसिक सुविधाएं है और नहीं मातृत्व के नाम पर मैटरनिटी लीव जैसा कोई प्रावधान है। क्योंकि मजदूरी के काम के स्टक्चर में एक दिन की छुट्टी मतलब कोई काम नहीं होता है न ही कोई पैसा होता है। इसलिए गरीब महिलाएं गर्भावस्था के बाद जल्द से जल्द अपने काम पर बच्चों के साथ लौटती दिखती हैं।
“मन तो नहीं करता था लेकिन बच्चे को छोड़कर आना पड़ता था”

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर जिले के कूकड़ा गांव की रहने वाली संजयबीरी शहर में स्थित गुड मंड़ी में मजदूरी करने वाली महिला हैं। उनकी उम्र पूछने पर वह कहती है कि उम्र का पता नहीं है लेकिन पिछले 18-19 साल से मजदूरी करती आ रही हैं। जब उनके बच्चे छोटे थे तब से ही मंड़ी में आड़ती की दुकान पर काम कर रही है। वह मंड़ी में अनाज बेचने आने वाले किसानों के फसल की सफाई, समान ढोना, फसल की ब्रिकी के बाद दुकान के सामने झाडू लगाने जैसे काम करती है। आज भी उन्हें किसानों की फसल साफ करने के बदले में गेहूं या चावल ही मिलता है न की कोई पैसा। काम के बदले कितना मिलेगा यह तय करने वाला भी किसान या आड़ती होता है।
संजयबीरी से उनके काम और बच्चे के पालन-पोषण के अनुभवों पर बात करने के दौरान उनका कहना है, “जब बच्चे छोटे थे हम तब भी काम पर आते थे। मजदूरी में छुट्टी कुछ नहीं होती है। काम नहीं मिलता, फसल का सीजन नहीं होता, बारिश होती है तो काम नहीं होता है तो ही समझो छुट्टी है। हमने बच्चों को भी पाला और मजदूरी साथ-साथ ही की है। शुरू में सुबह बच्चे को दूध पिलाकर आ जाते थे और शाम को ही जाकर पिलाते थे। कई बार तो यह सोचकर उस समय बुरा भी लगता था कि टाइम पर अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिला पाए। एक वक्त़ बाद तो बस घर जाकर जल्दी से बच्चे को दूध पिलाने की भी लगती थी। बाद में कई बार यहां भी साथ में लाए। कपड़ा बिछाकर बैठा देते थे, कुछ चीज दिला देते थे वे खेल में लग जाते थे। पेड़ की टहनी तोड़ कर दे दी उससे खेल में लग जाते थे। बस ऐसे ही पाला हमने तो बच्चों को। सुबह आने से पहले सारा काम किया, दोपहर की रोटी बनाकर आए क्योंकि शाम को ही घर वापस जाया जाता है। फिर दो गेहूं के दानों का लालच भी रहता है और यह सब भी सिर्फ बच्चों के पेट भरने के लिए ही किया। मन तो नहीं करता था बच्चे को ऐसे छोड़ कर आने का लेकिन करना पड़ा।”
“छोटी उम्र में बच्चों को काम के वास्ते छोड़कर आना पड़ता है”

मुज़फ़्फ़रनगर जिले की रहने वाली गुलमाला सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाती हैं। पति की मृत्यु के बाद वह पूरी तरह से अब ये काम कर रही हैं हालांकि पहले वह ये काम पूर्णरूप से नहीं करती थी। काम और बच्चे को पालने के अनुभव पर बात करते हुए उनका कहना है, “देखो यही अंतर है कि ना चाहते हुए भी छोटी उम्र में बच्चों को काम के वास्ते छोड़कर आना पड़ता है। मेरे मन में हमेशा ठीस रहती थी लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं किया जा सकता था। साइड में बैठकर बच्चे को दूध भी पिलाया है, ग्राहक भी संभाले है और घर के अन्य सारे काम भी किये है।”
“एक ख्वाहिश मेरी भी है कि मेरा बच्चा मजदूर न बने”
मुज़फ़्फ़रनगर जिले के अलमासपुर की रहने वाली मुनिया (बदला हुआ नाम) मंड़ी में फसल ढ़ुलाई, सफाई का काम करती हैं। उनका कहना है, “काम करते हुए वह अपने दोनों बच्चों को भी पाल रही हैं और घर भी संभाल रही है। एक हाथ में बच्चा और एक हाथ से काम भी किया है। तमाम तरह की परेशानी झेली है और चुप रहकर सब किया और ऐसे ही कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चा आराम की जिंदगी जिए, अच्छा खाएं और आगे जाकर कुछ अच्छा करे। इन्हीं सब बातों को सोचकर बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद में काम पर आ गई ताकि ज़रूरतों के लिए और पैसा जोड़ लूं। सुबह दूध पिलाकर आ जाती थी, कई बार तो बीच में छाती में दूध आ जाता था और कोई काम नहीं होता था तो बीच में भी भागी-भागी दूध पिलाने घर चली जाती थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं बच्चे को कभी भी अपने काम पर लाऊं लेकिन मजबूरी में लाना भी पड़ा। मजूदर है लेकिन एक ख्वाहिश हमारी भी होती है कि कम से कम हमारा बच्चा मजदूर न बनें। उसे कोने में बैठाकर दिनभर यहां धूप-धूल में रहना ना पड़े लेकिन कई बार ऐसा ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। फसल के सीजन पर ज्यादा काम होता है, सुबह जल्दी आ जाते है और देर तक काम करना पड़ता है। उस समय बैचेनी रहती है क्योंकि 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक काम करना और बच्चों को अपने से दूर छोड़ना केवल मजबूरी है। घर में और लोग हैं लेकिन माँ का मन तो अपने बच्चों में ही रहता है।”
भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला मजदूरों और कामगारों के बच्चों की देखभाल के लिए स्व-नियोजित सेल्फ एम्पलॉयडेट वीमंस एसोसिएशन (सेवा) अहमदाबाद में अपने सदस्यों की देखभाल के लिए एक चाइल्ड केयर चलाता है। सेवा से जुड़ी महिलाओं के सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हैं।
मजूदरी करने वाली इन महिलाओं ने अपने बच्चों की देखभाल करने, स्तनपान कराने और अपने काम करने के लिए बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। ये महिलाएं सालों साल से मजूदर करती आ रही हैं लेकिन मजूदर महिला और मातृत्व के दौरान उनके लिए विशेष सेवाओं और बच्चों के लिए डे केयर जैसी बातों से वे अनजान है। चाइल्ड केयर व्यवस्था के बारे में बताने पर इस सभी महिलाओं का एक कहना तो था कि अगर ऐसा होता तो हमारे बच्चे कितना अच्छा जीवन जीते और हम भी चिंतामुक्त रह कर काम करते। लेकिन आज भी बहुत ही छोट बच्चों की माँ जो मजदूरी कर रही हैं उनके लिए तंत्र में कोई व्यवस्था नहीं है।
द कन्वेशनन वेबसाइट में प्रकाशित लेख के अनुसार महिलाएं अब बदलाव की मांग कर रही हैं। औपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियनों के सहयोग से अनौपचारिक श्रमिक संगठन गुणवत्तापूर्ण पब्लिक चाइल्ड केयर सर्विस की मांग कर रहे हैं। घरेलू कामगार, रेहड़ी-पटरी वाले, बाजार में व्यापारी और कूड़ा बीनने वाले लीमा से बैंकाक तक नगरपालिका और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर राज्य उनकी बात नहीं सुन रहा तो वह खुद समाधान निकालने की ओर बढ़ रहे हैं।
भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला मजदूरों और कामगारों के बच्चों की देखभाल के लिए स्व-नियोजित सेल्फ एम्पलॉयडेट वीमंस एसोसिएशन (सेवा) अहमदाबाद में अपने सदस्यों की देखभाल के लिए एक चाइल्ड केयर चलाता है। सेवा से जुड़ी महिलाओं के सभी बच्चे स्कूल में नामांकित हैं। जो महिलाएं अपने बच्चे को डे केयर में भेजती है वे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भी इच्छुक रहती है क्योंंकि उनके ऊपर शिक्षा पर खर्च करने का भार नहीं होता है साथ उनके ऊपर से बच्चों की देखभाल का तनाव भी खत्म हो जाता है।
लाखों की संख्या में महिलाएं बेहद कम रूपये के बदले दिन भर बाहर रहकर काम कर रही हैं। इस वजह से इनके बच्चों का बचपन असुरक्षित वातावरण और अधूरे पोषण में बीतता है। मजदूरी, खनन या अन्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को चाइल्ड केयर की सुविधा देना न केवल वक्त की आवश्यकता है बल्कि महिलाओं के श्रम के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। महिलाओं के कार्यस्थल या आसपास के क्षेत्र में चाइल्ड केयर की सुविधा होने की वजह से महिलाएं ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकलकर काम कर सकती हैं।