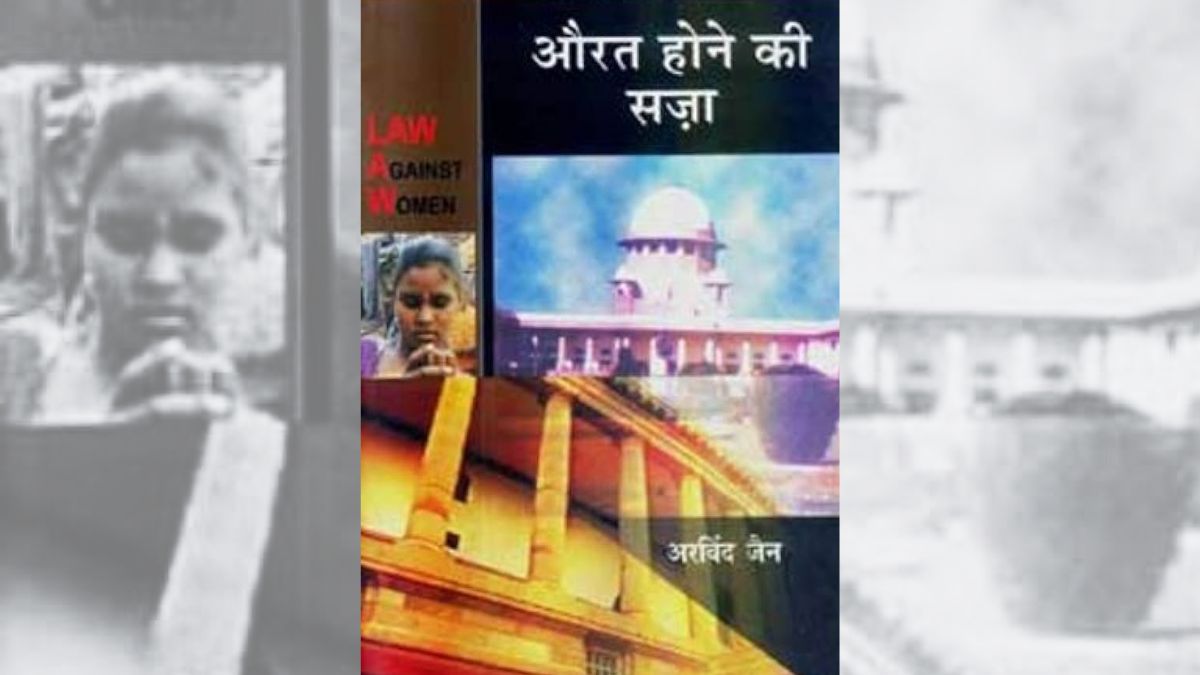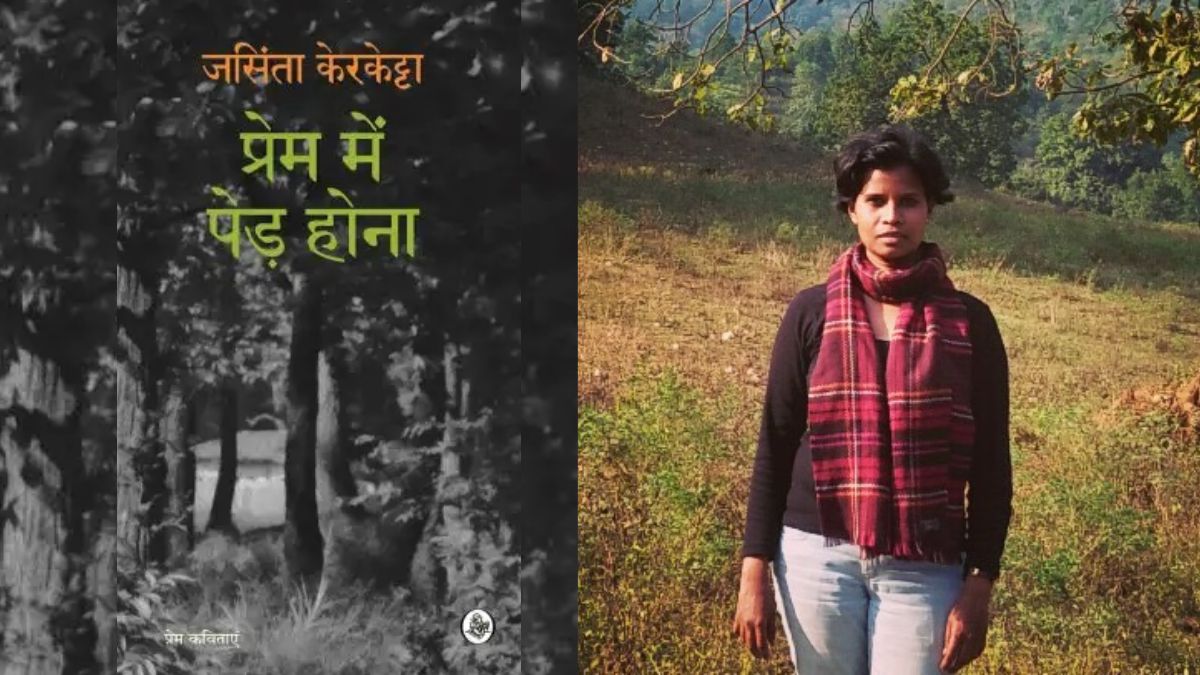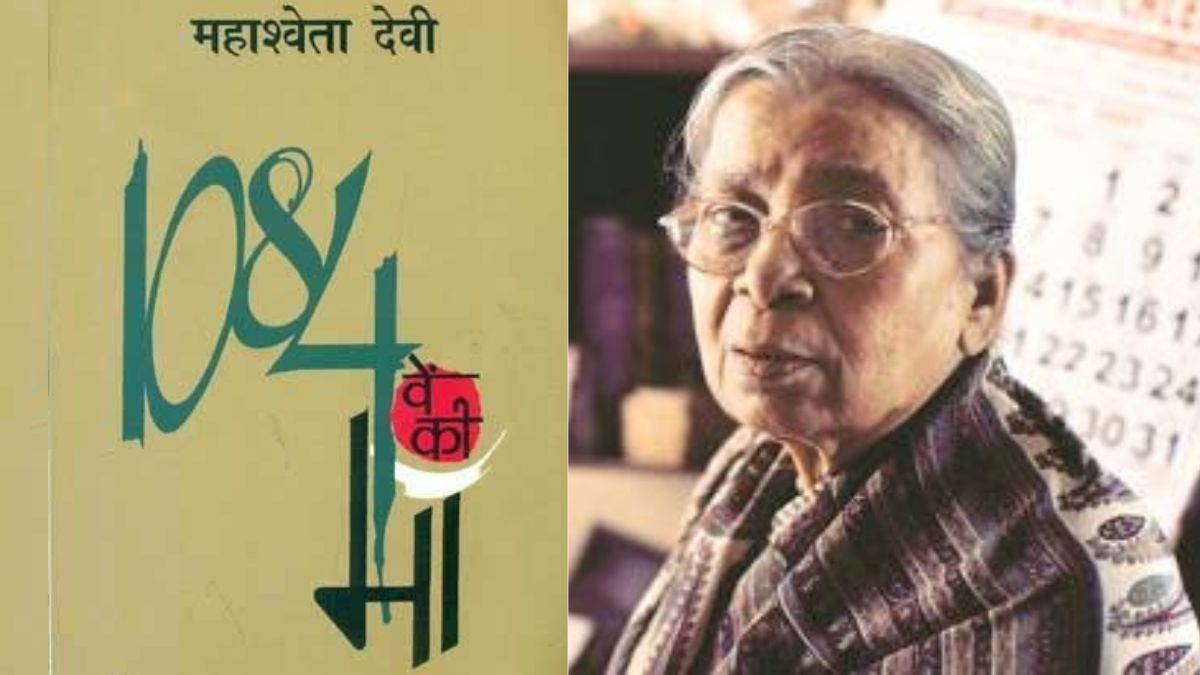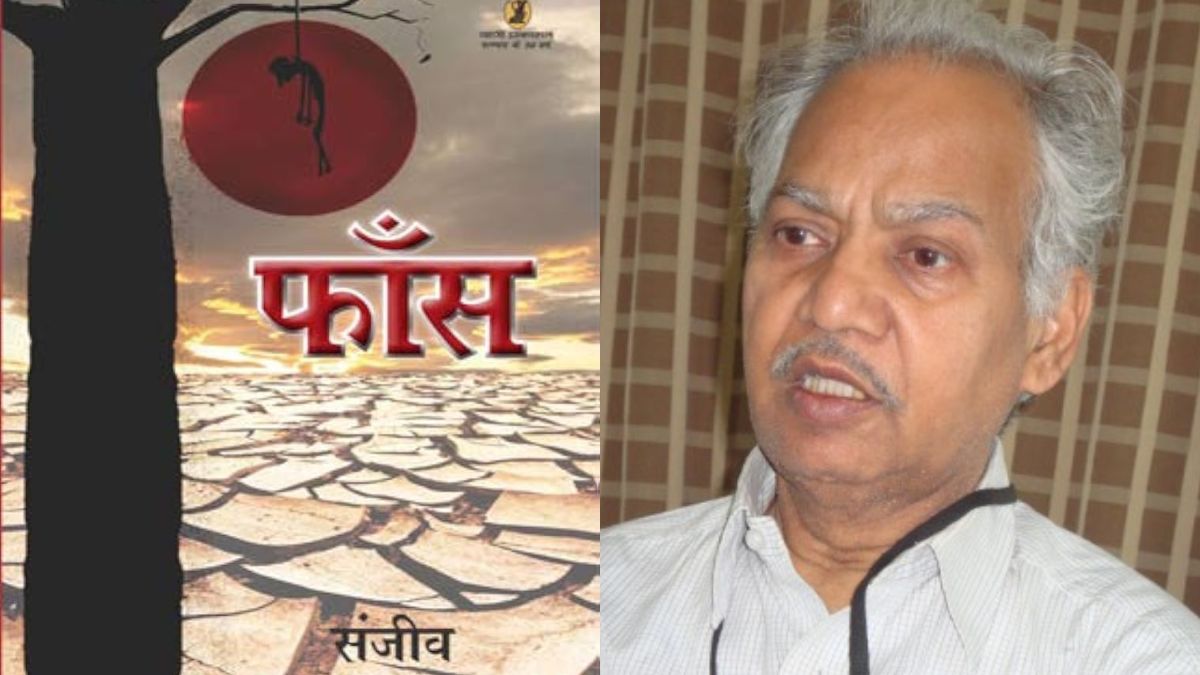‘औरत होने की सज़ा’ इस किताब की समीक्षा करते समय यही महसूस हो रहा है कि, क्या छोड़ दूं और क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा है। इस किताब के बारे हंस के एक सम्पादकीय में राजेंद्र यादव ने लिखा था, “कितना सही नाम रखा है अरविंद जैन ने अपनी किताब का ‘औरत होने की सज़ा।’ कहती रहिए आप सारे कानूनों को सामन्ती, सवर्णवादी या मेल-शावेनिस्टिक, हम क्यों आसानी से उस कानून में फेर- बदल करें जो हमारे ही वर्चस्व में सेंध लगाता हो?” अरविंद जैन का कहना है, “समाज ,सत्ता , संसद और न्यायपालिका पर पुरुषों के अधिकार होने की वजह से सारे कानून और उनकी व्याख्याएं इस प्रकार से की गई हैं कि आदमी के बच निकलने के हजारों चोर दरवाज़े मौजूद हैं जबकि औरत के लिए कानूनी चक्रव्यूह से निकल पाना एकदम असंभव।”
कानूनी प्रावधानों की चीर-फाड़ करते और अदालती फैसलों पर प्रश्नचिन्ह लगाते इस किताब के लेख कानूनी अंतर्विरोधों और विसंगतियों के प्रामाणिक खोजी दस्तावेज हैं जो गम्भीर अध्ययन, मौलिक चिंतन और गहरे मानवीय सरोकारों के बिना संभव नहीं। कानूनी पेचीदगियों को साफ, सरल और सहज भाषा में ही नहीं, बल्कि बेहद रोचक, रचनात्मक और नवीन शिल्प में भी लिखा गया है। किताब पढ़ने के बाद हो सकता है, आपको भी लगे, “अरे ऐसी भी कानून है? मुझे तो अभी तक पता नहीं था !” या फिर “हम तो सोच भी नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट से सजा के बावजूद हत्यारे सालों आज़ाद घूम सकते हैं।” किताब के पहले परिचय में वे स्त्रीवाद की सैद्धांतिकी पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि ‘स्त्रीवाद क्या हैं?’ सूत्र रूप में वह बताते हैं कि सामाजिक संरचना में व्यवस्थित रूप से स्त्री को निर्णयों में भागीदारी से वंचित किया गया है, स्त्री को दोयम बनाने वाली समस्त व्यवस्था में परिवर्तन स्त्रीवाद के मूल में है। इसमें वे हाशिये के विमर्शों के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारत में स्त्रीवादी आन्दोलनों को लेकर पुरुषों, राजनीतिज्ञों, न्यायालय के नियम कानून और मीडिया के कुटिल मुस्कान के साथ उपेक्षा किए जाने की पड़ताल करते हैं।
उन्होंने ‘स्त्रीवाद’ को एक राजनीतिक और दार्शनिक अवधारणा माना है। यह किताब समाज में व्याप्त रूढ़ियोंपर प्रश्न करती हैं, जो जैसा है वैसा ही मान लेना कदाचित उचित नहीं है और महिलाओं के परिस्थितियों को समझने के लिए झकझोर कर रख देती है। इस किताब को शुरू से अंत तक समझने के लिए, ख़ाका तैयार करके कुछ महत्वपूर्ण किस्सों को रेखंकित करना होगा। इस किताब का पहला अंक है, ’होई हे सोई जो पुरुष रचि राखा’ इस शब्द जाल से बहुत ही बारीक ढंग से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जा रहा रहा है कि किस प्रकार से महिलाए पुरुषों के तले दबी हुई है और निकलने के लिए छटपटा रही हैं। इसमें मूल रूप से औरतों के शोषण और समर्पण का व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है।
लेखक का मानना है, “स्त्रीवाद का पहला चरण स्त्री मुद्दों के राजनीतिकरण का ही दौर है जिनका राजनीतिकरण होता है, वे मुद्दें ध्यान पाते हैं और जिन्हें संस्कृति या निजी और घरेलू के नाम पर दबाया जाता है, वे दरअसल यथास्थिति को बनाए रखने के लिए नज़रअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि हम उन पर बात नहीं करना चाहते।”
इस किताब का केंद्रबिंदु पुरुष द्वारा संचालित कानून और पितृसत्ता है जिसे कटघरे में खड़ा करने का कार्य लेखक ने बखूबी किया है। यहां महिलाओं के दो रूप स्पष्ट होते हैं। एक तरफ़ जहां महिलाओं को पितृसत्ता के चंगुल में पहले फंसाया जा रहा है फिर उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है वहीं, दूसरी ओर क़ानून महिलाओं के मुद्दों को लेकर तार्किक होते हुए भी महिला विरोधी है और पुरुषों के बचाव के लिए एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं। यह किताब बताने में सफल होता है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी समाज में प्रेम का कोई स्थान नहीं है औरतों के लिए।
किताब में बापू के तीन बंदरों का भी ज़िक्र किया गया है। बंदर से तात्पर्य समाजिक प्राणियों से है। पहला बंदर, कानों पर हाथ धरे बैठा रहता है कुछ सुनता नहीं है। न जाने क्या- क्या बोलता रहता है। झूठे वादे, खोखले आश्वासन और हवाई घोषणाएं। क्या करे, किसी की भी तो नहीं सुनता मानता। दूसरा बंदर, सब कुछ देखता है और सबकी सुनता रहता है मगर बोलता कुछ नहीं है। और तीसरा, सालों बाद तो सुनता है और न मालूम कैसे कैसे बहुती फैसले सुनाता रहता है मगर देखता कुछ नहीं है। तीनों मिलाकर बहरा गूंगा और अंधा होने का नौटंकी करते रहते हैं। और तीनों बंदरों के सुरक्षित ओट में छिपा वह जो चौथा बंदर है जो सब कुछ देखता सुनता और बोलता है, मगर हमेशा भ्रामक और सनसनीखेज।
इस किताब का पहला अंक है, ’होई हे सोई जो पुरुष रचि राखा’ इस शब्द जाल से बहुत ही बारीक ढंग से पितृसत्तात्मक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया जा रहा रहा है कि किस प्रकार से महिलाए पुरुषों के तले दबी हुई है और निकलने के लिए छटपटा रही हैं। इसमें मूल रूप से औरतों के शोषण और समर्पण का व्यावहारिक विश्लेषण किया गया है।
अरविंद बताते हैं कि यहां से सोचना शुरू करता हूं तो पितृसत्ता रोज़ नया मुखौटा लगा सामने आ खड़ी होती है। कुछ समझ ही नहीं आता कि कहां कैसे क्या और क्यों हो रहा है? कौन है इस नौटंकी का सूत्रधार? इसी तरह के दिलचस्प अंकों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से शब्दों में गूंथा गया है। लिंग परीक्षण की दोधारी तलवार, बाल विवाह कानून में झोल, कन्यादान अनिवार्य नहीं, कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बदनामी का भय और खामोशी के खतरे, बनते कानून, टूटते परिवार, बच्चे का दावा, बच्चों पर माँ के अधिकार;कोख, कानून और क्रूरता, पिता पुत्री संवाद, गुजारा-भत्ते की समस्या, दूसरी औरत होने की सज़ा, सौतेला होने का मतलब, पितृत्व परीक्षण: न्यायपालिका धर्म संकट में; अदालती, अंधेरा और आधी दुनिया, आत्महत्या से मौत का मौलिक अधिकार, वधुओं को जलाने की संस्कृति, कितनी है बदनसीब नयना कफन के लिए, अश्लीलता: देह के दोराहे, व्याभिचारी कौन? बहन के नाम पाती,शोषण से दबी स्त्री देह, कैबरे और कानून, जीने का मौलिक अधिकार और बलात्कार, बचपन से बलात्कार, बलात्कार: पीड़ा की हार, गरीबी चरित्रहीनता है?
बलात्कार कुछ शांति प्रस्ताव और अप्राकृतिक यौन शोषण, यौन हिंसा और आंकड़ों का आतंक, यौन हिंसा और न्याय की भाषा, धर्मांतरण और संविधान, उत्तराधिकार या पुत्राधिकार इन सभी अंकों में लेखक के द्वारा बड़ी ही महीन कढ़ाई करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के लिए कानून मात्र ढकोसला है। यह किताब इस बात को साबित करने में सफल सिद्ध होती है। आज भी ज्यादातर औरतों के सिर पर घने काले बादल के साये मडरा रहे हैं। उनका भविष्य बच्चों को जन्म देने और परिवार का भरण-पोषण करने तक ही सीमित रह गया है। कानून की धाराएं औरतों को न्याय दिलाने से मुंह मोड़ ले रही है या मुंह मोड़ दिया जा रहा है यह हमें समझने को मिलेगा।
इस किताब का केंद्रबिंदु पुरुष द्वारा संचालित कानून और पितृसत्ता है जिसे कटघरे में खड़ा करने का कार्य लेखक ने बखूबी किया है। यहां महिलाओं के दो रूप स्पष्ट होते हैं। एक तरफ़ जहां महिलाओं को पितृसत्ता के चंगुल में पहले फंसाया जा रहा है फिर उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है वहीं, दूसरी ओर क़ानून महिलाओं के मुद्दों को लेकर तार्किक होते हुए भी महिला विरोधी है और पुरुषों के बचाव के लिए एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं।
लेखक का मानना है, “स्त्रीवाद का पहला चरण स्त्री मुद्दों के राजनीतिकरण का ही दौर है जिनका राजनीतिकरण होता है, वे मुद्दें ध्यान पाते हैं और जिन्हें संस्कृति या निजी और घरेलू के नाम पर दबाया जाता है, वे दरअसल यथास्थिति को बनाए रखने के लिए नज़रअंदाज किए जाते हैं, क्योंकि हम उन पर बात नहीं करना चाहते।” वह साफगोई से स्वीकार करते हैं कि स्त्रीवाद के अपने विरोधाभास है और स्त्रीवादी बहसें बहुत हद तक भटके हुए और गतिहीन हैं। इसके कारणों की पड़ताल करते हुए वह कहते हैं, “स्त्रीवाद कोई इकहरी विचारधारा नहीं है। अलग-अलग समय पर अपने अलग-अलग उद्देश्यों के साथ यह अलग-अलग शत्रुओं के खिलाफ उभरती रही है।” उनका मानना है कि नयी लड़ाइयों और नई चुनौतियों ने ही सोशलिस्ट स्त्रीवाद, व्यक्तिवादी स्त्रीवाद, अराजक स्त्रीवाद, ब्लैक स्त्रीवाद, दलित स्त्रीवाद, मार्कसिस्ट स्त्रीवाद, समाजवादी स्त्रीवाद, भौतिकतावादी स्त्रीवाद, लिबरल स्त्रीवाद, क्वीयर स्त्रीवाद, रैडिकल नारीवाद, ईको फेमिनिज़म जैसे विभिन्न स्त्रीवादी आन्दोलनों को जन्म दिया।
यह भारतीय समाज में स्त्रियों की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के साथ-साथ बदलते वैश्वीकरण के प्रभावों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करते हैं। इसमें संविधान द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत विभिन्न विद्वानों के विचार को समाहित करते हुए, आज़ादी से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात को रेखांकित करते हुए नारी के अतीत, वर्तमान, भविष्य को पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में परखते हुए भारतीय नारीवाद के संघर्ष के इतिहास को दर्ज करने की कोशिश करते है। इस किताब का सबसे आखिरी अंक है देश के मर्दों, एक होओ। इस नारे से इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा की पितृसत्ता किस तरह औरतों के रूप से डरने लगी है, पुरुषों को भय है कि राजनीतिक क्षेत्र के संसदीय प्रणाली में यदि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर सुनिश्चित हो गई तो सभी कानून उनकी सुविधा अनुसार बनाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं पुरुषों की वर्चस्वता एवं दादागिरी सीमट कर रह जाएगी।
यह किताब संतुलित तरीके से पितृसत्ता और कानून व्यवस्था की नाकामी प्रस्तुत करने में सफल होती है। अंत में किताब कुछ चुभते प्रश्न छोड़ जाती है। कुल मिलाकर किताब पितृसत्ता को स्त्री शोषण के मुख्य शत्रु यह के रूप में चिह्नित करती है; परिवार, समाज, धर्म, राजनीति सब उसके औजार हैं। किताब बेहद पठनीय है। भाषा में रवानगी है। सूक्तियों, मुहावरों व फ़िल्मी डायलॉग्स का प्रयोग भाषा को जीवंत बनाता है।
पुरुषों को भय है कि कहीं उन्हें चूल्हे में मुंह डालकर न जीना पड़े अर्थात रसोई घर में पुरुषों को हाथ न बंटाना पड़ जाए। वे कहते हैं कि जब महिलाएं भी सभी क्षेत्रों में सामान भागीदारी दर्ज कराएगी तो कहीं न कहीं पुरुषों को चुनौती देती फिरेंगी। इसी के चक्कर में आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में पास न हो सका। महादेवी वर्मा ने शृंखला की कड़ियां में लिखा है कि समाज ने स्त्री के संबंध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है की साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर संपन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कहीं जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन अर्थ की संबंध में सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की व्यवस्था के बंधन में बंधी हुई है।
कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और कही अपने स्वामित्व की सख्ती से लाभ उठाकर उसे इतना अधिक परावलम्बी बना दिया है कि वह उसकी सहायता के बिना संसार-पथ पर एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती। स्त्री आत्मकथा का दायरा बेहद व्यापक है एक किताब में समेटना असंभव है फिर भी प्रयास जबरदस्त है। इसीलिए समीक्षा में सभी अंकों को हाई लाइट करना मुश्किल हो रहा था। यह किताब संतुलित तरीके से पितृसत्ता और कानून व्यवस्था की नाकामी प्रस्तुत करने में सफल होती है। अंत में किताब कुछ चुभते प्रश्न छोड़ जाती है। कुल मिलाकर किताब पितृसत्ता को स्त्री शोषण के मुख्य शत्रु यह के रूप में चिह्नित करती है; परिवार, समाज, धर्म, राजनीति सब उसके औजार हैं। किताब बेहद पठनीय है। भाषा में रवानगी है। सूक्तियों, मुहावरों व फ़िल्मी डायलॉग्स का प्रयोग भाषा को जीवंत बनाता है।