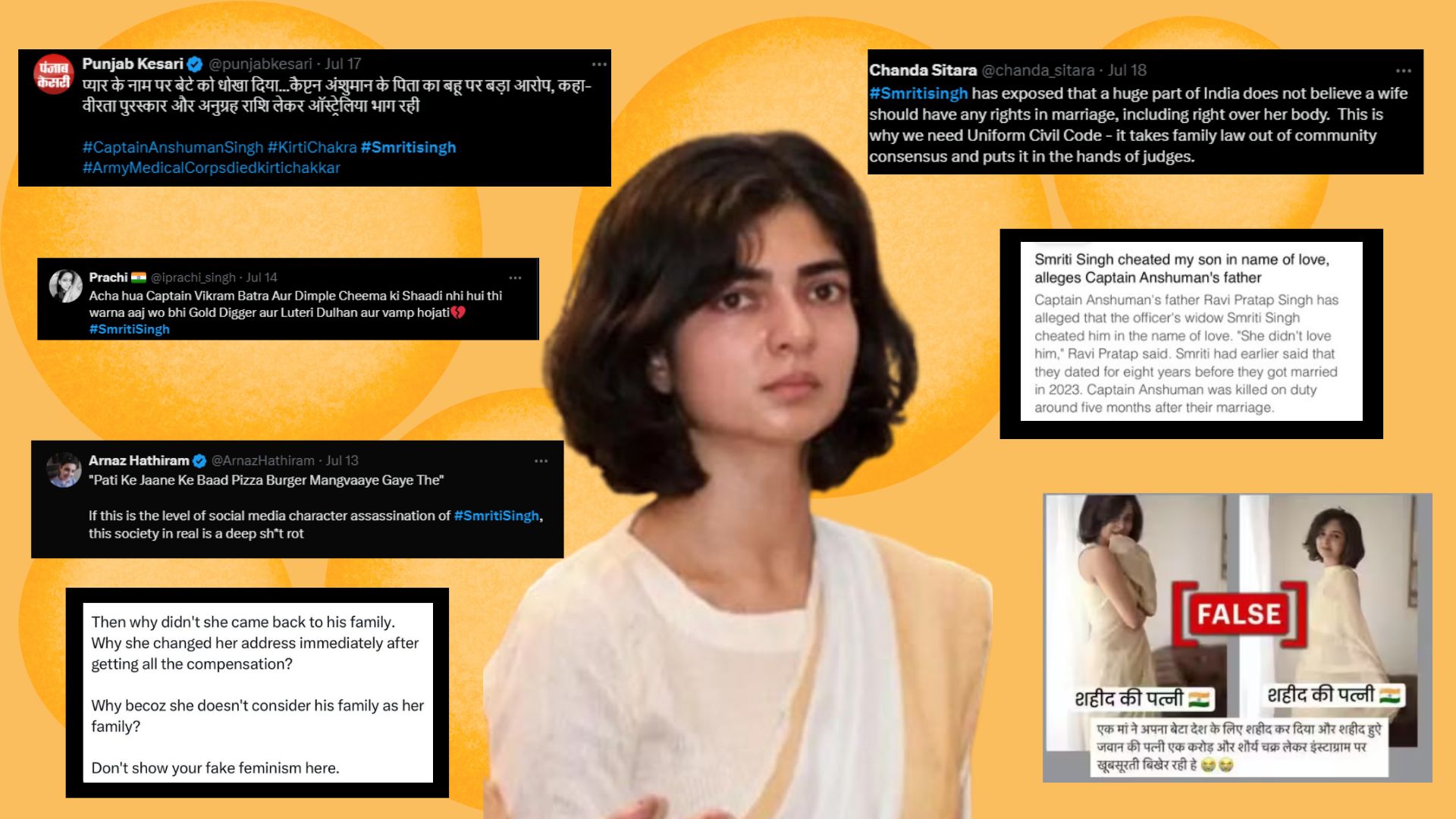अप्रैल 2014 में कार-स्कूटर दुर्घटना में जान गंवाने वाले दंपत्ति के परिजनों के मुआवज़े संबंधित केस में फैसला सुनाते हुए बीते 5 जनवरी 2021 को सुप्रीन कोर्ट ने कहा कि घरेलू काम करने वाली महिला के श्रम का मूल्य किसी मायने में उसके पति द्वारा कार्यालय में किए गए श्रम से कमतर नहीं आंका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस कथन को समाज के प्रगतिशील समूहों द्वारा महिला और पुरुष की सामाजिक भूमिका और आर्थिक बंटवारे को लेकर लगातार किए जाने वाले सवालों पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मानना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष के श्रम का विभाजन ऐतिहासिक रूप से चलता आ रहा विभेद है, जिसकी जड़ें आज के उत्तर-आधुनिक विश्व में भी उतनी ही मज़बूत हैं। जब भी घरेलू काम जैसे रोटी बेलने, कपड़े धुलने या झाड़ू लगाने की बात की जाती है, सहज भाव से हमारे मन में औरत का चित्र उभरता है। जब भी, परोपकार या सेवा भाव की बात की जाती है, तब भी ज़हन में औरतों की छवि ही आती है; यह इस तरह से सामान्यीकृत विचार बन चुका है कि स्कूलों की किताबों तक में पुरुष कार्यालय में दिखते हैं और औरतें किचन में; अक्सर ही हमें ‘सीता खाना पकाती है’ और ‘राम स्कूल जाता है’ जैसे उदाहरण देकर वाक्य-विन्यास और अनुवाद सिखाया जाता है; और तो और आपने ज़रूर ही वह गीत सुना होगा जिसमें मचलते हुए बच्चे गाते हैं ‘पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल’।
लब्बोलुआब यह है कि पिता हमेशा पैसा कमाने के लिए जाने जाते हैं, यानि उनके पास आर्थिक शक्ति है,इसलिए परिवार में शक्ति उसके पास है, समूची व्यवस्था का संचालक वह है और निर्णयात्मक क्षमता उसके हाथ में है। वहीं, एक औरत जो दिनभर घर में लगे रहने के बावजूद कुछ भी नहीं है। नेशनल स्टैस्टिकल ऑफिस द्वारा 2019 में जारी की गई रिपोर्ट ‘टाइम यूज़ इन इंडिया’ के अनुसार भारत में औसतन एक महिला हर दिन लगभग 299 मिनट की अवैतनिक घरेलू सेवाएं प्रदान करती है, वहीं पुरुषों के लिए यह मात्र 97 मिनट है। इस रिपोर्ट के अनुसार, घर के लोगों की देखभाल में एक औरत दिन के तकरीबन 134 मिनट लगाती है, वहीं पुरुषों के लिए यह मात्र 76 मिनट है। कुल मिलाकर, एक औरत अपने कुल समय व श्रम का क़रीब 16.9 फ़ीसद व 2.6 फ़ीसद भाग घरेलू अवैतनिक सेवा देने में लगाती है, वहीं उसके सहयोगी पुरुष के लिए ये आंकड़े मात्र 1.7 फ़ीसद व 0.8 फ़ीसद हैं।
और पढ़ें : क्यों हमें अब एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जो घर के काम में बराबरी की बात करे?
इसलिए, ज़रूरी हो जाता है कि औरतें द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का विश्लेषण केवल एक भावनात्मक आवरण में लिपटी त्याग मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अधिक खुलेपन के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में की जाए। इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। असलियत में, औरत को गृह-स्वामिनी या मालकिन भले ही कहा जाता है, लेकिन परिवार में उसकी भूमिका सीमित है। समाज, जिसकी केंद्रीय नियंत्रक शक्ति पितृसत्ता है, वह गृह-स्वामिनी जैसे अन्य कुछ और विशेषणों से लादकर औरत को भावनाओं में उलझा देता है और उन्हें सत्ता व निर्णयात्मक भूमिकाओं से बाहर कर देता है। यह पित्रसत्तात्मक साज़िश ही है, जिसके तहत औरतों को एकजुट नहीं होने के लिए वैचारिक-सामान्यीकरण का एजेंडा चलाया गया है जो यह प्रेषित करता है कि औरतें एक दूसरे की शत्रु हैं। यानी नाम के लिए तो औरतें गृहणी और गृह-स्वामिनी हैं, लेकिन संसाधन उनके पास नहीं हैं, उनका पति किसी भी समय उनपर ‘घर में बैठे रहने और ‘कुछ नहीं करने का’ आरोप लगाकर उनकी अवैतनिक मेहनत को नज़रअंदाज़ कर सकता है। इसलिए, ऐसे दौर में, जब समाज में बहुत से बदलाव आ रहे हैं, यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति भी बदलनी चाहिए, और इस दिशा में सोचने पर पहली चीज़ जो ध्यान में आती है, वह है-औरतों के श्रम का हिसाब।
चूंकि ऐतिहासिक रूप से औरतों के श्रम का कोई हिसाब नहीं दिया गया है और उन्हें संसाधनविहीन करके उनका शोषण होता चला आ रहा है। नारीवादी अक्सर ही इस विमर्श को उठाते रहे हैं। इस संबंध में ‘फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स’ की जनक मानी जाने वाली नारीवादी चिंतक मैरीलिन वेरिंग अपनी किताब ‘इफ़ वीमेन कॉउंटेड’ में बताती हैं कि अगर सभी मुल्कों की आधी आबादी के श्रम को जीडीपी में बदलकर देखें तो महिलाओं का अबतक का सारा मुफ़्त श्रम दुनिया के 50 सबसे ताकतवर मुल्कों की समूची जीडीपी के बराबर ठहरता है। निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ी ऐतिहासिक चोरी ही है। मानव सभ्यता के इतने लंबे इतिहास में बहुत से बदलाव आने के बाद भी औरतों की स्थिति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आने के पीछे कोई सोची-समझी गढ़ी योजना ही है, जिसको बदलकर सामाजिक न्याय स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन. वी रमना ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक़ क़रीब 159.85 मिलियन महिलाओं ने ‘घरेलू काम’ को अपने पेशे से रूप में दर्ज किया है, पुरुषों के मामले में यह आंकड़ा मात्र 5.79 मिलियन है। इस प्रकार, हम देख पाते हैं कि भारतीय महिलाओं की एक बड़ी आबादी घरेलू काम-काज में लगी हुई है, ऐसे में उनके श्रम का हिसाब दिया जाना चाहिए।
और पढ़ें : कामकाजी महिलाओं पर घर संभालने का दोहरा भार लैंगिक समानता नहीं| नारीवादी चश्मा
औरतें द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का विश्लेषण केवल एक भावनात्मक आवरण में लिपटी त्याग मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अधिक खुलेपन के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में की जाए।
इस संबंध में एक और ज़रूरी बात समझ लेना जरूरी है। दरअसल, घरेलू काम-काम के लिए महिलाओं को वेतन दिया जाना उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगा, लेकिन इससे समाज में मौजूद विभेद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इससे सामंती ‘श्रम के विभाजन’ का ढांचा नहीं टूट रहा है। यह वही ढांचा है, जो घरेलू काम-काज औरतों के जिम्मे थोपकर उनकी आज़ादी को सीमित करता है और यही कारण है कि यदि पति और पत्नी दोनों ही बाहर काम करते हैं, तब भी घरेलू जिम्मेदारी औरत की ही होती है। बच्चे होने पर उसे ही अपनी नौकरी छोड़कर परवरिश करनी होती है और इस तरह से, आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री भी पितृसत्ता के जाल से निकल नहीं पाती। साथ ही, घरेलू काम-काज की मेहनत का ‘एकनॉलेजमेंट’ सराहनीय है, लेकिन औरतों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए राज्य को बुनियादी सुधार करने की ज़रूरत है।
सुधारों और बदलावों के किए जाने पर एक और बात जो ध्यान आकर्षित करती है, वह है- औरतों द्वारा इनका विरोध किया जाना और अक़्सर इस विरोध के दमपर रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक समूह यह धारणा गढ़कर चलते हैं कि यदि यह सुधार औरत के लिए ज़रूरी है तो दूसरी औरत इसका विरोध क्यों कर रही है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं– सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘होममेकर’ के लिए एक निश्चित आय तय करने का मुद्दा दरअसल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के साथ-साथ एक स्वीकारोक्ति है; उन महिलाओं की भूमिकाओं की, जो इस क्षेत्र में सामाजिक-सांस्कृतिक नियमों अथवा चयन से शामिल हैं। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट यह स्वीकार करता है कि समाज के पारंपरिक ढांचे में आर्थिक तंत्र से महिलाएं बहिष्कृत रही हैं, लेकिन परिवार और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उनका हस्तक्षेप उल्लेखनीय है और बदलती मानसिकता के तहत कोर्ट सभी नागरिकों को उचित सम्मान प्रदान करने को अपना कर्तव्य मानता है।’
और पढ़ें : अनपेड केयर वर्क महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा के लिए ज़िम्मेदार: रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस कथन पर बहुत सारे एक्टिविस्ट और नेताओं ने सहमति दिखाते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार का एक जरिया माना, वहीं बहस बढ़ने पर बहुत सारी परंपरावादी महिलाएं इसका विरोध करते हुए इसे ‘ममता व प्रेम की कीमत’ कहते हुए इसे नकारतीं दिखीं। यह सोच दरअसल, पितृसत्ता द्वारा ही महिलाओं के भीतर भरी गई है, जिससे कई बार वे भी इसकी संरक्षक बन जाती हैं। इस संदर्भ में ‘द क्रिएशन ऑफ पेट्रिआर्की’ में जेर्डा लर्नर बताती हैं कि यह पुरुषों की ही सोची समझी चालबाज़ी है, जिसने औरतों को पितृसत्ता के संरक्षक के रूप में खड़ा कर दिया है और वे अनजाने में पहली पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। असल मे, सांस्कृतिक रूप से पित्रसत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इसलिए इसके बहुत सारे तत्व व व्यवहार इतने सामान्यीकृत हो गए हैं कि इन्हें आसानी से विघटित करना संभव नहीं है।
इसलिए, बुनियादी स्तर से वैचारिकी को बदलना होगा, जो कि राज्य के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा, हालांकि अभी के राज्य की संरचना पर ग़ौर करें तो उसमें भी पितृसत्ता के तत्व भीतर तक पैठे हुए हैं। इसलिए धीरे-धीरे लिए जाने वाले निर्णयों से ही बदलाव के बारे में सोचना होगा। इस दिशा में महाराष्ट्र की स्कूल की किताबों में घरेलू भूमिकाओं तक स्त्रियों के सीमित किए जाने वाली धारणा खण्डित करते हुए नया प्रयास किया गया है। उसी क्रम में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं की भागीदारी और श्रम के महत्व को स्वीकारना भी एक अहम कदम माना जाना चाहिए और धरातल तक इसकी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए राज्य को सशक्त और कल्याणकारी भूमिका अदा करनी चाहिए।
और पढ़ें : लॉकडाउन में महिलाओं पर बढ़ता अनपेड वर्क का बोझ
तस्वीर साभार : Scroll