“रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से इलाज करवाओगे तो मर जाओगे,” एक टीचर अपने पास खड़ी बच्चियों के झुंड से यही कह रही थीं। यही नहीं ऐसी और तमाम घटनाएं मेरे दिल-ओ-दिमाग़ में चस्पा हैं। यह स्कूल था ‘विद्या भारती।’ मुझे आठवीं पास करके नौवीं में एडमिशन लेना था तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था, “विद्या भारती के स्कूल बढ़िया होते हैं।” शायद तब मेरा परिवार और मैं भी यह नहीं जानते थे कि ‘विद्या भारती’ आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ’ से जुड़े हुए स्कूल हैं। ऐसे तमाम स्कूल देश के कोने-कोने में मौज़ूद हैं जिनमें लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की साल 2016 की रिपोर्ट के अनुसार देशभर में ऐसे 12 हज़ार स्कूल हैं जिनमें 32 लाख से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। आज के अपने इस लेख में एक आरएसएस के स्कूल में पढ़ते हुए मेरे जो अनुभव रहे वह साझा करने कर रही हूं।
मैंने अपने शहर के ‘विद्या भारती बालिका विद्यालय’ में नौवीं से बारहवीं तक पढ़ाई की है। यह स्कूल मैंने ख़ुद चुना था। नर्सरी से बारहवीं तक के इस विद्यालय में आठ हज़ार से ज़्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। स्कूल की बस में ही बच्चों के साथ टीचर्स भी आती थीं। वह मेरी पहली सुबह थी उस बस में। मैं अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और हम अपने पुराने स्कूल की बातें कर रहे थे जो कि एक ‘को-एड’ स्कूल था। हम हमारे साथ पढ़े लड़कों की बात कर रहे थे और हंस रहे थे। इस बीच हमें बिलकुल ध्यान नहीं रहा कि एक टीचर हमसे आगे वाली सीट पर बैठी हैं। वह कुछ देर तक हमारी बातें सुनती रही और अचानक हम पर चिल्लाते हुए कहा, “चुप रहो! बहुत देर से बकवास कर रही हो। कल से अलग-अलग बैठना।”
पितृसत्तात्मक सोच को दिया गया बढ़ावा
यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था जहां लड़कों के बारे में बात करने के लिए इतनी बुरी तरह डांटा गया था। धीरे-धीरे पता चला कि इन स्कूलों में लड़कियों की कंडीशनिंग इसी तरह होती है कि उन्हें लड़कों के बारे में बात नहीं करनी है। अगर वे ऐसा करती हैं तो उनके चरित्र में ख़राबी है। एक चलन और था इस स्कूल में जो कि अब बंद कर दिया गया है। किसी भी प्रतियोगिता में जीतने वाली छात्राओं को पुरस्कार के रूप में कटोरियों के सेट, जूस सेट, कप-प्लेट के सेट दिए जाते थे।
जैसे कि लड़कियां सिर्फ़ रसोई और घर तक ही सीमित हैं और इस तरह का पुरस्कार उनके हिस्से का हक़, उनके हिस्से की तारीफ़ हो सकती है जो कि सरासर पितृसत्तात्मक सोच है। इस तरह इन संस्थानों में लड़कियों को पितृसत्तात्मक सोच रखने में, उसे बढ़ाने में अग्रणी बनाया जाता है। इस बीच महसूस हुआ लड़कियों को यहां किस तरीके से ‘संस्कार’ में बांधा जाता है। संस्कार से मतलब ‘सहना’, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सहने लायक बनाया जाता है।
एक तरह की प्रार्थना और पॉज़िटिव खबरें
हर स्कूल की तरह यहां भी प्रार्थना होनी थी। प्रार्थना आधे से लेकर एक घंटे की होती थी जिसमें ‘मॉर्निंग ग्रिटिंग्स’ संस्कृत में किए जाते थे। अख़बार की वही खबरें सुनाई जाती थीं जो ‘पॉज़िटिव’ हो जैसे कि “फलां-फलां महिला ने ये अवॉर्ड जीता” आदि। मैं यह सब पहली बार महसूस कर रही थी क्योंकि मैं आठवीं तक जितने भी विद्यालयों में पढ़ी वे सब ‘सेक्युलर’ थे। वे संविधान की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा के अंतर्गत अपना संस्थान चला रहे थे। जहां सुबह की असेंबली में “हम होंगे कामयाब” से ज़्यादा कुछ नहीं दोहराया जाता था। हालांकि, कुछ दिनों बाद मैंने अपना ‘राइट टू साइलेंस’ के अधिकार का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा जो कि मेरे स्कूल के आख़िरी दिन तक जारी रहा।
इन संस्थानों में लड़कियों को पितृसत्तात्मक सोच रखने में, उसे बढ़ाने में अग्रणी बनाया जाता है। इस बीच महसूस हुआ लड़कियों को यहां किस तरीके से ‘संस्कार’ में बांधा जाता है। संस्कार से मतलब ‘सहना’, पितृसत्तात्मक व्यवस्था को सहने लायक बनाया जाता है।
इस सबके बीच क्लास शुरू हुई ‘सिलेबस ओरिएंटेड’ क्लास जो कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था में गहराई तक रचा-बसा हुआ है। क्लासेज लगने के बाद लंच का टाइम हुआ जिसमें लंच करने से पहले एक मंत्र का जाप करना होता था। इस मंत्र के ज़रिये अन्न के लिए ईश्वर का शुक्रिया कहा जाता था। ऐसे हालातों में पहला दिन गुज़रा और यही सब देखते-देखते एक अच्छा खासा वक़्त गुज़र गया।
जातिवादी सोच को पोसता स्कूल का माहौल
इसी बीच ‘रोहित वेमुला’ की ‘सांस्थानिक हत्या’ का मामला सामने आया जिसने मुझे झकझोर दिया। उसी के बाद ऐसा हुआ कि मैं सीधे तौर पर ‘कास्ट कॉन्शियस’ बनी और तकरीबन हर घटना को ‘कास्ट-कॉन्शियस’ होने के नज़रिये से देखना शुरू किया। अगर शायद ऐसा न होता तो मैं भी पितृसत्ता की वाहक के तौर पर स्थापित हो चुकी होती। मैंने रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या से जुड़े कुछ सवाल अपनी मैडम से किए और उन्होंने मुझे भरी क्लास में ‘चुप’ करवा दिया। इस घटना ने मुझे और आहत किया।
हर रोज़ इस माहौल को देखते-देखते मैं चुप रहने लगी थी। एक रोज़ नौवीं में दसवीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बच्चों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाए जा रहे थे। मुझे भी मेरी क्लास टीचर ने बुलाया। कुछ ज़रूरी जानकारियां भरीं, उसके बाद फॉर्म में ‘जाति’ का कॉलम आया। उन्होंने पूछा- “कास्ट” और मैंने कहा ”एससी।” पता नहीं वह सच में सुन पाई थीं या नहीं या फिर दोबारा सुनना चाहती थीं। उन्होंने फिर पूछा “जाति?” मैंने कहा-“एससी।” आगे उन्होंने कहा “आर यू श्योर?” मैंने कहा “हां।” इस हां के बाद मेरी आंखें भर आईं मैं अपनी सीट पर आ गई। मेरी सहेलियों ने पूछा कि “क्या हुआ?” तब मैंने कहा “अब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी क्योंकि मैं एक एससी हूं।”
नहीं पता मैंने कैसे अपनी सहेलियों से कह दिया कि वे मुझसे दोस्ती तोड़ देंगी। शायद चौदह साल के बच्चे में इतनी ही अक्ल हो पाती है। इस तरह जीवन में पहली बार ‘दलित’ होने का अनुभव, भेदभाव का अनुभव हुआ। सिर्फ़ मुझसे “आर यू श्योर क्यों पूछा गया? आज मैं इसे याद करते हुए कह सकती हूं, इस देश के सवर्ण एक दलित को कुछ गंदे मैले कपड़ों में सड़क किनारे झाड़ू लगाते या फिर अपने इलाके के इस ‘सिस्टम’ द्वारा ख़राब कर दिए गए सरकारी विद्यालयों तक सीमित देखना चाहते हैं। इसीलिए जब वे हमें संवैधानिक अधिकारों के बूते अपनी संस्थानों में संवरकर आते हुए देखते हैं तब वे “आर यू श्योर” जैसे सवाल करते हैं। इस सवाल के ज़रिये ब्राह्मणवादी व्यवस्था तहत “दलित अब दलित कहां रहा” जैसे मानक गढ़ते हैं। इस तरह आरएसएस के इस स्कूल में मुझे एक वाक्य भर से पूरी जाति व्यवस्था का इतिहास और वर्तमान याद करवा दिया गया।
मैं नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने के दौरान बीमार रही। मुझे स्ट्रेस से बहुत जल्दी-जल्दी बुखार आने लगा था इसी स्ट्रेस की वजह से मैं माइग्रेन के दर्द से भी ग्रसित हो गई। मेरा परिवार बाबा साहेब से भली-भांति परिचित था। उन्हें ‘जाति’ का सच और हमारे आदर्शों के बारे में भी पता था। लेकिन मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं बताया गया था कि मैं उनके लिए बच्ची थी। मैं अपने माँ-पिता के लिए बच्ची थी लेकिन विद्यालय और उसके शिक्षकों के लिए नहीं।
मैंने ये महसूस किया जब-जब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस मनाए गए उनमें से दो शब्द हमेशा गायब थे संविधान और भीमराव आंबेडकर। इन दो नामों को छोड़कर उनके भाषणों में सब शामिल था जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर का सबसे पहले आकर “बोल… बांके बिहारी लाल की जय” और जवाब में लड़कियों की तरफ़ से भी “जय” का उद्घोष। मैं कभी नहीं समझ पाई देश की आज़ादी, देश के संविधान को निर्मित करने में ‘इनके’ बांके बिहारी की आख़िर भूमिका क्या थी?
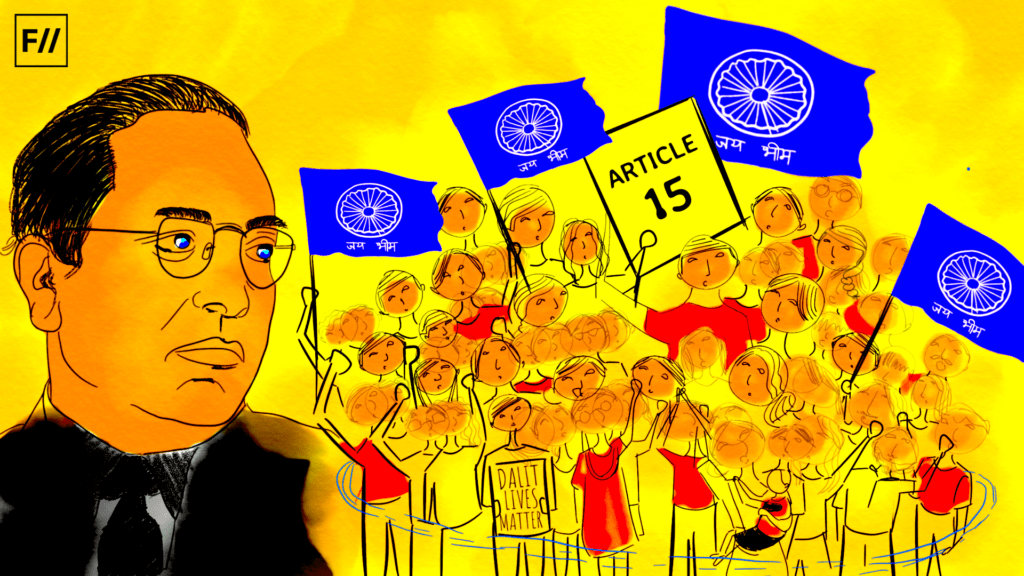
आज मैं इसे याद करते हुए कह सकती हूं, इस देश के सवर्ण एक दलित को कुछ गंदे मैले कपड़ों में सड़क किनारे झाड़ू लगाते या फिर अपने इलाके के इस ‘सिस्टम’ द्वारा ख़राब कर दिए गए सरकारी विद्यालयों तक सीमित देखना चाहते हैं। इसीलिए जब वे हमें संवैधानिक अधिकारों के बूते अपनी संस्थानों में संवरकर आते हुए देखते हैं तब वे “आर यू श्योर” जैसे सवाल करते हैं।
इसी का नतीजा ये रहा एक साल ही 26 जनवरी और 15 अगस्त के प्रोग्राम मैंने देखे उसके बाद बाकी बचे तीन सालों में मैं कभी इन कार्यक्रमों में नहीं गई। सबसे गौरतलब मेरे लिए ये रहा कि चौदह अप्रैल से एक दिन पहले जब प्रार्थना होती तब ‘बाबा साहेब’ के बारे में बताने के लिए कोई टीचर आती तो उनके पास बाबा साहेब के बारे में उनके जन्म, उनकी शिक्षा और ‘दलितों के मसीहा’ से ज़्यादा कुछ नहीं होता था। जिस देश की लड़कियों के हित में ‘हिन्दू कोड बिल’ ना मानने पर अड़ी संसद से जिस आदमी ने इस्तीफ़ा दे दिया उस आदमी को इन्हीं संस्थानों में ना तो पढ़ाया जाता है ना बताया जाता है। ना इन संस्थानों में सावित्रीबाई फुले की बात की जाती है ना फातिमा शेख़ की। हां दुर्गा, काली बनने कि बातें यहां आम हैं।
आरक्षण विरोधी सोच
जाति, पितृसत्ता इन सबसे रोज़ मुखातिब होते हुए दसवीं में ही एक और घटना घटी। सामना हुआ ‘रिजर्वेशन के तानों’ से और ये जाना कि ये ताने अब तक मेरा और मुझ जैसे तमाम दलित-बहुजन-आदिवासी बच्चों का पीछा नहीं छोड़ पाए हैं। एक टीचर ने डिबेट शुरू की ‘आधार कार्ड’ पर जो ख़त्म हुई ‘आरक्षण’ पर । मैं बहुत अचंभित रहती हूं आख़िर सवर्णों की किसी भी विषय पर शुरू हुई डिबेट आरक्षण पर आकर कैसे खत्म हो जाती है? मैं उस वक़्त तीसरी पंक्ति में पहली सीट पर अकेले ही बैठती थी। पचास बच्चों की क्लास में मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं था, हर वक़्त लगता कि कहीं कोई ‘जातिसूचक शब्द’ कह देगा और मुझसे सहन नहीं होगा। इस सबके बीच मैं अलग रहने लगी थी, मुझे किसी का साथ पसंद नहीं था। सवर्ण लड़कियों के दिमाग़ में ये चीज़ बैठा दी गई हैं कि उनका हक़ एससी, एसटी, ओबीसी खा रहे हैं। मैं अपनी सीट पर खड़े होकर डिबेट में अपनी राय दे रही थी। 50 बच्चों में मैं अकेली थी जो आरक्षण के पक्ष में थी और मैडम समेत सब विपक्ष में।
आप इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तमाम दलित बच्चे हर रोज़ किन परिस्थितियों में जीकर, किस मानसिक स्थिति से गुज़रकर स्कूल, कॉलेजों तक आते हैं। लड़कियों को किसी के कपड़े अच्छे नहीं लगते थे तो वे सीधा कहतीं, “चमरिया मत बन।” उन्हें किसी का खाना पसंद नहीं आता तब वे कहती “भागियों-सा खाना कौन खाता है?”
मुझे मैडम ने मेरी सीट से बुलाया और पहली पंक्ति में बैठी कुछ लड़कियों के बीच बैठा दिया, मैं तब भी पक्ष में बोल रही थी। इस बीच पीरियड खत्म होते ही मैडम चली गई। लेकिन वे सब लड़कियां मुझे घेरे हुए खड़ी थीं जिनसे मेरी बहस अभी भी चालू थी। मैं तमाम राजनीतिक तंत्र के लिए ‘सिस्टम’ शब्द का इस्तेमाल कर रही थी और उनमें से एक कहती है सिस्टम, कौन सा? नर्वस? इम्यून? ये सुनते ही मैं चुप हो गई क्योंकि उनसे बहस करना अब बेकार लग रहा था, निरर्थक। मैं चुप होकर चलने को थी ही कि इतने में एक लड़की कहती है- “तू ख़ुद नीची जाति से है क्या? लगती तो ठाकुर है।” तब मैंने उन्हें पलटकर सिर्फ़ इतना कहा – “जो तुम हो वही हूं मैं” उसने फिर कहा, “ठाकुर है?” मैंने कहा “नहीं, इंसान!”
इसके बाद मैं क्लास से बाहर निकल गई। उस वक़्त लग रहा था जैसे वह पूरी सवर्ण लड़कियों की भीड़ मुझे मार देगी। उस दिन फिर कोई क्लास नहीं ली मैं अपने फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठी रही। आप इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं तमाम दलित बच्चे हर रोज़ किन परिस्थितियों में जीकर, किस मानसिक स्थिति से गुज़रकर स्कूल, कॉलेजों तक आते हैं। लड़कियों को किसी के कपड़े अच्छे नहीं लगते थे तो वे सीधा कहतीं, “चमरिया मत बन।” उन्हें किसी का खाना पसंद नहीं आता तब वे कहती “भागियों-सा खाना कौन खाता है?” ये शब्द मुझसे नहीं सहे जाते थे। हालांकि वे आपस में ऐसा बोलती और हंसती तब भी मुझे ख़राब लगता था। यही वजह रही कि मेरी दोस्ती कभी गहरी नहीं हुई किसी से। ग्यारहवीं में मैंने ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ली और इससे रास्ता और कठिन हो गया। तब आरक्षण पर बहसें और आम हो गई।

ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी गई है इन संस्थानों में जो न सोचती है ना समझती है और इनकी तादाद करोड़ों में है। इन शैक्षणिक संस्थानों में ये ‘सवर्ण रोबोट्स’ तैयार किए हैं जो वक़्त-वक़्त पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं ‘ब्राह्मणवादी सत्ता’ के पक्ष में खड़े होते दिखते हैं।
टीचर्स तक “रिजर्वेशन वाले डॉक्टर तो पेशेंट को मार देते हैं” जैसे वाक्यों का इस्तेमाल खुले-आम करते थे तब उनसे इसी विषय में बहस करना मुझे अपनी एनर्जी और वक़्त दोनों की बर्बादी लगती थी इसीलिए बोलना ही बंद कर दिया था। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी ‘कटुए’, ‘मुल्ले’ जैसे तमाम नफ़रत भरे शब्द भी आम थे। एक बार हद तब हो गई जब राजनीति विज्ञान की मैडम ने कहा कि ‘व्यवस्था पहले ही अच्छी थी, ‘पंडित’ पढ़-लिख सकते थे, शूद्र कचड़ा साफ़ करते थे। अब तो पण्डित की नौकरियाँ भी यही खा जाते हैं।” इस स्टेटमेंट पर सब लड़कियों ने सहमति जताई।
मैंने तब भी कुछ नहीं कहा लेकिन ये ज़रूर सोचा कि ये जिस व्यवस्था की बात कर रही हैं वह ‘मनुस्मृति की व्यवस्था‘ है जिसमें औरतें चार दीवारों में पुरुषों के अधीन ही रह सकती हैं। ऐसी व्यवस्था में क्या ये यहां पढ़ा रही होतीं? शायद इसीलिए भी पूरे स्कूल में दो सौ से ज़्यादा टीचर्स होने के बावज़ूद एक भी दलित टीचर नहीं थी/था। पचास साठ बच्चों की हर क्लास में दस से ज़्यादा एससी के बच्चे नहीं थे, एसटी तो थे ही नहीं, ओबीसी भी कुछ ही थे। ऐसे अनुभवों से गुज़रकर आख़िर में मेरा स्कूल ख़त्म हुआ। पढ़ाई ख़ुशी की वजह बननी चाहिए थी वह मेरे लिए ‘बीमारी’ की वजह बनी। इस तरह जातिगत भेदभाव ने अंदर तक वार किया, परेशान किया। मैं जब यह सब लिख रही हूं तब ऐसा लग रहा है जैसे उस सारे वक़्त को दोबारा जी रही हूं और ये भी कम पीड़ादायी नहीं है।
ऐसा क्यों था कि बाक़ी बच्चे ख़ुश थे लेकिन उनकी बातों से मैं आहत थी। मेरा आहत होना, मेरे जैसे तमाम दलित बच्चों का इन संस्थानों में ऐसे आहत होना जातिगत भेदभाव का एक और प्रकार है जिसमें पितृसत्तात्मक सोच साथ-साथ दोहरी मार दे रही होती है। जातिगत मानसिकता के बच्चे इन आरएसएस की शैक्षणिक संस्थानों में तैयार किए जाते हैं। सवर्ण लड़कियां सिर्फ संस्कार, परिवार और सपने पूरे कर पाएं तो भी ब्राह्मणवाद से लैस रहें, उस तरह के सांचे में ढाली जाती हैं। ऐसी पीढ़ी तैयार कर दी गई है इन संस्थानों में जो न सोचती है ना समझती है और इनकी तादाद करोड़ों में है। इन शैक्षणिक संस्थानों में ये ‘सवर्ण रोबोट्स’ तैयार किए हैं जो वक़्त-वक़्त पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं ‘ब्राह्मणवादी सत्ता’ के पक्ष में खड़े होते दिखते हैं।




