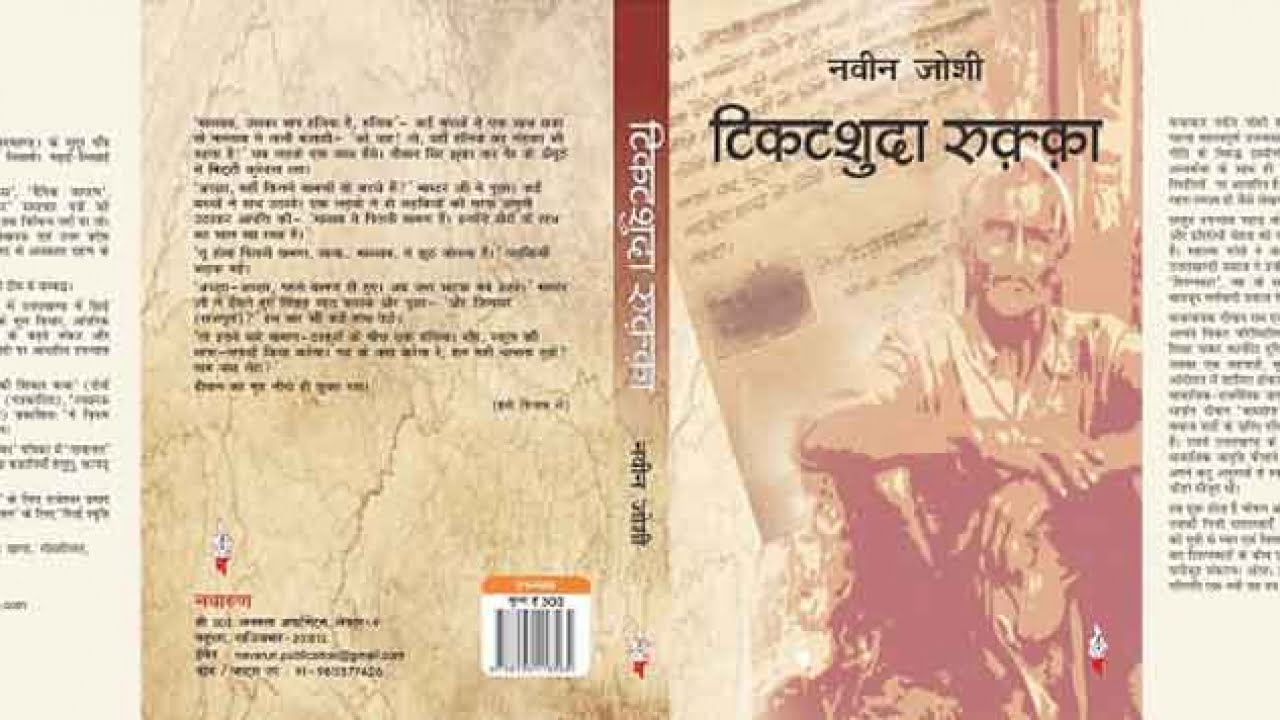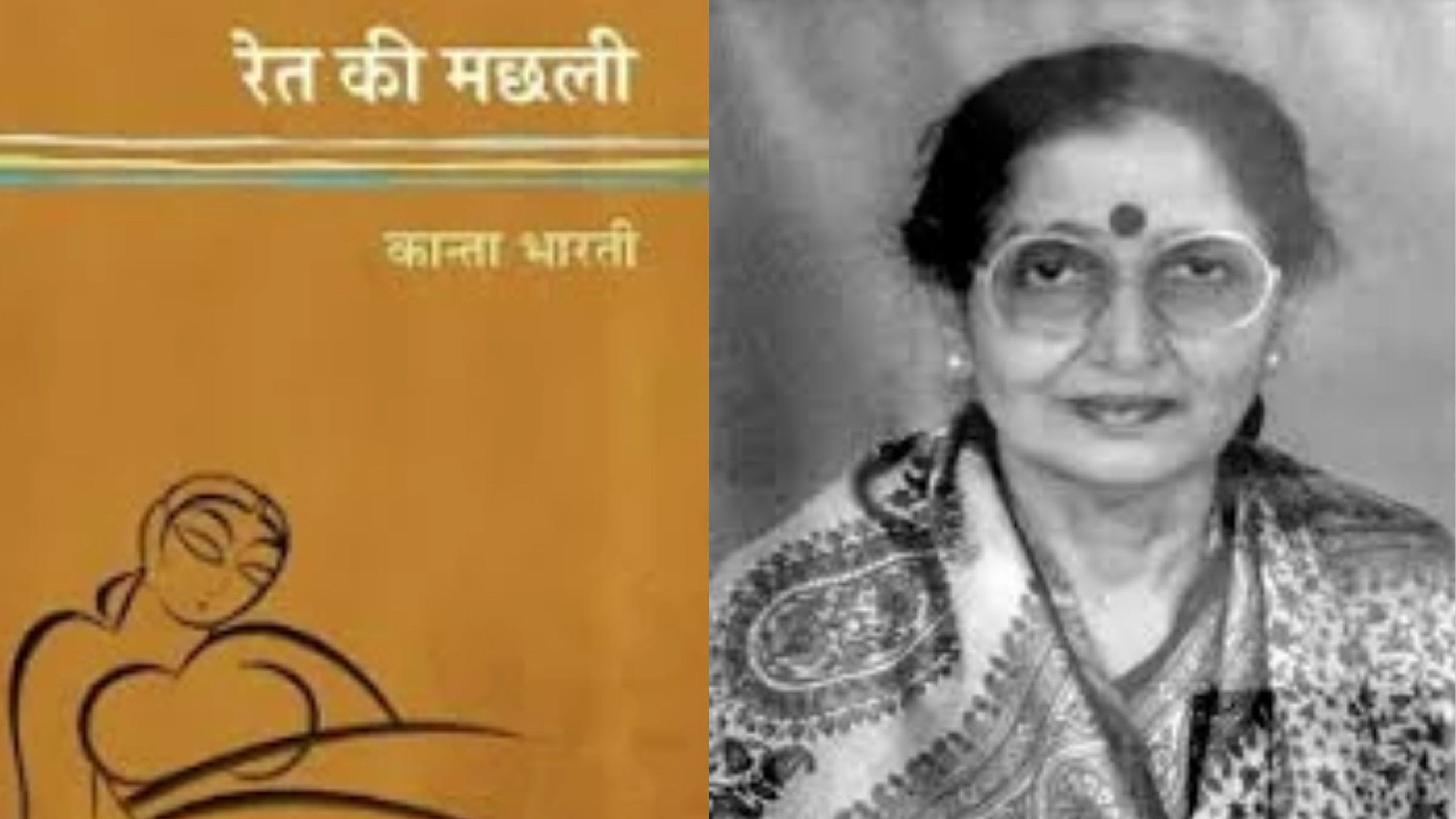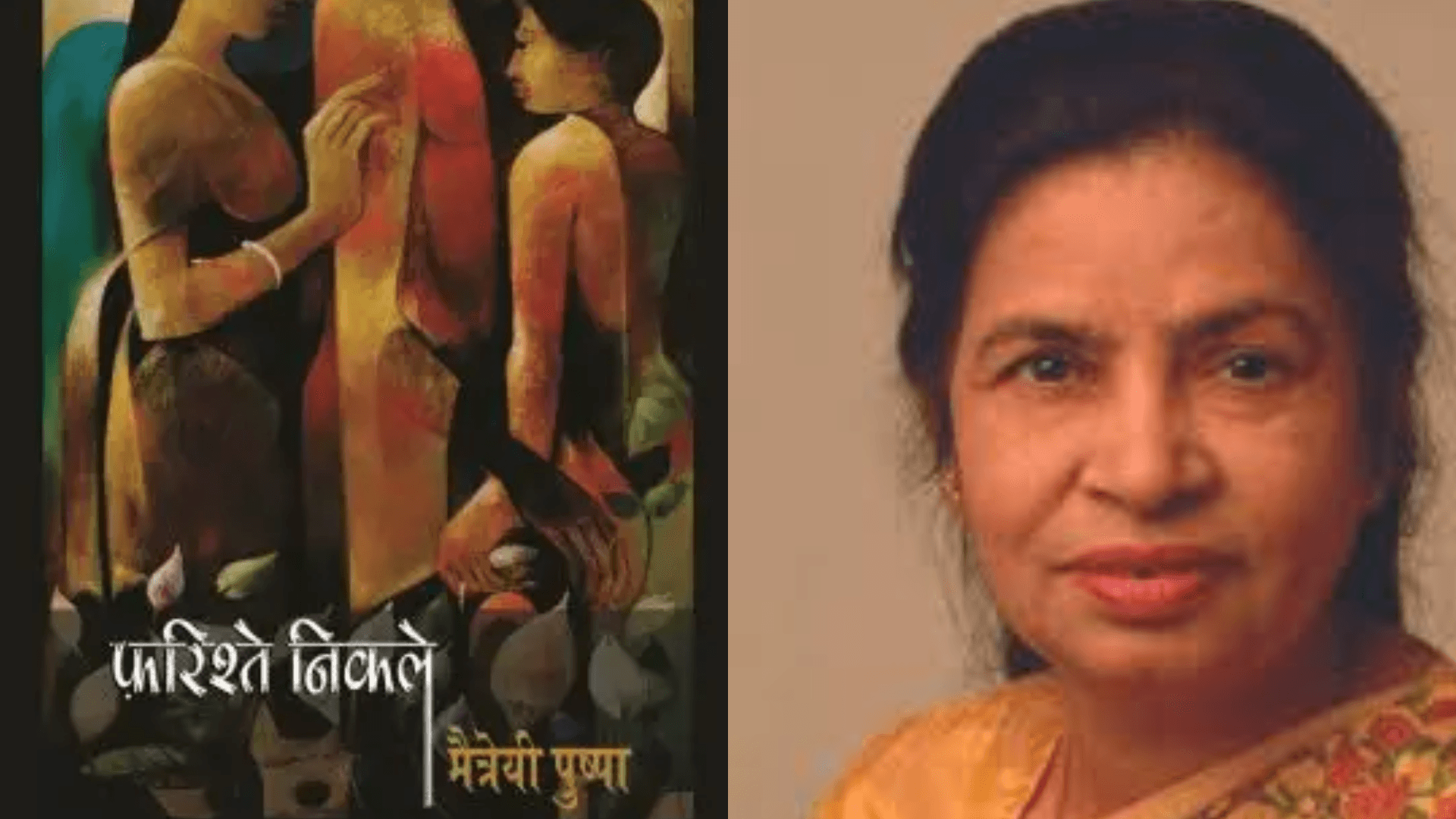जातिवादी समाज, छुआछूत का समाज, अस्पृश्यता और भेदभाव का समाज, गैरबराबरी के ये सारे ढांचे बहुत जड़ता और क्रूरता से निर्मित होते हैं। बहुत गहरी खाई ये बनाते हैं समाज के आर्थिक और सामाजिक स्वरूप के पूरे गठन में। आंदोलन कोई भी हो, जब तक सामाजिक और राजनीतिक दोनों आंदोलनों के मध्य एक गहरा संबंध नहीं स्थापित हो तो आंदोलन कहां सफल होते हैं। समाज का जो मूलभूत ढांचा है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होते जब तक सांस्कतिक रूप से कोई बदलाव नहीं होता। पहाड़ी जनजीवन पर नवीन जोशी का लिखा उपन्यास ‘टिकटशुदा रुक्का’ पढ़ते हुए यही बात मन में चलती रही कि आखिर लड़ाइयां धारा के सबसे निचले पायदान पर जीवन जीते जन की पीड़ाओं तक क्यों नहीं पहुंचती। यह उपन्यास एक प्रगतिशील व आधुनिक चेतना से भरे दलित युवक के गहरे अंतर्द्वंद का दस्तावेज है।
इस अंतर्दशा को सहजता से सामने रखने के लिए लेखक अंत के हिस्से में शिल्प के रूप में उसकी डायरी का सृजनात्मक प्रयोग करता है। साथ ही उत्तराखंडी समाज में अब तक व्याप्त इस विडंबना को विश्वसनीय और ठोस तरीके से सामने रखता है। उत्तराखंड में लगातार जमीनें फसलें न बोई जाने के कारण बंजर होती जा रही हैं। जैव विविधता से भरा उत्तराखंड अपनी संपदा खोता जा रहा है। पहाड़ से पलायन इस कदर दिखाई देता है कि गाँव के गाँव आबादी विहीन या सिर्फ बुजुर्गों से भरे दिखाई देते हैं।
कहानी जहां से शुरू होती है वह दृश्य एक समाज की जाहिलियत से मिली कठिन पीड़ा की पुकार है। उपन्यास का नायक दीवान राम जो एक मल्टीनैशनल कंपनी में उच्च अधिकारी है वह हॉस्पिटल में नीम बेहोशी में ईजा! ईजा! पुकारता है। बेहोशी में वह बार-बार कहता है ईजा मैं आ रहा हूं…! उसकी पत्नी शिवानी और डॉक्टर परेशान हैं कि उसे क्या हुआ है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है जिसमें दीवान राम का बचपन और पहाड़ का उसका छूट गया गाँव है। जहां वह शिल्पकार का बेटा है, जहां घोर गरीबी और यातना का जीवन है। दीवान राम की माँ सरूली को कोढ़ हो गया है और उसे गाँव के बीठ (सवर्ण) गाँव से निकाल देते हैं। अपने दुधमुंहे बच्चे के लिए तड़पती सरूली फांसी लगा लेती है। यह बात दीवान राम को पालनेवाली उसकी दीदी गोपुली ने ससुराल जाते हुए अपने छोटे से भाई को बताई है और यहीं अंतर्द्वंद्व है नायक के मन का जिससे वह लगातार जूझता है जो एक दिन अचानक उसे अस्पताल पहुंचा देता है।
पहाड़ के समाज में मैदानों की तरह जंमीदार या सामंत नहीं थे लेकिन सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण वहां बहुत था। छुआ-छूत अस्पृश्यता का वह समाज था, दीवान जिसे नियति मानकर चुप रहता था अब वे उसके भीतर आक्रोश को जन्म देने लगे थे। लखनऊ से एक साल बाद जब वह गांव लौटता है तब उसे पिता से धुंए से काले पडे़ कटे-फटे टिकट शुदा रुक्कों से पता लगता है कि 1833 में अंग्रेजों द्वारा दास प्रथा की कानूनी मान्यता खत्म होने के बावजूद उसके पिता गांव के सवर्णों के दास हैं।
उपन्यास में एक हलिया के बेटे की कथा चलती है लेकिन यह पूरे एक सामाजिक परिवेश की कहानी है जिसे हम सब जानते, समझते हैं। यह जाति और अस्पृश्यता, रूढ़ि से बने सामाजिक जीवन की विसंगतियों का सच है। उपन्यास पढ़ते हुए डॉ तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया की याद आई। उपन्यास पर बहुत लिखा जा सकता है पर जब पढ़ा तो लगता है कि कहीं न कहीं हम सब इस दुख के कारण और हिस्सेदार हैं। अस्पृश्यता और भेदभाव का ये चलन, मनुष्य से मनुष्य की घृणा और चालाकी का आधार है। ऐसी यातना, पीड़ा का ऐसा रूप समझना और उससे जल्दी बहुर न पाना मन लौट- लौटकर वहीं जाता है और सालती रहती है सामाजिक व्यवस्था की वह टीस जो इतनी गहरी है कि इतनी लड़ाइयां, इतने आंदोलन और इतने काननू के बाद भी अब तक बची हुई है। जब मन लौट पड़ता है अन्याय से बनी उस दुनिया में जहां मनुष्य से मनुष्य को इतना कमतर किया गया कि उसके स्पर्श से वहीं दूसरे मनुष्य अपवित्र हो जाता है तब कला, सौंदर्य और करुणा, प्रेम आदि की कोई कविता-फबिता अच्छी नहीं लगती। आत्मा सवालों से भरी रहती है वही सवाल जो दीवान राम अपने प्रिय मास्टर सोहन सिंह से भी नहीं पूछ पाया जिनसे वह गले लगने के लिए आजीवन तड़पता रहा। ये सवाल आज भी जिंदा हैं और फल-फूल भी रहे जो सवाल कथा का नायक अपनी चेतन अवस्था में कभी किसी से नहीं पूछ सका।
वे सवाल जाकर दीवान राम की आत्मा के तल में बैठ गए थे कहीं और एक दिन वह अस्पताल के बेड पर पड़े नीम बेहोशी की हालत में वही सवाल पूछता है, यहीं से उसके भीतर मचे भीषण अंतर्द्वंद का पता चलता है। दीवान का बचपन भी वैसे ही बीता है जैसा 70 के दशक में एक दलित हलवाहे के बेटे का हो सकता है। सोहन का अपने मास्टर साहब के बदौलत हौसला बना रहता है। सवर्ण सहपाठियों की मारपीट, प्रताड़ना, अमानवीय व्यवहार, नये आए स्कूल मास्टर की बदसलूकी के बावजूद वह गांव के स्कूल फिर कांडा के कॉलेज से इंटर तक पढ़ाई करके लखनऊ विश्वविद्यालय में साइंस में दाखिला लेता है। यहां आकर उसके सामने एक नयी दुनिया खुलती है, जिसमें विश्वविद्यालय के पढ़ाई के साथ उसका रूम पार्टनर देवराज उसे स्टडी सर्किल में ले जाता है। जहां साहित्य, संस्कृति, राजनीति पर बातें होती हैं। उनके साथ बहस और बातों से दीवान राम के भीतर कई सवाल जो अनसुलझे थे या उन पर कभी सोचा ही नहीं था, उस पर नज़र जाने लगती है।
किसान का तो मिट्टी से लगाव समझ में आता है क्या गुलामों का भी मालिक की मिट्टी से कोई मोह होता है? आखिर यह दर्शन उनकी सोच का हिस्सा कैसे बन गया। आज के समय का जो पूरा परिदृश्य है सजे संदर्भ में यदि इस सवाल को सामने रखकर सोचें तो देखेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा यह प्रासंगिक हो उठा है।
पहाड़ के समाज में मैदानों की तरह जंमीदार या सामंत नहीं थे लेकिन सामाजिक, मानसिक और आर्थिक शोषण वहां बहुत था। छुआछूत, अस्पृश्यता का वह समाज था, दीवान जिसे नियति मानकर चुप रहता था अब वे उसके भीतर आक्रोश को जन्म देने लगे थे। लखनऊ से एक साल बाद जब वह गांव लौटता है तब उसे पिता से धुंए से काले पडे़ कटे-फटे टिकट शुदा रुक्कों से पता लगता है कि 1833 में अंग्रेजों द्वारा दास प्रथा की कानूनी मान्यता खत्म होने के बावजूद उसके पिता गांव के सवर्णों के दास हैं। हलिया की परंपरा उसी का बदला हुआ रूप है। उसके दादा भी इन्हीं सवर्णो के दास थे। कुछ सौ रुपयों के चलते वे आज तक सवर्णों की गुलामी कर रहे थे। कॉलेज में हो रही बहसों को सोचता ,उसे उनकी बातें सच लगती सोहन सिंह मास्टर साहब से किया वादा और अपना संकल्प वह दोहराता है कि पढ़-लिखकर वापस आऊंगा और अपने लोगों में जागृति पैदा करूंगा, इस शोषण के खिलाफ एकजुट करूंगा।
लखनऊ लौटकर वह अपनी पढ़ाई पूरी करता है। इसी बीच उसका अपनी क्लासमेट से शिवानी से प्रेम होता है, जो शहर के प्रतिष्ठित दलित वकील की बेटी है। वह एक कॉरपरेट कंपनी में काम करने लगता है। शिवानी से शादी और एक बच्ची का पिता भी बन जाता है। एक तरफ उसका संकल्प दूसरी तरफ कंपनी की नौकरी करता तरक्की के पायदान चढ़ता। लेकिन उसके भीतर इन सबके बीच भीषण अंतर्द्वंद मचा रहता है, जो उसे अपना संकल्प पूरा करने के निर्णायक अंत की तरफ ले जाता है। इस मूल कथा को रचते हुए लेखक कथा के समय, घटनाओं और जिन चरित्रों के माध्यम और तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों का वर्णन करता है वह इस उपन्यास को हमारे समय का एक जरूरी दस्तावेज बना देते हैं।
उपन्यास में एक हलिया के बेटे की कथा चलती है लेकिन यह पूरे एक सामाजिक परिवेश की कहानी है जिसे हम सब जानते, समझते हैं। ये जाति और अस्पृश्यता, रूढ़ि से बने सामाजिक जीवन की विसंगतियों का सच है।
कैसे कोई समाजिक कंडिशनिग हमारी चेतना पर अधिकार कर लेती उस मानसिक जकड़न को ही हम नियति मान लेते हैं। उपन्यास में एक प्रसंग है इस जकड़न का एक उदाहरण खुद नायक अपने भाई का अपनी डायरी में 5 मार्च 1987 को दर्ज करता है। वह अपने बड़े भाई से कहता है कि वह पैसे भेजेगा। मालिक लोगों का ब्याज सहित सब कर्जा चुकाकर सिर्फ अपना काम करो और मुक्त हो जाओ इन रुक्कों से। जवाब में भाई कहता है, “बाबू कहते थे, एक धरम इस देह का है, एक धरम इस मिट्टी का है, जब तक जान है यह धरम निभाने हैं हमने।” नायक चकित है इस दर्शन पर। किसान का तो मिट्टी से लगाव समझ में आता है क्या गुलामों का भी मालिक की मिट्टी से कोई मोह होता है? आखिर यह दर्शन उनकी सोच का हिस्सा कैसे बन गया। आज के समय का जो पूरा परिदृश्य है सजे संदर्भ में यदि इस सवाल को सामने रखकर सोचें तो देखेंगे कि पहले से कहीं ज्यादा यह प्रासंगिक हो उठा है।
समय है अस्सी का दशक, देश में टीवी, कंप्यूटर आ चुका है। तमाम मल्टीनैशनल भारत के बाज़ार में पांव जमाने और गला काट प्रतिस्पर्धा में लिप्त हैं। चमकीले विज्ञापनों से आकर्षित करने और उपभोक्ता तैयार करने के लिए भारत के बाजार पर कब्जा जमा कर मुनाफा कमाने की होड़ लगी है। हर प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए फिल्मी सितारों, मॉडलों, अखबारों में लेख लिखवाने, क्रीम से गोरा होने से लेकर रेशम से बाल, और दांतो को भीतर तक साफ करनेवाले ढेरों-ढेर विज्ञापनों की चमकीली बाढ़ आई हुई है। जैसे इसके पहले पूरे देश का शरीर गंदगी से ही लिथडा़ हुआ था। नायक दीवान राम को कंपनी के लिए नया आईडिया अपनी ज़मीन और अपने परिस्थिति जन्य अनुभवों से ही आते हैं। यह अलग बात है कि वह एमबीए भी है और प्रतिभा संपन्न भी। लेकिन उसकी सारी मेधा कंपनी को मुनाफा कैसे हो इसके लिए ही इस्तेमाल हो रही है। बदले में पैसा है, गाड़ी है, सारी सुख-सुविधा है लेकिन दीवान के भीतर बैठा संकल्प उसे रह-रहकर कचोटता रहता है।
उसके द्वंद के साथ-साथ लेखक कॉरपोरेट का रेशा-रेशा उघाड़ता चलता है। कंपनी को मुनाफा हो रहा है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं, इसलिए लोगों की छंटनी करो। दीवान राम को बेहतर से बेहतर डॉक्टर को दिखाओ इसलिए नहीं कि वह ठीक हो जाए बल्कि इंडिया डायरेक्टर की चिंता यह है कि कहीं उनका एडल्ट डायपर का प्रोजेक्ट पिछड़ ना जाए जिसपर सबका प्रमोशन और वेतन भत्ते में वृद्धि निर्भर करती है। इस बहुत महीन शोषणकारी मुनाफे की मशीन जहां कोई भी बस उसका पुर्जा है, जरा भी कमजोर पड़ा तो बदल दो। मुनाफे की मशीन की गति कम नहीं होनी चाहिए। इस पूंजी के मशीन के अमानवीय चेहरे की शिनाख्त लेखक करता है पांच दिन बाद दीवान राम ठीक होकर अस्पताल से घर आता है। कंपनी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से उससे जाकर मिलने और विश्वास में लेकर दीवान से आईडिया जान लेने को कहता है और उसके बाद उसे किसी गैर महत्वपूर्ण जगह पर तैनात करने का आदेश देता है।
कॉरपोरेट की दुनिया में रहते हुए दीवान राम इन सबसे बेहतर तरीके से परिचित हो चुका था। उसे पता था कंपनी क्या करेगी? उसके दादा और पिता जिन परिस्थितियों में उन टिकट शुदा रुक्कों के कारण भू दास बनकर रह गए थे वह इन स्थितियों से निकल सकता है। जिन रुक्कों पर उसने अपनी मर्जी से सोच समझकर हस्ताक्षर किए थे उसे वह फाड़ सकता है। घर, परिवार, शिवानी की चिंता उसे जरूर हो रही थी लेकिन सोहन सिंह मास्टर साहब का कथन कि पढ़-लिखकर अपने समाज के लिए कुछ सोचेगा या तू भी पहाड़ के और नौजवानों की तरह बाहर जाकर नौकरी वाला हो जाएगा। यह कहते हुए उनके दुख से भरी आंखें उसे याद आती हैं, इजा की आर्त पुकार। वह आत्मा तक आती पुकार उसकी धरती के पुकार में बदल जाती है। सहपाठी सुरेश के तंज कैसे ‘पीड़ित अभिजात’ जो अपने समुदाय से कटकर शोषकों के ही पुर्जे बन जाते हैं याद आते हैं। इस सारी जद्दोजहद में कथा नायक दीवान स्वेच्छा से अपने दास बन जाने के रुक्कों को फाड़ देता है और अगले ही दिन दफ्तर जाकर अपना इस्तीफा दे आता है। अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उपन्यास में लेखक बहुत सहजता से कहता है कि सामंतवाद में तो हम जन्म और समाज के कारण फसते हैं जबकि पूंजीवाद जो सामंतवाद से कहीं ज्यादा क्रूर और भयावह है बल्कि यूं कहें कि सामंतवाद का दैत्य रूप है पूंजीवाद उसमें हम फंसते चले जाते हैं।