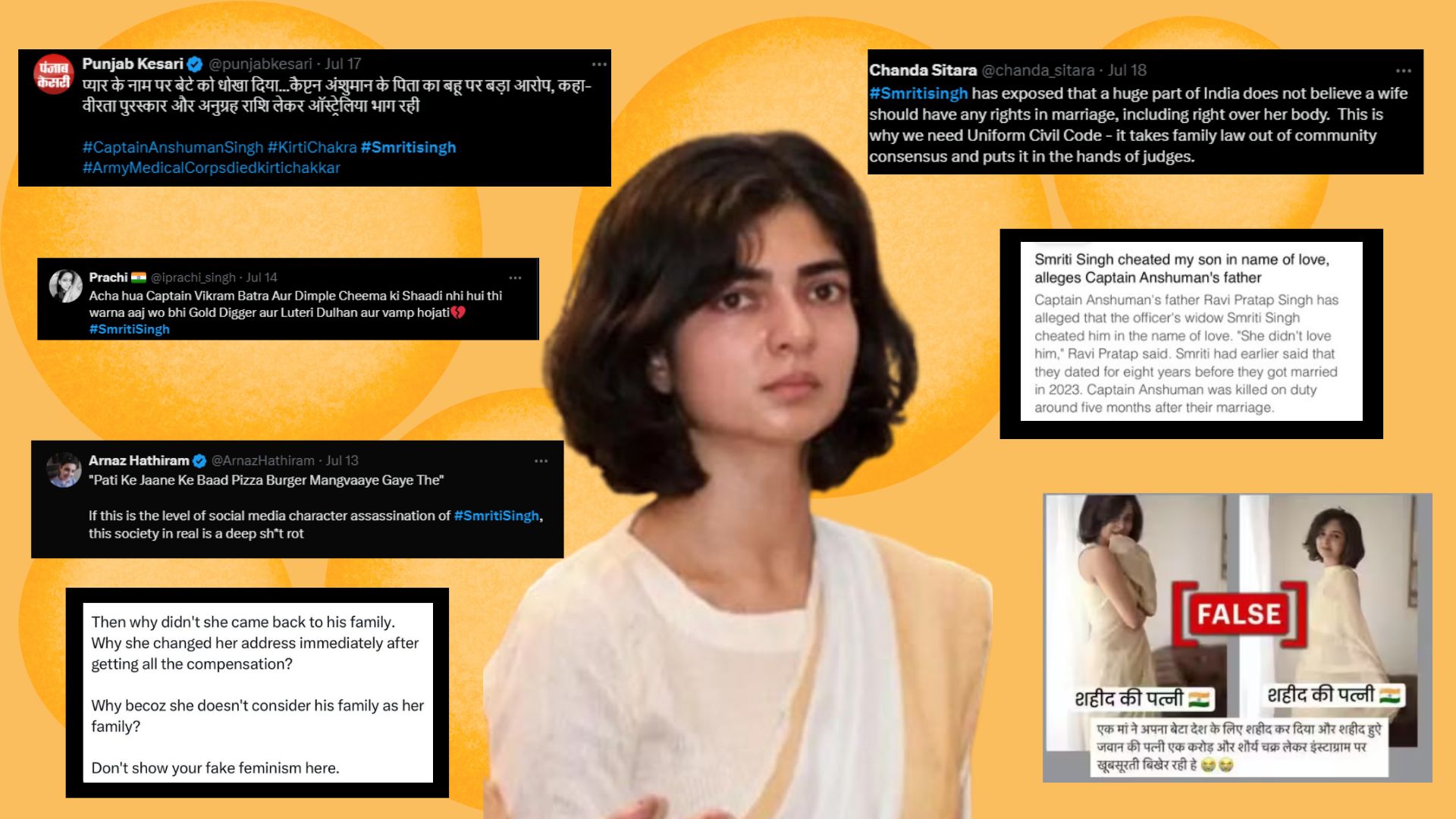हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री, सभी उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों को मुकदमे के कागजात में लिटीगेंट की जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा को रोकने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि इस प्रथा को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष दायर किसी भी याचिका में पक्षकारों के ज्ञापन में मुकदमा करने वाले की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हमें इस न्यायालय या नीचे की अदालतों के समक्ष किसी भी लिटीगेंट की जाति या धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं दिखता है। इस तरह की प्रथा को त्याग दिया जाना चाहिए और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसलिए यह निर्देशित करते हुए एक सामान्य आदेश पारित करना उचित समझा जाएगा कि अब से इस न्यायालय के समक्ष दायर याचिका या कार्यवाही के पक्षकारों के ज्ञापन में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा, भले ही नीचे की अदालतों के समक्ष ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत किया गया हो। सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश राजस्थान की एक पारिवारिक अदालत में लंबित वैवाहिक विवाद में स्थानांतरण याचिका की अनुमति देते हुए दिया।
आम तौर पर कोर्ट तक जाने की प्रक्रिया ही अपनेआप में कठिन, लंबा और खर्चीला होता है। कई बार हाशिये पर रह रहे समुदायों के लिए कोर्ट तक जाना या न्याय की आशा रखना ही एक विशेष मांग है, जिसके लिए उन्हें कई प्रकार से कीमत चुकानी पड़ती है।
क्या असर करेगी यह फैसला
आम तौर पर यह फैसला अपरंपरागत ही सही, लेकिन बहुत सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष लग सकता है। पर क्या सचमुच हमारे देश के कानून से न्याय की गुहार लगाने वालों का धर्म और जाति मायने नहीं रखता? आम तौर पर कोर्ट तक जाने की प्रक्रिया ही अपनेआप में कठिन, लंबा और खर्चीला होता है। कई बार हाशिये पर रह रहे समुदायों के लिए कोर्ट तक जाना या न्याय की आशा रखना ही एक विशेष मांग है, जिसके लिए उन्हें कई प्रकार से कीमत चुकानी पड़ती है।

भारतीय जाति व्यवस्था देश में प्रमुख पहलुओं में से एक है, जहां लोगों को वर्ग, विश्वास, क्षेत्र, जनजाति, लिंग और भाषा के मध्यम से सामाजिक रूप से अलग किया जाता है। ये मूल रूप से भेदभाव का कारण बन जाते हैं। साथ ही, यदि इनके कुछ आयाम एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो व्यक्ति का धन, आय, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच जैसे कारकों को सीधे तौर प्रभावित करते हैं।
न्यायपालिका तक किसकी है पहुंच
हालांकि भारत की न्यायपालिका दुनिया में सबसे बड़ी है और न्याय व्यवस्था को लोगों का खास भरोसा मिलता है। लेकिन, लोग न्यायपालिका के साथ कैसे बातचीत करते हैं या उस तक कितना पहुंच है, या उन तंत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी है जिनके माध्यम से आम जनता में संरचनात्मक असमानता को संबोधित किया जाता है। असल में इसमें कौन भाग ले रहा है, ये समझने के लिए हमें कई मामलों के तह तक जाने की जरूरत है। कोर्ट में केस लड़ने के लिए, याचिका दायर करने या यहां तक कि पुलिस तक जाने के लिए भी देश में आम तौर पर न सिर्फ लैंगिक रूप से वर्चस्व होने की जरूरत है बल्कि शिक्षित और जागरूक होने की भी आवश्यकता होती है।
विश्व बैंक के ब्लॉग में बिहार में औपचारिक न्याय व्यवस्था में व्यक्ति की ‘पहचान’ की भूमिका पर किए गए शोध के परिणाम को बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार, जजों को छोड़कर इन सभी डेटा सेटों में शीर्ष 10 अंतिम नाम; कुमार, सिंह, सिन्हा, मिश्रा, प्रसाद, यादव, रामानंद और झा पाए गए।
विश्व बैंक के ब्लॉग में बिहार में औपचारिक न्याय व्यवस्था में व्यक्ति की ‘पहचान’ की भूमिका पर किए गए शोध के परिणाम को बताया गया। इसमें साल 2009 और 2019 के बीच पटना उच्च न्यायालय में दायर दस लाख से अधिक मामलों के एक डेटासेट का उपयोग किया गया। इसमें लोगों के आर्थिक, जातिगत और सामाजिक स्थिति के साथ न्याय व्यवस्था तक पहुंच और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, जजों को छोड़कर इन सभी डेटा सेटों में शीर्ष 10 अंतिम नाम; कुमार, सिंह, सिन्हा, मिश्रा, प्रसाद, यादव, रामानंद और झा पाए गए। न्यायायिक प्रक्रियाओं के साथ आय, शिक्षा और जागरूकता भी जुड़ी है। यह रिपोर्ट बताती है कि विशिष्ट व्यवसायों में कुछ उपनाम अधिक हैं।
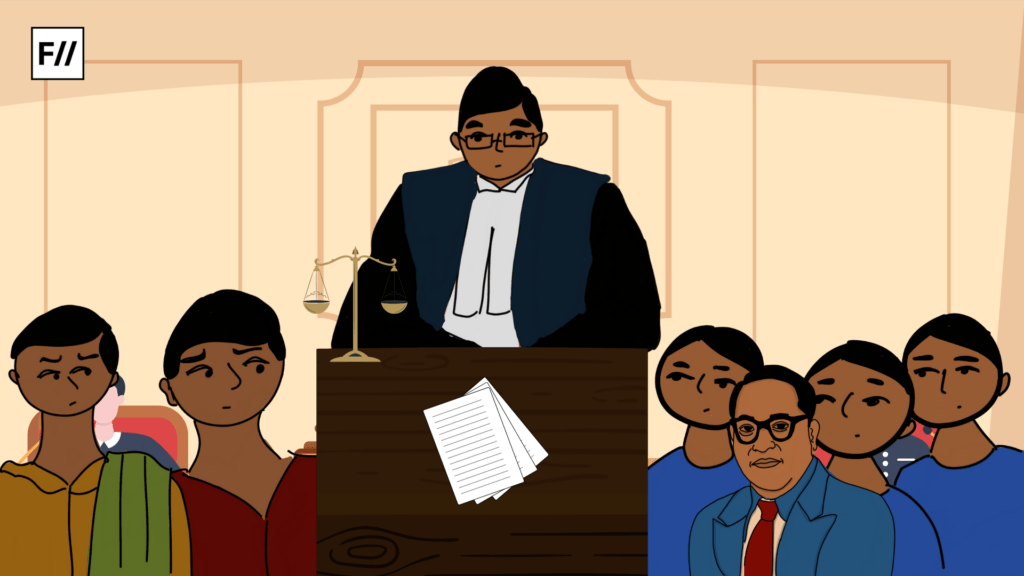
उदाहरण के लिए, सभी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों में से 19 फीसद कुमार हैं। लेकिन किसान केवल 7 फीसद और सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) डेटा में 2 फीसद हैं। वहीं न्यायाधीशों की बात करें, तो इसमें पुरुषों और हिन्दू धर्म का वर्चस्व देखा गया। इस 11 साल की अवधि में 84 न्यायाधीशों में से केवल 6 फीसद महिलाएं और 10 फीसद से कम मुस्लिम थे। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जाति के आधार पर न सिर्फ शादियां बल्कि नौकरी से लेकर स्कूलों में नामांकन तक होता है। जातिगत भेदभाव और असमानता से बचने का सबसे आसान तरीका ‘जाति-तटस्थ’ उपनाम का इस्तेमाल है, जो बिहार जैसे राज्य में आम है। इस शोध में पाया गया कि जिन संस्थानों पर विचार किया जा रहा था, उनमें नामों की शीर्ष 10 सूची में अधिकांश उपनाम जाति-तटस्थ हैं।
टेलर और फ्रांसिस ऑनलाइन में छपे एक शोध मुताबिक 2013 के बाद से पूरे भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कम से कम 80 प्रासंगिक मामलों की पहचान की गई थी। इनमें से 78 मामलों का निपटारा हो चुका है, जबकि 2 का निपटारा अभी नहीं हुआ है।
क्या बताते हैं आंकड़े
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है अनुसूचित जाति (एससी) के खिलाफ अपराध करने के लिए 57,582 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2021 50,900 मामलों की तुलना में 13.1 फीसद वृद्धि है। वहीं 2022 में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध 14.3 फीसद बढ़ गए। देश में जाति और धर्म कितना मायने रखता है, इसे कुछ मामलों से समझने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में भारत में कम से कम दो अधिनियमों, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इन अधिनियमों में कई खामियों के बावजूद जमीनी स्तर के गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट और मीडिया खबरों से पता चलता है कि ये पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं। इनके बुनियाद पर बमुश्किल कोई गिरफ्तारी हुई है, न ही मैनुअल मैला ढोने वालों को काम पर रखने वाले, चाहे वो सार्वजनिक एजेंसियां हों या निजी व्यक्ति किसी पर कोई केस नहीं हुआ है।
इंडिया टूडे में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश एक नियमित दिन में सुनवाई पर औसतन दो मिनट समय खर्च कर सकता है। ऐसे में यह और भी जरूरी है कि मुकदमा लड़ने वाले की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का अंदाज़ा न्यायाधीश के पास हो ताकि फैसले सही और जल्दी हो।
जाति या धर्म आधारित हिंसा और भेदभाव नहीं हुई है बंद
इस मामले में सटीक आंकड़े अस्पष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार के अपराध के आंकड़े उन्हें प्रकाशित नहीं करते हैं। लेकिन, इसका मतलब ये नहीं कि जाति आधारित ये रोजगार बंद हो गया है या मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होती। जैसे, कर्नाटक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2013 और 2019 के बीच 70 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से केवल एक में सजा हुई। हालांकि यह दलील दी जा सकती है कि क्रिमिनल केस में जाति या धर्म मायने रखता है, जबकि सिविल केस में नहीं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। टेलर और फ्रांसिस ऑनलाइन में छपे एक शोध मुताबिक 2013 के बाद से पूरे भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित कम से कम 80 प्रासंगिक मामलों की पहचान की गई थी। इनमें से 78 मामलों का निपटारा हो चुका है, जबकि 2 का निपटारा अभी नहीं हुआ है। 2013 के बाद से समाप्त हुए 78 मामलों में से 80 प्रतिशत से अधिक मामले सिविल पिटिशन यानि नागरिक याचिकाओं के रूप में दायर किए गए थे, और सात प्रतिशत जनहित याचिकाएं थीं। भारत में हजारों ऐसे भयानक और क्रूर घटनाएं हुई हैं, जहां महज जाति या धर्म के आधार पर हिंसा हुई है। चाहे वह 1991 में राजस्थान के भंवरी देवी का मामला हो, या साल 2016 में तमिलनाडु की नंदिनी का मामला हो।
ध्यान दें इस केस में एक उच्च जाति के व्यक्ति ने नाबालिग दलित लड़की के साथ यौन संबंध बनाए। लेकिन जब वह गर्भवती हो गई, तो उसने उसकी जाति के कारण शादी करने से इनकार कर दिया और उस पर अबॉर्शन का दबाव डाला। लड़की के इनकार करने पर, आरोपी और तीन अन्य लोगों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी गई।हालांकि इतिहास में देखा गया है कि हमारा न्यायायिक व्यवस्था भी जाति और धर्म आधारित पूर्वाग्रह से परे नहीं है। इसलिए, महज जाति या धर्म का उल्लेख न करना इसका हल नहीं हो सकता। खासकर तब, जब हमारे कई कानून जाति, समुदाय और धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा हमारे न्यायायिक व्यवस्था में कोर्ट में न्यायाधीश और लोगों के पास संसाधनों की कमी है। इंडिया टूडे में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश एक नियमित दिन में सुनवाई पर औसतन दो मिनट समय खर्च कर सकता है। ऐसे में यह और भी जरूरी है कि मुकदमा लड़ने वाले की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का अंदाज़ा न्यायाधीश के पास हो ताकि फैसले सही और जल्दी हो। हाशिये पर रह रहे समुदायों को सामाजिक और कानूनी तौर पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून जरूरी हैं और इसमें धर्म, समुदाय या जाति अपनी अहम भूमिका निभाता है।