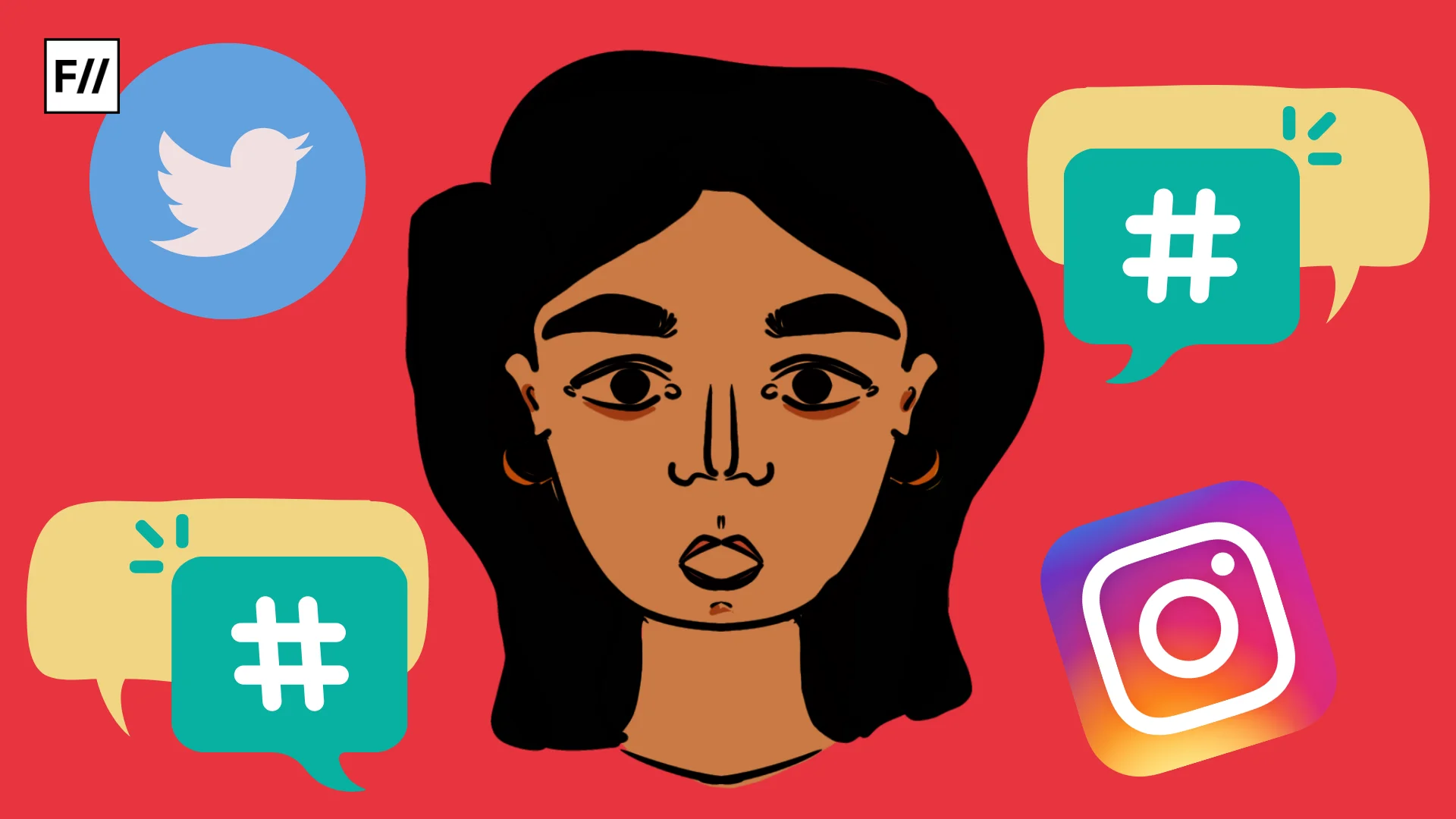साल 2025 बस खत्म होने को है। हर साल की तरह इस साल भी फेमिनिज़म इन इंडिया आपके लिए लेकर आया है उन बेहतरीन 25 लेखों की सूची जिन्हें आपने सबसे ज्यादा पसंद किया और पढ़ा।
1- हिन्दी साहित्य में एक महिला का ‘लेखिका’ बनने का संघर्ष!- रूपम मिश्र
आज हिंदी साहित्य में महिलाओं की भूमिका का काफी हद विस्तार हुआ है। लेकिन, इसके साथ ही उनके संघर्ष और चुनौतियां भी बढ़ी हैं। आज लेखिकाएं संस्मरण और आत्मकथाओं से लेकर निबंध, व्यंग्य, आलोचना और कविताओं तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। साहित्य में महिलाओं की लेखनी व्यापक स्तर पर फैला हुआ दिखता है। लेकिन हिंदी साहित्य में स्त्रियों के लेखन की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी हमारी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद, जिस तरह से हिंदी साहित्य में महिलाओं ने अपनी जगह बनायी है, वो अनोखा और काबिलेतारीफ़ है। इस दशक में हिंदी साहित्य में स्त्री कविता का उदय होना भी एक बड़ी घटना है। आज बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी-अपनी कविताओं के साथ हिंदी साहित्य की जमीन को और मजबूत कर रही है।
2- मेरा फेमिनिस्ट जॉय: गरीबी और संघर्ष से विश्वविद्यालय तक का मेरा सफर– करीना जगत
मेरा बचपन गरीबी, भूख, लैंगिक भेदभाव और जातिगत अन्याय के साये में गुजरा। ये सब मेरी जिंदगी के हिस्से नहीं, बल्कि हर दिन की हकीकत थे। हमारे घर और समुदाय में बच्चों की शिक्षा एक सपना था, जो हकीकत से बहुत दूर लगता था। हमारे परिवार के लिए पेट भर खाना जुटाना ही बड़ी चुनौती थी। कभी घर में खाना बनता, तो कभी नहीं। ऐसे दिनों में माँ आंगनवाड़ी से लाए सत्तू का घोल बनाकर हमें पिलाती थीं, जिससे हमारी भूख कुछ समय के लिए शांत हो जाती। मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि पापा को काम मिल जाए, ताकि रात का खाना मिल सके। मेरा भाई पास के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और मैं घर के पास की बालवाड़ी जाती थी। वहां एक दीदी हमें पढ़ाती थीं। हर दिन, मैं एक वैन को बस्ती में आते देखती, जिसमें बड़े बच्चे बैठकर स्कूल जाते थे। बाद में मुझे पता चला कि यह स्कूल एक संस्था द्वारा चलाया जाता है।
3- क्यों महिलाओं के लिए ‘संडे’ हॉलिडे नहीं होता है?– पूजा राठी
सुबह छह बजे तेजी से डेयरी से दूध लेकर घर की ओर जाने वाली सरोज की साल दर साल की यह दिनचर्या है। उनके इस काम के बीच न कोई बारिश, न कोई तूफान बाधा डालता है और न ही उनका कोई छुट्टी का दिन होता है। दरअसल अक्सर हमारे समाज में महिलाएं घर के कामों में या नौकरीपेशा होकर लगातार बिना किसी ब्रेक के काम करती है। इतना ही उनके काम की कोई सीमा भी नहीं है। महिलाएं लगातार बिना किसी छुट्टी के अवैतनिक काम करती है जिससे हमारे और आपके घर चलते हैं। हाल ही में एल एंड टी के चेयरमेन एसएन सुब्रह्मणयम ने इस बात पर अफसोस जताया कि वे अपने कर्मचारियों से रविवार को काम नहीं करवा सकते हैं। उन्होंने सफलता के लिए एक सप्ताह में 90 घंटे काम करने पर जोर दिया है। अपने व्यंग्यात्मक बयान में उन्होंने यह तक कहा कि आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक घूर सकते हैं?
4- भारत में दलित नारीवाद का इतिहास और वर्तमान– वर्षा प्रकाश
आज भी सैद्धांतिक रूप से मुख्यधारा का नारीवाद अपने भीतर की खामियों को दूर करने की राह पर है। ये वे खामियां हैं जिसकी जड़ें भारतीय नारीवाद के विकास के इतिहास में उभरकर आनी शुरू हुईं। इतिहास में मुख्यधारा के नारीवादी विमर्श में दलित महिलाओं को जोड़ने का सवाल और बहस इन्हीं खामियों से संबंधित हैं। भारतीय समाज में दलित महिलाओं के साथ सदियों के शोषण, अपमान, भेदभाव और उत्पीड़न में न केवल उनका ‘महिला होने’ का कारण शामिल है बल्कि ‘तथाकथित निचली जाति से होने’ का कारण भी बराबर शामिल है। जैसे अफ्रीकन-अमेरिकन समाज में ब्लैक महिलाएं एक महिला होने की वजह के साथ-साथ नस्लवाद जैसी वजह से भी दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। ऐसे दोहरे भेदभाव की प्रवृति दलित महिलाओं के साथ भी दिखाई देती है। दलित महिलाओं को लैंगिक भेदभाव, छुआछूत और जाति आधारित अत्याचारों के कारण तथाकथित उच्च जाति के लोगों द्वारा तो प्रताड़ित किया ही गया, साथ ही अपने पुरुषों के द्वारा भी सताया गया है जिसकी असल वजह ‘ब्राह्मणवादी व्यवस्था’ है।
5- सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय की युवतियों की अपनी-अपनी सावित्री!- सबा खान
सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका हैं। उन्होंने देश में लड़कियों और औरतों के शिक्षा के अधिकारों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ीं। अंग्रेजी शासन के दौर में जब अंग्रेज भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे थे तब भी भारतीय समाज में महिलाओं को केवल घर के कामों तक सीमित रखा जा रहा था। ऐसे समय में सावित्री बाई ने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया। इतना ही नहीं उन्होंने विधवा विवाह, गर्भवती बलात्कार सर्वाइवरों का पुनर्वास और छुआछूत मिटाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। हर साल तीन जनवरी को सावित्री बाई फुले का जन्मदिवस मनाया जाता है। अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। भोपाल शहर में स्थित सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख लाईब्रेरी और सेंटर्स पर इस दिन को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। किशोर और किशोरियां सावित्रीबाई की कविताएं पढ़ते हैं। सावित्रीबाई और फातिमा शेख की दोस्ती को दिखाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। कोई सावित्रीबाई की तरह कपड़े पहनता है। शिक्षा जगत में उनके योगदान के बारे में किशोर और किशोरियों के बीच चर्चा होती है। युवा लड़कियों में खूब जोश दिखाई देता है। इन सेंटरों पर अधिकतर हाशिये के समुदाय की लड़कियां आती हैं जो अलग-अलग समय पर सावित्रीबाई के संघर्षों उनके कामों को याद कर खुद में ताकत महसूस करती हैं। सावित्रीबाई “यानि हमारी पुरखिन“ कैसे हमारी प्रेरणाओं का स्त्रोत हैं और पुस्तकालय आने वाली किशोरियों और युवाओं के लिए उनका होना क्या मायने रखता है यह हमने जाना।
6- ‘मेनोपॉज’ के बारे में कितनी जागरूक हैं ग्रामीण महिलाएं?– राखी यादव
मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच होता है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर में आने वाला एक जैविक परिवर्तन है, जो उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से होता है। फिर भी, समाज में इसे लेकर कई तरह की भ्रांतियां और कलंक जुड़े हुए हैं, जिससे लोगों को विशेषकर महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरों की तुलना में ग्रामीण भारत में पीरियड्स की तरह ही, मेनोपॉज को लेकर भी जागरूकता कम है। जहां पीरियड्स में महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तो वही मेनोपॉज में पीरियड्स साइकिल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट अनुसार भारत में 66 फीसद महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं मेनोपॉज पर बात करने में आज भी असहज महसूस करती हैं। महिलाओं में इस दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से हॉट फ़्लैशेज़ (अचानक तेज़ गर्मी महसूस करना), चिड़चिड़ापन, नींद ना आना जैसी समस्याएं हो सकती है। इन समस्याओं के बावजूद, गांवों में जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के कमी के चलते महिलाओं के लिए इसपर खुलकर बात करना मुश्किल है।
7-आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद महिलाओं को सम्मान और बराबरी क्यों नहीं मिलती?– शहनाज़
कुछ समय पहले एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी। उस दोस्त का कहना था कि पैसा अपने साथ एक क़िस्म की ताकत लेकर आता है। जब आप अच्छा कमाते हो तो घर में आपका मूल्य और सम्मान बढ़ जाता है। अगर महिलाएं ज़्यादा कमाएंगीं तो परिवार में उनका रुतबा बढ़ जाएगा। आम धारणा के उलट, अगर इस बात पर गौर करें, तो किसको सामाजिक तौर पर कितना सम्मान मिलता है इसके पीछे बहुत से कारक काम करते हैं। वास्तव में नौकरीपेशा महिलाओं को समाज और परिवार कितना महत्त्व देते हैं, इसे समझने के लिए न सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है बल्कि नौकरीपेशा महिलाओं के अनुभवों को समझने को दर्ज करने की ज़रूरत है। आज से कुछ साल पहले तक नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम थी। लेकिन अब पहले की अपेक्षा कई महिलाएं नौकरीपेशा हैं।
8- कोरबा की कोयला खदानें: विकास की कीमत पर उजड़ते घरों का जिम्मेदार आखिर कौन?– रचना
भारत अपनी विविधता और लोकप्रिय संस्कृतियों के लिए मशहूर है। भारतीय संस्कृति की तरह यहां की जनजातियां भी बहुत अलग-अलग हैं। हर जनजाति की अपनी खास पहचान होती है, जैसे उनकी भाषा, पोशाक, रहन-सहन, लोक नृत्य, कला और परंपराएं। ये सब उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं और उन्हें समाज में अलग पहचान दिलाते हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की एक पुरानी और महत्वपूर्ण जनजाति है भील समुदाय, जो अपनी ‘हलमा’ परंपरा के लिए जाना जाता है। हलमा एक खास लोक कला और सांस्कृतिक अनुष्ठान है, जो राज्य के कई हिस्सों में प्रचलित है। यह खासतौर पर आदिवासी इलाकों में सामूहिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हलमा भील समाज की एक ‘मदद की परंपरा’ है। जब कोई व्यक्ति या परिवार किसी संकट में फँस जाता है और खुद उससे नहीं निकल पाता, तो पूरे गांव के लोग उसकी मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं।
9- नारी बहिनी का संघर्ष: बंगाल के तेभागा आंदोलन की अनसुनी कहानियां– सौरभ खरे
महिला इतिहास को जानने के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि हम उन योगदानों की बात और समीक्षा करें जहां महिलाओं ने प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में हिस्सेदारी निभाई है। भारतीय इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण लेकिन कम प्रतिनिधित्व वाला अध्याय है साल 1946-47 में बंगाल का तेभागा आंदोलन। पश्चिम बंगाल भारत के कृषक आंदोलनों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जहां किसान शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। नील विद्रोह, पाबना कृषक आंदोलन से लेकर सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों तक, इस क्षेत्र ने सशक्त ग्रामीण प्रतिरोध देखा है। इन सभी में, साल 1946–47 का तेभागा आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जिसने बटाईदार किसानों के अधिकारों की लड़ाई को नया आयाम दिया। यह आंदोलन किसानों ने शुरू किया था और वामपंथी संगठनों का समर्थित था।
10- बिहार में शराबबंदी के बाद महिलाओं के अनुभव और चुनौतियां- सुष्मिता मंडल
बिहार के मझोलिया गांव में, घरों के सामने अपने व्यस्त दिन के बाद महिलाएं आग जलाए घर के बाहर आँगन में बैठी हुई थीं। ठंड का मौसम था इसलिए आग के पास बैठकर ठहाके चल रहे थे। बिहार में शराब बंदी का निर्णय 2016 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य समाज में घरेलू हिंसा पर रोक, स्वास्थ्य और सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना था। बिहार सरकार ने शराब बंदी लागू करके एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा। प्रशासन ने अवैध बाजार को रोकने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन भ्रष्टाचार और अपर्याप्त निगरानी के कारण कई बार यह प्रयास सीमित साबित हुए। इन महिलाओं से बिहार में शराबबंदी पर पूछे जाने पर उनकी आँखों में हलचल सी दिखी। कुछेक हंसने लगी। इस विषय पर पश्चिमी चंपारण जिले की लौरिया व्यासपुर गांव की कुर्मी समुदाय की 70 वर्षीय सरला (बदला हुआ नाम) कहती हैं, “कौन सी बंदी? यहां तो हर कहीं मिल जाता है।”
11- दिल्ली के वायु प्रदूषण में जूझते दिहाड़ी मजदूरों का संघर्ष– ज्योति कुमारी
दिल्ली की बदलती वायु प्रदूषण ने लोगों का जीवन गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसकी वजह से लोगों को तरह-तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदूषण से सभी प्रभावित होते हैं लेकिन, अगर वायु प्रदूषण की बात करें, तो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित ‘डेली वेज वर्कर’ यानी दिहाड़ी मजदूर होते हैं। दिल्ली में हर साल सर्दी की शुरुआत होते ही आंखों में जलन और सांस फूलने की समस्या आम हो जाती है। एक समय ऐसा भी आता है जब दिल्ली धुंध के चेम्बर में तब्दील होती नजर आती है। साल दर साल बढ़ता प्रदूषण और जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस बीच दिहाड़ी मजदूरों की चुनौतियों और समस्याओं को समझने के लिए फेमिनिज़म इन इंडिया ने कुछ लोगों से बातचीत की।
12-क्यों बार-बार सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं आशा कार्यकर्ताएं?– अतिका सईद
भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का अहम हिस्सा निभाती आशा कार्यकर्ता, आज भी खुद ही बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। साल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त इन महिलाओं की ज़िम्मेदारियां लगातार बढ़ी हैं, लेकिन उन्हें अब भी ‘स्वयंसेविका’ के रूप में बताया जाता है। इसका मतलब है कि न तो इन्हें अच्छा मानदेय दिया जाता है, न पेंशन और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। प्रोत्साहन आधारित भुगतान प्रणाली में उन्हें हर सेवा के लिए कुछ सौ रुपये मिलते हैं, जो कई बार महीनों तक लंबित रहता है। साल 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ) ने उन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से नवाज़ा, लेकिन भारत में यह सम्मान नीतियों में बदलाव नहीं ला सका है। देशभर में आशा कार्यकर्ताएं नियमित वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए हजारों आंदोलन कर चुकी हैं।
13- ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को चुनौती देती, स्त्री अस्मिता की आवाज़ है कृष्णा सोबती की ‘मित्रो मरजानी’– सरला अस्थाना
‘मित्रो मरजानी’ कृष्ण सोबती की लिखी हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी उपन्यास है। साल 1967 में प्रकाशित यह उपन्यास साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे पुरस्कारों से सम्मानित होने के बावजूद, कृष्णा सोबती की लेखनी आलोचनाओं का कम सामना नहीं की है। मित्रो मरजानी के प्रकाशन के बाद उनपर जातिवादी होने का गंभीर आरोप लगाया गया। नारी स्वतंत्रता को केवल यौनिकता की परिधी तक सीमित रखने की बात भी की गई। जब कोई लेखक किसी नए परिप्रेक्ष्य को पाठकों के सामने रखते हैं, जो सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से अलग होता है, तो उसकी किसी न किसी रूप में आलोचना तय होती है। मित्रो मरजानी के माध्यम से सोबती सबसे अनछुए पहलू को बहुत ही बेबाकी से लोगों के सामने रखती हैं।
14- क्यों जाति और जेंडर तय करते हैं खाने का ‘अधिकार’?– अनामिका
मनुष्य की आधारभूत जरूरतों में से भोजन भी एक अहम हिस्सा है। भोजन सिर्फ थाली और खाने वाले तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जगह, वर्ग और जाति जैसे कारकों के हिसाब से बदलता रहता है। इसी के हिसाब से पारंपरिक व्यंजन भी अलग-अलग होते हैं। खाने की इच्छा हर व्यक्ति में एक जैसी होती है फिर भी इसके नियम सभी के लिए एक नहीं है। भोजन को सार्वजनिक रूप से खाने और बनाने के नियम एकदम अलग हैं और यह नियम समस्या तब बन जाते हैं, जब जाति और लिंग इनके आड़े आता है। एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति के लिए यह सोच पाना भी मुश्किल होगा कि कोई खाने के प्रति जातिवादी कैसे हो सकता है? अमूमन ये कहा जाता है कि दलित और महिलाएं दोनों की स्थिति एक जैसी है।
15- कैसे उत्तराखंड की महिलाएं होमस्टे के व्यवसाय से बदल रही हैं अपनी दुनिया– दया
उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पर्यटन क्षेत्र को एक नए रोजगार के रूप में अपना रही हैं। यह उनके लिए न केवल एक नया अनुभव है, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। दरअसल, पर्यटन जैसे कार्यों पर लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में महिलाओं का इस क्षेत्र में आना एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है। परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों की महिलाएं सदियों से कृषि और पशुपालन जैसे कामों में संलग्न रही हैं। लेकिन अब वे अपने घरों को होमस्टे में बदलकर पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, खानपान और पहाड़ी जीवनशैली का अनुभव दे रही हैं। इस पहल से न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। होमस्टे के ज़रिए महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मज़बूती दे रही हैं। पर्यटन के माध्यम से महिलाएं अब सेवा क्षेत्र में एक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
16- मेरे पहले पीरियड्स में डर और चुप्पी से जागरूकता तक का सफ़र– नाज़नीन
भारत में आज भी पीरियड्स को लेकर खुलकर बात करना आसान नहीं है। यह एक जैविक प्रक्रिया होते हुए भी शर्म, सामाजिक चुप्पी और रूढ़ियों से घिरी हुई है। खासकर किशोरावस्था में जब लड़कियां अपने शरीर में होने वाले बदलावों को समझने की कोशिश कर रही होती हैं, तब उन्हें डराया या चुप कराया जाता है और कई बार गलत सूचनाएं दी जाती हैं। द हिन्दू में छपी रिपोर्ट अनुसार एक गैर सरकारी संगठन का किया एक सर्वेक्षण से पता चला है कि करीब 12 फीसद युवतियां पीरियड्स का सही कारण नहीं जानतीं और मानती हैं कि यह ईश्वर का श्राप है या बीमारी के कारण होता है। नतीजा यह होता है कि वे अपने अनुभवों को छिपाने लगती हैं और उस अकेलेपन या समस्याओं का सामना करती हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। पीरियड्स को लेकर जो पहली यादें होती हैं, उनमें डर, दर्द और ढेर सारी चुप्पी शामिल होती हैं। मेरी भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। यह सिर्फ मेरी नहीं, देश की लाखों लड़कियों की साझा सच्चाई है।
17- अरुणा रॉय की ‘द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल’: जहां निजी अनुभव बनते हैं राजनीतिक बदलाव की बुनियाद– शिवानी खत्री
अरुणा रॉय की किताब ‘द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल’ सिर्फ उनकी ज़िंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हमारे अपने निजी अनुभव भी राजनीति से जुड़े हो सकते हैं। इस किताब में अरुणा बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर गांवों में लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने यह सीखा कि असली समझ सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ जीकर आती है। किताब की शुरुआत से ही रॉय की आवाज़ सोचने-समझने वाली लगती है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस ) जैसी बड़ी नौकरी छोड़ दी और राजस्थान के गांवों की ओर चली गईं। उन्होंने तिलोनिया के बेरफुट कॉलेज में काम किया, जहां उन्होंने उन लोगों के बीच असली ज्ञान को महसूस किया जो पढ़ – लिख नहीं पाए थे।
18- कैसे बिहार की राजनीति में महिलाएं संघर्ष से निर्णायक नेतृत्व तक भूमिका निभा रही हैं– रोकैया बुशरी
बिहार का राजनीतिक क्षेत्र हमेशा से अपने उतार-चढ़ाव और गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभावों के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस बदलाव ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा है, वह है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हमेशा से चर्चा का विषय रही है। इंडिया टुडे के मुताबिक, यह बदलाव साल 2010 में शुरू हुआ । उस साल, 162 निर्वाचन क्षेत्रों में 54 फीसदी महिलाओं ने मतदान किया, जो पहली बार पुरुषों की तुलना में 51 फीसदी से ज़्यादा था। साल 2015 में, यह अंतर और बढ़ गया, जब 60 फीसदी महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों ने केवल 50 फीसदी मतदान किया।
19- आत्मकथाएं और मानसिक स्वास्थ्य: स्त्री लेखन की चुप्पी तोड़ती आवाज़ें– शिरीष फिरोज़
हिंदी साहित्य में आत्मकथा लेखन एक ऐसी विधा है, जहां व्यक्ति अपने मन और जीवन के अनुभवों को समाज के सामने रखता है। यह सिर्फ़ जीवन की कहानी नहीं होती, बल्कि अपने समय और समाज का आईना होती है। स्त्री आत्मकथाएं और भी खास हैं, क्योंकि इनमें महिलाएं अपने जीवन की सच्चाइयों, संघर्षों और मनोवैज्ञानिक अनुभवों को खुलकर लिखती हैं। इन आत्मकथाओं में हिंसा, वर्जनाएं, मानसिक पीड़ा और समाज की पितृसत्तात्मक संरचनाएं झलकती हैं। ऐसे लेखन में हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, बचपन की प्रताड़ना, और सामाजिक दबाव किस तरह स्त्रियों के मन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। स्त्री आत्मकथाएं सिर्फ़ व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि समाज में स्त्रियों के दमन और मानसिक संघर्षों का दस्तावेज़ भी हैं।
20- क्यों ज़रूरी है भारत में सेक्स एजुकेशन का सामान्य होना?– मानसी सिंह
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्स एजुकेशन की शुरुआत कक्षा 9 से नहीं, उससे पहले होनी चाहिए। यह बात सिर्फ़ नीति से जुड़ी नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक संवेदनशील सुझाव भी थी। अदालत ने कहा कि जब तक कोई बच्चा किशोरावस्था की दहलीज़ पर पहुंचता है, तब तक वह इंटरनेट से अधूरी या ग़लत जानकारी के संपर्क में आ चुका होता है। यह टिप्पणी हमारे समाज के लिए एक आईना है। असल में हमारे बच्चे सवाल पूछने को तैयार हैं, लेकिन समाज अब भी सेक्शुअल एजुकेशन से जुड़े जवाब देने से कतराता है। हमारी शिक्षा प्रणाली जीव विज्ञान तो पढ़ाती है, पर जीव और संबंधों पर बात करने से अब भी झिझकती है। सेक्शूअलिटी एजुकेटर और अनटैबू की संस्थापक अंजू किश सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करती हैं।
21. कन्वर्ज़न थेरेपी: प्यार और आस्था के नाम पर क्वीयर लोगों के खिलाफ़ होती हिंसा– मालविका धर
हिमाचल प्रदेश के 33 वर्षीय क्वीयर, जेंडर फ्लूइड मृणाल कहते हैं, “मेरा परिवार बहुत धार्मिक है और कुछ हद तक अंधविश्वासी भी। मेरी माँ को मेरे यौनिकता के बारे में पता चलने के बाद, उन्होंने मेरे इलाज के लिए धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दीं। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा परिवार संतुष्ट रहे। बाद में, उन्होंने एक पारिवारिक परिचित व्यक्ति से मेरे यौनिकता के इलाज के बारे में पूछा। उन्होंने एक तरीका सुझाया जिसमें वह मेरा जांच करते। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ये एक कमरे में अकेले करें। वह मुझे इरेक्शन के लिए मजबूर करता और मुझे लगातार छूता रहता। इस तरह यह यौन हिंसा सालों तक चलता रहा, जब तक कि मैंने उस व्यक्ति के साथ एक रात अकेले बिताने से इनकार नहीं कर दिया।”
22. कैसे ब्रेस्टफीडिंग पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जरूरी विकल्प है?-सविता चौहान
जब हम पर्यावरण की रक्षा, संसाधनों की बचत और स्थायित्व या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो अक्सर बड़ी-बड़ी तकनीकी पहलें ग्रीन एनर्जी, या वृक्षारोपण जैसे समाधान हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि एक मां का अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग या स्तनपान कराना भी पर्यावरण की रक्षा में उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है? ब्रेस्टफीडिंग केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक, स्थायी और संसाधन-संरक्षण करने वाली प्रक्रिया है, जो ना केवल शिशु और मां के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है।
23- इतिहास और साहित्य में महिलाओं की अनुपस्थिति वर्जीनिया वुल्फ़ की दृष्टि से– मंशा मिश्रा
बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपीय समाज परिवर्तन के दौर से गुज़र रहा था। औद्योगिक क्रांति, राजनीतिक उथल-पुथल और युद्धों के बीच मनुष्य की चेतना भी अपने भीतर नए प्रश्नों का सामना कर रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में जन्म लेती, आधुनिक स्त्री-चेतना का मजबूत स्वर वर्जीनिया वुल्फ़ के लेखन में साफ़-साफ़ सुनाई देता है। वुल्फ़ न केवल आधुनिक अंग्रेज़ी साहित्य की अग्रणी उपन्यासकार थीं, बल्कि नारीवादी चिंतन की एक महत्वपूर्ण विचारक भी रही। उनका प्रसिद्ध निबंध अपना कमरा एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसमें उन्होंने इतिहास और साहित्य से महिलाओं की अनुपस्थिति की समस्या को बहुत ही बारीकी से उजागर किया है। उनका मुख्य प्रश्न यह है कि इतिहास की पुस्तकों में महिलाएं कहां हैं? यह सवाल केवल उपस्थिति का संकेत नहीं, बल्कि उस सामाजिक और ज्ञानात्मक संरचना की आलोचना है, जिसने सदियों तक महिलाओं को विषय नहीं, बल्कि वस्तु के रूप में देखा।
24- जेलों में महिला कैदियों की पीरियड्स से जुड़ी चुनौतियां– मासूम क़मर
भारत में पिछले कुछ सालों में पीरियड्स और स्वच्छता को लेकर कुछ सकारात्मक बदलाव दिखे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019–2020 के अनुसार, 15 से 24 वर्ष की उम्र की लगभग 10 में से 8 युवतियां अब सुरक्षित स्वच्छता उत्पादों का इस्तेमाल कर रही हैं। खासकर शहरी इलाकों और कुछ वर्गों में स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन इस सुधार की तस्वीर पूरी नहीं है। समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले समूहों में से एक–जेलों में बंद महिलाएं अब भी इस बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। देश में जेलें एक ऐसा संस्थान है, तो आम तौर पर राजनीतिक चर्चा से एकदम अदृश्य है। सामाजिक पूर्वाग्रह और व्यवस्था की लापरवाही के कारण उनकी ज़रूरतों को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है।
25- भारत में कला और एक्टिविज़्म की कुछ सशक्त क्वीयर आवाज़ें– इमरान खान
प्राइड मंथ एक ऐसा वैश्विक पर्व है जो केवल उत्सव नहीं, बल्कि इतिहास, पहचान और संघर्ष की स्मृति है। यह महीना क्वीयर समुदाय के आत्मसम्मान, अधिकारों और उपलब्धियों को सम्मान देने का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम किसी भी परिभाषा में सीमित नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। आज प्राइड का स्वरूप केवल बड़े शहरों, रंग-बिरंगी परेड या कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। यह ग्रामीण इलाकों, आदिवासी समुदायों और तकनीकी दुनिया जैसे उन क्षेत्रों तक भी पहुंच चुका है जहां पहले क्वीयर पहचान को जगह नहीं मिलती थी। प्राइड मंथ अब वह स्पेस बन चुका है, जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले क्वीयर लोगों की आवाज़, संघर्ष और रचनात्मकता को सामने लाता है।