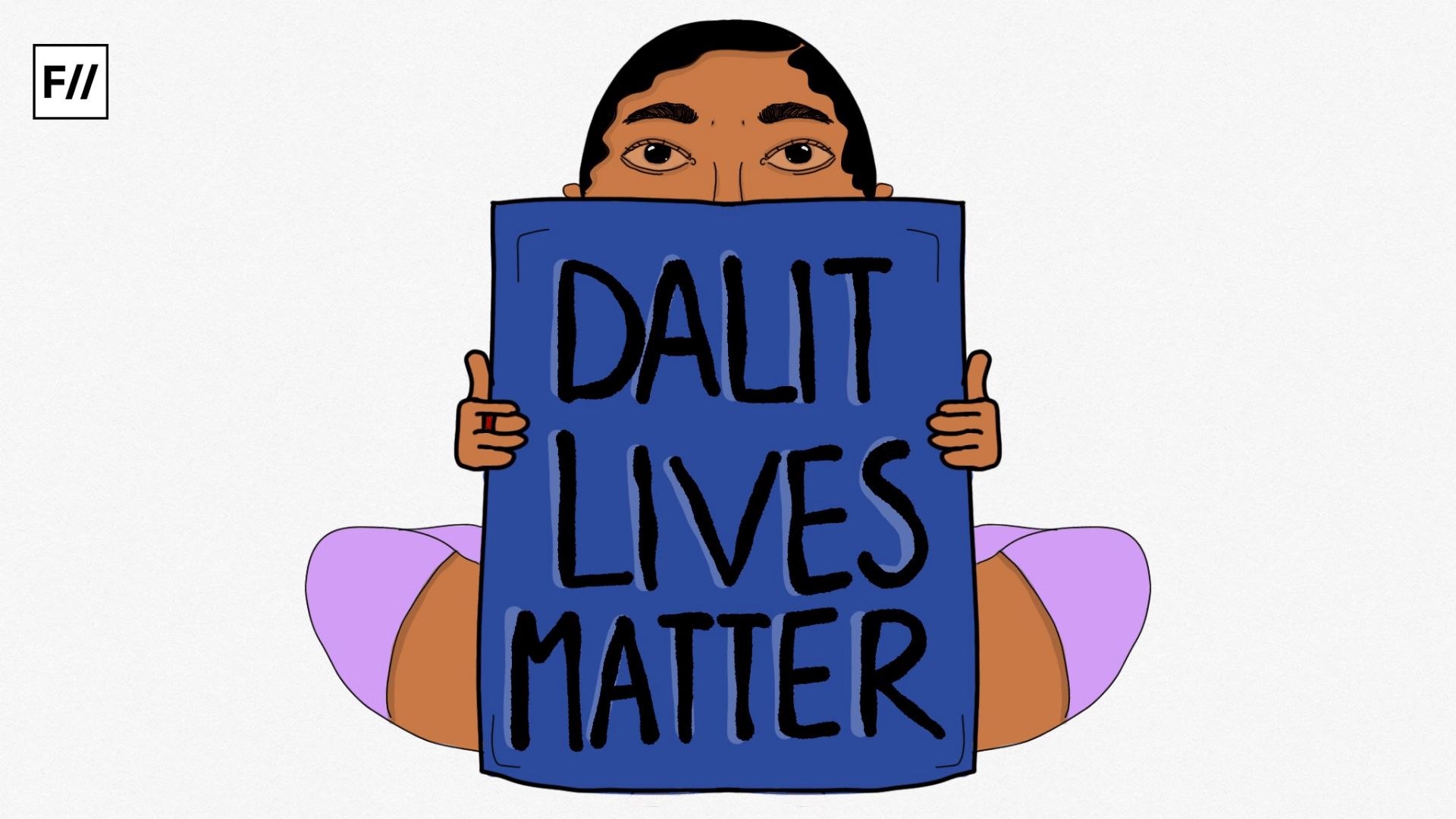शहर का नाम सुनते ही मन के भीतर कई अनगिनत विचार आने लगते हैं। ये विचार इतने आदर्शवादी होते हैं कि शहर तमाम पूर्वाग्रहों से अछूते दिखाई देने लगते हैं। शहर की खूबसूरत और बाहरी विरासत की चकाचौंध से लेकर यहां के तमाम खुले और प्रगतिशील लगनेवाले चलन लोगों को लुभावने लगते हैं। यह शहरों को लेकर एक सामान्य सा नज़रिया है। यहां रहनेवाले और नये-नये बसनेवाले, दोनों तरह के लोगों के बीच बननेवाले आपसी संबंध एक मुख्य कारक से ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
यह कारक या तो दिमाग में बैठी कुंठा को व्यवहार में बाहर ला देगा या तो नयी दोस्ती को अंजाम देगा। वह कारक है-जाति। कोई आपसे आपकी जाति या तो सीधे-सीधे पूछने लगेगा या तो आपके सरनेम को इस तरह से टटोलना शुरू कर देगा कि वह आपकी जाति तक पहुंच सके। शहर में जातिवाद की यह संस्कृति इतनी सामान्य हो चुकी है की उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही इसमें सहजता से खुद को समायोजित कर चुके हैं।
“अब जात-पात कहां ही है”
महानगरों में अधिकतर लोग पूरे भरोसे के साथ इस बात से सहमत होते नहीं थकते कि शहरों में अब जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद के अस्तित्व को नकारने की यह धारणा ऐसे दिखाई देती है मानो इरादे से खुद को तसल्ली देने के लिए अपने भीतर पैदा की गई हो। यह धारणा हमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिग्मंड फ्रायड के एक विचार की याद दिलाता है। फ्रायड के इस विचार के अनुसार जब कभी लोग किसी बात से चिंतित, कम आत्मविश्वासी, किसी बात को एहतिहात से छिपाना चाहते हैं तो वे इन सभी परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ करने के लिए अपने भीतर मौजूद ‘रक्षा तंत्र’ का इस्तेमाल करते हैं’। फ्रायड के रक्षा तंत्र, ‘डिनायल’ में मानव अपने भीतर और बाहर कोई मौजूदा या घटित बात को मानने से इनकार करने की कोशिश करता है।
इस इनकार को हम दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे कई लोगों के इस कथन में देखने की कोशिश कर सकते हैं जो जातिवाद के बरक़रार अस्तित्व को जानबूझ कर नकारते हुए कहते हैं, “आज कल शहरों में कहां ही जातिवाद होता है।” इस कथन का शहरों में अत्यधिक सामान्यीकरण हो चुका है। वे लोग जो पहले से ही शहरों में रह रहे होते हैं या जो लोग अपने गांवों और छोटे शहरों को छोड़कर महानगरों में काम करने और पढ़ने आते हैं, दोनों ही इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि जातिवाद आज भी बरक़रार है।
हो सकता है अगर सोचने भी लगे या इस बात को स्वीकार कर लें कि महानगरों में जातिगत भेदभाव बेहद अंदर तक धंसा हुआ है तो उनकी प्रगतिशीलता को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। फिर ये शहर ही तो है जहां का पढ़ा-लिखा वर्ग आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था को हर रोज़ धिक्कारने में लगा रहता है। शहरों में लोगों के ज़हन में बने जातिवादी चेहरे, प्रतीकात्मक रूप से उनके व्यवहार के जरिये सामने आते हैं। हमने इस लेख में बड़े शहरों की सच्चाई को बयां करते जातिवादी व्यवहार को झेलनेवाले लोगों के अनुभवों को सामने लाने का प्रयास किया है। ये सिर्फ अनुभव ही नहीं हैं बल्कि ये हमें कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते लोकतंत्र की सफलता के लेखाचित्र को भी बयां करते हैं।
विद्यार्थियों को घर से मिलनेवाली जातिवादी सीख
आजकल बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों में जातिवाद का सामना करते विद्यार्थियों से जुड़ी खबरें लगातार आती रहती हैं। शिक्षण संस्थानों में जातिवादी मानसिकता के रवैये का यह प्रकोप इतना ज़्यादा बना हुआ होता है की इसके असहनीय यातनाओं से तंग आकर दलित विद्यार्थी आत्महत्या से मौत जैसे कदम उठा रहे हैं या फिर कई चुपचाप इसे सहते आते हैं। जातिवाद मानसिकता परिवार के द्वारा प्राथमिक समाजीकरण के दौरान मिली ख़राब रूढ़िवादी मूल्यों और विचारों को व्यक्ति के दिमाग में भरने का ही नतीजा होती है।
वे लोग जो पहले से ही शहरों में रह रहे होते हैं या जो लोग अपने गांवों और छोटे शहरों को छोड़कर महानगरों में काम करने और पढ़ने आते हैं, दोनों ही इस बात से वाकिफ़ होते हैं कि जातिवाद आज भी बरक़रार है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.ए हिंदी की पढ़ाई कर रहे चंदर बिहार के रहनेवाले हैं। जब वह दिल्ली अपनी पढ़ाई के लिए आ रहे थे तो उन्हें उनके परिवारवालों ने सख़्त जातिवादी हिदायतें दी थीं। चंदर को यह कहा गया कि वह बाहर पढ़ने तो जा रहे हैं लेकिन वह किसी भी दलित-बहुत जाति के लोगों से मित्रता नहीं रख सकते हैं। चंदर अपने परिवार से मिली इस सीख को अपने दोस्तों के बीच बताते नहीं हिचकते हैं। वह बताते हैं, “जिस गांव से हम आते हैं वहां जातिवाद आज भी क़ायम है। जिसे हम वहां अपने आस-पास के लोगों के व्यवहार में आसानी से देख और समझ सकते हैं।” चंदर ने परिवार से मिलने वाली जातिवादी सीख को हमसे साझा कर यह बताने का प्रयास किया कि बड़े शहरों में पढ़ने आने का एक नतीजा यह हो सकता है कि हम अपनी पूर्वधारणाओं को टूटते हुए देख सकते हैं।
स्कूल के भीतर जातिवादी बर्ताव
एक दलित विद्यार्थी जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत ही समाज में मौजूद जातिवादी मानसिकता का एहसास करवाया जाता है। स्कूलों की इसी जातिवादी व्यवस्था का अनुभव दिल्ली के मोहम्मदपुर में रहनेवाले अंकुर (24) ने किया। जब अंकुर नौवीं में पढ़ रहे थे तब वह अपने स्कूल के दोस्तों के एक ग्रुप के साथ फुटबॉल खेला करते थे। ग्रुप में सबसे बेहतर फुटबॉल खेलने के लिए अंकुर को कोई प्रशंसा नहीं मिली पर जातिवादी बर्ताव ज़रूर झेलना पड़ा। उनके दोस्तों ने यह कहकर समाज में उनकी ‘हैसियत’ महसूस करवाई कि ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, हमें पता है की तू किस जाति से आता है।
जातिवाद के इस अमानवीय बर्ताव ने अंकुर को भीतर तक हिलाकर रख दिया था। वह आज भी 16 साल की उम्र में हुई इस घटना को याद करते हैं। वह कहते हैं, “मुझे मेरे दोस्तों के व्यवहार से ऐसा लगा जैसे मेरी जाति मेरे लिए असुरक्षित है। उनके व्यवहार ने लंबे समय तक नीच होने की पहचान के साथ मुझे अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर किया।” इस घटना ने अंकुर के भीतर एक ऐसी सोशल एंग्ज़ायटी को पैदा किया जिससे उन्हें बाद में दोस्त बनाने और हम उम्र के लोगों से संवाद करने में हिचक पैदा होने लगी थी।
क्या शहरों के प्रगतिशील होने में यहां के लोगों की मानसिकता की कोई भूमिका नहीं है? क्या इन शहरों का प्रगतिशील होना लुभावनी राष्ट्रीय शान और विरासत तक ही सीमित है? क्या जातिवाद सोच का यह घृणित चेहरा यहां के समतामूलक समाज और सफल लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाता है?
अपनी ही दिल्ली में किया पराया
दिल्ली के आरके पुरम की रहनेवाली शालिनी (29) दलित हैं। दिल्ली से उनका नाता पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुराना है। इससे पहले वह पूर्वी दिल्ली में रहा करती थीं। पड़ोस में आसपास रहनेवाले भी अनुसूचित जाति से थे। एक ही समुदाय से आनेवाले पड़ोसियों की पहचान से वाकिफ़ होना उनके और उनके परिवार के लिए बिना किसी चिंता के साधारण और सहज जीवनयापन का सूचक रहा था। लेकिन जब वह दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम में शिफ़्ट हुई तो उन्हें कई सालों तक अपनी जातिगत पहचान पड़ोसियों से छिपानी पड़ी थी। एक झगड़े के दौरान घर के पास ही के एक तथाकथित उच्च जाति से वास्ता रखनेवाले एक पड़ोसी को उनकी जाति का मालूम पड़ा तो उनके परिवार को उनसे कई बार जातिसूचक शब्दों का सामना करना पड़ा था। शालिनी के अनुसार, “हमें अक्सर अपनी ही ज़मीन पर पराया किया गया था।”
कॉरपोरेट ऑफिस का जातिवादी माहौल
रेखा (30) गुड़गांव में रहती हैं। वह दिल्ली की रहनेवाली हैं। एक साल पहले शादी के बाद वह गुड़गांव शिफ्ट हो गईं। वह पांच सालों से एक अमरीकन एमएनसी के लिए काम कर रही हैं। वह समाज में जातीय तौर पर किस समुदाय से आती हैं इस तथ्य को आज तक उन्होंने किसी सहकर्मी से साझा नहीं किया है। उन्हें डर है कि अगर वह ऐसा करती हैं तो लोग ऑफिस में उनसे दूरी बना सकते हैं। कॉरपोरेट माहौल में व्यक्ति की सोशल क्लास, सरनेम और स्टेटस सिंबल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तब और भी ज़्यादा रखते हैं जब आप बाकियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे होते हैं।
रेखा बताती हैं, “मैंने पांच साल के अंदर दो कंपनियों में काम किया है। दोनों ही ऑफिस में मैंने सहकर्मियों के बीच खुद को उच्च जाति की पहचान के साथ परिचित करवाया है। एमएनसी में काम करने वाले मेरे एक-दो दोस्त हैं जिन्होंने अपनी जातिगत पहचान के कारण ऑफिस में आइसोलेशन झेला है। मैं तो एक युवती हूं। मेरे साथ और ख़राब बर्ताव होने की संभावना हो सकती है अपनी असल जातीय पहचान बताकर।”
ये सभी अनुभव हमें शहर की जाति आधारित मानसिकता और व्यवस्थाओं को उजागर करते हैं। शहरों को मानव के जीवन के अनेकों विकास के लिए प्रगतिशील माना जाता है। इन सभी अनुभवों के आलोक में प्रश्न यह उठते हैं कि क्या शहरों के प्रगतिशील होने में यहां के लोगों की मानसिकता की कोई भूमिका नहीं है? क्या इन शहरों का प्रगतिशील होना लुभावनी राष्ट्रीय शान और विरासत तक ही सीमित है? क्या जातिवाद सोच का यह घृणित चेहरा यहां के समतामूलक समाज और सफल लोकतंत्र की स्थिति को दर्शाता है? अच्छी शिक्षा व्यवस्था, नौकरियों, उच्च मजदूरी के वादों, भव्य इमारतों के कदों के अलावा भी शहर बहुत कुछ है। सबका अपना शहर उनकी मानसिकता में भी बस्ता है। हम यहां के चाहे कितने भी भौतिक सुख के लाभ उठाएं पर एक जातिवादी ज़ेहन के साथ हम शहर को शहर नहीं बना सकते हैं।